नारी को अधिकार दो
एक जागृति
लीना चावला राजन
तुम बदलोगे, जग बदलेगा
महात्मा गांधी
भूमिका एक पुकार हमारे जीवन में औरत की अहमियत
समाज में औरत की भूमिका
अर्थ व्यवस्था में औरत की भूमिका
औरत के ख़ास गुण
आज के समय में औरत की हालत
बेटे की चाह
दहेज
लिंग चुनाव
हमारी करनी का नतीजा
बच्चों पर प्रभाव
आदमियों पर प्रभाव
समाज में औरतों के प्रति बढ़ता अपराध
समाज में बढ़ती अशांति
हम क्या चाहते हैं?
हम परिवार में क्या चाहते हैं?
हम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं?
आध्यात्मिक दृष्टिकोण
मक़सद को ध्यान में रखते हुए कर्म करना
औरत को बराबरी का हक़
हत्या करना पाप है
दूसरे जीव को दु:ख देना
अपनी इच्छाओं पर क़ाबू पाना
हमारे कर्मों का फल
परमात्मा की रज़ा में रहना
परमार्थ हमारा मूल
पुराने रीति रिवाज तोड़े जा सकते हैं
औरतों की दु:ख़ी हालत का ज़िम्मेदार कौन है?
इस समस्या का हल क्या है?
औरतों की सोच में बदलाव लाना
औरत के प्रति आदमी की सोच में बदलाव
बदलाव के लिये आगे बढ़ना
नारी को अधिकार दो जागृति जागो, मेरे दोस्त
आख़िरी संदेश: बड़े पैमाने पर कन्या हत्या
2. क्या हमारे देश में कानून लागू हो रहा है?
3. मदद के लिये एक पुकार
हुआ बेटा तो ढोल बजाया! हुई बेटी तो मातम छाया! संदर्भ ग्रंथ पुस्तक एवं लेखक परिचय संपर्क संबंधी जानकारी और अन्य सूचना
प्रकाशक:
जे. सी. सेठी, सेक्रेटरी
राधास्वामी सत्संग ब्यास
डेरा बाबा जैमल सिंह
पंजाब 143 204
© 2010 राधास्वामी सत्संग ब्यास
सर्वाधिकार सुरक्षित
पहला संस्करण 2010
मुद्रक: 978-93-89810-97-4
भूमिका
कोई तो इस पतन को रोकेगा,
फिर तुम क्यों नहीं?
लॉरेंस स्कूल सनावर, विद्यालय गीत
नारी को अधिकार दो एक साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि हमारे समाज में हो रही एक घोर समस्या का नपा तुला जवाब है। यह घोर समस्या क्या है? आज हमारे देश में, जब माँ-बाप को पता चलता है कि माँ के पेट में बेटी पल रही है, कई माँ-बाप उस मासूम बच्ची की भ्रूण रूप में ही हत्या कर देते हैं। कन्या भ्रूणहत्या का यह चलन बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिये कि औरतों के प्रति हमारी सोच बिलकुल ग़लत है। इसलिये कि हम अपनी आध्यात्मिक बुनियाद को भूल चुके हैं। इसलिये भी कि हम ‘कर्म सिद्धांत’ के प्रति आँखें मूँद लेते हैं। हम भूल चुके हैं कि मालिक के दरबार में हमारे हर कर्म का हिसाब रखा जाता है—जैसा करेंगे, वैसा भरेंगे।
यह पुस्तक हमें प्रेरणा देती है कि हम ज़रा रुककर सोचें—समाज का हिस्सा होने के नाते हमारी भी कुछ आध्यात्मिक और नैतिक ज़िम्मेदारियाँ हैं। क्या हमारी करनी और हमारी ज़िम्मेदारियों का आपस में तालमेल है? इन ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिये हमें सबसे पहले अपनी सोच में ज़बरदस्त बदलाव लाना होगा। इस पुस्तक के लेखकों ने तथ्य और आँकड़े पेश करते हुए औरतों के जीवन की वास्तविक घटनाओं का वर्णन इस उम्मीद से किया है कि इन्हें पढ़कर हम जागें और अपने रवैये में बदलाव लायें।
यह पुस्तक हमारे ध्यान को इस सवाल का जवाब खोजने पर मजबूर करती है कि आज हमारे देश में ज़्यादातर औरतें इतनी दु:खी क्यों हैं? जवाब मिलेगा—इसलिये कि सदियों से हमारे समाज में औरतों को मर्दों के मुक़ाबले बहुत नीचा दर्जा दिया गया है। इसलिये भी कि हम अपनी करनी की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते। आज हम सब जानते हैं कि लिंग चुनाव और कन्या भ्रूणहत्या ग़लत है, पाप है, ग़ैरकानूनी है। हम यह भी जानते हैं कि अगर यह परंपरा बढ़ती गई तो इसका नतीजा ख़ौफ़नाक हो सकता है। फिर भी हममें से कोई इस समस्या की ज़िम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है। सब एक दूसरे की तरफ़ उँगली उठा रहे हैं और अंत में कोई अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं समझता, लेकिन कर्मों के कानून को कोई नहीं रोक सकता। यह संसार कर्मों की खेती है—जो बीज बोएँगे वही फसल काटनी पड़ेगी। अगर हम हिंसा का बीज बोएँगे तो हमें हिंसा की फसल मिलेगी। अगर हम दूसरों को दु:ख देंगे तो हमें भी दु:ख भोगना पड़ेगा। कर्म विधान के अनुसार जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। लिंग चुनाव के संबंध में औरतों को जो कष्ट भोगना पड़ता है उसके लिये हम सब ज़िम्मेदार हैं।
हमारा समाज सदियों से पुरुष प्रधान समाज रहा है। यहाँ आदमियों की विचारधारा समाज की बुनियाद मानी जाती है। अगर आदमी एक औरत को माँ या बहन के रूप में देखता है तो उस औरत का सम्मान बढ़ जाता है और वह पूजनीय हो जाती है। यदि आदमी उसी औरत को वासना की नज़र से देखता है और अगर उस वासना का बुरा नतीजा होता है, तो समाज बेचारी औरत पर आरोप लगाता है कि उसी ने आदमी को मोहित किया होगा, लेकिन उस आदमी को रत्ती भर भी दोष नहीं दिया जाता। यह कैसा इंसाफ़ है? अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हमारे समाज की हालत ही ऐसी है। इस पुरुष प्रधान नज़रिये को बदलना बहुत ज़रूरी है। वक़्त की पुकार है कि हम जागें और सच्चाई को परखें। यह बदलाव, यह जागृति कहाँ से शुरू होगी? पुरुषों से। क्योंकि हमारे समाज में सत्ता अब भी पुरुषों के हाथ में है और सदियों से पुरुषों के हाथ में ही रही है, इसलिये बदलाव लाने की ज़िम्मेदारी पुरुषों की है। इस काम में पुरुषों को ही अगुआई करनी होगी।
लिंग चुनाव की स्थिति दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों और आनेवाली पीढ़ी को एक सुनहरा और स्वस्थ समाज मिले, तो हमें आज ही लिंग चुनाव को रोकने के लिये सख़्त क़दम उठाने होंगे। क़दम उठाने से पहले हमें यह समझना चाहिये कि सिर्फ़ लिंग चुनाव को रोकने की कोशिश करने से ही काम नहीं बनेगा। हमें लिंग चुनाव की कुप्रथा की जड़ों तक पहुँचना होगा—औरतों के प्रति असमानता और अत्याचार को जड़ से उखाड़ना होगा, तभी हमारे समाज में आवश्यकता के अनुसार बदलाव आएगा।
नारी को अधिकार दो पुस्तक का यह संदेश नहीं है कि नारी पुरुष पर बिना वजह अपना अधिकार जमाना शुरू कर दे और यह जताए कि औरत का दर्जा पुरुष से ऊपर होना चाहिये। इस पुस्तक का यह संदेश है कि हम मिलकर ऐसा समाज बनाएँ जहाँ औरत और आदमी में बराबरी का दर्जा हो, जहाँ वे एक दूसरे की योग्यता की क़द्र करें और एक दूसरे की कमियों के प्रति सहनशील हों। ऐसा सुखद समाज बनाने की ज़िम्मेदारी हम सब की है और हम सब अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी और हमारे समाज से इस ज़हर को निकालने के लिये हमें औरतों के प्रति अपने नज़रिये को बदलना होगा। सही रास्ता चुनना हमारे हाथ में है।
जी.एस.ढिल्लों
दिसंबर 2009
एक पुकार
‘देश मृनमोए नोए, देश चिनमोए’
देश सिर्फ़ धरती का एक टुकड़ा ही नहीं,
देश हमारी चेतनता की कहानी है।
रवीन्द्रनाथ टैगोर
नारी को अधिकार दो पुस्तक एक पुकार है—कुछ करने की पुकार। इस पुस्तक में यह संदेश है कि समाज के रीति रिवाज हमने ख़ुद ही बनाए हैं और इन्हीं रीति रिवाजों की वजह से आज हमारे देश की औरत बेहद दु:ख सह रही है।
एक तरफ़ तो हमारा देश धर्म प्रधान देश माना जाता है। यहाँ हमें जगह-जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर बने मिलते हैं। संसार के सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग यहीं बसते हैं। हमने आज़ादी अहिंसा से पाई और सारे संसार को अहिंसा का संदेश दिया। हमारे देश की धार्मिक परंपराएँ सदियों पुरानी हैं।
दूसरी तरफ़, हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ औरतों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। हमारे समाज में लड़कियों का पैदा होना इतना नापसंद है कि लाखों लड़कियों को जन्म से पहले ही गर्भ में या जन्म लेते ही जान से मार दिया जाता है। जो लड़कियाँ किसी वजह से बच जाती हैं, उनका बचपन दु:खों और ज़ुल्मों का सामना करने में निकल जाता है। यहाँ तक कि हम लड़कियों को उनके भाइयों के बराबर का खाना-पीना नहीं देते, पढ़ाई का मौक़ा नहीं देते और किसी भी काम में उनको बराबरी का दर्जा नहीं देते। कई लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। शादी में दहेज भी देना पड़ता है और दहेज के कारण माँ-बाप क़र्ज़ के बोझ तले दब जाते हैं। ज़्यादातर औरतें पैसों के मामले में आदमियों की मोहताज होती हैं। उन्हें बचपन से ही दबाव में रखा जाता है और समझाया जाता है कि वे आदमियों के मुक़ाबले में कमज़ोर हैं। बहुत-सी औरतें आदमियों के हाथों मारपीट या बुरे बर्ताव का शिकार होती हैं।
एक तरफ़ तो हम देवी रूप में नारी की पूजा करते हैं; मंदिर में जाकर लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ को पूजते हैं। हम ‘माँ’ को इतना आदर देते हैं कि जिस ज़मीन पर रहते हैं उसे ‘धरती माता’ कहते हैं, जिस देश में रहते हैं उसे ‘मातृभूमि’ कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ़ हम एक बच्ची की जान ले लेते हैं, क्योंकि वह लड़की है! क्या भारत जैसे धार्मिक देश को अपनी आधी जनसंख्या—औरतों के साथ इस तरह का बर्ताव करना चाहिये? हम अपने धर्मग्रंथों में पढ़ते हैं कि परमात्मा की नज़रों में सभी बराबर हैं। परमात्मा प्रेम का रूप है और उसकी बनाई दुनिया में हमें सबसे प्यार करना चाहिये। इसके बावजूद हम अपने बेटों से प्यार करते हैं, अपनी बेटियों से नहीं!
क्या हमने कभी सोचा है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं?
औरतों की ज़िंदगी को सुधारना—यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई सरकारी और ग़ैरसरकारी संस्थाएँ औरतों की पढ़ाई, सेहत, खान-पान और सुरक्षा को सुधारने के लिये लगातार क़दम उठा रही हैं। नारी को अधिकार दो पुस्तक इन सभी समस्याओं का हल ढूँढ़ने की कोशिश नहीं है, बल्कि इस पुस्तक में एक बहुत ज़रूरी मुद्दे की तरफ़ ध्यान खींचने की कोशिश है और वह है—अगर समाज में कभी भी कोई बदलाव आया है तो उसकी शुरुआत किसी एक व्यक्ति ने ही की है। आजकल हमारे देश में पैदा होनेवाले बच्चे के लिंग चुनाव का चलन इतना बढ़ता जा रहा है कि यह एक भारी समस्या बन गई है। हम अपने मन में विचार करें कि इस समस्या के बारे में हम कितना जानते हैं? और अगर जानते हैं तो इसे सुधारने के लिये हमने क्या क़दम उठाए हैं? यह नहीं सोचना चाहिये कि हम अकेले हैं और बदलाव लाना अकेले इनसान के वश में नहीं है। सच तो यह है कि हर इनसान का अपना महत्त्व है, क्योंकि इनसान मिलकर परिवार बनाते हैं और परिवारों से समाज बनता है।
इस किताब में आपसे एक निवेदन है—आओ! हम जागें और अपनी इनसानियत को पहचानें। अच्छी सोच और दया—ये दो गुण हमें सच्चा इनसान बनाते हैं और ये गुण हम सब में मौजूद हैं। महान् कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि हमारा देश सिर्फ़ धरती का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी चेतनता की एक कहानी है। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जो फ़ैसले हम आज ले रहे हैं उनका असर सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा।
नारी को अधिकार दो पुस्तक की पुकार है कि हम ज़रा रुकें और अपनी आत्मा की गहराइयों में झाँकें और परखें—क्या औरतों के साथ हमारा बर्ताव सही है? जिस परमपिता परमात्मा की हम पूजा करते हैं, क्या वह चाहेगा कि औरतों के साथ हमारा बर्ताव ऐसा ही रहे? इस किताब का संदेश है कि औरत बोझ नहीं, बल्कि इस दुनिया में एक अनमोल रत्न है। आज के वक़्त की पुकार है कि हम जागें और मिलकर औरत को मज़बूत और शक्तिशाली बनाएँ।
हमारे जीवन में औरत की अहमियत
औरत संपूर्ण है क्योंकि उसमें जीवन देने की, पालन-पोषण करने की और बदलाव लाने की शक्ति है।
डाऐन मरीचाइल्ड
एक औरत के कई रूप हैं और उसका हर रूप अपने आप में ख़ास और अनमोल है।
परिवार में औरत की भूमिकाहमारी संस्कृति को क़ायम रखने में औरत का बहुत बड़ा योगदान है। ज़रा सोचिये! दादी-माँ की कहानियों के बिना, माँ के प्यार-दुलार के बिना, पत्नी के जीवन भर के साथ के बिना, हमारी ज़िंदगी कैसी होती? बहन की प्यार भरी छेड़छाड़, एक बेटी की प्यार भरी देखभाल, इसके बिना हमारा जीवन कितना नीरस होता? औरत ही सब में प्यार और ख़ुशी बाँटती है, सबका ध्यान रखती है। क्या हम सोच सकते हैं कि औरत के बिना हमारा परिवार कैसा होता?
भगवान् ने औरत को जननी होने की एक अनमोल देन और ख़ास ज़िम्मेदारी दी है—केवल औरत में जन्म देने की सामर्थ्य है। संसार को नवजीवन का उपहार केवल औरत ही दे सकती है।
सब को प्यार देना—यह ख़ूबी, यह शक्ति, औरत में तब और उभर आती है, जब वह माँ बनती है। माँ बनना, यह औरत को भगवान् का वरदान है।
मदर टेरेसा
माँ की ममता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। औरत अपनी जान को ख़तरे में डालकर, बेहद शारीरिक पीड़ा सहकर, ख़ुशी-ख़ुशी अपने बच्चों को जन्म देती है। बच्चों की देखभाल करते हुए वह अपने आराम के बारे में नहीं सोचती। वह बेग़रज़ होकर अपनी ज़िम्मेदारी निभाती है। ज़रूरत पड़ने पर ख़ुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है। बच्चों को चोट लगने पर बड़े प्यार और दुलार से मरहम-पट्टी करती है। अगर बच्चे बीमार हो जाएँ तो रात भर जागकर उनकी देखभाल करती है। थकान की परवाह किये बिना वह अपने बच्चों की हर ज़रूरत का ध्यान रखती है—बच्चों ने क्या खाया, क्या वे ठीक तरह से पढ़-लिख रहे हैं, क्या वे अच्छी संगति में हैं, क्या वे ख़ुश हैं? बच्चे बेशक अपनी माँ को भूल जाएँ या बेपरवाह हो जाएँ, लेकिन माँ का प्यार कभी कम नहीं होता।
वह कौन है, जो मुझे प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा? वह कौन है जो मेरी हर ग़लती के बावजूद मुझे नहीं ठुकराएगा? वह तुम हो, मेरी माँ।
टॉमस कारलायल
माँ के प्यार में उसका अपना मतलब नहीं झलकता। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक माँ के प्यार से ज़्यादा पवित्र प्यार किसी का नहीं हो सकता।
भगवान् हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिये उसने माँ को बनाया।
यहूदी कहावत
एक बच्चे का सबसे पहला और प्रभावशाली गुरु उसकी माँ होती है। दुनिया की हर संस्कृति और समाज में यही दिखाई देता है कि बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा वक़्त माँ ही गुज़ारती है, ख़ासकर उसके बचपन में। वह अपने बच्चे को बोलना सिखाती है—उसको ‘मातृभाषा’ सिखाती है। वह अपने बच्चे को ज़िंदगी के उसूल सिखाती है और सही-ग़लत में फ़र्क़ करना बताती है। माँ अपने बच्चे की सोच और उसके चरित्र को सँवारती है। उसकी आदतों, धारणाओं और दृष्टिकोण पर गहरा असर डालती है।
एक अच्छी माँ सौ अध्यापकों के बराबर है।
जॉर्ज हर्बर्ट
पढ़ी-लिखी समझदार माँ न केवल पढ़ाई-लिखाई में अपने बच्चे की मदद करती है, बल्कि उसके सुरक्षित और अच्छे भविष्य की नींव रखती है।
एक बच्चे के भाग्य का निर्माण उसकी माँ ही करती है।
नपोलियन बोनापार्ट
मेरी माँ सबसे सुंदर औरत थी ìआज मैं जो कुछ हूँ उसी की बदौलत हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि मुझे सदाचार, समझदारी और सफलता देनेवाली शिक्षा अपनी माँ से ही मिली।
जॉर्ज वॉशिंग्टन
औरत सहज ही अपने घर में प्यार, अपनापन, साफ़-सफ़ाई और सुखद माहौल पैदा करती है। औरत हमें दुनियादारी के तौर-तरीक़े सिखाती है कि परिवार में और समाज में किस ढंग से एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिये, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिये।
जीवन को सही तरीक़े से जीने के लिये जो सभ्य आचरण होना चाहिये, वह हमें औरत ही सिखाती है, जैसे—एक दूसरे का आदर करना, वे छोटी-छोटी बातें जिनसे हम दूसरों का दिल जीत सकें, हालात के मुताबिक़ अपने रवैये को ढालना और समाज के साथ क़दम मिलाकर चलने के तौर-तरीक़े आदि।
रेमि द गूरमौं
एक सच्चे साथी के रूप में औरत ही अपने पति का साथ निभाती है। वह सुख-दु:ख में वफ़ादारी से उसका साथ देती है। वह न केवल अपने माता-पिता को प्यार और इज़्ज़त देती है, बल्कि अपने पति के परिवार को भी प्रेम की डोरी में बाँध लेती है। वह सभी रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के साथ मेलजोल बढ़ाकर, अपनेपन से रिश्तों का एक सुंदर और मज़बूत ताना-बाना बुन लेती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों और बीमारों तक, सभी की देखभाल प्रेम और प्यार से करती है।
औरत घर की शांति और ख़ुशहाली की कुंजी है। वास्तव में औरत ही घर को बनाती है।
समाज में औरत की भूमिकाहमारी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को जीवित रखने में औरत का बड़ा योगदान है। सदियों से औरतें अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती आई हैं जो उन्होंने अपनी माँ और दादी से सुनी थीं। औरतों की वजह से ये कहानियाँ और लोककथाएँ आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। अगर हम अपनी संस्कृति के किसी भी पहलू पर नज़र डालें—चाहे लोक संगीत, नृत्य या कला हो, चाहे कपड़े पहनने का, भोजन बनाने का या पूजा-पाठ करने का ढंग हो—इन सभी रिवाजों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने में औरतों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इनके ज़रिये औरत उन सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाती है जो परिवार और समाज को जोड़े रखते हैं।
लड़ाई के मैदान में जब हज़ारों आदमी शहीद हो जाते हैं, उस समय औरतें कई मुश्किलों का सामना करते हुए भी परिवार को जोड़े रखती हैं। उस वक़्त औरतें बूढ़ों, बीमारों और ज़ख़्मियों की सेवा करती हैं और बच्चों की देखभाल करती हुईं अगली पीढ़ी को तैयार करती हैं। औरत हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है।
अगर समाज को तेज़ी से बदलना है तो औरतों को एकजुट होकर आगे बढ़ाना होगा।
चार्ल्ज़ मलिक, पूर्व अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ—जनरल असेम्बली
आजकल वोट के अधिकार का इस्तेमाल करनेवाली औरतों की गिनती बढ़ती जा रही है। इसके ज़रिये वे अपने मुद्दों की सुनवाई करवा रही हैं। आजकल हर जगह औरत आगे बढ़ रही है—चाहे वह सरकारी नौकरी हो या पुलिस विभाग, चाहे वकील, जज या ज़ोरदार नेता। वे मीडिया के ज़रिये समाज में बदलाव ला रही हैं। इसके अलावा बहुत-सी औरतें समाज सुधार का काम कर रही हैं। बहुत-सी सरकारी और ग़ैरसरकारी संस्थाएँ औरतों द्वारा चलाई जा रही हैं। चाहे बच्चों का कल्याण हो या पर्यावरण, इन सब बातों में औरतें काफ़ी बदलाव ला रही हैं।
अर्थ व्यवस्था में औरत की भूमिकाऔरत न सिर्फ़ समाज का एक ज़रूरी हिस्सा है, बल्कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्था यानी धन संबंधित प्रबंध व्यवस्था में भी मददगार साबित हो रही है। आजकल बहुत-से परिवार ऐसे भी हैं जिनमें यदि औरत कामकाज करके धन कमाकर न लाए, तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पुराने ज़माने में कुछ काम औरत की शारीरिक शक्ति के बाहर माने जाते थे जैसे—शिकार करना, लड़ाई के मैदान में लड़ना, हल चलाना आदि। इसलिये वह अपने शरीर की ताक़त के मुताबिक़ घर के कामकाज सँभालती थी। हालाँकि घर सँभालना भी बड़ा महत्त्वपूर्ण काम है।
अब दुनिया बदल रही है। आजकल ज़्यादातर कामों के लिये ताक़तवर होना उतना ज़रूरी नहीं है। आज अगर औरत को बराबर का मौक़ा मिले तो कौन-सा ऐसा काम है जो वह नहीं कर सकती। आज औरतें भी डॉक्टर, वकील, जज, नेता, व्यापारी, इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं। वे खेलकूद, कला और मीडिया में भी आगे हैं। औरतें फ़ौज और पुलिस में भी शामिल हैं। आज की औरत देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, ट्रैक्टर चलाने या हवाई जहाज़ उड़ा सकने में भी औरत पीछे नहीं है। यहाँ तक कि वह चाँद तक भी पहुँच सकती है।
शोध-अध्ययनों से साबित हुआ है कि औरतें कामकाज में कई ख़ूबियाँ ला रही हैं।1 आज औरतें कई कंपनियों की मैनेजर हैं। वे अपनी कंपनी के विकास की अच्छी समझ रखती हैं और अपने कर्मचारियों से काम लेने की सूझबूझ रखती हैं। वे बहुत-सी ज़िम्मेदारियाँ एक साथ निभा लेती हैं। औरत नरमी और प्यार से अपनी बात मनवा लेती है और सब को साथ लेकर आगे बढ़ती है। उसमें दूसरों का नज़रिया समझने का गुण होता है और इसी वजह से औरतों के साथ काम करनेवाले यह समझते हैं कि उनके काम और योग्यता की क़द्र है।
आज के नये ज़माने में गुणों के मूल्यांकन में औरतों का दर्जा ऊँचा है। मिल-जुलकर काम करना और दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ना सफलता की निशानी है और औरतों में ये गुण भरपूर हैं।
रोज़ाबेथ मॅास कैन्टर, हार्वर्ड बिज़्नस स्कूल प्रोफ़ेसर
हालाँकि कंपनी में औरतों को पुरुषों के बराबर की संख्या में नौकरी पर रखना, न तो ज़रूरी है और न ही कोई कानूनी मजबूरी है, फिर भी आजकल ज़्यादातर कंपनियाँ औरतों के काम करने के ढंग को देखते हुए उन्हें ही नौकरी पर रखना पसंद करती हैं, क्योंकि वे कामकाज और व्यापार के लिये फ़ायदेमंद साबित हुईं हैं।
औरत के ख़ास गुणपुराने ज़माने से ही हम यह मानते चले आ रहे हैं कि कुछ ख़ासियत और गुण सिर्फ़ आदमियों से जुड़े हुए हैं, जैसे—ताक़त, अधिकार जमाना, हिम्मत, मनमानी करना, लीडरी, दलीलबाज़ी आदि। इसी तरह कुछ ख़ासियत और गुण औरतों से जुड़े हुए हैं, जैसे—सूझबूझ, सहनशीलता, नम्रता, सब्र, दया, त्याग भरा प्यार आदि।
इसका मतलब यह नहीं है कि आदमियों में सिर्फ़ आदमियोंवाले और औरतों में सिर्फ़ औरतोंवाले गुण होते हैं। औरतों और आदमियों में दोनों प्रकार के गुण अलग-अलग मात्रा में होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यह मात्रा कैसे तय होती है? यह कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला कारण है पैदाइशी गुण। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि पैदा होते ही कुछ गुण हमारे अंदर होते हैं, जैसे—औरतों में बच्चों के लिये स्वाभाविक प्यार या आदमियों में अधिकार जमाने की भावना।
दूसरा कारण है समाज के बनाए नियम और घर-घर के अपने क़ायदे-कानून, जो बच्चों के विचारों पर गहरा असर डालते हैं। बचपन से बच्चों को यही समझाया जाता है कि ‘लड़के नहीं रोते।’ जब बचपन से लड़कों को सिखाया जाता है कि अधिकार जमाना, रोब और अहंकार उनके अधिकार हैं तब सब्र, दया और सहानुभूति जैसे गुण, जो जन्म से उनमें मौजूद होते हैं, धीरे-धीरे दब जाते हैं। ऐसे गुण अगर न दबें तो दुनिया उन्हें कमज़ोर कहेगी। ठीक इसी तरह कई घरों में लड़कियों को बलिदान की मूरत बनने और दबकर रहने की शिक्षा दी जाती है। ताक़त, अधिकार जमाना, लीडरी आदि गुण जो आदमियों में शोभा बढ़ानेवाले माने जाते हैं, यही गुण औरतों में ग़लत माने जाते हैं। ज़िंदगी भर इन बातों को सुनते-सुनते, बच्चे इन ‘आदमियों’ और ‘औरतों’ वाले गुणों को अपनाकर अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं।
सच तो यह है कि सबसे ज़्यादा सफल और संतुष्ट आदमी वही है जिसमें दोनों प्रकार के गुणों का संतुलन होता है। यही संतुलन आदमी को एक बेहतर और पूर्ण इनसान बना सकता है और यही बात औरतों के बारे में भी सच है।
दूसरी सच्चाई यह है कि अगर हमें क़ुदरत में संतुलन बनाए रखना है, तो हमें दोनों गुणों की ज़रूरत है। अगर संसार में, देश में या हमारे अंदर, केवल आदमियों के ही गुण हों तो ज़्यादा युद्ध होंगे, ज़्यादा ग़ुस्सा होगा और संसार में हाहाकार मच जाएगा। इस नज़रिये से औरत केवल क़द्र के लायक़ ही नहीं, बल्कि उसके गुण समाज में प्यार और संतुलन बनाए रखने के लिये बेहद ज़रूरी हैं।
परिवार में, समाज में और संसार में,
औरत का योगदान है बेमिसाल।
उसके बिना पूर्णता नहीं जीवन में,
और न ज़िंदगी बनती है ख़ुशहाल॥
आज के समय में औरत की हालत
आप किसी भी देश की हालत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो वहाँ की औरतों की हालत देखकर लगा सकते हैं।
जवाहरलाल नेहरू
अगर हम अपने देश की औरतों की हालत देखें और उससे देश की हालत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो हम क्या पाएँगे? यही कि आज़ादी के बाद औरतों की सेहत और शिक्षा में बेहतरी लाने के लिये बहुत-से क़दम उठाए गए हैं, जिनकी वजह से आज हमारे देश में कई औरतें राजनेता, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी हैं। यह तो साफ़ ज़ाहिर है कि आज बहुत-सी औरतें हमारी माँ और दादी-माँ से कहीं ज़्यादा आज़ादी का जीवन जी रही हैं, लेकिन यह आज़ादी और बराबरी अभी तक छोटे शहरों और गाँवों तक नहीं पहुँच पाई जो कि बड़े दु:ख की बात है।
असमानता की एक झलकअनपढ़ होना
हमारे देश में उसी को पढ़ा-लिखा माना जाता है जो अपना नाम लिख सकता है या किसी भी भाषा में एक आसान वाक्य यानी लाइन लिख सकता है। सन् 2001 की जनगणना के मुताबिक़ भारत में 100 में से सिर्फ़ 54 औरतें पढ़ी-लिखी थीं, इसके मुक़ाबले 100 में से 75 आदमी पढ़े-लिखे थे।2 जिन औरतों को पढ़ा-लिखा माना जाता है, उनमें 100 में से 60 ने तो सिर्फ़ पाँचवीं कक्षा या उससे भी कम पढ़ाई की होती है।2इससे साफ़ ज़ाहिर है कि हमारे देश में अनपढ़ आदमियों के मुक़ाबले अनपढ़ औरतें कहीं ज़्यादा हैं।
हमारे देश में औरतों की शिक्षा को बढ़ावा देने में काफ़ी तरक्की हुई है। भारत में 14 साल तक की लड़कियों को मुफ़्त शिक्षा दी जाती है और कानून के मुताबिक़ 14 साल से कम उम्र की लड़कियों को स्कूल भेजना ज़रूरी है। लेकिन लड़कियों को कई सालों तक स्कूल भेजते रहना माँ-बाप के लिये बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार माँ-बाप लड़कियों का स्कूल जाना इसलिये छुड़वा देते हैं, क्योंकि उन्हें घरेलू काम करने होते हैं, जैसे—पानी लाना, जलाने की लकड़ी और भूसा लाना, छोटे भाई-बहन की देखभाल करना, खाना पकाना या सफ़ाई करना आदि। ऐसा माना जाता है कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा घरेलू काम करती हैं, इसलिये उन्हें घर पर रखना फ़ायदेमंद है। ऐसा भी माना जाता है कि बेटियों को पढ़ाने-लिखाने का ख़ास फ़ायदा नहीं होता। इसके अलावा कई माँ-बाप को यह भी चिंता रहती है कि अगर बेटी ज़्यादा पढ़-लिख गई तो उसकी शादी में परेशानी आएगी। पढ़ी-लिखी लड़की के लिये उससे भी ज़्यादा पढ़ा-लिखा लड़का ढूँढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसी से जुड़ी एक और चिंता है कि अपनी बेटी के लिये जितना ज़्यादा पढ़ा-लिखा लड़का ढूँढ़ा जाएगा उतना ही ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। कई बार लड़कियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए माँ-बाप उन्हें स्कूल ही नहीं भेजते। कई माँ-बाप अपनी बेटियों को पुरुष अध्यापकों से नहीं पढ़वाना चाहते तो कई अन्य उन्हें सिर्फ़ लड़कियों के स्कूल में ही भेजना चाहते हैं। अगर स्कूल घर से काफ़ी दूर हो तो इसे भी बेटी की सुरक्षा के लिये ख़तरा माना जाता है।
बाल विवाहहमारे देश में कानून के मुताबिक़ शादी की उम्र 18 साल है, लेकिन यहाँ 100 में से 47 यानी आधी लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती है।3 कम उम्र में शादी करने की बहुत-सी वजहें बताई जाती हैं जैसे—कुँवारी लड़कियों की सुरक्षा का ख़तरा बना रहता है; छोटी उम्र में शादी करने पर दहेज कम देना पड़ता है, छोटी लड़कियों के लिये दूल्हा ढूँढ़ना आसान होता है। भारत के कई प्रदेशों में पुराने रिवाज और सामाजिक दबाव की वजह से भी बेटियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है और माँ-बाप के लिये विरोध करना बड़ा मुश्किल होता है। देश के कुछ हिस्सों में लड़कियों की गिनती लड़कों से काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ज़्यादा बाल विवाह हो रहे हैं।
पूरी दुनिया में 100 में से 40 बाल विवाह हमारे देश में होते हैं।3
ख़राब सेहतआज के समय में बच्चे को जन्म देते वक़्त हर पाँच मिनट में एक औरत की मौत हो जाती है।4 यह संख्या दूसरे देशों के मुक़ाबले भारत में बहुत ज़्यादा है। 100 में से 20 जच्चा-बच्चा की मौत सिर्फ़ भारत में हो रही है, मौत की यह दर पूरी दुनिया का पाँचवाँ हिस्सा है।4 हमारे देश में बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे की मौत इतनी अधिक संख्या में क्यों हो रही है? इस सवाल का सीधा रिश्ता बाल विवाह से है। एक बालिग़ औरत के बजाय जब एक पंद्रह साल से भी कम उम्र की नाबालिग़ लड़की बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म के वक़्त उस लड़की की मौत का ख़तरा पाँच गुणा ज़्यादा हो जाता है।5 डॉक्टरी सुविधा न मिल पाना भी एक वजह है, क्योंकि जन्म देते समय आधी से भी ज़्यादा औरतों को डॉक्टर की देखरेख नहीं मिल पाती।6
भारत में कई परिवारों में औरतें परिवार को खाना खिलाकर, ख़ुद सबसे बाद में खाती हैं। गर्भावस्था में भी उन्हें भरपूर खाना और आराम नहीं मिल पाता। लगभग 100 में से 60 गर्भवती औरतें ‘ख़ून की कमी’ का शिकार हैं।6 कई कम उम्र की अनपढ़ लड़कियाँ गर्भवती हो जाती हैं। उनके पास सही जानकारी नहीं होती कि अपनी सेहत को सुधारने के लिये उन्हें क्या करना चाहिये। गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत के लिये उन्हें ख़ुद क्या खाना चाहिये? छोटे बच्चे को क्या खिलाना चाहिये? बच्चे को डॉक्टर के पास कब ले जाना चाहिये? टीका कब लगवाना चाहिये? इन मासूम लड़कियों को यह समझ भी नहीं है कि अगर यह सब नहीं किया तो इसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है।
हमारे देश में पाँच साल से कम उम्र के आधे बच्चे (100 में से 48) ऐसे हैं जो बेहद कमज़ोर हैं और 100 में से 70 बच्चे ऐसे हैं जो ‘ख़ून की कमी’ का शिकार हैं।6 अच्छी ख़ुराक न मिलने की वजह से ये बच्चे जल्द ही बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जिससे उम्र भर के लिये उनका शरीर और दिमाग़ कमज़ोर रह जाता है। अगर यह बच्चा लड़की है तब तो उसकी हालत और भी ख़राब होती है, क्योंकि लड़कियों के साथ खानपान में फ़र्क़ किया जाता है। लड़कों को ज़्यादा समय तक माँ का दूध पिलाया जाता है। लड़कियों की डॉक्टरी जाँच कराना तो दूर की बात है, उन्हें तो ज़रूरी टीके भी नहीं लगवाए जाते।
शिक्षा, सेहत और बाल विवाह—ये सब मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर जिस माँ ने कुछ साल स्कूल में जाकर पढ़ाई की होती है उसमें जागरूकता आ जाती है, जिसकी वजह से जच्चा-बच्चा की मौत की दर काफ़ी कम हो जाती है।7
पैसों के मामले में आज़ादी न होनाबहुत-सी औरतें सारी ज़िंदगी काम करती हैं, क्योंकि बहुत-से घरों का ख़र्च इन औरतों की कमाई के बिना चल नहीं सकता। लेकिन दु:ख की बात यह है कि ज़्यादातर औरतों का काम दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि न तो उनके परिवार के लोग उनके काम की क़द्र करते हैं और न ही सरकार उनके कामकाज को गिनती में लाती है जैसे—ज़्यादातर औरतें घर के लिये पानी, लकड़ी और चारा लाने का काम करती हैं, जिसके लिये उन्हें कभी-कभी कोसों दूर तक चलना पड़ता है। औरतें खाना पकाती हैं, सफ़ाई करती हैं, बच्चों को पालती हैं, बड़े बूढ़ों की सेवा करती हैं, अपने खेतों में या कारोबार में बिना पैसे लिये काम करती हैं, परंतु ये सभी काम गिनती में नहीं लिये जाते। हालाँकि औरतों के काम से कुछ कमाई भी होती है, तब भी उनके काम को घरेलू ही माना जाता है।
आदमियों की प्रधानता का संबंध कई बातों से है, उनकी ‘कमाऊ’ होने की स्थिति भी इसमें शामिल है। उनकी पैसे कमाने की ताक़त उनके परिवार में उनकी इज़्ज़त का कारण होती है। जबकि औरतें कहीं अधिक समय तक रोज़ाना घर पर काम करती हैं, परंतु इस काम के बदले पैसे नहीं मिलते। इसलिये परिवार की ख़ुशहाली में उनके हाथ बँटाने को कोई अहमियत नहीं दी जाती।
डॉ.अमर्त्य सेन
बहुत-सी औरतों को बाहर का काम नहीं करने दिया जाता, क्योंकि कई परिवारों में माना जाता है कि अगर घर की औरतें बाहर काम करेंगी तो समाज में उनके परिवार की इज़्ज़त कम हो जाएगी। जो औरतें घर में और आमदनी के लिये घर के बाहर काम करती हैं, असल में उनके काम करने के घंटे दुगुने हो जाते हैं। वे बाहर का काम भी करती हैं और घर का भी सारा काम निबटाती हैं। आम तौर पर औरतों और आदमियों के काम साफ़ तौर पर बँटे होते हैं। कई आदमी औरत के हिस्से के कामों को करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं।
बहुत-सी फ़ैक्ट्रियों और खेतों में एक जैसे काम के लिये औरतों को आदमियों से कम पैसे दिये जाते हैं। ज़मींदार लोग कम मज़दूरी लेनेवाली औरतों को ही ज़्यादा से ज़्यादा काम पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वे औरतों को काम देना पसंद करते हैं, क्योंकि औरतें ज़्यादा मेहनती होती हैं, जल्दी-जल्दी आराम नहीं करतीं और वे पुरुष मज़दूरों की तुलना में (30% से 50%) कम मज़दूरी पर मिल जाती हैं।8 यह औरतों के प्रति बेइंसाफ़ी है।
इतने क़ीमती योगदान के बाद भी ज़्यादातर घरों में औरत का अपनी कमाई पर पूरा हक़ नहीं होता। उसका पति या पिता उसकी कमाई को रखकर उसके इस्तेमाल का फ़ैसला करता है। जहाँ औरतों को अपनी कमाई पर हक़ दिया जाता है वहाँ देखा गया है कि औरत अपनी कमाई का ज़्यादा हिस्सा अपने परिवार की भलाई के लिये ख़र्च करती है, जबकि अपनी ख़ुद की ज़रूरतों के लिये बहुत कम रखती है। आदमी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने ऊपर ही ख़र्च करता है।
एक और दु:ख की बात है कि ज़्यादातर परिवारों में माँ-बाप अपनी मौत के बाद अपनी बेटियों के लिये कुछ नहीं छोड़ जाते। उनके नाम कोई जायदाद नहीं होती और न ही उन्हें परिवार की जायदाद में से कोई हिस्सा मिलता है। भारत की कुल संपत्ति का 1% से भी कम हिस्सा स्त्रियों के नाम है।9
समाज में औरत की स्थितिहमारे देश में ज़्यादातर औरतें आज़ाद नहीं हैं। चाहे समाज में उनकी अहमियत का मामला हो या पैसों का, इन सभी के लिये उन्हें आदमियों का मुँह देखना पड़ता है। इस संबंध में समाज भी उन्हें बहुत थोड़ी छूट देता है। ज़्यादातर परिवारों में लड़कियाँ शादी से पहले अपने पिता या भाइयों की निगरानी में रहती हैं और शादी के बाद पति या ससुरालवालों की निगरानी में। बचपन से ही लड़कियों को आज्ञाकारी और घरेलू बनना सिखाया जाता है। उन्हें अपने जीवन के किसी भी पहलू पर फ़ैसला लेने का अधिकार नहीं दिया जाता। उन्हें सिखाया जाता है कि उनका मुख्य काम परिवार के बाक़ी सदस्यों के आराम का ध्यान रखना है—कर्तव्य पालन करनेवाली बेटी, प्यार देनेवाली माँ, आज्ञाकारी बहू और वफ़ादार दब्बू पत्नी के रूप में। ‘लड़की’ होने की वजह से उसके घूमने फिरने, पढ़ाई-लिखाई और व्यवसाय सीखने पर रोक लगाई जाती है। ऐसी कोशिश की जाती है कि वह अपने ख़र्च के लायक़ पैसा न कमा ले या पैसे के मामले में आज़ाद न हो जाए। कई औरतों को तो बुनियादी फ़ैसले भी नहीं लेने दिये जाते जैसे—उसे कब बच्चा चाहिये या फिर चाहिये भी या नहीं। उन पर इतनी कड़ी निगरानी रखी जाती है कि उन्हें अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने या बाज़ार जाने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है।
पैसे से जुड़ी मोहताजी की वजह से औरतें कमज़ोर और दब्बू हो जाती हैं तथा आसानी से मारपीट का शिकार हो जाती हैं। आज हमारे देश में 100 में से 40 औरतें अपने पति की पिटाई का शिकार हैं।10 बड़े अफ़सोस की बात है कि कई परिवारों में औरतों की पिटाई को उचित समझा जाता है। उन्हें क़ायदे में रखना ज़रूरी समझा जाता है, ताकि वे अपने कर्तव्य को ठीक तरह निभाना सीखें। अफ़सोस की बात तो यह है कि औरतें भी इसे अपनी क़िस्मत मानकर सह लेती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि आज आधी से ज़्यादा शादीशुदा औरतें मारपिटाई को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानने लगी हैं और लगभग इतनी ही औरतें मानती हैं कि कुछ हालात में पत्नी की पिटाई ज़रूरी है।11
इसके बावजूद ज़्यादातर औरतें सोचती हैं कि यह दु:खभरी शादीशुदा ज़िंदगी विधवा होने से तो बेहतर है। हमारे समाज में हम विधवा औरत को बेहद दु:खी रखते हैं। कई बार पति की मौत के बाद उसके परिवारवाले बहू को कोसते हैं कि वह बदक़िस्मत है और अपने पति की मौत के लिये ज़िम्मेदार है। विधवा औरतों को समाज से बाहर ही रखा जाता है। शादी, नामकरण, जन्मदिन आदि के मौक़ों पर विधवा को मनहूस समझकर दूर रखा जाता है। उसके जीवन में पाबंदी लग जाती है। वह क्या पहनती है, क्या खाती है, कैसे रहती है—सबकुछ कड़े क़ायदे-कानून के मुताबिक़ चलता है।
औरतों के साथ भेदभाव की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। औरतों के जीवन में और भी कई मुश्किलें हैं—एड्स से लेकर औरतों के प्रति बढ़ते ज़ुल्म और अपराध के मामले। इसके अलावा अगर औरत ग़रीब परिवार की हो तो ये सब मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में औरतें ग़रीबी में जी रही हैं।
यह सब क्यों हो रहा है? हम औरतों के साथ ऐसा सलूक क्यों करते हैं? यदि हम पीछे मुड़कर परंपराओं और रीति रिवाजों को देखें तो इस प्रश्न का जवाब साफ़ ज़ाहिर है।
बेटे की चाहइतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय समाज में पुरुषों की प्रधानता रही है। हमें हमेशा ही बेटे का मोह रहा है। इतनी तरक्की और नये ज़माने की शिक्षा के बावजूद भी एक इच्छा जो नहीं बदली, वह है—परंपरा से हमारे अंतर में बसी ‘बेटे की चाह’।
बेटे को पूँजी समझा जाता हैहमारे समाज में कई कारणों से बेटों को परिवार की पूँजी माना जाता है। एक तो यह समझा जाता है कि बेटे वंश को आगे बढ़ाते हैं; यदि परिवार में सिर्फ़ बेटियाँ हों तो वंश ही ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि बेटे परिवार की धन-संपत्ति को बढ़ाते हैं। बेटे का होना एक व्यापारी या ज़मींदार परिवार के लिये और भी ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि बेटे के होने से परिवार की संपत्ति ‘परिवार में ही रहती है।’
एक बेटा ही होता है जो पिता को ‘मर्द’ होने का एहसास दिलाता है और बुढ़ापे में उसका सहारा बनता है। हमारे पास काफ़ी ज़मीन है और अगर बेटा नहीं होगा तो यह सारी ज़मीन मेरी बहन के बेटों को मिल जाएगी।
एक ज़मींदार, ‘सायलेंट जेनोसाइड,’ अरूती नैयर, द ट्रिब्यून, 6 मई, 200112
पुराने रीति रिवाजों की वजह से ऐसा माना जाता है कि बुढ़ापे में माँ-बाप की देखभाल की ज़िम्मेदारी बेटे की होती है। ज़्यादातर माँ-बाप अपनी शादीशुदा बेटी के साथ रहना नहीं चाहते, यहाँ तक कि कई माँ-बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। वे मानते हैं कि बेटी ‘दूसरे परिवार’ की सदस्य हो गई है। बेटा होने के कुछ और भी फ़ायदे माने जाते हैं—जब माँ-बाप की मृत्यु होती है तब बेटा ही परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार और इससे जुड़े अन्य क्रियाकर्म करता है। कई लोगों का ऐसा विश्वास है कि अगर अंतिम संस्कार बेटे के हाथों न हो, तो उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसा भी विचार है कि बेटा ही परिवार की रक्षा करता है और परिवार की ताक़त बनता है। परंपरागत तौर से कुछ क्षत्रिय जातियों में बेटे ताक़त और शान की पहचान माने जाते थे जबकि, बेटियाँ परिवार की कमज़ोरी की पहचान मानी जाती थीं।
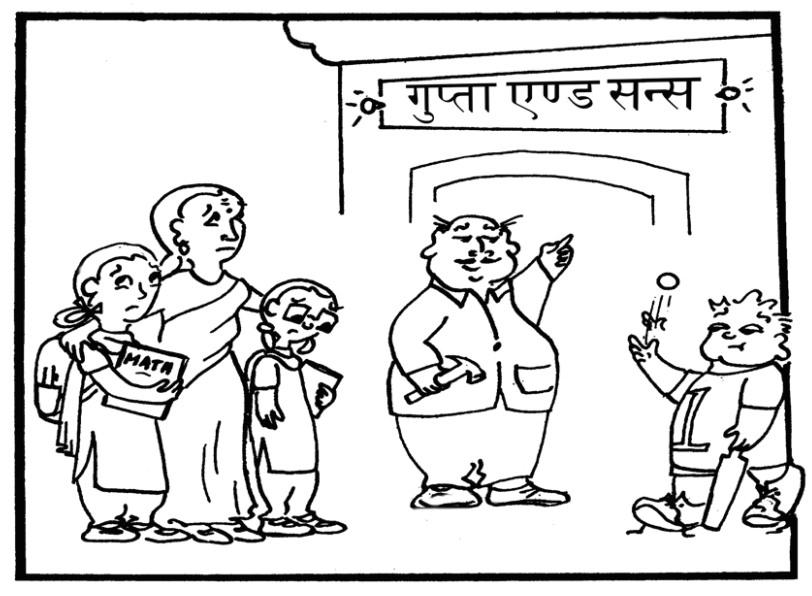
देखा जाए तो सिर्फ़ आदमी ही नहीं, ज़्यादातर औरतें भी बेटा ही चाहती हैं। इन सब कारणों के अलावा इसका एक और कारण है—जब बेटे की शादी होती है तो सास के रूप में औरत की हैसियत बढ़ जाती है।
बेटियों को बोझ समझा जाता हैबेटियाँ भारी बोझ मानी जाती हैं। हमारे समाज में बेटियों को पराया धन समझा जाता है। बहुत-से माँ-बाप मानते हैं कि बेटियों के रहन-सहन या खान-पान पर किया जानेवाला ख़र्च उन्हें नहीं, बल्कि उनके ससुरालवालों को फ़ायदा पहुँचाता है। अगर बेटी काम करती हो और कमाती भी हो तो माँ-बाप उसकी कमाई पर कोई हक़ नहीं रखते, सब ससुराल को ही मिलता है। एक पुरानी कहावत है ‘बेटियों को पालना ऐसा है जैसे पड़ोसी के बगीचे में पानी देना।’
शायद सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बेटियाँ भारी आर्थिक बोझ हैं, ख़ास तौर पर ग़रीबों और आम लोगों के लिये। लगातार बढ़ता हुआ शादी और दहेज का ख़र्च इस सोच की वजह है। इसके अलावा बेटियों में कमाने की ताक़त भी बेटों से कम होती है। एक परंपरा यह भी है कि बेटियों को माँ-बाप की देखभाल करने का हक़ नहीं है। एक और बात जो बेटियों के हक़ में नहीं है, वह यह कि बेटियों की देखभाल बहुत सावधानी से करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे समाज में औरतें काफ़ी असुरक्षित हैं। बेटियों की ज़िम्मेदारी उनकी शादी के साथ ही ख़त्म नहीं हो जाती। पति के द्वारा या ससुराल द्वारा उसे तंग किया जाना या मारपीट करके उसे दु:खी करना हमारे समाज में आम बात है। अपनी बेटी के दु:ख को विवश होकर देखना माँ-बाप के दु:ख को और बढ़ाता है।
ऊपर लिखी सभी बातों का नतीजा यह होता है कि बेटियों का जन्म सुख देने के बजाय परेशानी का कारण बन जाता है। शायद हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिये—अगर हमारे सामाजिक रीति रिवाज माँ‑बाप को ही अपनी नन्ही बेटी के जन्म पर ख़ुश नहीं होने देते, तो हम क्या आशा रख सकते हैं कि वही समाज उस लड़की को आगे चलकर ख़ुशी और इज़्ज़त से जीने देगा?
दहेजप्रभुजी, मैं तोरी बिनती करूँ, पैंया पड़ूँ बार-बार,
अगले जन्म मोहि बिटिया न दीजे, नरक दीजे चाहे डार।
उत्तर भारत का एक लोकगीत
दहेज भारतीय समाज की एक ऐसी परंपरा है, जिसने कोई फ़ायदा पहुँचाने के बजाय समाज में सिर्फ़ ज़हर ही फैलाया है। कुछ समय पहले यह सोच थी कि जैसे-जैसे हमारे देश में तरक्की होगी और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, धीरे-धीरे अपने आप ही दहेज की प्रथा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके बिलकुल उलट हुआ है। पिछले बीस-तीस सालों में यह प्रथा काफ़ी बढ़ गई है। पहले तो दहेज प्रथा सिर्फ़ अमीरों में थी, लेकिन धीरे-धीरे इसने ग़रीब परिवारों में भी अपनी जगह पक्की बना ली है। इसका नतीजा यह है कि ग़रीब परिवार क़र्ज़े तले दबते जा रहे हैं।
जिन परिवारों में पैसों की तंगी है, वे दहेज की वजह से बेटी के जन्म को परेशानी की वजह मानते हैं। वे जानते हैं कि बेटी की शादी और दहेज का ख़र्चा उनकी पैसे की तंगी को कई गुणा बढ़ा देगा। ऐसी तंग हालत में भी दहेज न देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कई बार तो दहेज के लिये ‘न’ बोलने का मतलब अपने परिवार की बेइज़्ज़ती कराना और अपनी बेटी को ज़िंदगी भर कुँवारी रखना है।
भारत में हर घंटे में एक दहेज हत्या होती है!
अफ़सोस की बात यह है कि कई परिवारों में दहेज सिर्फ़ एक बार दिये जानेवाली धन-संपत्ति नहीं है, इसकी माँग तो शादी के कई साल बाद तक होती रहती है। धार्मिक त्यौहार और बच्चों के जन्म के मौक़ों पर भी पैसे, कार या घरेलू वस्तुओं की माँग की जाती है। अगर लड़की के परिवारवाले रोज़-रोज़ होनेवाली इन माँगों को पूरा नहीं कर पाते तो बहुओं के साथ बदसलूकी, मारपीट करना या तलाक़ की धमकी देना आम बात है।
ज़्यादातर मामलों में लड़की के माँ-बाप को पता होता है कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन वे इसके ख़िलाफ़ कुछ बोल नहीं पाते, इस डर से कि कहीं समाज उनके ख़िलाफ़ न हो जाए। कई बार यह बुरा व्यवहार सहना इतना मुश्किल हो जाता है कि अपने माँ-बाप को और ज़्यादा परेशानियों और क़र्ज़ के बोझ से बचाने के लिये कई जवान लड़कियाँ आत्महत्या तक कर लेती हैं। कई बार बहुओं को ससुरालवाले मार देते हैं और कह देते हैं ‘रसोई में दुर्घटना हुई है’ ताकि वे अपने बेटों की दोबारा शादी कर सकें। यह दूसरी शादी भी एक नये सिरे से पैसा कमाने का ही ज़रिया होती है।
यूँ तो दहेज प्रथा पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन आजकल दहेज से जुड़े अपराध बहुत बढ़ गए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है—दुनियावी पदार्थों का बढ़ता लोभ। भारत में दहेज हत्या का पहला मामला 1970 के आसपास सामने आया था।
हैरानी की बात यह है कि:
- आज लगभग हर घंटे में कहीं न कहीं एक दहेज हत्या का मामला किसी कचहरी में दर्ज किया जाता है।13
- हर 7 मिनट में पति और उसके परिवारवालों के निर्दयी बर्ताव के मामले की रिपोर्ट होती है।13
बार-बार औरतें पुलिस के पास शिकायत लेकर जा रही हैं, क्योंकि उनके पति के परिवारवाले दहेज की वजह से उन पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन कचहरी में दर्ज किये गए मामले दहेज अपराध की असली संख्या से काफ़ी कम हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से मामले हैं जो दर्ज ही नहीं करवाए जाते। ज़्यादातर औरतें ससुराल में चुपचाप अत्याचार सहती रहती हैं, क्योंकि पैसों के मामले में वे अपने पति पर निर्भर होती हैं या अपने बच्चों की ख़ातिर या फिर इसलिये कि पति के घर के सिवा उनके पास और कोई ठिकाना नहीं है। घर छोड़कर जाएँ तो कहाँ जाएँ? आश्रय स्थल आम तौर पर न साफ़ होते हैं और न सुरक्षित। समाज भी घर छोड़नेवाली औरतों को दोषी मानता है और माँ-बाप समाज के डर से अपनी बेटी को आसरा नहीं देते। ऐसे मामलों में कानून भी सख़्ती नहीं बरतता।
लाचार औरत के पास क्या चारा है? वह बेचारी चुपचाप घोर अत्याचार सहती रहती है।
बेटे की चाह, दहेज प्रथा और हमारे लोभ का असरहालाँकि बेटे की चाह और दहेज प्रथा पुरानी परंपराएँ हैं, लेकिन अब ये भारत में नयी विचारधारा के साथ मिलकर नया रूप ले रही हैं। आज आधुनिक सुविधाओं के साथ शानशौक़त की ज़िंदगी जीने का अंदाज़ टी.वी. पर रोज़ दिखाया जा रहा है। जो लोग इस ‘शानशौक़त की ज़िंदगी’ की चाह रखते हैं, उन्होंने दहेज के रूप में दौलत पाने का एक आसान तरीक़ा ढूँढ़ निकाला है। इसके अलावा लोग दिखाना चाहते हैं कि समाज में उनका कितना ऊँचा स्थान है। इसलिये वे समझते हैं कि बेटों का होना बहुत ज़रूरी है। बेटे ज़्यादा कमाते हैं, बेटे दहेज लाते हैं, बेटे संपत्ति को बढ़ाते हैं और इसे परिवार में ही रखते हैं। इसके अलावा बेटे विदेशों में काम करने जाते हैं जिससे माँ-बाप का सामाजिक रुतबा और बढ़ता है। इसके फलस्वरूप बेटों की चाह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
अब यह नौबत आ गई है कि परिवार में बेटा पैदा होना माँ-बाप के लिये शान की बात है, जबकि बेटी का पैदा होना माँ-बाप के लिये दु:ख की बात है।
बेटे की चाह और दहेज प्रथा गंभीर सामाजिक बुराइयाँ हैं जिनका हमारी बेटियों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दु:ख की बात तो यह है कि इन सामाजिक बुराइयों से लड़ने के बजाय, हम इनका हल बेटी पैदा होने से पहले ही उसकी हत्या के ज़रिये ढूँढ़ रहे हैं। हम यह सोचते हैं कि अगर बेटी नहीं होगी तो परेशानी भी नहीं होगी।
लिंग चुनावजन्म लेते ही छोटी बच्चियों को मार देने की प्रथा ‘कन्या हत्या’ भारत में कई सदियों से चली आ रही है।
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नवजात बच्चियों को मारने का रिवाज इतिहास की जड़ों में है। परिवार के मुखिया के कहने पर दाई बच्ची के एक हाथ में गुड़ और दूसरे में रूई की पूनी रखकर कहती थी, ‘पूनी कत्तीं ते गुड़ खाईं वीरे नूं भेजीं, आप न आईं।’ फिर बच्ची को मिट्टी की हाँडी में डालकर, हाँडी का मुँह बंद कर दिया जाता था और दाई उसे दूर सुनसान जगह पर रख आती थी। चूँकि समाज में इसकी मंज़ूरी थी, अत: न तो इसे पाप माना जाता था और न ही अपराध।
डॉक्टर कीर्ति केसर ने जैसा विकास शर्मा को बताया ‘वक़्त बदल देगा तसवीर’ दैनिक भास्कर, 22 अक्तूबर, 2009
आशा के उलट ‘कन्या हत्या’ की प्रथा कम होने के बजाय पिछले कुछ दशकों से बढ़ती जा रही है।
जब लड़के का जन्म होता है तो औरतें थाली बजाकर या हवा में आग उछालकर उसके जन्म की घोषणा करती हैं। लेकिन अगर लड़की पैदा हो जाए तो परिवार की कोई बुज़ुर्ग औरत जाकर परिवार के आदमियों से पूछती है, ‘बारात रखनी है या लौटानी है?’ अगर आदमी जवाब दें ‘लौटानी है’ तो सब लोग चले जाते हैं और जच्चा माँ को नन्ही बेटी के मुँह में तंबाकू रखने के लिये कहा जाता है। जच्चा माँ के इस बात का विरोध करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि विरोध का मतलब है, जच्चा माँ की जान को ख़तरा या उसे घर से निकाला जाना।
निजी बातचीत पर आधारित, 45 मिलियन डॉटर्स मिसिंग 14
आज नयी-नयी तकनीकों के आने से ‘कन्या हत्या’ की प्रथा एक ज़्यादा ख़तरनाक प्रथा, ‘कन्या भ्रूणहत्या’ में बदलती जा रही है। अब ऐसी-ऐसी मशीनें आ गई हैं जिनसे गर्भ में ही बच्चे के लिंग का पता लगाया जा सकता है। यह पता लगने पर कि गर्भ में एक लड़की पल रही है, कई माँ-बाप उसे गिराने का फ़ैसला कर लेते हैं।
लिंग चुनाव की दर क्या है?हमारे देश में लिंग जाँच कितने लोग करवाते हैं, इसका पता लिंग अनुपात से चलता है—इसका मतलब यह है कि 1000 आदमियों की तुलना में औरतों की संख्या कितनी है। बहुत-से देशों में औरतों की संख्या आदमियों से ज़्यादा है। ऐसा इसलिये, क्योंकि आदमियों की तुलना में औरतें कई ज़्यादा साल तक ज़िंदा रहती हैं। वर्ष 2008 में जापान में 1000 आदमियों की तुलना में 1053 औरतें थीं और अमेरिका में 1027 थीं, जबकि उसी साल भारत में औरतों की संख्या 1000 आदमियों की तुलना में सिर्फ़ 936 ही थी।
लिंग चुनाव का पता लगाने का एक और भी अच्छा तरीक़ा है, बच्चों का लिंग अनुपात देखना: 0-6 साल की उम्र के 1000 लड़कों में कितनी लड़कियाँ हैं? 2001 की जनगणना में 1000 लड़कों में से सिर्फ़ 927 लड़कियाँ थीं।
एक अनुमान के अनुसार हमारी जनसंख्या में से 5 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें कम हैं। इसकी एक मुख्य वजह लिंग चुनाव है। यूनाइटेड नेशन्स फ़ैमिली प्लानिंग एसोसिएशन (UNFPA) की एक रिपोर्ट के अनुसार 1991 में भारतीय जनसंख्या में 4 करोड़ 80 लाख औरतों की कमी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर केरल प्रदेश जैसा लिंग अनुपात पूरे देश में होता तो भारत में 4 करोड़ 80 लाख औरतें और होतीं।15 अगर 1991 की जनगणना में कम होनेवाली औरतों की संख्या इतनी ज़्यादा थी, तो आज यह कितनी बढ़ी होगी? इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
शायद हमारे मन में यह ख़याल आता है कि ऐसी घटनाएँ गाँवों में ज़्यादा होती होंगी या ग़रीब और अनपढ़ लोगों में। लेकिन सच्चाई इसके उलट है।
लिंग चुनाव गाँव के बजाय शहरों में ज़्यादा हो रहा हैगाँव के बजाय शहरी इलाक़ों में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है, ख़ासकर बड़े शहरों में। आज कुछ गिने-चुने शहरी समाजों में तो 1000 लड़कों की तुलना में सिर्फ़ 300 लड़कियाँ ही हैं। इसका कारण है कि शहरों में लिंग चुनाव की तकनीक का फ़ायदा आसानी से उठाया जाता है।
लिंग चुनाव ग़रीबों से ज़्यादा अमीर कर रहे हैंउम्मीद के उलट अमीर और मध्यम आमदनी के लोग, ग़रीब लोगों के बजाय कई गुणा तेज़ी से अपनी बेटियों को मार रहे हैं। ग़रीब आदमी बेटी को गर्भ में इस डर से मार डालता है कि वह उसके लिये दहेज कैसे जुटाएगा? अमीर परिवारों में दहेज इकट्ठा करना दिक्क़त की बात नहीं होती, लेकिन परिवार का कारोबार या ज़मीन वे बेटे को ही देना चाहते हैं। इसलिये वे बेटे की चाह से मन नहीं हटा पाते।
लिंग चुनाव अनपढ़ों से ज़्यादा पढ़े-लिखे कर रहे हैंशायद हम सोच रहे हैं कि शिक्षा के ज़रिये लिंग चुनाव की समस्या को दूर किया जा सकता है, लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि आज पढ़े-लिखे परिवार अनपढ़ परिवारों की तुलना में कहीं ज़्यादा लिंग चुनाव करते हैं। पढ़े-लिखे, शहरी और अमीर माँ-बाप छोटा परिवार चाहते हैं। उन्हें नयी-नयी तकनीकों का ज़्यादा पता रहता है। वे अल्ट्रासाउंड और गर्भपात का ख़र्च भी आसानी से उठा सकते हैं। इसका नतीजा यह है कि अब ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग अपने परिवार को ‘संतुलित’ करने के लिये इस तकनीक का इस्तेमाल करने लगे हैं।
पी.सी. & पी.एन.डी.टी. (PC & PNDT) कानून को 1994 में बनाया गया और 2003 में बदला गया था। इस कानून के मुताबिक़ लिंग चुनाव ग़ैरकानूनी और सज़ा के लायक़ है। इस कानून को सख़्ती से लागू न किये जाने की वजह से सरकार इस भयानक जुर्म को रोक नहीं पाई है।
पुस्तक के अंत में ‘आख़िरी संदेश’ में लिंग चुनाव के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी गई है। लिंग चुनाव अब हमारे देश में कितना बढ़ गया है? सरकार और समाज इसका क्या हल निकाल रहे हैं? जो औरतें रोज़ यह अन्याय सह रही हैं, उनका क्या अनुभव है? इन सब सवालों के जवाब आख़िरी अध्याय में हैं।
एक सोची समझी नीति के अनुसार हमारे समाज में
बेटियों की सत्ता को मिटाया जा रहा है।
स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कुछ लोग इसे गुप्त रूप से हो रहा
जनसंहार और क़त्ले आम कहने लगे हैं।
हमारी करनी का नतीजा
जब तक हम बेटी के जन्म का भी वैसे ही स्वागत नहीं करते जितना बेटे के जन्म का, तब तक हमें समझना चाहिये कि भारत विकलांग रहेगा।
महात्मा गांधी
सच्चाई तो यह है कि आज हमारा देश विकलांग है। क्या औरतों के प्रति इतनी लापरवाही, असमानता और अत्याचार का बर्ताव यों ही लगातार चलता रहेगा? इसके दु:खदायी नतीजे क्या हो सकते हैं? हम ज़रा चारों तरफ़ नज़र दौड़ाएँ और देखें कि असमानता और लिंग चुनाव का हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है।
नारी जाति पर प्रभाव‘शत पुत्रवती भव’ (तुम सौ पुत्रों की माँ बनो), यह एक बड़ा मशहूर आशीर्वाद है जो नयी शादीशुदा लड़कियों को अकसर दिया जाता है। हमारे देश में औरतों पर बेटा पैदा करने का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, इस हद तक कि अगर वे बेटा न पैदा कर पाएँ तो उन्हें यह बताया जाता है कि वे ज़िंदगी में हार गई हैं, वे कुछ नहीं कर पाईं। कई बार उनको धमकाया जाता है कि अगर वे गर्भ में पल रही लड़की को नहीं गिराएँगी, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा या तलाक़ दे दिया जाएगा।
हर औरत की इच्छा होती है कि वह कम से कम एक बेटे की माँ बने। जिस औरत का कोई बच्चा न हो उसे अधूरी माना जाता है और जिसकी केवल बेटियाँ हों, उसे भी कुछ हद तक अधूरी ही माना जाता है। औरत को समाज में इज़्ज़त तभी मिलती है, जब वह बेटे को जन्म देती है।
एक व्यक्ति के विचार, ‘सायलेंट जेनोसाइड’, अरूती नैयर, द ट्रिब्यून, 6 मई, 2001 12
गर्भपात के कारण औरतों की सेहत के लिए ख़तरा बढ़ता जा रहा है। लिंग चुनाव से जुड़े सभी गर्भपात चौथे से छठे महीने में होते हैं। जब औरतें गर्भपात के लिये चौथे, पाँचवें या छठे महीने तक इंतज़ार करती हैं, तब उनकी मौत का ख़तरा लगभग दस गुणा ज़्यादा होता है। ऐसी भी मिसालें हैं कि परिवार में बेटे को जन्म देने की चाह को पूरा करने के लिये औरत को लगातार आठ बार गर्भपात करवाना पड़ा। भारत में ज़्यादातर औरतें ‘ख़ून की कमी’ का शिकार हैं और लगातार गर्भपात से उनकी सेहत ख़राब हो जाती है। बहुत-सी औरतें शारीरिक पीड़ा और दिमाग़ी तनाव में रहती हैं, क्योंकि उन्हें बार-बार गर्भपात के लिये मजबूर किया जाता है। कितनी ही ग़रीब औरतें गर्भपात के वक़्त पूरी सुविधाएँ न मिलने के कारण बीमारियों का शिकार हो जाती हैं या बिस्तर पर पड़ जाती हैं, यहाँ तक कि कई बार उनकी मौत भी हो जाती है।
आदमी और औरत में अलग-अलग गुणसूत्र (क्रोमोसोम्ज़) होते हैं। गुणसूत्र दो तरह के होते हैं—X और Y। विज्ञान हमें बताता है कि बच्चे के जन्म में औरत सिर्फ़ X गुणसूत्र देती है। अगर आदमी X गुणसूत्र देता है तो लड़की पैदा होगी और अगर आदमी Y गुणसूत्र देता है तो लड़का पैदा होगा।
इसलिये बच्चे का लिंग आदमी के गुणसूत्रों से ही तय होता है। इसमें औरत का कोई हाथ नहीं होता।
बच्चों पर प्रभाव
आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। माँ ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है। बच्चे के जीवन पर उसका गहरा असर पड़ता है। ज़्यादा दहेज लाने की माँग से या सिर्फ़ बेटे को ही जन्म देने के दबाव से जो माँ हर वक़्त दु:खी और परेशान हो, वह अपने बच्चों के जीवन में ख़ुशी और शांति कैसे ला सकती है? जिस घर में माँ को हर वक़्त दबाया और सताया जाता हो, उस घर के मासूम बच्चों से हम आदर्श जीवन जीने की क्या उम्मीद रख सकते हैं? ज़रा सोचिये! ऐसे बच्चे बड़े होकर समाज में कैसा व्यवहार करेंगे?
आदमियों पर प्रभावआज लिंग चुनाव की वजह से हमारे समाज में औरतों की बहुत कमी हो रही है। औरतों की इस कमी की वजह से कई आदमी अपना जीवन साथी नहीं ढूँढ़ पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आनेवाले समय में ज़िंदगी को ख़ुशियों से भरपूर करनेवाली पत्नी को साथी और सहयोगी के रूप में पाना, कई आदमियों के लिये सपना बनकर रह जाए।
हमारे समाज में शादी एक ज़रूरी रस्म मानी जाती है। आम तौर पर शादीशुदा और बाल-बच्चेवाले परिवार को बिरादरी में ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। जो आदमी अपने लिये जीवन साथी नहीं ढूँढ़ पाते, वे समाज से अलग होने का दर्द और अकेलेपन को महसूस करते हैं।
समाज में औरतों के प्रति बढ़ता अपराधजो लोग लिंग जाँच कराना चाहते हैं, वे कहते हैं कि लिंग चुनाव से औरतों का फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। वे कहते हैं कि अगर समाज में औरतें कम होंगी तो उनकी माँग बढ़ेगी और इससे समाज में उनकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी।
जो जैसे चल रहा है उसको बिना रोके वैसे ही चलने दो। इससे औरतों की क़द्र बढ़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब औरतें, आदमियों को ले जाने के लिये घोड़ों पर चढ़कर आएँगी।
गर्भपात के पक्ष में बहस करते एक डॉक्टर की राय, ‘सायलेंट जेनोसाइड’ अरूती नैयर, द ट्रिब्यून, 6 मई, 2001 12
लेकिन सच्चाई इसके बिलकुल उलट है। इतिहास गवाह है कि समाज में जब भी औरतों की कमी होती है, उस वक़्त औरतों के प्रति ज़ुल्म कम नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं। आज भारत में जिस गाँव या शहर में औरतों की कमी है वहाँ औरतों के प्रति ज़ुल्म बढ़ रहे हैं। सन् 2007 में औरत संबंधी अपराधों के निम्नलिखित मुख्य तथ्य सामने आए:13
- हर 48 मिनट में एक औरत अश्लीलता और ज़बरदस्ती का शिकार हुई।
- हर 26 मिनट में एक औरत या नाबालिग़ लड़की का अपहरण हुआ।
- हर 25 मिनट में एक औरत का बलात्कार हुआ।
- हर 14 मिनट में औरत के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई।
इन वारदातों का हमें तब पता चलता है जब कोई मामला दर्ज होता है। सच्चाई तो यह है कि हमारे देश में औरतों के ख़िलाफ़ ज़्यादातर अपराधों को दर्ज ही नहीं किया जाता और न ही कराया जाता है।
यूनाइटेड नेशन्स इंटरनेशनल चिल्डरेन्ज़ ऐमर्जैंसी फ़ंड (UNICEF) की एक रिपोर्ट के अनुसार ‘भारत में बच्चों का लिंग अनुपात तेज़ी से बिगड़ रहा है। इसके कारण आनेवाले समय में ज़्यादातर लड़कियों की कम उम्र में ही शादी हो जाया करेगी। ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। कम उम्र में बच्चा पैदा करनेवाली औरतों की मौत की संख्या बढ़ेगी। लड़कियों और औरतों के प्रति अत्याचार बढ़ेंगे जैसे—बलात्कार, अपहरण, लड़कियों का व्यापार और एक औरत का कई आदमियों के साथ ज़बरदस्ती शादी कराने का रिवाज।’16
औरतों का व्यापार और द्रौपदी प्रथाभारत में ग़रीब इलाक़ों या पिछड़ी जातियों की लड़कियाँ ख़रीदकर उनसे ज़बरदस्ती शादी करने का रिवाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। औरतों के इस व्यापार को दलाल चला रहे हैं और यह व्यापार ख़ूब फल-फूल रहा है। इन ख़रीदी हुई औरतों के पास अपनी शादी का कोई पक्का सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से उनके पति के दोस्त और रिश्तेदार भी उन्हें सताते हैं। इन औरतों को सिर्फ़ अपने पति की ही नहीं, बल्कि उसके भाइयों की भी पत्नी बनने के लिये मजबूर किया जाता है। ऐसी भी मिसाल है जहाँ एक औरत की आठ भाइयों के साथ शादी हुई है। इन औरतों को ‘द्रौपदी’ बुलाया जाता है। परिवार और समाज में इनको सबसे नीचा दर्जा दिया जाता है। अपने ही परिवार में, अपने ही आदमियों के हाथों, इनका लगातार बलात्कार होता है और मारपीट भी होती रहती है।
समाज में बढ़ती अशांतिभारत के बहुत-से गाँवों और शहरों में ऐसे कई आदमी हैं जो औरतों की कमी की वजह से जीवन साथी नहीं ढूँढ़ पा रहे हैं और समाज से अलगाव महसूस करते हैं। जब इस तरह के आदमियों की संख्या बढ़ जाती है, तब इनके अपराध करने की संभावना भी बढ़ जाती है। ऐसे हालात में मारपीट, दंगा-फ़साद और अत्याचार की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। समाज से अलग हुए ये आदमी समाज की सुरक्षा और शांति के लिये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाते हैं।17
क्या हम ऐसे दूषित समाज में जीना पसंद करेंगे?
क्या हम अपने बच्चों को यही आदर्श और मूल्य
विरासत में देना चाहते हैं? आओ! ज़रा उन रीति
रिवाजों पर नज़र डालें जो हमारी चाहतों को
प्रेरणा देते हैं।
हम क्या चाहते हैं?
जब भी समाज में अत्याचार होता है—आत्मसम्मान
इसी में है कि उठो और कहो कि यह अत्याचार
आज ही ख़त्म करना होगा, क्योंकि न्याय पाना मेरा
हक़ है।
सरोजिनी नायडू
इस किताब में दी गई जानकारी को पढ़कर हमारे मन को शायद धक्का लगा होगा। ऐसा होना भी चाहिये। जब हम इस बात को हर तरफ़ से देखते हैं कि लिंग चुनाव में हो रही बढ़ोतरी का नतीजा कितना भयंकर हो सकता है तो इसकी चिंता हमें होनी भी चाहिये। इसी बात पर हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे।
हम समाज में क्या चाहते हैं?क्या हमारा देश क़ातिलों का देश है? हमारी बेटियों की रक्षा की ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या एक लड़की को हमारे देश में पैदा होने का हक़ नहीं है?
आख़िर कब तक हम अपने रीति रिवाजों के नाम पर औरतों पर अत्याचार करते रहेंगे? हम अपने रिवाजों पर एक नज़र डालें तो हमें क्या दिखाई देता है? हमारे समाज में शादी के बाद ज़्यादातर औरतों को अपने माँ-बाप से अपना रिश्ता ख़त्म ही करना पड़ता है। जब माँ-बाप बूढ़े हो जाते हैं तो औरत को यह हक़ नहीं दिया जाता कि वह उनकी सेवा कर सके। इस रिवाज से समाज को क्या फ़ायदा मिलता है? मौत के बाद ज़्यादातर माँ-बाप अपना सब कुछ बेटे के नाम छोड़ जाते हैं। क्या एक बेटी का कोई हक़ नहीं बनता? हमारे समाज की उन्नति में इन पुराने रिवाजों का क्या हाथ रहा है? कुछ भी नहीं। जब हम संविधान को एक तरफ़ रखकर देश की आधी आबादी को सेहत, पढ़ाई और आज़ादी का बराबर हक़ नहीं देते तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा?
इक्कीसवीं सदी में दहेज जैसे रिवाज की क्या ज़रूरत है? दहेज में एक परिवार को सब कुछ मिलता है, दूसरे परिवार को सब कुछ देना पड़ता है। आज के ज़माने में यह एकतरफ़ा रिवाज क्यों? जिस तरह सती के रिवाज को हमने इतिहास के पन्नों में दफ़न किया था, उसी तरह क्या आज वह समय नहीं आ गया कि दहेज के रिवाज को भी हम दफ़ना दें?
बेटियों की हत्या के बाद माँ-बाप अपने बेटों के लिये बहुएँ कहाँ से लाएँगे? ज़रा सोचें! जब हमारे समाज में हज़ारों, लाखों आदमी ऐसे होंगे जो औरतों की कमी की वजह से शादी नहीं कर पाएँगे, वे समाज से नाराज़ रहेंगे और अपने आप को समाज से अलग मानने लगेंगे, तब हमारे समाज की हालत कितनी ख़तरनाक हो जाएगी? आज जिस तेज़ी से औरतों के प्रति ज़ुल्म बढ़ रहे हैं, क्या उन्हें देखकर हमारा मन बेचैन नहीं होता? क्या हमें डर नहीं लगता? औरतों की कमी की वजह से औरत को ख़रीदकर ज़बरदस्ती बहू बनाना या एक औरत को ‘द्रौपदी’ बनाकर चार भाइयों के बीच बाँटना—क्या ये रिवाज हमें सही लगते हैं? क्या यही है हमारे देश का भविष्य?
जब हम अख़बार में पढ़ते हैं कि दहेज की वजह से किसी औरत को जला दिया गया या लड़की होने के कारण किसी बेटी को गर्भ में ही मार दिया गया तो हम अख़बार के पन्नों को पलटकर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम इन्हीं बातों को सालों से पढ़-पढ़कर पत्थरदिल हो गए हैं? या शायद हम सोचते हैं कि इन रिवाजों को बदलने की ताक़त तो हममें है ही नहीं, इसलिए हम शिथिल पड़ गए हैं! लेकिन सोचने की बात यह है—इस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ अगर हम आवाज़ नहीं उठाएँगे तो कौन उठाएगा?
हम परिवार में क्या चाहते हैं?कितने ही लोग अपनी आदतों से मजबूर हैं। कितने लोग लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। इनमें कुछ लोग बेख़बर हैं, कुछ डरे हुए हैं और कुछ बेपरवाह हैं। अगर हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें हर वक़्त सचेत रहना होगा।
एल्बर्ट आइंस्टाइन
हम भारतवासी अपने मूल्यों पर बहुत गर्व करते हैं। एक क्षण के लिये रुककर ज़रा विचार करें ìक्या हैं हमारे मूल्य? क्या हैं हमारे आदर्श? अपने बेटे से प्यार करना लेकिन अपनी बेटी से नहीं या अपने बेटे से प्यार करना लेकिन अपनी बहू से नहीं, क्या यही हैं हमारे आदर्श? कम उम्र में अपनी मासूम बेटी की शादी करवाकर उसे बेहद दु:ख पहुँचाना या दहेज के बाज़ार में उसे बेच देना, क्या यही हैं हमारे उसूल? अपनी मौत के बाद बेटी के लिये कुछ नहीं छोड़ जाना या बेटी को गर्भ में ही मार देना, क्या यही हैं हमारे मूल्य? क्या ये सब गर्व की बातें हैं?
हमारी कोशिश तो यह होनी चाहिये कि हम ऐसा परिवार बनाएँ जिसमें सबको एक समान प्यार, इज़्ज़त और शिक्षा तथा एक समान मौक़ा मिले, ताकि ज़िंदगी में वे कुछ बन सकें। यह बात शायद हम जानते ज़रूर होंगे कि परिवार के किसी एक सदस्य के साथ अगर हमारा बर्ताव ठीक नहीं है, तो इसका बुरा असर सारे परिवार पर पड़ता है।
अगर हम अपने बच्चों को सही उसूलों से जीने की शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे अपने उसूल उसी समाज से सीखेंगे जिसमें वे पले हैं। फिर उसका नतीजा हमारे बच्चों और हमें, दोनों को ही भुगतना पड़ेगा।
स्टीफ़न कवी
विवाह हमारे समाज और सभ्यता का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। शादी को सफल बनाने के लिये दो का होना ज़रूरी है—एक औरत और एक मर्द—एक दूसरे का साथ निभाते हुए वे ज़िंदगी का सामना करते हैं। शादी के बाद आदमी और औरत मिलकर एक परिवार बनाते हैं, यह परिवार समाज की दीवार की एक ईंट है, एक ज़रूरी हिस्सा है। समाज इस परिवार के ज़रिये अगली पीढ़ी को अच्छे संस्कार और आदर्श देता है। जब इसी परिवार के बच्चे अंदर ही अंदर दु:खी और बेचैन होते हैं, तो ये कमज़ोर बच्चे बड़े होकर समाज को कमज़ोर बनाते हैं।
जो परिवार में ख़ुशियाँ बाँटता है, जिसके बच्चों को सही शिक्षा और अच्छे संस्कारों का मज़बूत आधार मिलता है, उस परिवार के बच्चों में आत्मसम्मान होता है और वे बड़े होकर समाज को नयी दिशा में ले जाते हैं।
हम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं?क्या परमात्मा कोई ग़लती करता है जब वह हमें लड़की देता है? क्या हम सोचते हैं कि हम भगवान् बन गए हैं जो हम परमात्मा की रज़ा में दख़ल देने की कोशिश करते हैं?
विज्ञान आगे बढ़ता ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन विज्ञान और आधुनिक तकनीक का प्रयोग हमारे हाथ में है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिये ताकि विज्ञान का सही इस्तेमाल हो सके। मिसाल के तौर पर एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके ज़रिये लाखों लोगों को बिजली पहुँचाई जा सकती है, लेकिन उसी तकनीक के ज़रिये लाखों लोगों को एक क्षण में मारनेवाला एटम बम भी बनाया जा सकता है। फ़ैसला हमारे हाथ में है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड तकनीक इसलिये बनाई गई थी ताकि हम शरीर में छिपी बीमारियों को ढूँढ़ पाएँ। इसी तकनीक के ज़रिये जच्चा और बच्चा की जान भी बचाई जाती है, लेकिन अफ़सोस! आज वही तकनीक बच्चे के लिंग की जाँच के लिये इस्तेमाल की जा रही है। यह सोच भी हमारे दिमाग़ की ही उपज है!
आज लिंग जाँच के बाद गर्भपात कराना हमारी अंतरात्मा को तो ग़लत लगता है, क्योंकि हमें मासूम बच्चे की जान लेनी पड़ती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता रहेगा। आज नयी वैज्ञानिक तकनीक पर खोज चल रही है, जिसके ज़रिये हम शुरू में ही डॉक्टर से कह पाएँगे कि हमें बेटा चाहिये तो बेटा ही होगा। इस तकनीक के ज़रिये, बच्चे को मारे बिना, गर्भपात किये बिना, हमें बेटा मिल जाएगा। अब हम अपने आप से यह सवाल पूछें—क्या ऐसा करना सही होगा? बिलकुल नहीं! क्योंकि लिंग चुनाव का अपराध तो फिर भी होगा। बच्चे के लिंग का चुनाव करना क्या हमारा काम है? वैज्ञानिक तकनीक इतनी तेज़ी-से बढ़ती जा रही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम यह भी चुन पाएँगे कि हमारा बेटा छ: फ़ुट लंबा, तेज़ दिमाग़वाला, सुंदर और बलवान् हो। क्या यह विकल्प हम स्वीकार करेंगे? सर्वगुण संपन्न बेटा पाने की हमारी कामना का क्या कहीं कोई अंत है?
ज़िंदगी में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा अहमियत है, उनको ऐसी चीज़ों के लिये नज़रअंदाज़ न करें जिनकी रत्ती भर भी अहमियत नहीं है।
गैटे
जीवन में सबसे अधिक अहमियत हमारी आत्मा की है, तो क्या धन दौलत, परिवार का नाम, शान और शौहरत, जिनकी ज़िंदगी के अंत में कोई क़द्र नहीं, इनके लिये अपनी आत्मा को बेच देना उचित है? हम बेटी की बलि देकर उसकी जगह बेटा पाकर अपनी संपत्ति और हैसियत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर बड़ी शानशौक़त से उसकी शादी करते हैं और उसमें ख़ूब दहेज पाने की उम्मीद रखते हैं। ऐसा करते हुए हम अपने क़ीमती उसूलों को क़ुरबान तो नहीं कर रहे? किसी भी जीव को दु:ख देकर क्या हम अपने जीवन में कभी ख़ुशी और शांति पा सकते हैं?
अपनी ज़िंदगी में, परिवार में और समाज में हम जो फ़ैसला
करते हैं, क्या हम उससे ख़ुश हैं? कुछ नहीं करना, यह भी
एक प्रकार की करनी है। चुप रहना, यह भी एक फ़ैसला
है। इस ज़ुल्म को रोकने के लिये अगर हम कुछ नहीं करते
तो अपनी चुप्पी का नतीजा हम सबको भुगतना पड़ेगा।
आध्यात्मिक दृष्टिकोण
अगर हम अपनी आत्मा को हारकर सारा संसार
जीत लें तो सोचिये! हमने क्या पाया?
मैथ्यू 16:26
हमने देखा है कि क़ुदरत में संतुलन बनाए रखने के लिये औरत का होना कितना ज़रूरी है। हम यह भी जान चुके हैं कि आजकल औरत कैसे हालात में से गुज़र रही है। यह भी साफ़ ज़ाहिर है कि अगर औरतों के प्रति असमानता इसी तरह चलती रही, तो समाज को कितना भयंकर नतीजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ़ धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो औरतों के साथ बेइंसाफ़ी के नतीजे बड़े गंभीर हैं।
सब धर्मों के संत-महात्मा और महान् विचारक हमें हर युग में साफ़-साफ़ लफ़्ज़ों में उपदेश देते रहे हैं कि आध्यात्मिक नज़रिये से औरत और आदमी बराबर हैं। औरतों की आज की दर्दनाक हालत देखकर वे संत-महात्मा क्या सोचते होंगे, यह सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिये।
क़ुदरत का संतुलन बिगाड़नाक़ुदरत में हमेशा संतुलन रहा है। संतुलन बनाए रखने के लिये भगवान् ने दुनिया में जोड़े बनाए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, जैसे—अँधेरा और रोशनी, दिन और रात, जवान और बूढ़ा, तेज़ और नर्म, औरत और मर्द। सृष्टि में संतुलन को बनाए रखने में इनकी अपनी-अपनी अहमियत है। औरत हो या मर्द, हर एक इनसान में क़ुदरती तौर पर औरत और आदमी दोनों के गुण मौजूद होते हैं। इसलिये औरत और आदमी दोनों मिलकर ही समाज में संतुलन क़ायम रखने के लिये अपना सहयोग देते हैं।
भगवान् ने हममें से कुछ को आदमी और कुछ को औरत क्यों बनाया है? क्योंकि औरत भगवान् के प्यार का एक रूप है और आदमी भगवान् के प्यार का दूसरा रूप है। दोनों को प्यार बाँटने के लिये बनाया गया है, लेकिन दोनों के प्यार का स्वरूप अलग है।
मदर टेरेसा
आजकल हमारे देश में लिंग चुनाव का प्रचलन बढ़ता जा रहा है जो हमारे समाज के लिये ख़तरे की निशानी है। कुछ इलाक़ों में तो आदमी ज़्यादा और औरतें कम होने की वजह से क़ुदरत का संतुलन बिगड़ने लगा है। जब समाज में आदमियोंवाले गुण ज़्यादा और औरतोंवाले गुण जैसे—नम्रता और सहनशीलता कम हो जाते हैं, तब समाज में अशांति फैल जाती है और इसका नतीजा समाज की बरबादी हो सकती है।
क़ुदरत अपना संतुलन ख़ुद बना लेती है। जब क़ुदरत के काम में हम अपना दख़ल देते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ने लगता है। ऐसे में क़ुदरत अपना संतुलन फिर से पाने की कोशिश करती है। संतुलन वापस लाने के लिये क़ुदरत जो तरीक़ा अपनाती है, वह हम सबके लिये बड़ा दु:खदायी हो सकता है।
मक़सद को ध्यान में रखते हुए कर्म करनाआओ! सोचें कि हमारे जीवन का असली मक़सद क्या है? अगर हमारा मक़सद परमार्थ है तो हमें अपने आप से सवाल पूछते रहना चाहिये, ‘क्या हमारे रोज़ के कार्य हमें उस मक़सद को हासिल करने के नज़दीक ले जा रहे हैं या उससे दूर?’ कई लोगों ने परमात्मा की पूजा के लिये एक ख़ास वक़्त और जगह तय की हुई है। उस वक़्त तो हम भगवान् की पूजा-पाठ की रस्म पूरी कर लेते हैं, लेकिन बाद में पूरा दिन हमारा ध्यान अपने असली मक़सद से हटा रहता है। ऐसी हालत में हम भ्रूणहत्या जैसे बहुत-से नीच कर्म कर बैठते हैं। दूसरों के साथ हमारा बर्ताव भी इतना कठोर और बुरा हो जाता है कि पूजा-पाठ के अच्छे कर्म का फल ख़त्म हो जाता है। क्या भगवान् रस्मी तौर पर की गई ऐसी पूजा क़बूल करेगा?
परमात्मा के दरबार में प्यार की एक रत्ती की क़ीमत भी दुनिया भर की धार्मिक रस्मों से कहीं ज़्यादा है।
हज़रत सुलतान बाहू, बैत 58
परमार्थ के ऊँचे मक़सद को पाने के लिये हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे ढाँचे में ढालना होगा, जिससे परमार्थ और स्वार्थ यानी रूहानियत और रोज़ाना की ज़िंदगी दोनों अलग-अलग न नज़र आएँ।
औरत को बराबरी का हक़संत हमें समझाते हैं कि हम सब परमात्मा के प्रकाश की किरणें हैं और हम सब पवित्र हैं।
एक नूर ते सभ जग उपजिआ, कउन भले को मंदे ॥
कबीर साहिब, आदि ग्रन्थ, पृ.134
आत्मा की शक्ति से आज हम ज़िंदा हैं उसका कोई लिंग नहीं है। भगवान् की नज़र में आदमी और औरत में कोई फ़र्क़ नहीं है—सब पवित्र आत्माएँ हैं, सब मालिक का रूप हैं और सब बराबर हैं।
हत्या करना पाप हैसंत-महात्मा हमेशा से कहते आए हैं कि हर जीव की ज़िंदगी क़ीमती है, उसकी अपनी अहमियत है। इसलिये हत्या करना पाप है। उनका उपदेश है कि ज़िंदगी देना या लेना मालिक के हाथ में है। भगवान् ने हमें यह हक़ नहीं दिया कि हम तय करें कि किसे ज़िंदा रखना है या किसे मारना है।
हत्या न करना।
बाइबल, मैथ्यू 5:21
आपको ग़रीबी के डर से अपने बच्चों की जान नहीं लेनी चाहिये। आपके और आपके बच्चों की देखभाल का इंतज़ाम हमने कर दिया है। बच्चों को मार डालना महापाप है।
क़ुरान [17:31]
प्रानी बध नहिं कीजियहि, जीवह ब्रह्म समान।
‘रविदास’ पाप नंह छूटइ, करोर गउन करि दान॥
रविदास दर्शन, पद 186
एक तरफ़ तो पेट में पलते हुए भ्रूण को हम ज़िंदा बच्चे के रूप में नहीं मान पाते, इसीलिये इस ग़लतफ़हमी का शिकार बने रहते हैं कि बच्चे में अभी जान नहीं पड़ी। दूसरी तरफ़ नवजात बच्ची की हत्या करना भी हमारे लिये आम बात हो गई है। बच्ची की हत्या करने के बाद हम अपने आप को गुनहगार तो ज़रूर महसूस करते हैं, क्योंकि माँ उस बच्ची को अपनी गोद में लेती है और हत्या करते वक़्त दाई भी देखती है कि वह बच्ची जीने के लिये कैसे हाथ पैर मारती है और चीख़ती है। पुराने ज़माने में बच्ची की हत्या के बाद घर में पंडित को बुलाकर पूजा-पाठ के ज़रिये देवी-देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि अंतरात्मा तो कोसती है कि हमने जो किया है वह ग़लत है।
अफ़सोस की बात यह है कि कन्या भ्रूणहत्या के वक़्त हमारी अंतरात्मा सोई होती है। डॉक्टर जब भ्रूणहत्या करता है, हम उस कमरे में नहीं होते, इसलिये हम अपने आप को इस पापकर्म के भागी नहीं समझते। इसके अलावा बच्ची ने अभी जन्म नहीं लिया होता, किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी होती और सबसे बड़ी बात यह है कि हम यह मानकर बैठ जाते हैं कि उसकी हत्या डॉक्टर ने की है, हमने नहीं। इस बारे में एक और तर्क दिया जाता है कि शिशु में आत्मा छठे महीने में प्रवेश करती है, इसलिये कन्या भ्रूणहत्या करना ग़लत काम नहीं है। हमें अपने आप से ज़रा पूछना चाहिये कि यह फ़ैसला लेनेवाले हम कौन हैं? इस तर्क में कहाँ तक सच्चाई है?
क़ुदरत ने माँ के गर्भ को इतना सुरक्षित बनाया है जहाँ मासूम शिशु अच्छी तरह पल सकता है। वह भ्रूण जो परमात्मा की एक अनमोल रचना है, मनुष्य जन्म में आने की तैयारी कर रहा होता है। इस भ्रूण में परमात्मा की अंश आत्मा बसती है, इसलिये उसे हर प्रकार का दु:ख-दर्द भी महसूस होता है। यह भ्रूण बच्ची के रूप में प्यार का वायदा लेकर आती है। उस मासूम की सुरक्षा और देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है।
दूसरे जीव को दु:ख देनाजब हम जीवों को परमार्थ की नज़र से देखते हैं तो हमारे अंदर दया भाव पैदा हो जाता है। हम यह समझने लगते हैं कि किसी की हत्या करना तो दूर की बात रही, हमें तो किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिये। हम अपनी बेटी, बहन, पत्नी या बहू का दिल दुखाकर यह आशा कैसे कर सकते हैं कि परमात्मा के घर में हमें कोई जगह मिलेगी?
अपनी इच्छाओं पर क़ाबू पानाकभी किसी के दिल को न दुखाओ। यह ऐसा पाप है जिसे मालिक भी माफ़ नहीं करता, क्योंकि यह परमार्थ की जड़ को ही काट देता है।
महाराज जगत सिंह
हम ज़रा सोचें ìजो हम कर रहे हैं, वह किस मतलब से कर रहे हैं? हम दहेज क्यों माँगते हैं? और अगर दहेज नहीं माँगते, लेकिन लड़कीवाले दे देते हैं तो हम उसे अपना हक़ समझकर क्यों ले लेते हैं? क्या हम समझते हैं कि लेना हमारा हक़ है और देना लड़कीवालों के नसीब में लिखा है?
क्या हमारी इच्छाएँ हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हैं? अच्छा टी.वी., नयी कार, बड़ा घर वग़ैरह पाने के लिये हम किस हद तक अपने उसूलों को क़ुरबान कर देते हैं? अगर हमारी सारी इच्छाएँ पूरी हो भी जाएँ तो क्या हमें सब्र आ जाता है? क्या हमारे मन में कोई नयी इच्छा नहीं जागती?
ज़िंदगी में हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिये कि हमारी इच्छाएँ हमारी ज़रूरतों से बाहर न जाएँ। अगर दुनियादारी की ख़ुशियाँ पाने के लिये हम एक बार भी अपनी ज़रूरतों से आगे निकल जाते हैं तो फिर उन इच्छाओं को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़रूरतों की हद पार करते ही हमारी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहती।
फ़िलोकैलिया
क्या हमने कभी इस बात पर ग़ौर किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी पदार्थों को पाने की लालसा का नतीजा हमें ही भुगतना पड़ेगा?
तुम ऐसी चीज़ों को पकड़े हो जो किसी और की हैं।
लेकिन मालिक सब सुनता है, सब जानता है।
इस लालच में खोकर
तुम नरक के कुएँ में गिर जाओगे,
बिलकुल बेख़बर हो कि आगे जाकर तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा।
गुरु अर्जुन देव
बेटे की इच्छा और पैसे के लालच में हम औरतों के ख़िलाफ़ न जाने कितने ही नीच और बेरहम कर्म कर बैठते हैं, लेकिन क्या बेटे और धन सच में हमारे हैं? जब हम दुनिया से जाएँगे, तो क्या हम इन्हें अपने साथ लेकर जाएँगे?
हमारे कर्मों का फलमूर्ख को यह सोच सताती रहती है
ये बेटे मेरे हैं,
ये धन मेरा है,
पर जब वह ख़ुद अपना नहीं है,
फिर ये बेटे उसके कैसे हो सकते हैं?
फिर ये धन उसका कैसे हो सकता है?
धम्मपद
कर्मों का कानून परमात्मा का बनाया हुआ है। सारा संसार कर्मों के कानून के मुताबिक़ चलता है। इस कानून के अनुसार हमारी हर सोच और हर कर्म का कोई न कोई नतीजा ज़रूर हमारे सामने आता है—जैसी करनी वैसी भरनी।
जेहा बीजै सो लुणै करमा संदड़ा खेत॥
गुरु अर्जुन देव, आदि ग्रन्थ, पृ.134
हमारी ज़िंदगी की हर करनी और सोच का हिसाब कर्मों के खाते में जमा किया जाता है। इन कर्मों का फल हमें या तो इस जन्म में या फिर अगले जन्मों में भुगतना ही पड़ता है। हम किसी भी हालत में कर्मों के फल से बच नहीं सकते। एक कहावत है कि कर्मों की चक्की धीमी चलती है, पर वह पीसती बड़ी बारीक़ी से है। इसके बारे में संत कबीर ने कहा है:
चलती चक्की देखि कै, दिया कबीरा रोय।
दुइ पट भीतर आइकै, साबित गया न कोय॥
कबीर साखी-संग्रह, पृ.66
महाभारत में एक कहानी है, जिससे हम कर्मफल के कानून को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और इस अभिशाप से वे बहुत दु:खी थे, परंतु कुछ पुण्य कर्मों की वजह से उनमें शक्ति थी कि वे अपने पिछले जन्मों के बारे में जान सकते थे। उन्होंने अंधेपन की वजह जानने के लिये अपने पिछले सौ जन्मों पर नज़र डाली, लेकिन उन्हें अंधेपन की कोई वजह नहीं मिली। पूछने पर भगवान् कृष्ण ने सलाह दी कि वे सौ जन्मों से भी पीछे के जन्मों पर नज़र डालें। राजा ने ऐसा ही किया और देखा कि किसी एक जन्म में उन्होंने बचपन के अनजानेपन में किसी जानवर को उसकी आँखों में काँटे चुभाकर अंधा कर दिया था। उस करनी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है, जिससे वे अंधे राजा के रूप में पैदा हुए।
ददै दोस न देऊ किसै दोस करंमा आपणिआ॥ जो मै कीआ सो मै पाइआ दोस न दीजै अवर जना॥
गुरु नानक देव, आदि ग्रन्थ, पृ.433
ग़लत काम करके भी हम कई बार बेफ़िक्र हो जाते हैं, क्योंकि हम दुनियावी कानून के शिकंजे से बच जाते हैं। हुज़ूर महाराज चरन सिंह जी कहा करते थे कि एक कमरे में अगर पाँच साल का बच्चा भी हो तो हम उस कमरे से एक पेंसिल भी नहीं चुराते, लेकिन परमात्मा के हमारे अंदर होते हुए भी हम क्या कुछ नहीं करते। इसलिये हमें सावधान रहना चाहिये—परमात्मा सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, हम उसे धोखा नहीं दे सकते।
धोखा मत खाओ; परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उडाया जाता;
क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, वही काटता है।
बाइबल, गलेशियन्ज़ 6:7
हमें इस ग़लतफ़हमी में कभी नहीं रहना चाहिये कि जो हम कर रहे हैं वह ठीक है, क्योंकि हम ऐसे कर्म या तो हालात से मजबूर होकर करते हैं या अपने प्रियजनों की ख़ातिर करते हैं। परमात्मा के दरबार में जब हमारे कर्मों का हिसाब होगा, तब इन कर्मों के लिये हमें ही ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। हमारे क़र्ज़ को कोई दूसरा नहीं चुका सकता।
हर आत्मा जो कुछ कर्म कमाती है, अपने लिये ही कमाती है। कोई किसी दूसरे के कर्मों का बोझ नहीं उठा सकता।
क़ुरान
हत्या करना महापाप है। यहाँ हर चीज़ की क़ीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि संसार में कोई भी चीज़ मुफ़्त नहीं मिलती। हमारे पास बेटा हो सकता है, धन भी हो सकता है, लेकिन जिस बेटे और धन को पाने के लिये हमने जो नीच कर्म किये, क्या उसके बाद हम कभी चैन से जी पाएँगे?
परमात्मा की रज़ा में रहनापरमात्मा की रज़ा में रहने का मतलब है कि इस बात को पल्ले बाँध लें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह बिना वजह नहीं हो रहा। हमने अपने पिछले जन्मों में जो कर्म किये थे, आज हम उन्हीं कर्मों का नतीजा भुगत रहे हैं। इसलिये अगर हमारी क़िस्मत में बेटी है तो यह मालिक की रज़ा है। हमें प्यार से उसका स्वागत करना चाहिये। माँ के गर्भ में बेटी का आना कोई दुर्घटना नहीं होती जिसका हमें इलाज करना पड़े, बल्कि यह उस कुल मालिक की रज़ा होती है।
उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
एक पंजाबी कहावत—महाराज चरन सिंह के शब्दों में
हम परमात्मा की रज़ा में क्यों नहीं रह सकते? हमें चिंता किस बात की है? हमें बेटा ही क्यों चाहिये? इसलिये कि वंश चलता रहे? इसलिये कि ज़मीन-जायदाद परिवार में ही बनी रहे? क्या बुढ़ापे में पैसे और सहारे के लिये? क्या अपने कारोबार या धन कमाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये? हमें ये सब चिंताएँ एक तरफ़ रख देनी चाहियें। हमें वही करना चाहिये जो सही है और जब बुरा वक़्त आए, हमें मालिक की तरफ़ मुँह मोड़ना चाहिये, इस विश्वास से कि वह हमारी मदद ज़रूर करेगा।
आपका चिंता करना यह बताता है कि आपको परमात्मा की रहमत में, ख़ुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है। मालिक को अपनी मौज के माफ़िक ही सबकुछ करने दो, उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश न करो। अपने आप को उसकी मौज और रज़ा में राज़ी रखो तो कभी दु:खी न होंगे।
महाराज जगत सिंह
जब परमात्मा फूलों की इतनी अच्छी तरह से देखभाल करता है जो आज हैं और कल नहीं होंगे, क्या वह तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा? तुम्हारे विश्वास में कमी है।
बाइबल, ल्यूक 12:23
अपने रिश्ते-नाते और दुनिया के साज़-सामान को अगर परमार्थ की नज़र से देखें तो सच्चाई हमारे सामने आ जाएगी और हमें एहसास होगा कि ये हमारे हैं ही नहीं। हमें जो मिला है वह कुछ समय के लिये है। इसलिये हम इन चीज़ों को अपना मानकर इनसे चिपक न जाएँ, अपने उसूलों के साथ समझौता न करें और न ही अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा से ऊपर मान लें। असल में सबकुछ मालिक का है, हम सिर्फ़ उन चीज़ों को सँभालनेवाले कारिंदे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना काम ईमानदारी और प्यार से करें और उस करनी का फल पूरे विश्वास के साथ मालिक के हाथों में छोड़ दें।
परमार्थ हमारा मूलअगर हम परमात्मा से मिलनेवाली हर चीज़ को उसकी बख़्श्शि समझकर अपनाएँ तो वह चीज़ पवित्र हो जाती है—अपमान सम्मान बन जाता है, कड़वाहट मिठास बन जाती है और अँधेरा प्रकाश बन जाता है। हर एक चीज़ में परमात्मा की महक आने लगती है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे परमात्मा का हाथ नज़र आने लगता है।
महाराज चरन सिंह
आइये! हम अपने आप से एक ज़रूरी सवाल पूछें—हम कौन हैं? शायद हम सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं, जो इस कठिन जीवन को जीने की कोशिश में लगे हुए हैं। ज़िंदगी का असली मतलब समझने के लिये हम कभी-कभी परमात्मा की खोज में भी लग जाते हैं, लेकिन संतों की सोच इससे बहुत ऊँची और अलग है। वे समझाते हैं:
हम केवल इनसान नहीं हैं जो रूहानियत का अनुभव कर रहे हैं, बल्कि रूहानी जगत् की आत्माएँ हैं जो इनसानी जीवन का अनुभव कर रही हैं।
पियेर तय्हार द शारदैं
यह विचार हमारी सोच को पलटने वाला है। क्या हम अपने आप को रूहानी जीव के रूप में देखते हैं? यह एक बहुत ज़रूरी और बुनियादी सवाल है, क्योंकि जिस नज़रिये से हम अपने आप को देखते हैं, उसी नज़रिये से हम सारी दुनिया को भी देखते हैं। ज़िंदगी में हम जो भी कर्म करते हैं, अपने नज़रिये से करते हैं। जब हममें आत्मसम्मान होगा, तभी हम दूसरों को सम्मान दे सकेंगे और जब हमें अपने अस्तित्व से प्यार होगा, हम दूसरों में भी प्यार बाँट सकेंगे। अपने आप को पवित्र आत्मा समझने लगेंगे और तब हम दूसरों के अंदर की पवित्रता को भी देख पाएँगे।
हम दूसरों से जो बर्ताव करते हैं वह एक आईना है जिसमें साफ़ झलक दिखाई देती है कि हम अपने आप को किस नज़र से देखते हैं।
अंत में यह कहा जा सकता है कि हम इस सच को अनदेखा नहीं कर सकते–एक बच्चे या भ्रूण को मारना पाप है। सोच के ज़रिये, शब्दों के ज़रिये या कर्मों के ज़रिये–किसी औरत का जी दुखाना पाप है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, उसे गाली देते हैं या उस पर ज़ुल्म करते हैं तो यह अच्छी तरह जान लें कि हमें अपनी करनी का नतीजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जब हम किसी को दु:ख देते हैं तो हमारी अपनी रूहानी तरक्की में रुकावट आ जाती है। इसलिये आओ! जागें और अपनी मानवता को पहचानें। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिये जिसमें हम सब जीवों को बराबर का दर्जा दें–चाहे वह आदमी हो या औरत, लड़का हो या लड़की। हम सब उस रूहानी नूर की किरणें हैं। जैसे कि कबीर साहिब ने कहा है:
एक नूर ते सभ जग उपजिआ, कउन भले को मंदे॥
पुराने रीति रिवाज तोड़े जा सकते हैं
किसी व्यक्ति से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज़ के, वह है इनसान की अंत:करण की आज़ादी—किसी भी हालत में अपना नज़रिया, अपना रास्ता, ख़ुद चुनने की आज़ादी।
विक्टर फ़्रैंक्ल
औरतों के दु:खों का ज़िम्मेदार कौन है? और इनका हल क्या है?
औरतें ही औरतों को दु:ख क्यों पहुँचाती हैं?हालाँकि ऐसा लगता है कि औरतों को आदमियों ने सताया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। लोग जल्द ही जान लेते हैं कि कई मामलों में औरतें ही औरतों को दु:ख पहुँचाती हैं। ऐसा क्यों? ख़ुद अत्याचार की शिकार होने के बावजूद कई औरतें दूसरी औरतों की मदद करने के बजाय उन्हें दु:खी क्यों करती हैं?
ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें बाहरी तौर पर दिखाई देता है कि एक माँ अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी की जान ले रही है या एक सास अपनी बहू को सता रही है। इन घटनाओं के पीछे औरत की क्या सोच है? उस औरत की सोच के पीछे क्या है?
एक ग़रीब या अनपढ़ औरत अपनी चौथी बेटी को जान से क्यों मार डालती है? क्योंकि शायद उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। अगर कोई चाहे कि बच्चे न हों तो उन्हें गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करना चाहिये; लेकिन उसका पति न गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करता है और न उसे करने देता है। बेचारी औरत के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वह एक और बच्चे को पाल सके, एक और दहेज का इंतज़ाम कर सके। शायद वह बच्चों को पैदा करने और पालने के चक्कर से बिलकुल तंग आ गई है, क्योंकि यह चक्कर न तो उसके बस में है और न कभी रुकता है। इसके अलावा शायद वह दुगुना बोझ उठा-उठाकर अब बेहद थक गई है—उसे बिना आराम, घर के बाहर भी काम करना है और घर की ज़िम्मेदारियों को भी निभाना है। शायद अब इस थकी-हारी औरत को एक ही रास्ता सूझता है—गर्भ गिरा देना।
यदि औरत निर्णय लेने में आज़ाद नहीं है तो जो वह मजबूरी में करती है उसे विकल्प नहीं कहा जा सकता।
एक अमीर पढ़ी-लिखी औरत, यह पता चलने पर कि गर्भ में कन्या है, गर्भपात क्यों कराती है? दुर्भाग्य की बात है कि औरत के पढ़े-लिखे और अमीर होने के बावजूद भी उसमें आत्मसम्मान की कमी पाई जाती है। शायद उस औरत के मन में यह बात पक्की तरह बैठा दी जाती है कि यही ‘ज़िंदगी का सच है’ कि बेटा होना ज़रूरी है—बेटा ही वंश को आगे बढ़ाता है, बेटा ही कारोबार और जायदाद का मालिक बन सकता है, बेटा ही बुढ़ापे में माँ-बाप का सहारा बनता है। शायद उस औरत पर पति और परिवार का बहुत दबाव बना रहता है कि ‘कोशिश करते रहो जब तक बेटा पैदा नहीं होता।’ इसलिये वह औरत इतना साहस नहीं जुटा पाती कि वह इस दबाव का विरोध कर सके।
औरतें आत्मसम्मान के साथ तो पैदा नहीं होतीं। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास—ये सब अनमोल तोहफ़े हैं जो माँ-बाप और समाज चाहें तो बेटियों को दे भी सकते हैं या उन्हें इनसे वंचित भी रख सकते हैं।
एक सास अपनी बहू को क्यों सताती है?
प्रीता मेहता (बदला हुआ नाम), उम्र 31 साल: जब से प्रीता ने एक बेटी को जन्म दिया है, उसकी सास उसको ताने देती रहती है कि उसके पति के चचेरे भाइयों के तो बेटे हुए हैं, लेकिन उसने अभी तक एक बेटे को भी जन्म नहीं दिया। उसकी सास ज़ोर डालती है कि परिवार का नाम आगे चलाने के लिये प्रीता को बेटा पैदा करना चाहिये। प्रीता कहती है, ‘मेरी सास ने मुझसे साफ़ तौर पर कहा है कि अगर लड़की हुई तो गर्भ गिरा देना।’ उसका पति भी अपनी माँ की बात को सही मानता है। प्रीता ख़ुद क्या चाहती है? ‘पता नहीं।
शेफ़ाली वासुदेव,‘मिसिंग गर्ल चाइल्ड’
औरतें दूसरी औरतों को दु:ख पहुँचाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक क़ैदी दूसरे क़ैदी पर अत्याचार करता है या जैसे एक भिखारी बच्चा गली के दूसरे भिखारी बच्चों को धमकाता है। हम इनसानों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब हम ज़रूरतमंद होते हैं तब एक और रोटी, कुछ और रुपये, थोड़ी ऊँची पदवी या थोड़ा ज़्यादा अधिकार और सुविधा पाने के लिये हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर परिवार में अनेक औरतें हैं और वे प्यार, इज़्ज़त, धन या देखभाल के मामले में एक आदमी पर निर्भर हैं, वह आदमी चाहे उनका पति, पिता, भाई या बेटा ही क्यों न हो, इस कारण उन औरतों में एक दूसरे के लिये ईर्ष्या बनी रहती है।
हमारे पुरुष प्रधान समाज में औरतों पर दबाव डाला जाता है कि वे अपने दायरे में रहें। अगर जन्म से ही बच्चों को सिखाया जाए कि औरतों का दर्जा आदमियों से नीचा है, तो बच्चे इस बात को सच मानने लगते हैं। लड़के रोब दिखाना शुरू करते हैं और लड़कियाँ दबने लगती हैं। बड़ी होकर लड़की में यह सोच घर कर जाती है कि औरतों को दबकर रहना चाहिये और वह अपनी बेटी और बहू को भी यही शिक्षा देती है।
मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में लड़की को बचपन से ही समझाया जाता था कि जवानी में विधवा होकर सती हो जाना, औरत अपनी क़िस्मत में लिखाकर लाती है। यह शिक्षा उसे किससे मिलती थी—माँ से। एक जवान लड़की को अपने पति की चिता पर जल जाने के लिये दुल्हन की तरह कौन तैयार करता था? उस विधवा के परिवार की औरतें, वे औरतें जो जानती थीं कि उन्हें भी पति की चिता पर सती होना पड़ सकता है।
एक औरत दूसरी औरत को इसलिये दु:खी करती है, क्योंकि उसको बचपन से ही यह पट्टी पढ़ाई जाती है कि उसका दर्जा आदमी से नीचे है। औरतों की इस सोच की वजह से ही समाज में पुरुषों की प्रधानता बड़ी कामयाबी से टिकी हुई है। हालात देखते हुए औरतें भी पुरुषों के प्रधान होने की मान्यता को मौन सहमति दे देती हैं।
अगर एक चिड़िया को बचपन से ही पिंजरे में बंद रखा जाए और फिर कई साल बाद पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया जाए, तो हम क्या उम्मीद रखते हैं कि वह उड़ जाएगी? अगर वह चिड़िया बाहर आ भी गई, कुछ वक़्त के बाद वह पिंजरे में ज़रूर लौटेगी, क्योंकि पिंजरे में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। यह जानते हुए कि उस पिंजरे में वह क़ैदी रहेगी, फिर भी उस पिंजरे की सुरक्षा को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उस पिंजरे के अलावा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा। उस चिड़िया के लिये आज़ादी ख़ुशी की बात नहीं, बल्कि एक डरावनी चीज़ है।
ठीक इसी तरह हमने बहुत-सी औरतों को अपंग बना दिया है। इन औरतों को परखने के बजाय हमें अपना दिल खोलकर उनका साथ देना चाहिये, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिये, क्योंकि दोष इन औरतों में नहीं है। दोष हमारे समाज में है, दोष हमारे रीति रिवाजों में है।
औरतों की दु:खी हालत का ज़िम्मेदार कौन है?जब हम औरतों पर किये अत्याचारों के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में पहला ख़याल यह आता है कि क़सूर किसका है? हम जानना चाहते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? सरकार क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? लेकिन ज़रा रुककर सोचें, शायद हम दोषी को ग़लत जगह खोज रहे हैं। इस बात का जो जवाब मिलेगा वह हमारी उम्मीद के मुताबिक़ नहीं होगा।
सबसे पहले हम सरकार की तरफ़ उँगली उठाते हैं। सरकार और पुलिस में समाज के वही लोग काम कर रहे हैं जिनकी सोच में औरत का दर्जा नीचा होने की बात बैठी हुई है। इसके अलावा सरकार, पुलिस विभाग और कोर्ट-कचहरी में बहुत कम औरतें हैं जो एक बदक़िस्मत औरत के दु:ख को औरत की नज़र से देख सकें।
कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि दु:खी औरत मजबूर होकर ही पुलिस का सहारा लेने आती है, क्योंकि दहेज की वजह से ससुरालवाले उसके साथ मारपीट करते हैं, लेकिन पुलिसवाले उसका मामला दर्ज नहीं करते। वे उसे सलाह देते हैं कि औरत की जगह उसके पति के साथ है और उसे घर जाकर प्यार से अपने पति को मना लेना चाहिये।
इसी तरह जजों की मिसाल ली जा सकती है। एक अध्ययन में यह जानने की कोशिश की गई कि जब औरतों के साथ मारपीट के मामले जज के सामने आते हैं, तो हमारे देश के बहुत-से जजों की सोच क्या है। हैरानी की बात यह है कि इस अध्ययन के मुताबिक़ काफ़ी जजों की यह सोच है कि ऐसे कई हालात हैं जिनमें अगर एक पति ने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा तो पति ने ठीक ही किया; कि चाहे पत्नी पर कितना भी अत्याचार क्यों न हो रहा हो, फिर भी उसका फ़र्ज़ है कि वह अपने परिवार को जोड़े रखे; कि अगर औरत ने ऐसे कपड़े पहने हों जिसमें उसका शरीर ज़रा-सा भी दिख रहा हो, तो यह छेड़छाड़ का न्यौता है और इसमें छेड़छाड़ करनेवाले पुरुषों की ग़लती नहीं है; कि दहेज हमारी संस्कृति की एक पुरानी परंपरा है जिसकी समाज में मान्यता है।18 These beliefs are deep-rooted in our society.
यह सोच कुछ जजों की है, लेकिन इस तरह की मिसालें हर क्षेत्र में मिल सकती हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यताओं की जड़ें बड़ी गहरी हो चुकी हैं।
हम सरकार की तरफ़ देखते हैं, लेकिन सरकार माँ-बाप की तरफ़ उँगली उठाती है। सरकार कहती है कि माँ-बाप अपनी मर्ज़ी से दहेज लेते हैं और देते हैं तो वह क्या करे? लिंग चुनाव के मामले में सरकार माँ-बाप और डॉक्टर दोनों की तरफ़ उँगली उठाती है। उसका कहना है कि अस्पताल के किसी बंद कमरे में डॉक्टर और माँ-बाप गर्भ में पल रही लड़की की हत्या का फ़ैसला लेते हैं, ऐसे मामलों में कानून लागू करना बहुत मुश्किल है।
लेकिन डॉक्टर माँ-बाप की तरफ़ उँगली उठाते हैं और कहते हैं कि माँ-बाप ख़ुद चलकर उनके पास कन्या भ्रूणहत्या की माँग लेकर आते हैं, तो वे क्या करें? अगर वे ‘न’ कर दें तो माँ-बाप किसी दूसरे डॉक्टर से यह काम करवा लेंगे। आज ऐसे कई डॉक्टर हैं जो मानते हैं कि कन्या भ्रूणहत्या करके वे समाज की एक ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। उनकी सोच है कि अगर वे उस लड़की को जीने दें तो उसे ज़िंदगी भर दु:ख झेलने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे समाज में औरतों की ज़िंदगी दु:ख भरी होती है। इन डॉक्टरों का मानना है कि कन्या भ्रूणहत्या करके वे उस बच्ची और उसके माँ-बाप पर रहम कर रहे हैं।
अगर एक माँ तीसरी या चौथी बेटी के बजाय एक बेटा चाहती है, तो आप उससे यह अधिकार कैसे छीन सकते हो? सदियों पुरानी सोच को एक तरफ़ रखकर आप यह नहीं कह सकते कि लड़के और लड़कियों का दर्जा एक बराबर है। ìएक अनचाही लड़की ज़िंदगी भर दु:ख सहती रहे, इससे तो अच्छा है कि उसके माँ-बाप आज ही उससे छुटकारा पा लें।
एक डॉक्टर के विचार, रीटा पटेल, ‘द प्रैक्टिस ऑफ़ 19
माँ-बाप अपने आप को दोषी नहीं समझते। वे समाज की तरफ़ उँगली उठाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे समाज के रीति रिवाजों ने उन पर इतना दबाव डाला है, उन्हें इतनी मुसीबत में फँसा दिया है कि अपनी बेटी से छुटकारा पाने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं है।
इस तरह घूमकर हम वापिस उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। औरतों के दु:खों का ज़िम्मेदार कौन है? इस प्रश्न का जवाब शायद हमें अच्छा नहीं लगेगा। वे हम हैं। याद रहे कि अगर हम दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने के लिये उनकी तरफ़ एक उँगली उठाते हैं, तो बाक़ी तीन उँगलियाँ हमारी तरफ़ भी उठती हैं। हम ही हैं जो इस समाज को बनाते हैं, हम माँ-बाप हैं, पड़ोसी हैं, डॉक्टर, पुलिस और जज हैं। हम सभी को अपना अंधविश्वास और ग़लत धारणाएँ बदलनी होंगी। हम ही वे अध्यापक हैं, जिन्हें बच्चों को शिक्षा देनी होगी कि लड़के और लड़कियाँ बराबर होते हैं। हम ही वे नेता और सरकार चलानेवाले हैं, जो कानून बनाते हैं और लागू करते हैं। हम ही वे मीडिया के लोग हैं, जिन्हें टी.वी., रेडियो और अख़बारों के ज़रिये लोगों को जाग्रत करके उनकी सोच में बदलाव लाना होगा।
देखा जाए तो ज़िम्मेदारी हम सब की है।
इस समस्या का हल क्या है?अगर हम सब इस समस्या के लिये ज़िम्मेदार हैं, तो फिर हम सबको इसके समाधान की भी ज़िम्मेदारी उठानी चाहिये। समाधान हमारे चुनाव पर निर्भर है और सही रास्ता चुनने का काम हम अकेले भी कर सकते हैं या फिर हम सब मिलकर समाज के रूप में भी कर सकते हैं।
परमात्मा ने हम इनसानों को एक अनमोल तोहफ़ा दिया है—वह है—विवेक। विवेक वह शक्ति है जिसके ज़रिये हम सही और ग़लत के बीच में फ़र्क़ देख सकते हैं। आइये! अब वक़्त आ गया है कि हम अपनी विवेक की शक्ति का इस्तेमाल करें और ग़लत रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पर चलें। अब हम ऐसे इनसान बनने की कोशिश करें जो संतोष, नम्रता और प्यार से भरपूर हों और देश के कानून का पालन करें।
सही रास्ते पर चलने के लिये हमें कुछ कुरीतियों को पीछे छोड़ना होगा। बेशक यह आसान काम नहीं है। हमारे पुराने रीति रिवाज और सोच अब हमारी जड़ों में बस चुके हैं, यहाँ तक कि जब हम देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, इन्हें भी अपने साथ ले जाते हैं। आज जो भारतीय अमरीका, कनाडा और इंग्लैंड जैसे देशों में बसे हैं, वे भी बड़ी संख्या में कन्या भ्रूणहत्या कर रहे हैं। इन देशों में बसे पढ़े-लिखे भारतीय नौजवान दुल्हन चुनने के लिये छुटि्टयों में देश लौटते हैं और इनमें से कई भारी दहेज की माँग भी करते हैं। वे सोचते हैं कि ज़्यादा दहेज माँगना उनका हक़ है, क्योंकि वे इतने पढ़े-लिखे हैं और विदेश में बसे हुए हैं।
पुराने रीति रिवाजों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन पर हमें अभिमान है। सदियों से माँ-बाप अपने बच्चों को इन रीति रिवाजों को सिखाते चले आ रहे हैं। क्योंकि बचपन से ही हम इन रीति रिवाजों को मान रहे हैं, इसलिये इनके पालन में हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इनको मानने से समाज के लोग हमारे ऊपर उँगली नहीं उठाते। इन रीति रिवाजों का एक मक़सद समाज को मज़बूती देना भी है। लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ समाज बदलता है; पुरानी परंपराएँ पीछे रह जाती हैं, नयी परंपराएँ उनकी जगह लेती हैं। समाज की बेहतरी के लिये यह ज़रूरी है कि वक़्त के साथ पुराने रिवाज और परंपराएँ भी बदलती रहें। हमारे देश की सबसे बड़ी ताक़त यह रही है कि कई सदियों से हमने भारत में आ बसनेवाले लोगों के रीति रिवाजों को भी अपने समाज में स्थान दिया है। उनकी संस्कृति को अपने समाज के साथ जोड़ा है। अपने आप को वक़्त के साथ बदला है। इसी वजह से आज हम गर्व से कहते हैं कि भारत की संस्कृति बेमिसाल है। ज़रा सोचिये! अगर हमने पुराने रिवाजों को पीछे छोड़ने का साहस न दिखाया होता, तो क्या आज औरत वोट डालने का अधिकार पाती? पढ़ाई कर पाती? नहीं! यह समाज अगर एक विधवा को फिर से विवाह करके अपना घर बसा लेने की इजाज़त न देता, तो आज भी उसे अपने पति की चिता पर सती होना पड़ता।
ये सब एक ज़माने में हमारे रिवाज थे, लेकिन अब हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। हम यह इसलिये कर पाए, क्योंकि हमने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। हम जानते थे कि अगर हम बिना सोचे-समझे, आँखें बंद करके इन रिवाजों को मानते रहे, तो ये समाज में ज़हर घोल देंगे और समाज को कमज़ोर बना देंगे। हम यह इसलिये भी कर पाए, क्योंकि उस समय हमारे समाज में कुछ साहसी लोग थे जो बदलाव के लिये अगुवा बने
बदलाव कहाँ से शुरू होता है?
औरतों की सोच में बदलाव लानायह कहना शायद सही होगा कि सबसे ज़्यादा बदलाव लाने की ज़रूरत दो जगह पर है—औरतों के बारे में आदमियों की सोच और औरतों के बारे में ख़ुद औरतों की सोच।
वेरा ब्रिटेन
हमारे समाज में बुनियादी बदलाव तब आएगा, जब औरतें अपनी सोच को बदलेंगी।
आज औरत की सोच, उसका पूरा विश्वास, उसका नज़रिया हमारे पुराने रीति रिवाजों पर आधारित है। दूसरे लोग उसे बताते हैं कि उसका आत्मसम्मान किन बातों पर निर्भर है। समाज उसके दायरों और उसकी ज़िम्मेदारियों को तय करता है। इस दायरे में अगर वह अपने बताए गए फ़र्ज़ को अच्छी तरह से निभाती है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ता है। आज की औरत के आत्मसम्मान में कमी है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि उसमें यह क़ाबिलीयत है कि वह अपने दायरों को बढ़ाकर आज़ाद हो सकती है।
लेकिन सच तो यह है कि हर औरत में अनोखी शक्ति होती है। वह अनमोल है। उसे डर और रुकावटों की परवाह किये बिना साहस और निश्चय से अपने सपनों को पूरा करना है और उसे यह क़दम सिर्फ़ अपने लिये ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिये भी उठाना है।
हर औरत अपनी बेटी के लिये एक आदर्श होती है। जब एक औरत में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास होता है, तभी वह अपनी बेटी को सिखा सकती है कि उसे भी अपनी योग्यता पर विश्वास करना चाहिये, उसे भी अपने आप को सम्मान देना चाहिये। जो औरत अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है, वह अपनी बेटी की कल्पनाओं को साकार करने में उसका साहस बढ़ाती है।
औरत के प्रति आदमी की सोच में बदलावहमारे पुराने रीति रिवाज इतनी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं कि अब ये हमारे दिलो-दिमाग़ में बस गए हैं। इसलिये आज बदलाव को अपनाना आसान नहीं है। ताक़त और ऊँचा दर्जा हमेशा आदमियों का हक़ रहा है। इस दर्जे पर वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आज अगर हम आदमियों से कह दें कि औरतों को अधिकार दो, औरतों का दर्जा बढ़ाओ तो ऐसा करने के लिये उन्हें बहुत साहस की ज़रूरत पड़ेगी। समाज में असली बदलाव तभी आएगा, जब आदमी अपनी सोच और बर्ताव में बदलाव लाएगा। आदमियों को यह समझना चाहिये कि अगर औरतों का दर्जा बढ़ेगा तो इससे आदमियों का दर्जा कम नहीं हो जाएगा। अगर औरतों की अहमियत बढ़ेगी तो इससे परिवार और समाज में अशांति नहीं फैलेगी, बल्कि औरत को इज़्ज़त और अधिकार देने से औरत ख़ुश रहेगी। इससे परिवार और समाज में प्रेम और शांति बढ़ेगी।
आज आदमियों में यह ताक़त है कि वे अपने परिवार की औरतों का दर्जा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर घर में औरत का दर्जा ऊँचा है तो बाहर की दुनिया भी उसे इज़्ज़त देगी। अगर घर में औरत के दायरे छोटे हैं, वह कमज़ोर है, उसे दबाया जाता है तो सोचिये घर के बाहर उसका क्या हाल होगा? जब हम औरत की ज़रूरतों और चाहतों की क़द्र करते हैं, तभी वह परिवार और समाज में अपने अमूल्य गुण बाँट सकती है। एक ख़ुश औरत ही घर और परिवार को प्रेम की बग़िया बनाती है और अपने बच्चों की सोच और नज़रिये को सही दिशा देती है
हर आदमी अपने बेटे के लिये एक आदर्श होता है। हमारे बच्चे केवल कहने से नहीं सीखते, वे हमारे बर्ताव को बड़े ध्यान से देखते हैं और उससे सीखते हैं। जब एक आदमी अपनी पत्नी की इज़्ज़त करता है और उसे ऊँचा दर्जा देता है, तब वह अपने बेटे को भी औरत की इज़्ज़त करना सिखाता है।
बदलाव के लिये आगे बढ़नाभारत के कोने-कोने से कई मिसालें सुनने को मिलती हैं, जिसमें किसी एक व्यक्ति ने अपनी आत्मा की पुकार को सुना और विरोध के बावजूद बड़े साहस से पुराने रिवाजों को तोड़ा।
शिवपुर काशी में कन्या लोहड़ी ...श्री गंगानगर के गाँव शिवपुर काशी में ऐसे ही बदलाव का एक क़िस्सा है। राजस्थान की इस तहसील में लड़कों के मुक़ाबले लड़कियों की संख्या बहुत कम है। गाँव के लोगों को साफ़ नज़र आ रहा था कि अगर लड़के और लड़कियों की गिनती में अंतर इसी तरह बढ़ता रहा, तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इसलिये उन्होंने इसके बारे में कुछ करने की ठानी। उन्होंने ‘कन्या लोहड़ी’ का त्यौहार मनाया जिसमें सात हज़ार लोगों के सामने 101 लड़कियों का आदर किया। यह उनकी तरफ़ से एक साहसी क़दम था, क्योंकि पुराने रिवाजों के अनुसार लोहड़ी के दिन, नवजात लड़कों की सेहत और लंबी उम्र के लिये प्रार्थना करके आग में मिठाई डाली जाती है, लेकिन इस गाँव ने नवजात लड़कियों को यह आदर दिया। फिर इसी गाँव में दो जवान लड़कियों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। सदियों पुराने रिवाज के मुताबिक़ माँ-बाप का अंतिम संस्कार सिर्फ़ बेटे ही कर सकते हैं, लेकिन शिवपुर काशी के लोगों ने इन लड़कियों का साथ दिया और उनकी सराहना की।
डॉक्टर मीता सिंह, ‘आउटकम्ज़ ऑफ़ द डिगनिटी ऑफ़ द गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम’ 20
यह कहानी देवड़ा गाँव की है। देवड़ा गाँव में छ: पीढ़ियों ने सौ सालों से भी ज़्यादा समय से किसी भी लड़की को ज़िंदा नहीं छोड़ा। कन्या की हत्या करना वहाँ का रिवाज था। लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। यह एक खुला राज़ था जो गाँव का हर व्यक्ति जानता था और ऐसा करता था। अगर गाँव से बाहर का कोई व्यक्ति इसका कारण पूछता, तो गाँववाले कहते कि हमारे कुएँ का पानी ही ऐसा है कि यहाँ लड़के पैदा होते हैं। इस रिवाज को गाँव के इन्द्र सिंह और उसकी पत्नी ने हिम्मत करके तोड़ा। उनके लड़के की मौत के पंद्रह दिन बाद उनके घर में लड़की पैदा हुई। दोनों पति और पत्नी का दिल नहीं माना कि वे उसे रिवाज के अनुसार मार डालें। उन्होंने अपनी बेटी जसवन्त कंवर को जीवन का तोहफ़ा दिया।
शुरू में छोटी जसवन्त गाँववालों को अजीब लगती थी। लेकिन उसके पिता ने (जो आगे जाकर गाँव के सरपंच बने) जसवन्त को आठवीं कक्षा तक पढ़ाया। उस समय गाँव का स्कूल इसी कक्षा तक था। इन्द्र सिंह के इस साहस को देखकर उसके भाई और चाचा ने भी अपनी लड़कियों को जीने का हक़ दिया। 1998 में जसवन्त कंवर की शादी धूमधाम से हुई। दूर-दूर से लोग इस शादी को देखने आए, क्योंकि इस गाँव में इससे पहले 1883 में ही बारात आई थी। आज भी देवड़ा गाँव में लड़कियों को जन्म के बाद मारने की परंपरा चल रही है, लेकिन अब गाँव में कई लड़कियाँ देखने को मिलती हैं। इन्द्र सिंह और उसकी पत्नी ने इस पुराने रिवाज को तोड़ने की हिम्मत की। देवड़ा गाँव के लोगों में बदलाव लानेवाले वे दोनों मुख्य माने जाते हैं।
राजेश सिन्हा, इण्डियन एक्सप्रेस, 10 मई, 1998, ‘115 साल बाद एक गाँव में लड़की की शादी’21
छत्तीसगढ़ के राजनन्द गाँव में, 80,000 औरतों ने एक दूसरे की मदद के लिये एक बैंक की शुरुआत की। यह बैंक माँ बामलेश्वरी बैंक के नाम से जाना जाता है। आज इस बैंक की 5372 शाखाएँ ज़िले के सभी गाँवों तक पहुँच गई हैं।
यह बैंक औरतों की ज़रूरतों के लिये बनाया गया है और इसे पूरी तरह से औरतें ही चला रही हैं। हर शाखा की औरतें ख़ुद पैसा जमा करने का तरीक़ा ढूँढ़ती हैं और ख़ुद निर्णय करती हैं कि किसको कितना क़र्ज़ दिया जाएगा। एक साल के अंदर ही इस बैंक में 1.19 करोड़ रुपये जमा हुए और 70 लाख का क़र्ज़ बाँटा गया है। ये क़र्ज़े छोटी और बड़ी हर तरह की माँगों के लिये दिये जाते हैं। सरकारी बैंक इस क़िस्म के क़र्ज़ों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते।
इस बैंक की सदस्य स्वाति अग्रवाल कहती हैं, ‘हम हर तरह की ज़रूरतों के लिये क़र्ज़ देते हैं—जैसे बच्चों के जन्म के समय, बच्चों को टीका लगवाने के लिये, बीमारी के इलाज के लिये या पुरानी साइकिल ख़रीदने के लिये।’ ये क़र्ज़े 200 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक, बीज ख़रीदने की ज़रूरत से लेकर ट्रैक्टर के पुर्ज़े ख़रीदने तक के लिये दिये जाते हैं। ज़िले की औरतें इस बैंक को चला रही हैं और वे किसी भी सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं हैं।
इण्डिया टुडे, 15 जुलाई, 2002, ‘रूरल विमिन स्टार्ट सकसैसफ़ुल, माइक्रो-बैकिंग स्कीम इन छत्तीसगढ़’22
यह अनीता कुशवाहा की कहानी है जो बिहार के किसी दूर इलाक़े में एक पिछड़ी जाति के परिवार में पैदा हुई थी। उसका पिता जनार्धन सिंह बिहार के मुजफ़्फ़रपुर के बोचाहा गाँव में एक छोटी पंसारी की दुकान पर मामूली नौकर था। सबने सोचा कि दूसरी लड़कियों की तरह अनीता भी बकरियों को चराएगी और छोटी उम्र में शादी करेगी। जनार्धन सिंह को भी अपनी बेटी से यही उम्मीद थी। परंतु जो इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं थी, वह थी अनीता। वह अपने बंधनों से आज़ादी चाहती थी। आज 21 साल की अनीता शहद के कारोबार की मालकिन है और वह सालाना ढाई लाख रुपये का कारोबार करती है। इस मक़सद तक पहुँचना आसान नहीं था। अनीता ने अपनी पहली लड़ाई छ: साल की उम्र में लड़ी। गाँव के एक अध्यापक की सहायता से उसने अपने माँ-बाप को उसे स्कूल भेजने के लिये राज़ी किया। अनीता कहती है, ‘मेरे माँ-बाप सिर्फ़ कहने से ही नहीं माने, बल्कि वे इसलिये राज़ी हुए क्योंकि हमारे गाँव में पाँचवीं क्लास तक पढ़ाई मुफ़्त है।’ लेकिन पाँचवीं क्लास के बाद पढ़ाई का ख़र्च उसके माँ-बाप नहीं उठा सकते थे, तो अनीता ने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि वह अपनी पढ़ाई का ख़र्च ख़ुद उठा सके। अनीता ने कहा, ‘उस वक़्त पड़ोसी गाँवों से मधुमक्खी पालनेवाले व्यापारी लीची के पेड़ों की वजह से हमारे गाँव आते थे। मैंने उनकी मदद करनी शुरू की और उनसे शहद बनाने का काम सीख लिया।’ इस तरह ग़रीबी से परेशान मज़बूत इरादों वाली अनीता ने यह व्यापार शुरू किया। बच्चों को पढ़ाकर बचाए हुए 5000 रुपये और कुछ रुपये अपनी माँ रेखा देवी से लेकर, 2002 में अनीता ने दो मधुमक्खी के बक्सों से अपना व्यापार शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने अच्छा ख़ासा मुनाफ़ा कमाया।
कई बार मधुमक्खियों के काटने से उसका चेहरा सूज जाता था और लोग उसका मज़ाक़ उड़ाते थे। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह कहती है, “लोग पूछते थे, ‘क्या मक्खियाँ तुम्हें काटती हैं?’ मैं कहती थी, ‘हाँ।’ ‘क्या दर्द होता है?’ मैं कहती थी, ‘हाँ’।”
अब अनीता के पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और अपनी बेटी के काम में उसकी मदद करते हैं। अनीता आज अंग्रेज़ी साहित्य की पढ़ाई कर रही है और उसने माँ-बाप से वचन लिया है कि वे उसकी शादी तब तक नहीं करेंगे, जब तक वह अपनी डिग्री नहीं पा लेती। झोंपड़ी की जगह अब उनका पक्का घर है। अनीता ने अपने छोटे भाई को मोटर साइकिल तोहफ़े में दिया है। समाज में उसकी इज़्ज़त की वजह से आज उसकी माँ गाँव में एक राजनैतिक दल की मुखिया है। उसकी इस जीत को देखकर गाँव के दूसरे लोगों ने भी मधुमक्खी पालने का काम शुरू किया है और गर्व की बात यह है कि आज गाँव की हर लड़की स्कूल जाती है।
अमिताभ श्रीवास्तव, इण्डिया टुडे, 1 मई, 2009, ‘ग्रिट एण्ड हनी’23
ये कहानियाँ उन साहसी लोगों की हैं जिन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की। हम सब में यह शक्ति है कि हम बदलाव ला सकें। हम सब में यह क़ाबिलीयत है कि हम अपनी बेटियों के भविष्य को सुनहरा बनाएँ और उनके साथ अपनी ज़िंदगी में भी बदलाव लाएँ।
नारी को अधिकार दो
सबसे बड़ा ख़तरा
इस बात का नहीं है हमें
कि हममें कम शक्ति है;
ख़तरा तो यह है
कि हमारी शक्ति अपार है।
सबसे अधिक हमें
अंदर का अँधेरा नहीं
बल्कि प्रकाश डराता है।
पूछते हैं हम ख़ुद से–
कि क्या हक़ है हमें
तेजस्वी, गौरववान्, प्रतिभाशाली,
या एक अद्भुत व्यक्ति बनने का?
असल में पूछना तो ख़ुद से यह चाहिये
क्यों नहीं बन सकते इस योग्य तुम?
प्रभु की संतान हो तुम
अपने दायरे को छोटा करोगे अगर
तो कोई लाभ न होगा संसार को।
हमारे इर्द-गिर्द दूसरे
ख़ुद को असुरक्षित न समझें–
इस विचार से
अपने दायरे को छोटा कर लेना
नहीं है लक्षण तेजस्वी व्यक्ति का।
जन्म लिया था हमने
अनुभव करने को अपने अंदर के
प्रभु की महानता का।
यह दिव्य महानता
हममें से कुछ में ही नहीं,
बल्कि सब में है।
और जब हम
संसार के सामने
प्रकट करते हैं
अपने आध्यात्मिक प्रकाश को
तो अनजाने ही
प्रेरणा देते हैं दूसरों को
कि वे भी ऐसा ही करें।
मेरीएन विलियम्सन
अगर हमें इस जीवन में औरत का साथ मिला है तो यह एक अनमोल तोहफ़ा है। इनसानियत के नाते यह हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे प्यार दें, इज़्ज़त दें और उसकी देखभाल करें। हमारे समाज में औरत को छोटा दर्जा दिया गया है, इसलिये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें ताकि वह अपने आप को समर्थ बना सके।
समर्थ औरत कौन है? यह समझना ज़रूरी है ताकि हम औरतों को आज़ादी हासिल करने में उनकी मदद करें, औरतों की आज़ादी से डरें नहीं। समर्थ औरत में आत्मविश्वास होता है—वह अपनी क़ाबिलीयत पर विश्वास करती है। वह आत्मसम्मान बनाए रखती है। इसी वजह से दूसरे भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। वह चाहे घर में काम करे या घर से बाहर, उसमें आत्मनिर्भर होने की भावना होती है। वह दया और प्यार से भरपूर होती है। ऐसी औरत अपने पति पर अधिकार नहीं जमाती, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ निभाती है। उसकी मौजूदगी से घर और आसपास का माहौल ख़ुशनुमा हो जाता है।
कई अध्ययनों से हमें यह पता चलता है कि समाज में जब औरत आत्मनिर्भर हो और समाज के कामों और फ़ैसले लेने में पूरी तरह से हिस्सा ले रही हो, तो इससे समाज को बहुत फ़ायदा पहुँचता है।
आशा-रोज़ मिगिरो, संयुक्त राष्ट्र संघ, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल
भारत बहुत समय से पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन अब समानता से आगे बढ़ने का वक़्त आ गया है। अब समय आ गया है कि हम ऐसा समाज बनाएँ जिसमें न आदमी प्रधान हो, न औरत; ऐसा समाज जिसमें आदमी और औरत का दर्जा बराबर का हो—सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से। यह एक नामुमकिन सपना नहीं है। ऐसे कई पश्चिमी देश हैं जो कुछ समय पहले तक पुरुष प्रधान देश थे, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिये उन्होंने कई सही क़दम उठाए जिनकी वजह से आज इन देशों में औरत का दर्जा बहुत ऊँचा है। अगर वे इस मक़सद को कुछ ही सालों में हासिल कर सके तो हम भी यह कर सकते हैं।
इस दिशा में कुछ क़दम उठाकर हम इन रीति रिवाजों की जकड़ से छूट सकते हैं और औरतों की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं।
• आओ! मिलकर कहें ‘दहेज नहीं लेंगे’दहेज माँगना या लड़कीवालों की ‘मर्ज़ी से दिये गए’ तोहफ़े लेने का रिवाज अब हमारी जड़ों में इस हद तक बस गया है कि ज़्यादातर लोगों को यह महसूस ही नहीं होता कि वे कुछ ग़लत कर रहे हैं या किसी परिवार को दुविधा की स्थिति में डाल रहे हैं। दहेज को ऐसी सामाजिक मंज़ूरी मिली हुई है कि लड़केवाले बड़ी शान से खुलेआम बोलते हैं कि उन्हें दहेज में कितना मिल रहा है, ‘दस लाख की पार्टी है,’ वग़ैरह। अफ़सोस की बात है कि शादी में आए मेहमानों के सामने लड़कीवाले जब दहेज का प्रदर्शन करते हैं तो देखनेवाले मेहमानों को भी बुरा नहीं लगता। दहेज प्रथा की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इन्हें जड़ से उखाड़ने के लिये बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी।
इस ज़हर को समाज से निकाल सकने की हिम्मत करना आज के नौजवानों में और उनके माँ-बाप के हाथों में है। दहेज माँगना ग़लत है, तोहफ़े लेना ग़लत है, चाहे वह बिना माँगे ही क्यों न मिले हों। दहेज ने औरत के दर्जे को पैसों से लेन-देन की वस्तु का रूप दे दिया है। दहेज औरत और उसके परिवार को कमज़ोर करता है। ऐसे माहौल में सच्चा प्यार, सुख और शांति कभी नहीं आ सकती। एक ताक़तवर आत्मसम्मान से भरपूर आदमी की निशानी यह है कि वह औरत को बराबर का दर्जा देता है।
जो नौजवान दहेज की शर्त पर ही शादी करता है, वह अपनी शिक्षा, अपने देश और नारी जाति सबका निरादर करता है।
महात्मा गांधी
यह सच है कि लड़की के माँ-बाप पर दहेज देने के लिये बहुत दबाव होता है, लेकिन अगर दहेज नहीं माँगा गया और हम इसे अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, तो समझ लीजिये कि हम अपनी लड़की के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। शादी के वक़्त तोहफ़े और पैसे देने की क्या ज़रूरत है? क्या हमारी बेटी ख़ुद एक तोहफ़ा नहीं है? हम कहते हैं कि हम लड़के-लड़की को नये जीवन में अच्छी शुरुआत देना चाहते हैं, लेकिन यह ज़िम्मेदारी सिर्फ़ लड़की के माँ-बाप पर क्यों है? क्या यह दोनों तरफ़ से नहीं होनी चाहिये?
जहाँ तक हो सके हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि लोग क्या कहेंगे, हमें सिर्फ़ अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोचना चाहिये। माँ-बाप का फ़र्ज़ सिर्फ़ यहाँ तक है कि वे अपनी बेटी को पढ़ाएँ-लिखाएँ, उसे अच्छे उसूल सिखाएँ। इसके बाद यह उस लड़के और लड़की की ज़िम्मेदारी है कि वे अपनी मेहनत और लगन से एक क़ामयाब ज़िंदगी बनाएँ। जब हम लड़के के परिवार को महँगे तोहफ़े देते हैं, ये तोहफ़े उनकी उम्मीदों को बढ़ाते हैं। जब माँ-बाप बार-बार तोहफ़े देने के लिये मजबूर होते हैं तो उनकी बेटी में हीनता का भाव आ जाता है। हीनता की बेड़ियों को वह ज़िंदगी भर नहीं तोड़ पाती। कितना अच्छा हो कि लड़केवाले दहेज की माँग न करें और लड़कीवाले तोहफ़े न दें। इसी में परिवार की इज़्ज़त और ख़ुशहाली है।
• आओ! अपने बेटे की शादी का ख़र्च बाँट लेंहम बिना सोचे-समझे इस परंपरा को क्यों मानते आ रहे हैं कि शादी का पूरा ख़र्च लड़कीवालों को ही उठाना चाहिये? क्या यह सही है? क्या यह न्याय है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़के और लड़की दोनों के परिवार शादी का ख़र्च मिलकर उठाएँ, ताकि सारा बोझ लड़कीवालों पर न पड़े। अगर हम बेटे के माँ-बाप हैं तो यह चुनाव करके हम एक नयी परंपरा की शुरुआत कर सकते हैं।
• आओ! शादियाँ सादगी से करेंकुछ परिवार शादी में बहुत ज़्यादा ख़र्च नहीं कर सकते, लेकिन लड़कीवालों पर समाज की तरफ़ से बहुत दबाव होता है कि वे ज़्यादा ख़र्च करके बेटी की शादी धूमधाम से करें। शानशौक़त से शादी करने की वजह से वे क़र्ज़ के बोझ तले दब जाते हैं और इस क़र्ज़ को वापिस करने में कई साल लग जाते हैं। कुछ लोग ख़ूब पैसेवाले होते हैं और उनका कहना है कि हम अपनी बेटी की शादी में ख़र्च क्यों न करें? हमें ख़ुद से पूछना चाहिये कि शादी में इतना ख़र्च करने के पीछे हमारा मक़सद क्या है? क्या यह हमारा अपनी बेटी के लिये प्यार है? क्या हमारा अहंकार अपना सिर तो नहीं उठा रहा? क्या हमारा असली मक़सद यह तो नहीं कि इस शादी के ज़रिये हम समाज को अपना दर्जा, अपनी अमीरी और ताक़त दिखा सकें? शाही शादी और महँगे तोहफ़े बेटी के प्रति प्यार की निशानी नहीं हैं।
अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो हम अपने बच्चों को ज़रूरत के समय दे सकते हैं या कहीं दान कर सकते हैं। दुनिया को इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन परमात्मा सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है।
समाज की भलाई के लिये शादियाँ जितनी सादगी से हों उतना ही अच्छा है। सादगी, सरलता और नम्रता बहुत बड़े गुण हैं।
• आओ! बेटियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले न करेंइसमें कोई शक नहीं है कि हम पर लड़कियों की शादी जल्दी करने का सामाजिक दबाव होता है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुँवारी लड़कियों की देखरेख की ज़िम्मेदारी भी हमारी ही है और इसकी वजह से हमें फ़िक्र लगी रहती है। लेकिन 18 साल से कम उम्र की लड़की एक बच्ची ही तो है। इस उम्र में वह मासूम है, अगर ससुरालवाले उस पर अत्याचार करें, तो वह अपने आप को बचाने के लिये कुछ नहीं कर सकती। कम उम्र में गर्भवती होने और बच्चे पैदा करने से उसकी सेहत ख़राब होती है और उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा आपकी बेटी पढ़ने का मौक़ा खो देती है, अपने चरित्र और गुणों के विकास का मौक़ा खो देती है। आज़ादी, ख़ुशी और हँसी-खेल से भरे बचपन के कुछ साल वह यूँ ही खो देती है। शादी के बाद तो परिवार की ज़िम्मेदारियों का बोझ ज़िंदगी भर उठाना ही होता है, लेकिन हर बच्चे का हक़ है कि उसे एक सुनहरा बचपन मिले। अगर यह हक़ बेटों को दिया जाता है, तो बेटियों को क्यों नहीं?
• आओ! जब बेटियाँ अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ—हम उनका साथ देंज़्यादातर जवान औरतें घोर अत्याचार चुपचाप सहन करती हैं, क्योंकि समाज उनका और उनके माँ-बाप का साथ नहीं देता। औरतों के ख़िलाफ़ अत्याचार और दहेज संबंधी मामले थानों में दर्ज ही नहीं होते, क्योंकि इन औरतों को डर होता है कि समाज इन्हें दोषी ठहराएगा। इन औरतों को परखने के बजाय हमें इनका साथ देना चाहिये।
• आओ! हम अपनी बहुओं को अपने बेटों की तरह मानेंहमें अपनी नयी बहू का ख़ुशी से स्वागत करना चाहिये और उसे अपने बेटे के बराबर ही प्यार और इज़्ज़त देनी चाहिये। इससे हमारे घर में प्यार, शांति और ख़ुशहाली का माहौल पैदा होगा।
• आओ! हम अपनी पत्नी या बहू कोबेटा पैदा न करने का दोष न देंअगर एक औरत को बच्चे नहीं होते तो इसमें उसका पति भी बराबर का ज़िम्मेदार हो सकता है। इसके अलावा, अगर एक औरत को बेटा नहीं होता तो इसके लिये वह बिलकुल भी ज़िम्मेदार नहीं है। सच तो यह है कि बच्चा लड़का हो या लड़की, इसमें औरत का कोई हाथ नहीं होता। इसके लिये उसका पति ही ज़िम्मेदार होता है।
• आओ! लिंग जाँच को ‘न’ कहेंलिंग जाँच बिलकुल नहीं करवानी चाहिये। बेटे की चाहत में औरत का बार-बार गर्भपात कराते रहना ग़लत है। बहुत-सी लड़कियों को जन्म देते रहना ग़लत है, इस उम्मीद में कि कभी न कभी बेटा होगा। देश और समाज के हालात देखते हुए आज के वक़्त की पुकार है कि ज़्यादा से ज़्यादा दो बच्चे हों तो अच्छा है। अगर भगवान् ने भाग्य में दोनों लड़कियाँ लिखीं हैं, तो हम इसे भगवान् की रज़ा मानकर स्वीकार करें।
• आओ! अपनी बेटियों को बेटों के बराबर की पढ़ाई करने का और आगे पढ़ने का मौक़ा देंलड़कियाँ लड़कों के बराबर ही क़ाबिल और होशियार होती हैं। जब हम स्कूलों और कॉलेजों या प्रशासनिक सेवा परीक्षा के नतीजे देखते हैं, तो यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि लड़कियाँ बहुत अच्छे नंबर ले रही हैं। आम तौर पर मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर ज़्यादातर लड़कियाँ ही होती हैं। लड़कियों को पढ़ाने से बहुत फ़ायदे हैं। एक कहावत है: जब आप लड़के को पढ़ाते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षा मिलती है, लेकिन जब आप लड़की को पढ़ाते हैं तो सारे परिवार को शिक्षा मिलती है। अगर हम आज के वक़्त में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाएँ तो उनकी कमाने की क़ाबिलीयत काफ़ी बढ़ जाती है।24
आइये! हम अपनी बेटी को वैसे ही पढ़ाएँ जैसे अपने बेटे को। उसे भी नयी चीज़ें सीखने के मौक़े दें। उसे भी अपने पैरों पर खड़े होने के क़ाबिल बनाएँ। हमें विवेक से रास्ता चुनने की ताक़त मिली है। तो आइये! पढ़ाई के ज़रिये, हम अपनी बेटियों को भी यह वरदान दें—सही और ग़लत के बीच फ़र्क़ देखने की क़ाबिलीयत और सही रास्ते को चुनने की हिम्मत।
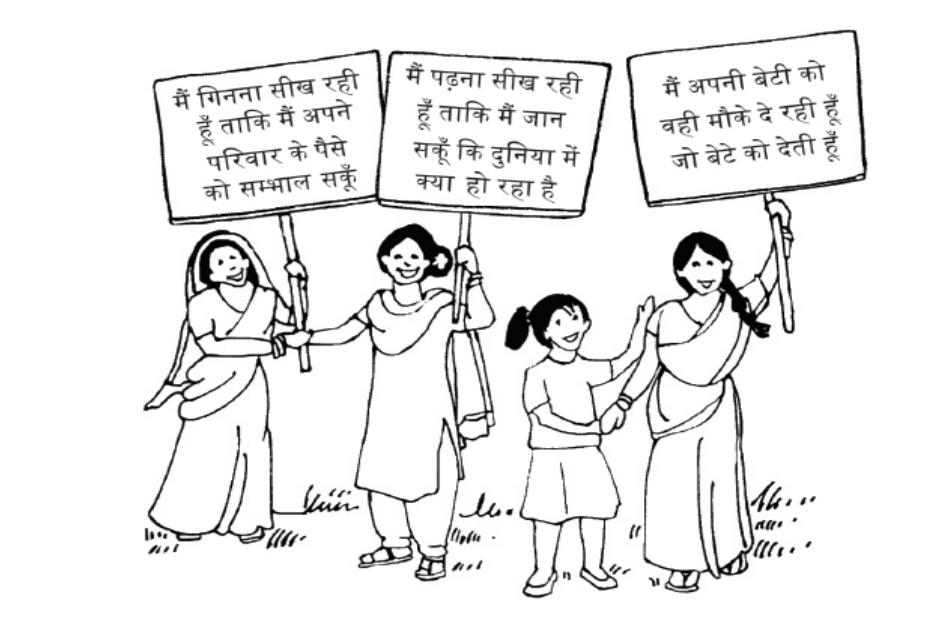
पैसा कमाने की योग्यता औरत को कई चीज़ें देती है—ख़ुद पर विश्वास, आज़ादी और सुरक्षा का एहसास, परिवार और समाज में इज़्ज़त और घर को चलाने में हिस्सा लेने का एहसास।
जब औरत घर के बाहर काम करके अपनी आमदनी लाती है, परिवार और समाज में उसकी अहमियत बढ़ जाती है। जब वह कमाती है तो परिवार की ख़ुशहाली में उसका सहयोग साफ़ नज़र आता है। परिवार में उसकी आवाज़ सुनी जाती है, क्योंकि वह किसी की मोहताज नहीं होती। इसके अलावा बाहर काम करने से पता चलता है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। इससे उसका ज्ञान बढ़ता है।
डॉ.अमर्त्य सेन
लेकिन ऐसी कई औरतें हैं जो घर से बाहर काम करना पसंद नहीं करतीं, शायद इसलिये कि वे घर के कामों में ही संतुष्ट हैं और परिवार को उनकी आमदनी की ज़रूरत नहीं है। औरत घर सँभाले या बाहर कोई व्यवसाय करने का इरादा करे, हमें उसे इज़्ज़त देनी चाहिये और एक-सा नज़रिया रखना चाहिये।
• आइये! विधवा औरत को सहयोग देंजब पति का देहांत हो जाता है तो उसकी पत्नी को क्यों कोसा जाता है? क्या जन्म से पहले वह अपने भाग्य में उम्र लिखवाकर नहीं लाता?
इस कठिन समय में हमें विधवा और उसके बच्चों की हर तरह से सहायता करनी चाहिये—पैसों से और हमदर्दी से। जहाँ तक हो सके उसे फिर से शादी करने का मौक़ा देना चाहिये, ताकि वह एक नयी ज़िंदगी शुरू कर सके।
• आओ! हम अपनी पत्नी और माँ के काम की क़द्र करेंज़्यादातर औरतों को महसूस होता है कि उनके काम की कोई क़द्र नहीं है। जो औरतें घर से बाहर काम नहीं करतीं उन्हें यह बात और भी ज़्यादा चुभती है। औरतें सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में लगी रहती हैं। वे सारा दिन छोटे-बड़े काम करती रहती हैं जैसे—बच्चे को जूते पहनाना, बच्चों के लिये ख़रीदारी करना, परिवार के लोगों के लिये खाना बनाना, बीमार रिश्तेदार की देखभाल करना वग़ैरह, लेकिन उन्हें लगता है कि अंत में उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और न ही किसी ने उनकी क़द्र की। सच बात तो यह है कि जो बातें आज छोटी लगती हैं, समय पाकर उनकी बड़ी अहमियत हो जाती है। इन्हीं बातों की वजह से बच्चे होनहार बनते हैं, सुख और शांति से भरे हुए घर बनते हैं और मज़बूत रिश्तेदारियाँ बनती हैं। इन्हीं छोटी-छोटी बातों की वजह से परिवार और समाज मज़बूत बनते हैं। लेकिन जब औरत ये सब करती है, हम उसका शुक्रिया तक नहीं करते, क़द्र नहीं करते।
आइये! अपनी पत्नी और माँ की क़द्र करें और शुक्रिया के तौर पर उनके कामों में हाथ बटाएँ। जब हम ऐसा करेंगे, तो हमें एहसास होगा कि इससे हमारे रिश्तों में सुखद बदलाव आ गया है। एक छोटे-से शुक्रिया कहने से ही घर में सुखद माहौल पैदा हो जाएगा।
• आओ! हम बेटियों को अपनी जायदाद में बराबर हिस्सा देंहम ऐसा क्यों सोचते हैं कि बेटियों को परिवार की जायदाद और व्यापार का हिस्सा नहीं देना चाहिये? क्या हमारी बेटियाँ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हैं? बेटियों को बराबर का हिस्सा देने में क्या नुकसान है?
जब हम सभी बच्चों को बताते हैं कि जायदाद में बेटी का बराबर का हिस्सा होगा, तो हम अपनी बेटी को सशक्त बनाते हैं। इसके उलट जब हम बेटी को बराबर के हिस्से से वंचित कर देते हैं, हम उसे संदेश देते हैं कि हम उसे बेटे के बराबर प्यार नहीं करते, उसकी क़द्र नहीं करते। इस संदेश के साथ हम अपनी बेटी को कमज़ोर कर देते हैं।
• आओ! हम अपने बेटों को जाग्रत करेंहम बदलाव की उम्मीद सबसे ज़्यादा आनेवाली पीढ़ी से करते हैं। आइये! अपने बेटों और बेटियों को बराबर का प्यार और दर्जा दें। भाइयों को सिखाएँ कि वे बहनों की इज़्ज़त और आदर करें। बेटों को सिखाएँ कि औरतें हर तरह से आदमियों के बराबर हैं। हालाँकि यह सोच समाज में चल रही सोच से बहुत अलग है, लेकिन बेटों को यह शिक्षा देना सही और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी सोच से ही हमारी अगली पीढ़ी की औरतों को बराबरी का हक़ मिल सकता है। यह अहम ज़िम्मेदारी बेटों के माँ-बाप की है।
• आओ! हम अपनी बेटियों को सबसे बड़ा तोहफ़ा दें—आत्मसम्मानआज हमारी बेटियाँ एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जिसमें बेटों को पूजा जाता है। बचपन से लड़कियों को पुरुष प्रधान समाज की परंपरा और मर्यादा सिखाई जाती है कि उनका दर्जा आदमियों से कम है।
हम अपनी बेटी को बड़े से बड़ा तोहफ़ा यही दे सकते हैं कि उसे सशक्त करके आत्मसम्मान दें। यह तभी हो सकता है जब उसे बराबर का प्यार, बराबर की पढ़ाई और बराबर के मौक़े दिये जाएँगे। उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। उसे ऐसी ज़िम्मेदारियाँ दें जो आज तक आदमियों को ही दी जाती रही हैं और शुरू से सबको बता दें कि बेटी जायदाद में बराबर की हिस्सेदार होगी।
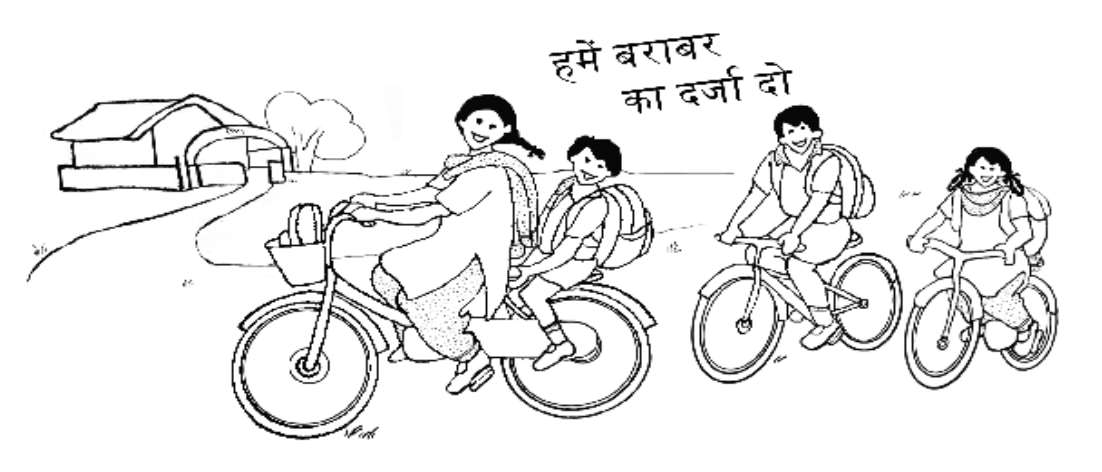
आत्मसम्मान से भरपूर बेटी एक दिन आपके लिये गर्व का कारण होगी। शादी के बाद अगर ससुरालवाले दहेज की माँग करेंगे तो उसमें ‘न’ कहने का साहस होगा। अगर लिंग जाँच करवाने का दबाव होगा तो उसमें मना करने का साहस होगा। अगर कन्या भ्रूणहत्या करने का दबाव होगा तो इस ग़लत बात को भी वह नहीं मानेगी। वह आत्मनिर्भर होगी, उसमें पैसा कमाने और सँभालने की शक्ति होगी। वह अपनी ज़िंदगी को इस तरह से जी सकेगी कि लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे और वह अपनी बेटी को भी वही संस्कार देगी जिससे उसकी बेटी आत्मसम्मान से भरपूर होगी। आत्मसम्मान से भरपूर औरत ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है।
मैं अपने माँ-बाप की लाडली बेटी थी। मैं आज जो भी हूँ, यह मेरे माँ-बाप की अच्छी परवरिश का नतीजा है। लड़की का भविष्य पूरी तरह से उसके माँ-बाप के आदर्शों पर निर्भर है कि वे उसका पालन पोषण कैसे करते हैं। उसे पढ़ाइये, उसे आदर दीजिये और पैसे के मामले में उसे ऐसी शक्ति दीजिये कि उसे कभी किसी का मोहताज न होना पड़े। ìअगर आज आप को लगता है कि आपकी बेटियाँ कमज़ोर हैं तो यह समझें कमज़ोर वे नहीं, बल्कि आपकी परवरिश में कोई कमी रह गई है। अगर मेरे माँ-बाप भी इसी तरह से सोचते तो मैं जो आज हूँ वह कभी नहीं बन सकती थी। उनकी सोच मज़बूत थी, इसलिये आज मैं एक शक्तिशाली औरत हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपनी बेटी को बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से पालो। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाओ। आत्मनिर्भरता ही शक्ति है और आत्मनिर्भर होने के लिये शिक्षा की ज़रूरत है। अगर आप अपनी बेटियों के लिये ऐसा करेंगे, तो वे आपकी इज़्ज़त करेंगी और ज़िंदगी भर आपका ख़याल रखेंगी।
किरन बेदी, भारत की सबसे पहली महिला पुलिस अफ़सर 25
जिस लड़की में आत्मसम्मान है वही समाज को बदलने के क़ाबिल होती है, क्योंकि आज की क़ाबिल बेटी कल की माँ और सास है। हमारे समाज में यह अन्याय और अत्याचार का चक्कर कब ख़त्म होगा? जब लड़कियाँ सीख जाएँगी कि वे क़द्र के लायक़ हैं और जब लड़के भी यह सीख जाएँगे कि लड़कियाँ उनके बराबर हैं। यदि हम लड़कियों में यह भावना जाग्रत करते हैं कि वे किसी से कम नहीं हैं, तो इसके साथ लड़कों में भी यह भावना लानी है कि लड़की और औरत किसी भी मामले में उनसे कम नहीं बल्कि बराबर है। उनकी क़द्र करो। ऐसा होने पर समाज में औरत के प्रति अन्याय और असमानता का भाव ख़त्म हो जाएगा।
• आओ! हम कानून का पालन करेंहमारे देश के कानून इस विषय पर बिलकुल साफ़ हैं—लिंग चुनाव करना कानून के ख़िलाफ़ है। इस कानून के तहत और भी बहुत से कानून हैं जैसे—लिंग जाँच करवाना ग़ैरकानूनी है; लिंग जाँच के व्यापार के बारे में लोगों को जानकारी देना भी ग़ैरकानूनी है; सरकार की इजाज़त के बिना क्लिनिक, अस्पताल या मोबाइल वैन चलाना ग़ैरकानूनी है। इसी तरह से दहेज लेना और देना भी कानून के ख़िलाफ़ है।
आओ! हम अपने देश के कानून का पालन करें।
• आओ! हम लिंग चुनाव के बारे में जानकारी बढ़ाएँहम जानते हैं कि कई लोग लिंग जाँच कराते हैं और यदि बेटी हो तो गर्भपात करा देते हैं, लेकिन बहुत-से लोग यह नहीं जानते कि आज हमारी जनसंख्या से 5 करोड़ से भी ज़्यादा औरतें कम हो गई हैं। लोग यह भी नहीं जानते कि यह समस्या कम होने के बजाय तेज़ी से बढ़ रही है। लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं कि यह काम सिर्फ़ किसी गाँव में ही नहीं हो रहा, बल्कि इसे अमीर, पढ़े-लिखे और शहरी लोग भी करवा रहे हैं। बहुत-से लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं कि लिंग चुनाव की वजह से हमारा समाज कितनी ख़तरनाक दिशा में जा रहा है।
अगर आप समाज की मदद करना चाहते हैं तो लोगों को इस समस्या के बारे में जानकारी दीजिये। अपने दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को इसके बारे में जानकारी दें। समाज के ऐसे लोगों से सहयोग की अपील करें जिनकी बात लोग सुनते हैं जैसे—अध्यापक, वकील, डॉक्टर, जज, नेता, सरकारी अफ़सर और मीडिया। इस समस्या के बारे में जानकारी बढ़ाना सबसे पहला क़दम है। लिंग चुनाव और औरतों के प्रति असमानता और अत्याचार तभी रुकेंगे, जब पूरे समाज की आवाज़ इनके ख़िलाफ़ उठेगी।
औरत को इज़्ज़त और बराबरी का दर्जा देने में समाज को अपनी भूमिका निभानी चाहिये। लेकिन औरतों को भी बहुत अच्छी तरह से यह सच्चाई समझ लेनी चाहिये—ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ें जैसे—आज़ादी, बराबरी और अधिकार—ये हमें कोई और नहीं दे सकता, ये हमें ख़ुद लेनी पड़ेंगी। जिस तरह रूहानियत के क्षेत्र में हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह इन कार्यों में सफलता के लिये हमें जूझना पड़ेगा। जब बेहद कोशिशों के बाद हमें अपने अधिकार पाने में सफलता मिल जाएगी, तब हमें इसकी अहमियत का एहसास होगा और फिर हम इसे कभी खोना नहीं चाहेंगे और हम इसके बचाव के लिये हमेशा सतर्क रहेंगे। अगर आज़ादी और बराबरी का हक़ हमें पकी-पकाई रोटी की तरह यानी बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो हमारे मन में इसकी अहमियत नहीं रहेगी और फिर हम इसे खो भी सकते हैं।
समाज हमारी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन यह हम औरतों की ज़िम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का साथ दें और मिलकर अपनी ताक़त बढ़ाएँ। यह हम पर निर्भर है—अपने आप को मज़बूत और शक्तिशाली बनाएँ।
जागृति
हज़ार मील का लंबा सफ़र,
पहले क़दम से ही शुरू होता है।
ताओ त्से चिंग
जागृति का मतलब है किसी अहम बात को पहचानना, उसे समझना और अपने नज़रिये को बदल लेना। आज हमारे समाज के हालात हमें पुकार रहे हैं कि जागो! इनसानियत का मतलब समझो। हमें इनसान का जन्म मिला है, हम बहुत उच्च कोटि के प्राणी हैं। जब हममें यह जागृति आएगी और हम अपने जीवन को पारमार्थिक मूल्यों के अनुसार जीने लगेंगे, तब अनुभव करेंगे कि हम सब एक इनसानी परिवार के सदस्य हैं—चाहे हम आदमी हैं या औरत, किसी भी वंश के हैं या किसी भी धर्म के। आज के हालात और उनके ख़तरनाक नतीजे हमें सावधान करते हैं कि पुरानी सोच और रीति रिवाजों को जल्द ही बदलना ज़रूरी है।
सदियों से इस दुनिया में महान् संत-महात्मा आते रहे हैं, जो हमें एहसास दिलाते रहे हैं कि हम अच्छाई, प्यार और इनसानियत के गुणों से भरपूर हैं। महात्मा बुद्ध, भगवान् महावीर, ईसा मसीह, गुरु नानक देव और उनकी परंपरा के अन्य गुरु, सूफ़ी संत, पैग़ंबर मुहम्मद साहिब आदि महान् संत या फिर महात्मा गांधी, मदर टेरेसा या नेल्सन मंडेला आदि महापुरुष जिनकी ज़िंदगी एक मिसाल बनी है, इन सभी ने हमें एक ही बात सिखाई है कि हम इनसान बेहद प्रेम के क़ाबिल हैं। उनके जीवन को देखकर हमारा दिल चाहता है कि हम भी अपने आप को छोटे-छोटे दायरों से बाहर निकालें, ज़ुल्म और अत्याचार की ज़ंजीरों से अपने आप को मुक्त करें। ये संत-महात्मा हमें निमंत्रण देते हैं कि उनके जीवन से मिसाल लेकर, उनके समझाए रास्ते पर चलकर, धीरे-धीरे हम अपने अंदर छिपी नेकी और इनसानियत को जगाएँ और मिलकर इस संसार को एक ख़ुशियों से भरी रूहानी जगह बनाएँ।
हमारी बेटियों की पुकार है कि हम जागें। वे चाहती हैं कि हम ग़लत रास्ते को छोड़ें। वे चाहती हैं कि हम अपने सामाजिक रिवाजों और परंपराओं के बारे में फिर से सोचें और उन्हें बदलें। वे चाहती हैं कि हम हिम्मत दिखाएँ, उन्हें अपना प्यार दें। वे चाहती हैं कि हम उन्हें उनके भाइयों के बराबर का दर्जा दें। उन्हें हमारी हिम्मत, हमारा सहयोग और सबसे महत्त्वपूर्ण हमारा प्यार चाहिये।
आइये! आज हम बदलाव की प्रतिज्ञा लें। आइये! पक्का इरादा कर लें कि हम जाग्रत इनसान बनेंगे, औरतों की क़द्र करेंगे, उन्हें शक्ति और आज़ादी भरा जीवन जीने का हक़ देंगे। हमें न सिर्फ़ औरतों के लिये, बल्कि अपने लिये भी ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़ुल्म और अत्याचार एक दिन हमारे ही जीवन में ज़हर बनकर लौटेगा। ठीक इसी तरह प्यार और हमदर्दी हमारे जीवन में ख़ुशी और शांति की लहर लाएगी।
अगर हम अपने दिल में बेटियों के लिये जगह बनाएँगे, अगर हम अपने बेटों और बेटियों को बराबर का दर्जा देंगे तो क़ुदरत हम पर आशीर्वाद की बौछार करेगी और हमारी बेटियाँ हमें कई गुणा ज़्यादा प्यार से निहाल कर देंगी। मालिक की रज़ा में रहनेवाला यह प्यार भरा नज़रिया न केवल हममें, बल्कि सारे समाज में बदलाव ला सकता है।
यह छोटी–सी पुस्तक एक पुकार है, एक निमंत्रण है कि जागो! एक ऐसे नेक इनसान बनो कि हर करनी में रूहानियत झलके। हमारी इनसानियत हमारी रूहानियत से जुड़ी हुई है।
जागो, मेरे दोस्त
जागो, मेरे दोस्त!
जीवन कर्म और फल के पहिये पर घूम रहा है—
लेने और देने के, करने और भुगतने के पहिये पर।
लेकिन जीने का एक अलग ढंग भी है,
है इस चक्कर में से निकलने का एक ढंग।
हाँ, है इस चक्कर में से निकलने का एक ढंग।
मनुष्य-जीवन है एक अनमोल अवसर,
जागने का और अपने दायरे को बढ़ाने का अवसर।
समझो इस जीवन के परम सत्य को।
हाँ, समझो इस जीवन के परम सत्य को।
सचेत रहो कि तुम क्या कर रहे हो,
पूरी सावधानी से चुनो अपने कर्म,
अनुकूल बनाओ अपने कर्मों को उस लक्ष्य के, प्रेम से।
हाँ, अनुकूल बनाओ अपने कर्मों को उस लक्ष्य के, प्रेम से।
एक अनमोल अवसर है यह क्षण अनंत काल का,
जो भी तुम करो, ले जाए तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर,
बढ़ाए तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर।
हाँ, बढ़ाए तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर।
दया और सच्चाई हो तुम्हारे व्यवहार में,
तब तुम स्वयं प्रभु-तुल्य हो जाओगे,
स्वयं प्रभु ही हो जाओगे।
एम.एफ.सिंह
आख़िरी संदेश: बड़े पैमाने पर कन्या हत्या
कोई भी काम करने से पहले उसके नतीजे को
ध्यान में रखो, ताकि जब कर्मों का
हिसाब देने का वक़्त आए तब पछताना न पड़े।
मौलाना रूम
इनसान की सोच की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उसे जब अपनी सोच के ख़िलाफ़ क़दम उठाना पड़े, तो उसका मन साहस नहीं कर पाता और इनसान उस काम को अनदेखा कर देता है। जब हम किसी काम को नहीं करना चाहते तब हम उसकी तरफ़ ध्यान नहीं देते, जैसे कि हम उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। लेकिन अब हमारी सोच में बदलाव लाने की सख़्त ज़रूरत है। इस भाग में कुछ चौंकानेवाले आँकड़े दिये गए हैं जो औरतों के नीचे दर्जे की गवाही देते हैं। अगर औरतों को आदमियों के बराबर का दर्जा दिया जाता तो आज हमारे सामने ये आँकड़े कुछ और ही होते।
1. हत्याओं के आँकड़ेजीवित प्राणी को मारना अपने आप को मारना है। दूसरे जीवों के प्रति हमदर्दी रखना अपने आप से हमदर्दी रखना है।
भगवान् महावीर
कहा जाता है कि जो बात एक तस्वीर व्यक्त कर सकती है, उसको हज़ार शब्द भी बयान नहीं कर सकते। आगे दिये गए चार्ट साफ़ तौर पर यह दर्शाते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी बेटियों के साथ क्या अन्याय हुआ है। अगर हम अपनी सोच में तुरंत बदलाव नहीं ला पाए तो 2011 की जनगणना तक लड़कियों की संख्या का अनुपात न जाने कितना बिगड़ जाएगा, ये आँकड़े और भी भयंकर होंगे।
- बच्चों में लिंग अनुपात पिछले 40 साल से तेज़ी से बिगड़ रहा है
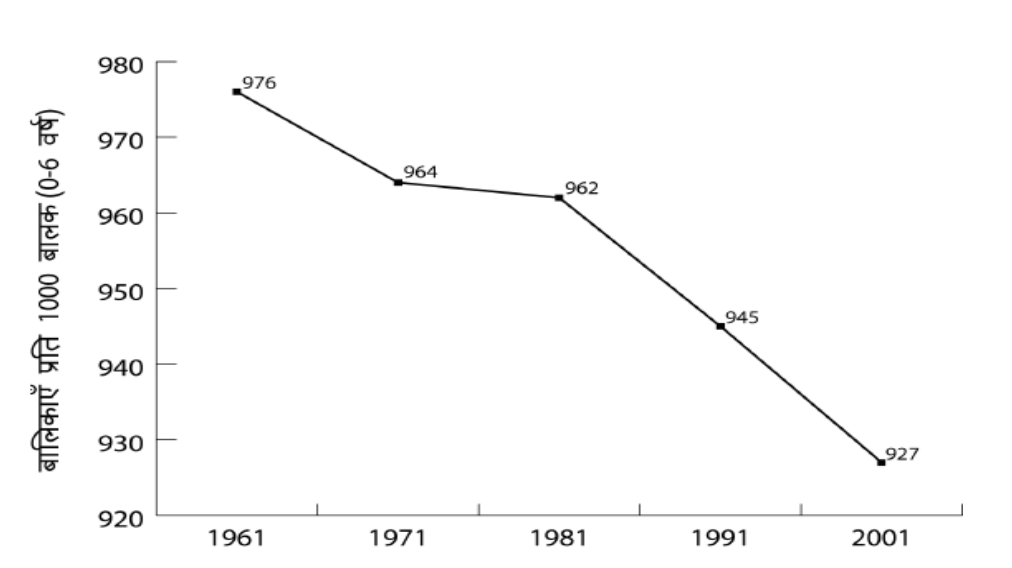
स्रोत: भारत की जनसंख्या 2001 अगर हमने अपनी सोच को बदलने के लिये सही दिशा में क़दम नहीं उठाए तो हमारे समाज में कई दशकों तक यह गंभीर ख़तरा मँडराता रहेगा।
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (गणना) - लिंग जाँच कराने में गाँव के मुक़ाबले शहरी लोग आगे
गाँव/शहरी लिंग अनुपात 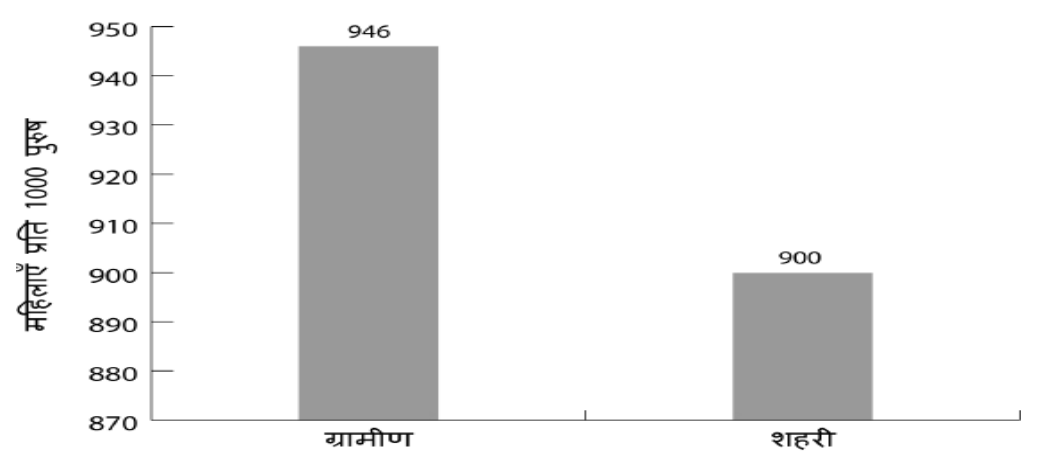
स्रोत: भारत की जनसंख्या 2001 - अनपढ़ परिवारों के मुक़ाबले पढ़े-लिखे परिवार ज़्यादा कन्या भ्रूणहत्या कर रहे हैं
माँ की पढ़ाई का स्तर और जन्म के समय लिंग अनुपात 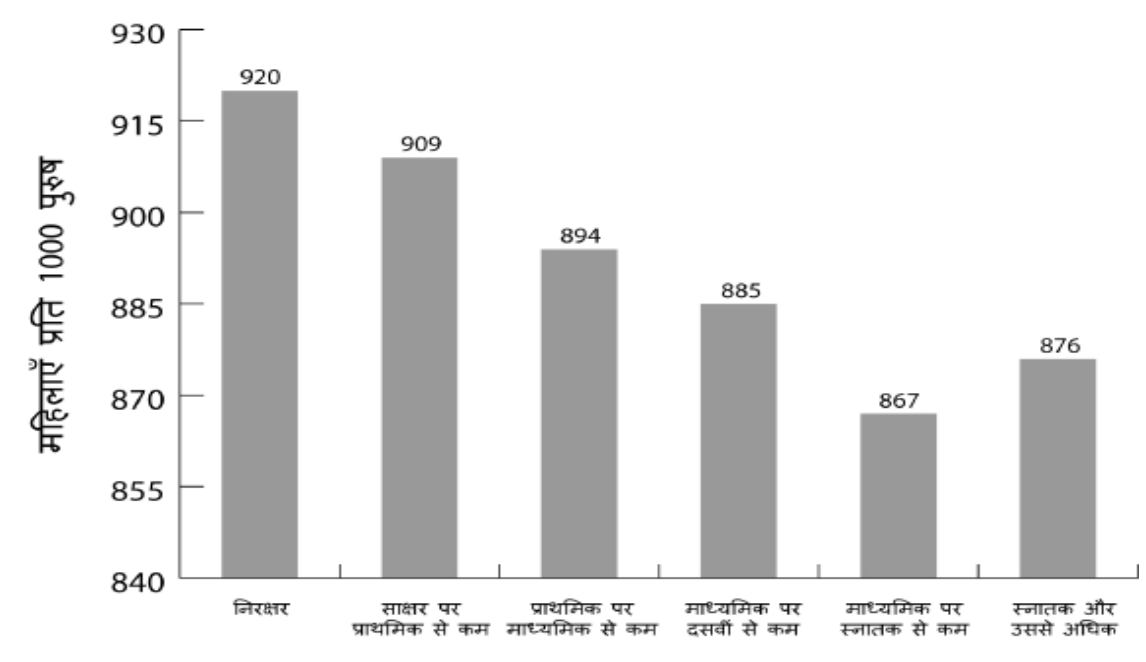
स्रोत: भारत की जनसंख्या 2001 - लिंग जाँच सभी धर्मों के लोग कर रहे हैं
धार्मिक संप्रदाय और बच्चों में लिंग अनुपात 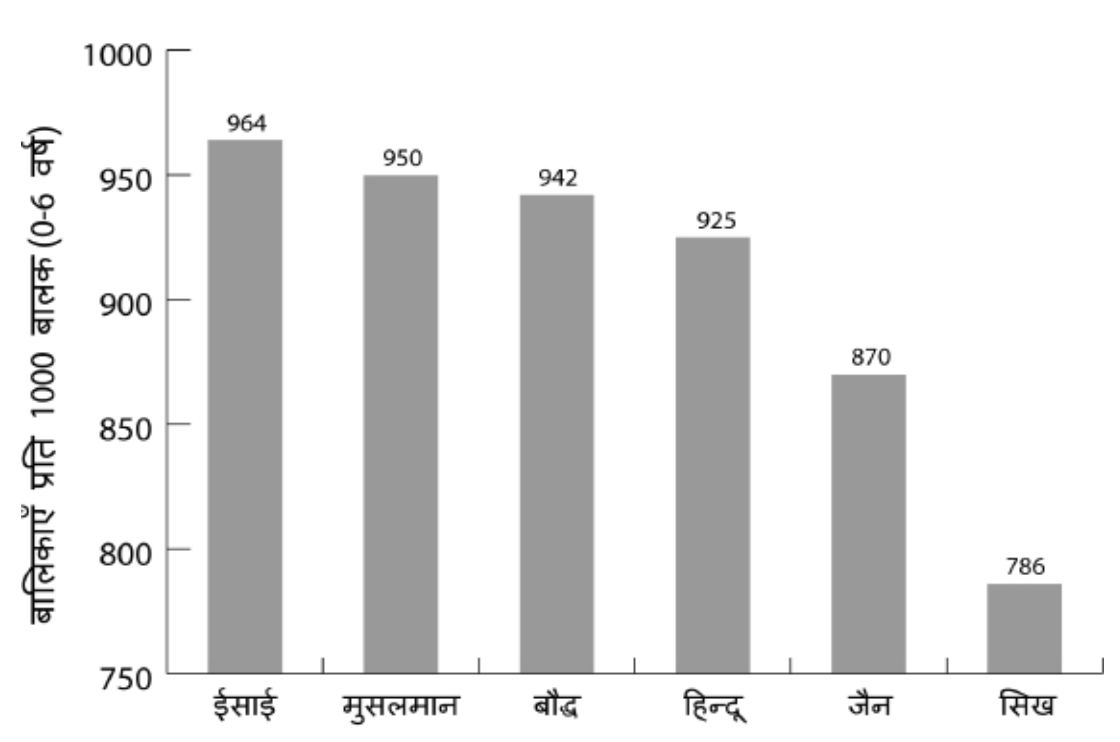
स्रोत: भारत की जनसंख्या 2001 - राष्ट्रीय औसत की वजह से असंतुलन की सही तसवीर सामने नहीं आती
राज्य, जिनमें बच्चों के लिए लिंग अनुपात में सबसे अधिक गिरावट हुई 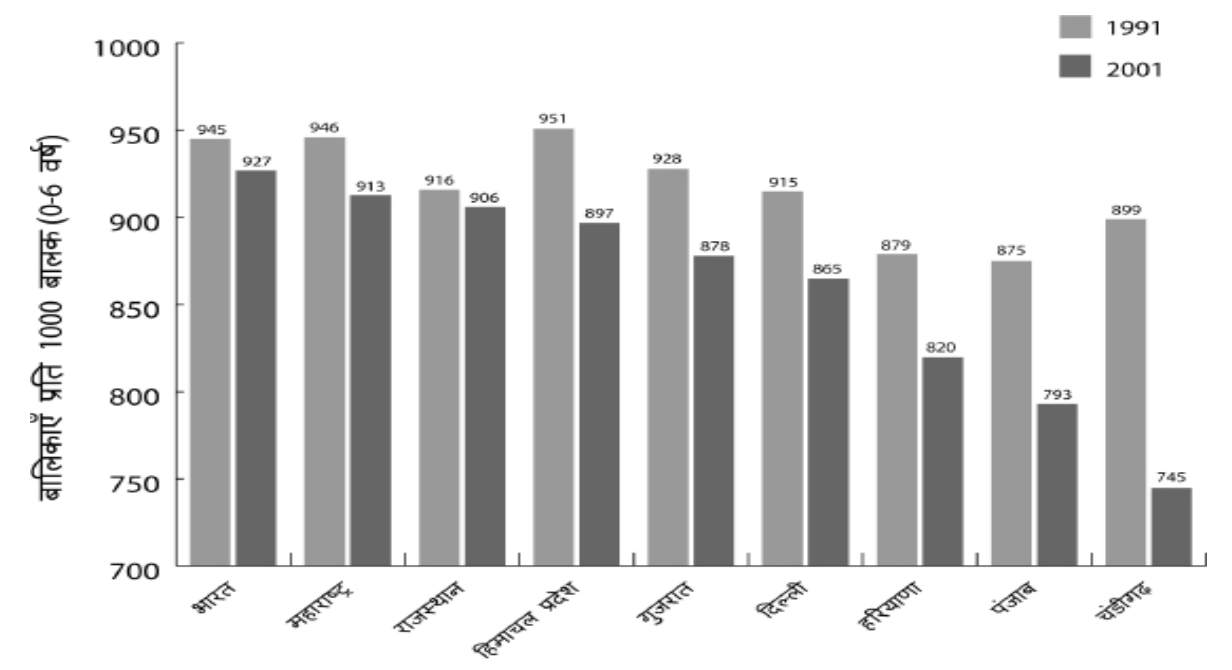
स्रोत: भारत की जनसंख्या 2001 इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी बड़ी संख्या में क़त्ले आम होता है तो सच्चाई को हमेशा शब्दों के ताने-बाने में छिपाया जाता है। आज भी ‘कन्या भ्रूणहत्या,’ ‘बेटे की चाह’ और ‘लिंग चुनाव’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके सच्चाई को छिपाया जा रहा है, हालाँकि ग़ैरकानूनी हत्या बहुत बड़े पैमाने पर करवाई जा रही है। माँ-बाप की इच्छा से डॉक्टर इस काम को धड़ल्ले से कर रहे हैं और हम उन्हें यह करने दे रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि माँ-बाप ग्राहक के रूप में अपनी पसंद रख सकते हैं।
डॉक्टर पुनीत बेदी, कार्यकर्ता, क्रिस्टीन टूमे के शब्दों में,‘जैन्डर जेनोसाइड,’द सण्डे टाइम्स, अगस्त 2007 - दुनिया के बाक़ी देशों के मुक़ाबले भारत में लड़कियों का लिंग अनुपात बहुत कम है और कहा जाता है कि जल्द ही चीन से भी कम हो जाएगा
दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों के आँकड़े, 2009 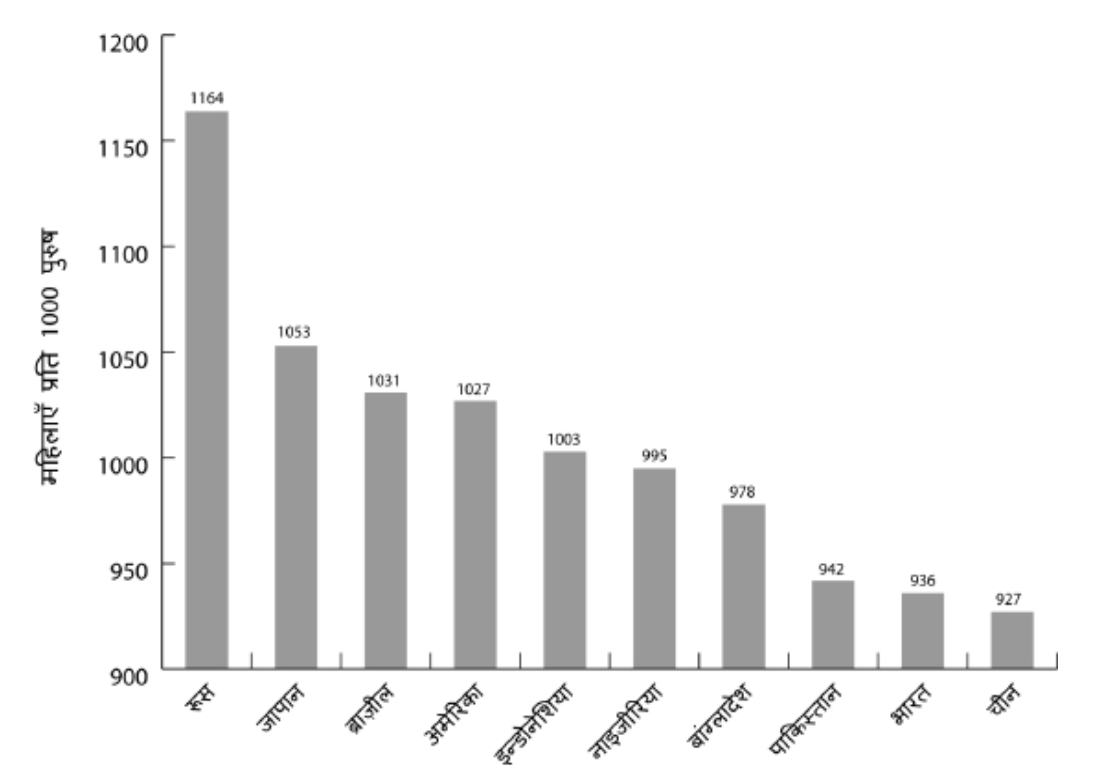
जनसंख्या विभाग के आर्थिक और सामाजिक संगठित
सचिवालय, दुनिया की जनसंख्या के आधार पर, 2008जब तक यह बेपरवाही चलती रहेगी, तब तक हमारी लड़कियों की संख्या में कमी होती जाएगी और अगले 10 सालों में हमारा देश लड़की को जन्म से पहले ही मार देने में चीन से भी आगे निकल जाएगा।
डॉक्टर साबू जॉर्ज, कार्यकर्ता, स्टीव हरमन के शब्दों में, वॉयस ऑफ़ अमेरिका, 5 मार्च, 2007
2006 में प्रतिष्ठित ब्रिटिश मेडिकल जरनल, द लैन्सेट में छपे एक अध्ययन में बताया गया कि भारत में पिछले 20 सालों में एक करोड़ कन्या भ्रूणहत्या हुई होंगी।26 इस अध्ययन से यह पता लगता है कि हर साल पाँच लाख कन्याओं की भ्रूणहत्या की जाती है। इसका मतलब है कि हमारे देश में लगभग हर एक मिनट में एक कन्या भ्रूणहत्या होती है, जबकि भारतीय डॉक्टरों के संगठन का इस संख्या पर मतभेद रहा है। वे कहते हैं कि हर साल हमारे देश में 5 लाख नहीं, बल्कि 2.5 लाख कन्या भ्रूणहत्या होती हैं।27
दिसंबर 2006 की यूनीसेफ़ रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत में हर रोज़ लगभग 7000 लड़कियाँ कम पैदा होती हैं और पिछले 20 सालों में जितनी लड़कियों को पैदा होना चाहिये था, उससे एक करोड़ कम लड़कियों का जन्म हुआ।28 यह गिनती द लैन्सेट की रिपोर्ट से मिलती है।
2007 में, ‘एक्शन ऐड’ ने उत्तर भारत के पाँच क्षेत्रों के 6000 परिवारों के लोगों से पूछताछ करके एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक़ हमारे देश में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ 1000 लड़कों के मुक़ाबले सिर्फ़ 500 लड़कियाँ ही हैं और कुछ ऐसे शहरी इलाक़े हैं जिनमें ऊँची जाति के परिवार रहते हैं, लेकिन जहाँ 1000 लड़कों के मुक़ाबले सिर्फ़ 300 लड़कियाँ ही हैं।29
द पाइनियर, 28 अक्तूबर 2001, अख़बार में लिखा है कि पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में 200 राठौर परिवार रहते हैं। हर परिवार में 2 से 4 लड़के हैं, लेकिन 200 परिवारों में सिर्फ़ 2 लड़कियाँ हैं। इसका मतलब इस बिरादरी में 400 लड़कों के मुक़ाबले सिर्फ़ 2 लड़कियाँ ही हैं।30
इस संकट का सही अनुमान हमें 2011 की अगली जनगणना के बाद ही लग पाएगा। लड़कियों की सही गिनती क्या है? इस बारे में विषय के जानकार अपनी-अपनी दलीलें दे रहे हैं। इस दौरान लड़कियों की हत्या का सिलसिला हर रोज़ जारी है।
2. क्या हमारे देश में कानून लागू हो रहा है?हक पराया जातो नाहीं, खा खा भार उठावेंगा।
फेर न आकर बदला देसें, लाखी खेत लुटावेंगा।
दाउ ला के विच जग दे जूए, जित्ते दम हरावेंगा।
साईं बुल्लेशाह
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कभी-कभी औरत को सुरक्षा की दृष्टि से गर्भपात कराने की ज़रूरत पड़ती है, भारत सरकार ने 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनन्सीज़ एक्ट (एम.टी.पी.एक्ट) नाम का कानून बनाया। औरतों को अनचाहे और ख़तरनाक गर्भावस्था से बचाने के लिये यह कानून बहुत ज़रूरी है। इस कानून के मुताबिक़ गर्भपात कराना कानूनी है, लेकिन एक नये कानून के मुताबिक़ लिंग चुनाव करना (पहले लिंग की जाँच कराना, फिर जब पता चले कि बेटी है, गर्भपात करा देना) बिलकुल ग़ैरकानूनी है। यह कानून प्री-कॉनसेप्शन एण्ड प्री-नेटल डायग्नॉस्टिक टेकनीक्स एक्ट (पी.सी. & पी.एन.डी.टी.एक्ट) 1994 में बनाया गया और 2003 में बदला गया। जानकारों का कहना है कि यह काफ़ी सख़्त कानून है, लेकिन हम इस कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं।
लिंग जाँच करवाना ग़ैरकानूनी हैकानून के मुताबिक़ लिंग जाँच करवाना ग़ैरकानूनी है।
सच्चाई तो यह है कि अगर हर साल पाँच लाख लड़कियों का गर्भपात किया जा रहा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में हर साल कम से कम 10 लाख ग़ैरकानूनी लिंग जाँच भी किये जा रहें हैं, क्योंकि साधारणत: हर दो जाँच में से एक लड़की होती है।
क्लिनिक को रजिस्टर्ड होना चाहियेकानून के मुताबिक़ जो भी जेनेटिक क्लिनिक, काउँसलिंग सेंटर या लेबॉरेट्री गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड करते हैं, उन्हें कानून के अनुसार रजिस्टर्ड होना चाहिये।
आज भारत में लगभग 30,000 रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड केंद्र हैं।31 लेकिन अनुमान है कि इससे दो या तीन गुणा ज़्यादा केंद्र ग़ैरकानूनी तौर से चलाए जा रहे हैं। आज हमारे देश में हज़ारों अल्ट्रासाउंड मशीनें वैन या मोटर साइकिल पर लगाई जाती हैं और पैसे के लालच में लोग इन्हें एक गाँव से दूसरे गाँव ले जाते हैं। वहाँ अनपढ़ लोगों से बहुत ज़्यादा धन लेकर लिंग जाँच और गर्भपात करवाए जा रहे हैं।
अजन्मे बच्चे का लिंग बताना ग़ैरकानूनी हैइस कानून के मुताबिक़ जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड टेस्ट करते हैं, उन्हें माँ-बाप को बच्चे के लिंग की ख़बर नहीं देनी चाहिये। बच्चे की माँ या उसके रिश्तेदारों को शब्दों से, इशारों से या किसी और तरीक़े से बच्चे के लिंग का संकेत देना ग़ैरकानूनी है।
विज्ञापन देना ग़ैरकानूनी हैकई डॉक्टर एक अनोखे तरीक़े से बच्चे के लिंग का संकेत माँ-बाप को देते हैं, जोकि बिलकुल ग़ैरकानूनी है।
‘नीले कपड़े ख़रीदने का वक़्त आ गया है,’ ‘पेड़े ख़रीदो’ या ‘जय श्री कृष्ण’—अगर गर्भ में बेटा है।
‘गुलाबी कपड़े ख़रीदने का वक़्त आ गया है,’ ‘बर्फ़ी ख़रीदो’ या ‘जय माता दी’—अगर गर्भ में बेटी है।
पी.सी. & पी.एन.डी.टी.एक्ट, हैण्ड बुक फ़ॉर द पब्लिक30
लिंग जाँच के बारे में किसी भी प्रकार का विज्ञापन देना ग़ैरकानूनी है।
कुछ डॉक्टर अब भी इस प्रकार के विज्ञापन देते हैं, ‘आज पाँच हज़ार रुपये ख़र्च करो, आगे चलकर पाँच लाख रुपये बच जाएँगे।’ इसका क्या मतलब है? कुछ डॉक्टर अपने धंधे को बढ़ाने के लिये लोगों से कह रहें हैं कि आज लड़की का गर्भपात करवाओ तो आगे चलकर दहेज के ख़र्च से बच जाओगे।
सज़ाइस कानून का पालन न करनेवाले डॉक्टर को जुर्माना देना पड़ सकता है। मई 2008 में यह जुर्माना 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक कर दिया गया था। अपराध करनेवाले को 3 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल भी भुगतनी पड़ सकती है।
यह कानून 1994 में लागू किया गया था, लेकिन सबसे पहला अपराध साबित हुआ मार्च 2006 में, जिसमें एक डॉक्टर को दो साल के लिये जेल भेजा गया।32
क्या औरतों को न्याय मिल रहा है?

ही चाहता है तो क्या ऐसा कानून कभी सही तरीक़े से
लागू किया जा सकता है?
आज हमारे देश में लिंग जाँच 400 करोड़ रुपये का कारोबार है और बढ़ता ही जा रहा है।27
कई डॉक्टरों को इस तकनीक को बढ़ावा देने से लाभ पहुँचता है। इसलिये डॉक्टरों की किसी भी संस्था ने इस ग़ैरकानूनी कारोबार के विरोध में कोई ठोस क़दम नहीं उठाया। सच तो यह है कि डॉक्टरों के संघ बहुत शक्तिशाली हैं और अपने कारोबार को बचाने के लिये कुछ डॉक्टर इस कानून के ख़िलाफ़ अदालत तक पहुँच गए हैं।
कुछ कंपनियाँ इस बात का ध्यान रखती हैं कि वे अल्ट्रासाउंड की मशीनें केवल रजिस्टर्ड क्लिनिक को ही बेचें, पर ज़्यादातर मशीनें बिना सही काग़ज़ी कार्यवाही के ही बेची जा रही हैं।
अल्ट्रासाउंड की मशीनें केवल लिंग जाँच के ही काम नहीं आतीं, बल्कि इनके द्वारा गर्भ में होनेवाले रोग का भी पता चलता है और माँ और बच्चे को चोट या हानि से बचाया जा सकता है। गर्भ से जुड़ी जानकारी के अलावा इनके द्वारा कैंसर जैसी बीमारियों का भी पता चलता है। लेकिन 20 सालों में इन मशीनों की बिक्री बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इसकी मुख्य वजह है लिंग जाँच करवाने की माँग। विदेशी कंपनियाँ इस ज़रूरत को पूरा करने के लिये हज़ारों मशीनें हमारे देश में भेज रही हैं।
2006 में अल्ट्रासाउंड की मशीनों की बिक्री से भारत में 308 करोड़ का कारोबार हुआ जो 2005 की तुलना में 10% ज़्यादा था।34
भारत संसार का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। हम दुनिया के सबसे पहले देशों में हैं, जहाँ सन् 1928 में औरतों को वोट देने का हक़ दिया गया। हमारा संविधान संसार के उत्तम संविधानों में एक है। सबके लिये न्याय का वायदा हमारे संविधान में है। हमें अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है और अपने धर्म को मानने की आज़ादी है। यहाँ धर्म, जाति, लिंग और जन्म-स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता।
क्या भारत में औरतों को अपने अधिकार मिल रहे हैं?
- लंबा जीवन जीने की आज़ादी
- अच्छी सेहत का हक़
- पढ़ने-लिखने का हक़
- बिना ज़ुल्म के काम करने की आज़ादी
- अपने फ़ैसले लेने की आज़ादी
- डर से छुटकारा पाने की आज़ादी
सच्चाई तो यह है कि जब औरत से उसके जीने का हक़ ही छीन लिया जाता है, तो उसे दिये गए ये सभी हक़ बेमतलब हो जाते हैं।
3. मदद के लिये एक पुकार
कई बार हम सोचते हैं कि ग़रीबी—सिर्फ़ भूखे रहना, कपड़े न होना और बेघर होना है। लेकिन जब किसी को तुम्हारी ज़रूरत न हो, कोई तुम्हारा ध्यान न रखे, तुम्हें किसी का प्यार न मिले—असल में ये सबसे बड़ी ग़रीबी है। अगर हम इस ग़रीबी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें इसकी शुरुआत अपने ही घर से करनी होगी।
मदर टेरेसा
जानकारी के लिये गणना, रेखाचित्र, आँकड़े—ये सभी ज़रूरी हैं, लेकिन ये एक औरत के असली दर्द की कहानी कभी नहीं बता सकते। आगे दिये गए उदाहरणों का मतलब किसी को परखना नहीं, बल्कि मक़सद सिर्फ़ यह है कि लोग इन्हें पढ़कर बेटियों के जीवन की सच्चाई को समझें, उनके दर्द को महसूस करें और उनकी सहायता के लिये सामने आएँ।
ख़ुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के सपने ...उन्नीस साल की रीना ने भी ख़ुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी के सपने देखे थे जो कभी पूरे न हो सके। शादी के एक महीने बाद दहेज की वजह से वह ससुराल में बुरी तरह से सताई गई और शनिवार की सुबह इन्द्रा नगर में जला दी गई। उसका पिता घनश्याम चंद मछली व्यापारी था, जिसकी मृत्यु एक साल पहले हो गई थी। उसकी पुत्री रीना की शादी 19अप्रैल को सुनील के साथ हुई थी ìशादी के तुरंत बाद सुनील के पिता ने एक रंगीन टेलीविज़न और मोटर साइकिल की माँग की। जब रीना की माँ उनकी माँगें पूरी न कर सकी, तो रीना को अपने पति और सास की मारपीट लगातार सहन करनी पड़ी। शनिवार की सुबह रीना की माँ को यह ख़बर मिली कि मिट्टी के तेल की लालटेन गिरने से रीना के कपड़ों ने आग पकड़ ली और वह जलकर मर गई। लेकिन उसकी जाँच के बाद पता लगा कि रीना के साथ कोई हादसा नहीं हुआ, बल्कि जान बूझकर उसे जान से मार दिया गया, क्योंकि उसके दाँत टूटे हुए थे और उसके हाथ और छाती पर भी घाव पाए गए।
टाइम्स ऑफ़ इण्डिया, लखनऊ, मई 27, 2001 [नाम बदले हुए हैं]
वीरो (बदला नाम) ख़ून की कमी और ठीक ख़ुराक न होने की वजह से अपनी असली उम्र 34 साल से भी बड़ी लगती है। उसका आधा जीवन पुत्र पैदा करने की लालसा में ही बीत गया; इस चाह की वजह से उसने लगातार चार गर्भपात कराए। बाक़ी ज़िंदगी इसी अफ़सोस में बीती कि उसको अंत समय में आग देने के लिये कोई पुत्र नहीं होगा। वह कहती है, ‘मुंडे दे बिना माँ-प्यो रुल जांदे ने।’ (बेटे के बिना माँ-बाप बरबाद हो जाते हैं।) उसकी आँखें आँसुओं से भरी हुई हैं और उनमें कोई अनजान डर छिपा हुआ है। वह मानती है कि उसकी तीन बेटियाँ अपनी हैं ही नहीं। वह कहती है, ‘औलाद ते मुंडा ही हुन्दा ऐ, कुड़ियाँ ते बेगानियाँ हुन्दियाँ नें।’ (औलाद तो बेटा ही होता है, बेटियाँ तो पराया धन होती हैं।)
अरूती नैयर, ‘सायलेंट जेनोसाइड’, द ट्रिब्यून, मई 6, 2001
जुलाई 23, 2007 के दिन, उड़ीसा पुलिस ने एक चौंकानेवाली खोज की। उन्हें एक सूखे कुएँ से 30 प्लास्टिक की थैलियाँ मिलीं जो कन्या भ्रूण और नवजात शिशुओं के छोटे-छोटे अंगों से भरी हुई थीं। यह कुआँ एक प्राइवेट अस्पताल के पास नयागढ़ में है जो भुवनेश्वर के नज़दीक है। इस कुएँ की जाँच इसलिये कराई गई, क्योंकि 15 जुलाई, 2007 के आस-पास कन्या भ्रूण से भरी सात थैलियाँ इसी गाँव के नज़दीक एक सुनसान जगह पर मिलीं। इन दोनों घटनाओं की वजह से पुलिस को शक हुआ कि यहाँ कोई कन्या भ्रूणहत्या की कड़ी है। कन्या भ्रूणहत्या देश के विभिन्न भागों में लगातार हो रही है। दिल्ली के नज़दीकी क्षेत्र में प्रसूति क्लिनिक की बेसमेंट में पुलिस को सैप्टिक टैंक में हड्डियाँ मिलीं, जिसके बाद एक डॉक्टर को 260 ग़ैरकानूनी कन्या भ्रूण गर्भपात करने के जुर्म में गिरफ़्तार किया गया।
‘भारत में कन्या भ्रूणहत्या का कोई अंत नहीं’ डाँस विद शैडोज़, 24 जुलाई, 2007
राजस्थान के एक छोटे-से गाँव में एक वर्कशॉप में एक औरत अपने 8 महीने के बेटे और 3 साल की बेटी के साथ आई थी। अचानक उसका बेटा तेज़ बुख़ार से बीमार पड़ गया। लड़के को साँस लेना भी मुश्किल लग रहा था। यह छोटा-सा गाँव, जहाँ कोई दवाख़ाना भी नहीं था। माँ ने अपनी बेटी की तरफ़ उँगली उठाकर कहा, ‘काश! ये इसको हुआ होता।’
पुत्र को किसी न किसी तरह अगले दिन अस्पताल में पहुँचाया गया और वह ठीक हो गया। बाद में जब मैंने उस माँ से कहा कि मैं उसकी बात से दु:खी हुई तो माँ ने जवाब दिया, ‘देखो, अगर मेरी बेटी मर जाती तो मैं फिर भी घर लौट सकती थी। लेकिन अगर मेरा बेटा, जो चार बेटियों के बाद पैदा हुआ है, मर जाता तो मुझे कोई घर में आने भी नहीं देता। मुझे ख़ुदकुशी ही करनी पड़ती। मुझे परिवार में कोई स्वीकार न करता, क्योंकि यह पुत्र अनमोल है।’
कोई भी माँ अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती, लेकिन औरत इसी प्रकार जीती आई है। दूसरों के द्वारा इसी तरह उसे दर्द दिया जाता है। उसके जीवन की सच्चाई यही है कि वह ख़ुद के लिये इतना भी निश्चित नहीं कर सकती कि वह कब दु:खी हो, किसके लिये दु:खी हो और कैसे दु:खी हो। यह औरत की ज़िंदगी की हक़ीक़त है।
आभा भइया, जागोरी, जैसे रशीदा भगत को बताया, ‘स्लॉटर इन द वूम्ब’
एक औरत को बताया गया कि उसका बच्चा स्वस्थ और सुंदर है, लेकिन उदास होकर उसने मुँह फेर लिया। नर्स ने बताया, ‘लड़की है, इसलिये।’ देश के किसी दूसरे हिस्से में एक चिंतित औरत अस्पताल में बच्चों के वॅार्ड में बैठी है। उसके गर्भ में सात महीने का बच्चा है। अल्ट्रासाउंड के स्कैन से यह पता चला है कि इस बार बच्चा लड़का है और वह अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। पिछली दो गर्भावस्था के बारे में कहती है; ‘दोनों टाइम टेस्ट में लड़की निकली तो सफ़ाई करा दी।’
वाई.के.सबरवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अपने भाषण में, ‘कन्या भ्रूणहत्या का अंत’
पंजाब और हरियाणा राज्यों में औरतों की कमी होने की वजह से आसाम राज्य से औरतों को लाकर बेचा जाता है। कभी-कभी देखने में आता है कि आसाम से लाई गई 4-5 नाबालिग़ लड़कियों को खुले आम, 10,000 रुपये से 30,000 रुपये में हरियाणा की कुछ पंचायतों में बेचा जाता है। हरियाणा में ऐसी कन्या ‘पारो’ के नाम से जानी जाती है।
रवि कांत, एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर, शक्ति वाहिनी, सुशान्ता ताल्लुकदार के शब्दों में, ‘ट्रैफ़िकिंग ऑफ़ विमिन फ़्रॉम आसाम ऑन द राइज़’
छत्तीस साल का सुखराज सिंह जो मिलान, इटली में एक डेरी फ़ार्म में मज़दूर का काम करता है, अमृतसर में एक काम से आया है। सुखराज और उसकी पत्नी बीड़ बाबा बुड्ढा के मंदिर में पुत्र के लिये प्रार्थना करने आए हैं। सात साल से बेऔलाद रहने के बाद पिछले साल उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया, तो दोनों पति-पत्नी बहुत दु:खी हुए। इसलिये इस साल वे वापिस आए हैं—बेटे के लिये प्रार्थना करने।
सुखराज कहता है, ‘इस मंदिर में हमने प्रार्थना की और हमें बेटी हुई, इसलिये हम फिर से इस मंदिर में वापिस आए हैं ताकि हमें बेटा हो।’ बहुत सालों से देश-विदेश से लोग इस तरह की प्रार्थना लेकर पंजाब के ऐसे मंदिरों और गुरुद्वारों में आते हैं। यहाँ बेटी की प्रार्थना करने कोई नहीं आता।
उन्नीस साल की रजवन्त कौर से मिलकर यह बात स्पष्ट हुई है कि भाई की प्रार्थना लेकर वह इन मंदिरों के चक्कर काटती रहती है। वह जानती है कि वह अपने परिवार पर बोझ है। ‘कोई भी परिवार अब लड़की नहीं चाहता, हर कोई लड़का चाहता है, क्योंकि माँ-बाप दहेज नहीं दे सकते। इसलिये वे प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में लड़कियाँ पैदा न हों।’
नीलांजना बोस, सीएनएन/आईबीएन, ‘सन टेम्पल्ज़ ऑफ़ पंजाब’
बलबीर कौर कहती है—‘यह भगवान् की मर्ज़ी है कि इस घर में अब सिर्फ़ बेटे पैदा होते हैं।’ उसके पीछे उसका पति टहल रहा है। ‘हम इस बात से परेशान नहीं हैं। असल में जायदाद अपने ही परिवार में रखना इसका मुख्य कारण है। पहले कन्या हत्या होती थी और अब कन्या भ्रूणहत्या, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता।’
जब बलबीर मुझे अपनी बहू कुलविंदर के साथ छोड़कर चली जाती है, तो बातचीत में एक उदासी आ जाती है। कुलविंदर कहती है, ‘काश! मेरी एक बेटी होती। औरत बेटी के बिना अधूरी है। बेटियाँ अपनी माँ की मदद करती हैं। मैं अभी भी इस बात को सोचकर उदास हो जाती हूँ।’ फिर मुँह फेरकर कुलविंदर कहती है, ‘लेकिन मेरे कई गर्भपात अपने आप ही हो गए।’
क्रिस्टीन टूमे, ‘जेन्डर जेनोसाइड’ द सन्डे टाइम्ज़, अगस्त 26, 2007. गाँव डेरा मीर मिरान, लिंग अनुपात 361 (जनगणना 2001)
हुआ बेटा तो ढोल बजाया!हुई बेटी तो मातम छाया!
नन्ही बेटी को जीवन का वर दो!
हत्या क्यों करते हैं गर्भ में उसकी,
चीख़ अनसुनी क्यों करते हैं मासूम की,
दोष उसका है क्या?
फ़र्क़ बेटी बेटे में हमने ही किया।हुआ बेटा तो ढोल बजाया! हुई बेटी तो मातम छाया!
ऐसा क्यूँ करते हैं हम?क्यूँ बेटी को दर्द हमने इतना दिया है,
प्रभु के उपहार को क्यूँ ठुकरा दिया है,
क्यूँ दो घरों की रौशनी को सिसका दिया है,
बेशर्मी से बेटी का सौदा किया है,
दहेज के हाट पर उसे बेच दिया है,
मालिक का खौफ़ और कानून का डर,
धन के लोभ ने सब भुला दिया है।नन्ही बेटी को जीवन का वर दो!
जगत जननी है वो, प्रेम की शक्ति है वो,
शीतल छाया है परिवार की आत्मा है वो।
ममता की प्यारी गोद किसे याद नहीं?
आँखों का छलकता सागर किसे याद नहीं
बेटी का लाड़, और पत्नी का स्नेह,
माँ का आशीर्वाद, किसे याद नहीं?नन्ही बेटी को जीवन का वर दो!
शिक्षा का सौभाग्य उसे दो,
बराबर के अधिकार उसे दो,
जीवन में सम्मान उसे दो।
आख़िर बेटी है किससे कम?गाँव की सरपंच रही,
क़ामयाब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रही,
ऐस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, प्रोफ़ेसर बनी,
उद्योगपति, पायलट, इंजीनियर बनी,
विज्ञान में, भक्ति में, साहित्य और कला में,
शोहरत है हासिल उसे हर क्षेत्र में।हत्या क्यों करते हैं गर्भ में उसकी,
चीख़ अनसुनी क्यों करते हैं मासूम की?बदलो! सोच अपनी अब तुम बदलो।
बदलो! समाज की कुरीतियाँ, मान्यतायें बदलो।
जागो! सुनो, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो।
बनो निर्भय, भरोसा प्रभु का करो।
उसकी नज़रों में सच्चे इनसान तो बनो।जब एक है परमात्मा और आत्मा उसकी अंश है,
तो भेद स्त्री और पुरुष में हमने क्यूँ किया है?नन्ही बेटी को जीवन का वर दो!
फिर घर-घर ढोल बजेंगे, बेटी बेटा दोनों हमारी ख़ुशी बनेंगे।नन्ही बेटी को जीवन का वर दो!

मम्मी! पापा!
आप मुझे दुनिया में लाए
मुझे मौक़ा तो दीजिए।
आत्मा न स्त्री है न पुरुष।
तुम में सुंदरता और शक्ति है उतनी
दुनिया की दूसरी आत्मा में है जितनी।
डॉ. ब्रायन एल.वाइस
संदर्भ ग्रंथ
- Research study in 2005 by Caliper, a USA-based consulting firm, and Aurora, a UK-based firm, “How Women are Redefining Leadership;” Pew Research Center, 2008, “Men or Women: Who’s the Better Leader?”
- 2001 Census of India.
- UNICEF Report: “State of the World’s Children – 2009.”
- UNICEF India, Newsline: Roopa Bakshi, April 2006, “UNICEF Unveils New Tool to Combat Maternal Mortality in India.”
- UNFPA Report: “State of World Population 2004, Adolescents and Young People: Key Health and Development Concerns.”
- National Family Health Survey (2005 – 2006) Report.
- Kalyani Menon-Sen and A. K. Shiva Kumar, 2001, “Women in India: How Free? How Equal?” A Report commissioned by the United Nations Resident Coordinator in India.
- National Centre for Labour, 1999.
- Srilata Swaminathan, “Female Foeticide: Facts and Figures.”
- INCLEN Survey 2000, “Indian Studies of Abuse in the Family Environment, 1998 – 2000,” A study conducted by IndiaSAFE and the Indian branch of the International Clinical Epidemiology Network (INCLEN).
- National Centre for Labour, 1999.
- Aruti Nayar, The Tribune, May 6, 2001, “Silent Genocide.”
- National Crime Records Bureau, 2007 statistics.
- “45 Million Daughters Missing: A Compendium on Research and Intervention on Female Foeticide and Infanticide in India.” Published by IFES and EKATRA, funded by USAID (The United States Agency for International Development).
- UNFPA Report, 1997, “India: Towards Population and Development Goals.”
- UNICEF India, Child Sex Ratio (www.unicef.org/india/CHILD-SEX-RATIOin.pdf).
- Valerie M. Hudson, Andrea M. den Boer, “Bare Branches: The Security Implications of Asia’s Surplus Male Population.”
- Sakshi, 1998, “Justice on Gender.”
- Rita Patel, Department of Maternal and Child Health, School of Public Health, “The Practice of Sex Selective Abortion in India: May You Be the Mother of a Hundred Sons.”
- Dr Meeta Singh, “Outcomes of the Dignity of the Girl Child Program” (Rajasthan University Women’s Association & IFES Initiative).
- Rajesh Sinha, Indian Express, May 10, 1998, “After 115 Years a Village Celebrates the Wedding of a Girl it Did Not Kill.”
- India Today, July 15, 2002, “Rural Women Start Successful Micro-Banking Scheme in Chattisgarh.”
- India Today, May 1, 2009, Amitabh Srivastava, “Grit and Honey.”
- Centre for Global Development, 2008, “Girls Count: A Global Investment and Action Agenda.”
- Times of India, April 10, 2009. Kiran Bedi was interviewed at the Launch of Laadli Week, a joint venture between Star Plus and Mahindra’s Nanhi Kali Project for educating the girl-child.
- The Lancet, January 2006, “Low Male-to-Female Sex Ratio of Children Born in India: National Survey of 1.1 Million Households.”
- Scott Baldauf, Christian Science Monitor, January 13, 2006, “India’s ‘Girl Deficit’ Deepest Among Educated.”
- UNICEF Report: “State of the World’s Children, 2007, Women and Children: The Double Dividend of Gender Equality.”
- Tim Sullivan, News Plus, April 17, 2008, “India Surges, But Shackles Of Sex-Selection Remain.”
- The Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act 1994, “Answers to Frequently Asked Questions, A Handbook For The Public.”
- BioEdge (BioEthics News from Around the World) May 2, 2007, “GE’s Ultrasound Machines and India’s Gendercide.”
- UNFPA Report: “Missing: Mapping the Adverse Child Sex Ratio in India.”
- Times of India, May 4, 2008, Kounteya Sinha, “Government Plans to Crack Down on Sex Determination Tests.”
- Wall Street Journal, Peter Wonacott, April 19, 2007, “India’s Skewed Sex Ratio Puts GE Sales in Spotlight.”
पुस्तक एवं लेखक परिचय
आइंस्टाइन, एल्बर्ट (Einstein, Albert) (879-1955): एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी (Germany) में पैदा हुए एक अमरीकन भौतिकशास्त्री थे। सन् 1921 में उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यद्यपि वे सबसे ज़्यादा रिलेटिविटी के सिद्धांतों के लिये जाने जाते हैं; उन्होंने 300 से भी ज़्यादा वैज्ञानिक कार्यों और 150 ग़ैर-वैज्ञानिक कार्यों को प्रकाशित किया। उनको विश्वास था कि विज्ञान की खोज आध्यात्मिक तजरबों की मदद से ही संभव हो सकती है। सन् 1999 में उनको टाइम मैग्ज़ीन (Time Magazine) द्वारा ‘शताब्दी के महापुरुष’ (Person of the Century) का नाम दिया गया। आइंस्टाइन की जीवनी लिखनेवाले डॉन हॉवर्ड (Don Howard) के शब्दों में, ‘विज्ञान से परिचित लोगों और आम जनता के विचारों में आइंस्टाइन एक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी (जीनियस) हैं।’
कबीर साहिब (Kabir Sahib) (1398-1518): संत कबीर का जन्म काशी (वाराणसी) में हुआ। कबीर साहिब कपड़े बुनकर अपना गुज़ारा करते थे। शब्द-धुन के अभ्यास का प्रचार करते हुए उन्होंने भारत का भ्रमण किया तथा हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के लोगों को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। कर्मकांडों और रीति रिवाजों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिये उनको पुजारी वर्ग के कड़े विरोध का लगातार सामना करना पड़ा। आज उनकी रचनाएँ, दोहे और शब्द पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं और बड़े प्रेम से गाए और सुने जाते हैं।
कवी, स्टीफ़न (Covey, Stephen R.) (1932-): सॉल्ट लेक सिटी, यूटा (Salt Lake City, Utah) में जन्मे डॉक्टर कवी ने द सैवन हैबिट्स ऑफ़ हाइली इफ़ैक्टिव पीपल (The Seven Habits of Highly Effective People) लिखी। उनके द्वारा लिखित अन्य किताबों में शामिल हैं—फ़र्स्ट थिंग्ज़ फ़र्स्ट (First Things First), प्रिंसिपल-सैंटर्ड लीडरशिप (Principle-Centered Leadership), द सैवन हैबिट्स ऑफ़ हाइली इफ़ैक्टिव फ़ैमिलीज़ (The Seven Habits Of Highly Effective Families), द एट्थ हैबिट (The 8th Habit) और द लीडर इन मी-हाऔ स्कूल्ज़ एण्ड पैरेन्ट्स अराउण्ड द वर्ल्ड आर इन्स्पाइरिंग ग्रेट्नैस, वन चाईल्ड ऐट अ टाईम (The Leader In Me - How Schools and Parents Around The World Are Inspiring Greatness, One Child at a Time)
कारलायल, टॉमस (Carlyle, Thomas) (1795-1881): कारलायल विक्टोरियन युग के स्कॅाटिश निबंधकार, इतिहासकार और शिक्षक थे। उन्होंने ऐडिनबर्ग ऐनसाइक्लोपिडिया (Edinburgh Encyclopaedia) के लिये लेख लिखे। वे विवादास्पद सामाजिक व्याख्याता बने। उनकी किताबों व लेखों ने समाज सुधारक जैसे—जॉन रस्किन (John Ruskin), चार्ल्स डिकन्स (Charles Dickens); जॉन बर्न्स (John Burns), टॉम मन (Tom Mann) और विलियम मॉरिस (William Morris) को प्रेरित किया।
क़ुरान शरीफ़ (Qur’an): क़ुरान शरीफ़ इस्लाम को माननेवालों का एक पवित्र धर्मग्रंथ है। यह अरबी भाषा में लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि सातवीं शताब्दी में अल्लाह ने इसे पैग़म्बर मुहम्मद साहिब पर नाज़िल किया। इसमें 114 अध्याय हैं जिनमें पवित्रता, नैतिकता, सामाजिकता, वैज्ञानिकता, रूहानियत आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है।
गुरु अर्जुन देव (Guru Arjun Dev) (1563-1606): गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक साहिब की गद्दी के पाँचवें गुरु थे। उन्होंने अत्यंत प्रयास करके गुरु साहिबान की वाणियाँ एकत्र कीं, उनका वर्गीकरण किया और उन्हें आदि ग्रन्थ में संकलित किया। गुरु अर्जुन देव ने भारतीय उपमहाद्वीप के कई अन्य महात्माओं की वाणियाँ भी इसमें सम्मिलित कीं जिनकी शिक्षा एक परमात्मा में आस्था, शब्द साधना का मार्ग, सामाजिक समानता और सत्य की खोज पर बल देती हैं।
गुरु नानक देव (Guru Nanak Dev) (1469-1539): गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के निकट तलवंडी नामक स्थान (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ। उन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भ्रमण करने और शब्द या नाम के अभ्यास की शिक्षा का प्रचार करने में गुज़ारा। इस भ्रमण को ‘उदासियाँ’ कहा जाता है। उन्होंने इन उदासियों में शब्द या नाम के अभ्यास की शिक्षा का प्रचार किया। वे दस गुरुओं की पीढ़ी के पहले गुरु थे जिनकी वाणी आदि ग्रन्थ में दर्ज है। आदि ग्रन्थ सिक्खों का पवित्र धर्मग्रंथ है। गुरु नानक देव ने लोगों को उनके रूढ़िवादी अंधविश्वासों से मुक्त करने का प्रयास किया और समझाया कि बाहरी पूजा और कर्मकांड सत्य की पहचान में सहायता नहीं करते।
गुरु रविदास (Guru Ravidas): संत रविदास काशी के रहनेवाले थे। वे राजस्थान के अलावा भारत के अन्य भागों में भी जाने जाते थे और स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे कबीर साहिब के समकालीन थे। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। वे स्वयं जूते गाँठकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उनकी रूहानी शिक्षा का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे मीराबाई एवं राजा पीपा के आध्यात्मिक मार्गदर्शक रहे। उनकी कुछ रचनाएँ आदि ग्रन्थ में सम्मिलित हैं।
गूरमौं, रेमि द (Gourmont, Remy de) (1858-1915): द गूरमौं, फ़्रांसिसी लेखक और कवि थे। उनकी रचनाएँ विश्वभर में प्रसिद्ध थीं। उनको टी.एस.एलियट (T.S. Eliot) और ऐज़रा पाउंड (Ezra Pound) द्वारा सराहा गया। वे कोटंटिन (Cotentin) के प्रकाशक परिवार से थे। द गूरमौं, अगस्त-मॅरी द गूरमौं (Auguste-Marie de Gourmont) और मैथिल्ड द मौंट्फ़र्ट (Mathilde de Montfort) के पुत्र थे। उन्होंने कैन (Caen) से वकालत की थी। उसके बाद वे पैरिस चले गए और वहाँ बिबलियोथैक नेशनल (Bibliotheque Nationale) में नौकरी की।
गैटे (Goethe) (1749-1832): गैटे एक जर्मन लेखक थे। जॉर्ज एलियट (George Eliot) के शब्दों में आप ‘जर्मनीज़ ग्रेटेस्ट मैन ऑफ़ लैट्र्स’ (Germany’s Greatest Man of Letters) थे। गैटे ने अपने जीवन का आधा समय कविताएँ, नाटक, साहित्य, धर्मशास्त्र, दर्शन, विज्ञान और मानवता के बारे में लिखने में लगाया। दो भागों में लिखे गये उनके नाटक फ़ॅास्ट (Faust) की प्रशंसा विश्व भर में हुई। उनके लेखन का प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा और उनके योगदान के कारण ही संगीत, नाटक, कविताओं में लोगों की रुचि बढ़ी। पश्चिमी सभ्यता में वे जर्मन भाषा के सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं।
टैगोर, रवीन्द्रनाथ (Tagore, Rabindranath) (1861-1941): रवीन्द्रनाथ बंगाल के कवि, चित्रकार, नाटककार, उपन्यासकार हुए हैं, जिनका कार्य विश्वभर में सराहनीय है। सन् 1913 में एशिया में नोबल पुरस्कार जीतनेवाले वे पहले व्यक्ति थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कविताओं का प्रथम संग्रह भानूशिंघो (सन-लायन) के उपनाम से प्रकाशित किया। 1877 में उन्होंने अपनी आरंभिक कहानियाँ और नाटक लिखे। बाद में टैगोर ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग दिया। टैगोर के जीवन की मुख्य उपलब्धि उनके काव्य तथा उनके द्वारा स्थापित विश्वभारती विश्वविद्यालय के रूप में स्थायी है। टैगोर ने उपन्यास, कहानियाँ, गीत, नृत्य-नाट्य के अतिरिक्त राजनीति तथा अन्य विषयों पर कई निबंध लिखे। उनके जाने-माने कार्यों में गीतांजलि, गोरा और घरे बाहरे बहुत प्रसिद्ध हैं।
ताओ त्से चिंग (Tao Tse Ching): ताओ मार्ग और उसकी शक्ति संबंधी पुस्तक ताओ त्से चिंग (The Book of the Way and Its Power) के मूल के बारे में जानना कठिन है। यह पुस्तक ताओ के मार्ग से संबंधित मूल ताओवादी सिद्धांतों को गद्य रूप में प्रतिपादित करती है। ये उच्च कोटि के वे सिद्धांत हैं जिनका पालन नम्रता और निष्काम कार्यों द्वारा किया जाता है। ताओ त्से चिंग शायद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में तैयार की गई थी, पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुस्तक चीन की मौखिक परंपरा पर आधारित है जो लिखे जाने के भी बहुत समय पूर्व से चली आ रही थी। यद्यपि इसके लेखन का श्रेय ‘लाओ ज़ू’ (Lao-Tzu) या ‘लाओ त्से’ (Lao-Tse) को दिया जाता है, पर आधुनिक विद्वानों को संदेह है कि इस नाम का कोई व्यक्ति वास्तव में हुआ भी था या नहीं। संभव है कि ‘लाओ ज़ू’ जिसका अर्थ ‘प्राचीन दार्शनिक’ अथवा ‘प्राचीन दर्शन’ है, इसका संबंध पुस्तक में दिये भिन्न-भिन्न विचारों और लेखों के प्राचीन मूल से है।
धम्मपद (Dhammapada) (सत्य का मार्ग): धम्मपद में दी गई कविताओं के रचनाकार का पता नहीं है पर ऐसा विश्वास है कि ये महात्मा बुद्ध की शिक्षा है। यह पुस्तक अपने मूल पाठ सहित महान् बौद्ध सम्राट अशोक के समय, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से चली आ रही है।
नायडू, सरोजिनी (Naidu, Sarojini) (1879-1949): सरोजिनी नायडू एक क्रांतिकारी और महान् कवयित्री थीं। सरोजिनी नायडू को हम भारत की कोयल (Nightingale of India) के नाम से जानते हैं। वे भारत की पहली महिला थीं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक सक्रिय महिला थीं। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ नमक बनाओ आंदोलन और डांडी यात्रा में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी के गिरफ़्तार होने के बाद, उन्होंने धरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता संग्राम में उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा।
नेहरू, जवाहरलाल (Nehru, Jawaharlal) (1889-1964): जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े राजनैतिक नेता, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस की जानी-मानी हस्ती थे। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो काफ़ी लंबे समय तक इसी पद पर बने रहे (1947-1964)। प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते महिला सुधार एवं समानता के अधिकारों के लिये वे संसद में आवाज़ उठाते रहे। औरतों को शक्तिशाली बनाने के लिये उन्होंने विवाह के लिये न्यूनतम आयु को 12 साल से बढ़ाकर 15 साल करवाया। उन्होंने तलाक़ और माता-पिता की जायदाद में लड़की को हिस्सा लेने का अधिकार देने की घोषणा भी की। भारतीय परंपराएँ एवं स्वतंत्र भारत के ढाँचे को नये रूप में परिवर्तित करने पर उनको ‘आधुनिक भारत का निर्माता’ कहा गया।
तय्हार द शारदैं, पियेर (Teilherd de Chardin, Pierre) (1881-1955): तय्हार फ़्रांस के दार्शनिक और जैज़्यूइट पादरी (Jesuit preist) थे। वे शिलालेख और भूविज्ञान में निपुण थे। इन्होंने ‘पीकिंग मैन’ (Peking Man) की खोज में भाग लिया। इन्होंने ओमेगा पौइंट (Omega Point) की विचारधारा का आधार रखा और व्लाडीमीर वैरनाडस्की (Vladimir Vernadsky) की नूस्फ़ीयर (Noosphere) की धारणा को आगे बढ़ाया। तय्हार की प्रमुख किताब द फ़िनौमिनन ऑफ़ मैन (The Phenomenon of Man) ने प्रकृति का ज्ञान दिया। उन्होंने बाइबल की पुस्तक जैनेसिस (Genesis) में उत्पत्ति के विचार का विरोध किया और पुराने विचारों को एक नया अलग-सा रूप दिया। रोमन क्यूरिया (Roman Curia) के कुछ अफ़सर इससे ख़ुश नहीं थे, क्योंकि यह सेंट ऑगस्टीन (Saint Augustine) द्वारा दिये गए 'ओरिजनल सिन' (Original Sin) के सिद्धांत की महत्ता को कम करता है। तय्हार के दृष्टिकोण का चर्च के अधिकारियों ने विरोध किया और रोमन अधिकारियों ने उनके लेखों को उनके जीवनकाल में प्रकाशित करने से रोक दिया।
फ़िलोकैलिया (Philokalia): फ़िलोकैलिया एक ऐसी रचना है जो चौथी और पंद्रहवीं शताब्दी के बीच आध्यात्मिक संतों द्वारा लिखी गई। यह ईसाई परंपरा पर आधारित थी।
फ़्रैंकल, विक्टर (Frankl, Viktor) (1905-1997): विक्टर फ़्रैंकल ऑस्ट्रिया के स्नायुतंत्र के विशेषज्ञ (neurologist) और मनोचिकित्सक (psychiatrist) होने के साथ एक होलोकॉस्ट सरवाइवर (Holocaust Survivor) भी थे। फ़्रैंकल ने लोगोथैरपी (logotherapy) का निर्माण किया जो एक्ज़िस्टैनशियल एनैलिसिस (Existential Analysis) ‘द थर्ड वीयनीज़ स्कूल ऑफ़ साइकोथेरेपी’ (The Third Viennese School of Psychotherapy) के जैसा है। उनकी सबसे लोकप्रिय पुस्तक मैन्ज़ सर्च फ़ॉर मीनिंग (Man’s Search for Meaning) उनके जेल के अनुभवों का चित्रण करती है और हर तरह की जीवन की स्थिति में मतलब ढूँढ़ने का वर्णन करती है। हर प्रकार की बुरी परिस्थिति में भी जीने का तरीक़ा बताती है। फ़्रैंकल का सिग्मंड फ़्रॉयड (Sigmund Freud) और ऐलफ़्रेड ऐडलर (Alfred Adler) के साथ संबंध था। फ़्रैंकल एक्ज़िस्टैनशियल थेरेपी (Existential Therapy) के लिए प्रसिद्ध हुए।
बाइबल (Bible): बाइबल या होली बाइबल (Holy Bible) यहूदियों और ईसाइयों का पवित्र धर्मग्रंथ है। यहूदी बाइबल हिब्रू भाषा में लिखी है। यह टोरा (Torah), प्रॉफ़िट्स (Prophets) और लेखों (Writings) में विभाजित है। यह ग्रंथ रचना के आरंभ से मानवता का इतिहास, धर्माध्यक्षों और पूर्व के इज़राइलियों का जीवन तथा उनके पैग़ंबरों और महापुरुषों की शिक्षा को दर्शाता है। यह विश्व की उत्पत्ति का इतिहास बताता है, पैट्रिआक्र्स (Patriarchs) की जीवनी और प्राचीन इज़राइल और उनके संतों की वाणी (शिक्षा) का ज्ञान देता है। ईसाइयों की बाइबल ओल्ड टैस्टामैंट (Old Testament) जिसमें जुइश बाइबल की किताबें और न्यू टैस्टामैंट (New Testament), जिसमें ईसा मसीह और उनके शिष्यों की जीवनी के बारे में लिखा गया है, उनका संग्रह है। इसमें ईसा मसीह के चार उपदेशक (मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन) और उनकी साहित्यिक रचना (जोकि शिष्यों की तरफ़ से पत्र हैं), द एक्ट्स ऑफ़ द अपॉसल्ज़ (The Acts of The Apostles) और ईश्वरीय भाषा जो ऐपोकैलिप्स (Apocalypse) के नाम से भी जानी जाती है, सम्मिलित हैं।
बेदी, किरन (Bedi, Kiran) (1949-): किरन बेदी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो भारतीय पुलिस ऑफ़िसर के रूप में रिटायर हुईं। वे पहली भारतीय महिला हैं जो 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुईं। वे बहुत-से चुनौतीपूर्ण कार्यों की सफल अधिकारी रहीं—जैसे कि नई दिल्ली की ट्रैफ़िक कमिश्नर, मिज़ोरम के अशांत क्षेत्रों में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस, नारकॉटिक कंट्रोल ब्यूरो की डायरेक्टर जनरल और तिहाड़ जेल की इंस्पेक्टर जनरल, जो विश्व की बड़ी जेलों में से एक मानी जाती है। जेल व्यवस्था को सुधारने में इनका विशेष योगदान रहा जिसके लिये इनको प्रतिष्ठित रेमन मैगसेसे अवॉर्ड (Ramon Magsaysay Award) से सम्मानित किया गया। बाद में वे डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस रिसर्च ऐण्ड डिवलपमेंट के रूप में नियुक्त हुईं, जहाँ से उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (इच्छानुसार रिटायरमैंट) ले ली। उन्होंने भारत में दो एन.जी.ओ. की भी स्थापना की: पहली, नवज्योति जो पुलिस व्यवस्था के सुधार के लिये शोध कार्य करती है और दूसरी, इण्डिया विज़न फ़ाउंडेशन (India Vision Foundation) के नाम से जानी जाती है। यह जेल के नियमों को सुधारने, नशा मुक्ति तथा बाल-कल्याण के लिये काम करती है।
बोनापार्ट, नपोलियन (Bonaparte, Napoleon) (1769-1821): नपोलियन बोनापार्ट सम्राट नपोलियन 1 के नाम से जाने गए। वे फ़्रांस के सैनिक और राजनैतिक नेता थे और उनके कार्यों ने उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपियन राजनीति को आकार दिया। उनका जन्म कोरसिका (Corsica) में हुआ था और वे फ़्रांस महाद्वीप में तोपची नियुक्त किये गए। बोनापार्ट ने सम्राट बनने तक अपनी शक्ति को बढ़ाया। उन्होंने फ़्रांस की सेना को यूरोपियन बलों के विरुद्ध किया और लगातार जीत हासिल करके यूरोप महाद्वीप पर शासन किया। वे सन् 1815 में ‘वॉटरलू’ (Waterloo) नामक स्थान पर संगठित बलों के साथ हुए युद्ध में हार गए। वे नपोलियनिक कोड (Napoleonic Code) के लिये याद किये जाते हैं जिसने पश्चिमी यूरोप के लिये शासन संबंधी और न्यायालय संबंधी अधिकारों की नींव रखी।
ब्रिटेन, वेरा (Brittain, Vera Mary) (1893-1970): वेरा मेरी एक शांतिप्रिय महिला होने के साथ अंग्रेज़ी लेखिका भी थीं जो औरतों के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाती थीं। उनको अपनी पुस्तक टैस्टामैंट ऑफ़ यूथ (Testament of Youth) के लिये याद किया जाता है जो उन्होंने 1933 में लिखी थी। पुस्तक में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवों का वर्णन किया और शांति का प्रचार किया।
बुल्लेशाह (Bulleh Shah) (1680-1758): साईं बुल्लेशाह का जन्म एक उच्च श्रेणी के सैयद परिवार में हुआ। उनका पालन-पोषण लाहौर के पास स्थित कसूर नामक स्थान में हुआ। जब वे लाहौर के रहस्यवादी संत इनायत शाह (जो एक साधारण से माली थे) के शिष्य बने तो उनको अपने समुदाय की नाराज़गी सहनी पड़ी। प्रभुभक्ति से ओतप्रोत उनकी कविताएँ और काफ़ियाँ आज भी भारत और पाकिस्तान में प्रेमपूर्वक पढ़ी और गायी जाती हैं।
भगवान् महावीर (Bhagwan Mahavir) (599-527 ईसा पूर्व): राजा वर्धमान को अकसर महावीर के नाम से जाना जाता है। भगवान् महावीर की शिक्षा आज भी जैन धर्म की मुख्य शिक्षा मानी जाती है। जैन धर्म में वे चौबीसवें और आख़िरी तीर्थंकर माने जाते हैं। उन्होंने भारत में आध्यात्मिक स्वतंत्रता की शिक्षा देने में अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपनी शिक्षा का पूरे भारत में प्रचार किया जिससे इस प्राचीन धर्म को जैन दर्शन के रूप में मान्यता मिली।
मदर टेरेसा (Mother Teresa) (1910-1997): मदर टेरेसा एलबैनियन रोमन कैथोलिक चर्च (Albanian Roman Catholic Church) की सेविका थीं। इन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त थी। एग्नेस गौनज़हा बोजाक्सहियू (Agnes Gonxha Bojaxhiu) मदर टेरेसा (Mother Teresa) के नाम से जानी जाती हैं। सन् 1950 में भारत में स्थित कोलकता में इन्होंने मिश्नरीज़ ऑफ़ चैरिटी (Missionaries of Charity) की स्थापना की। इन्होंने 45 सालों तक ग़रीब, बीमार, अनाथ लोगों की सेवा की और साथ में मिश्नरीज़ ऑफ़ चैरिटी को बढ़ावा दिया। बाद में इन्होंने पूरे विश्व को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। सन् 1979 में इनको नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1980 में मानवता के प्रति कार्य के लिए भारतरत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
मरीचाइल्ड, डाऐन (Mariechild, Diane): डाऐन मरीचाइल्ड मदर विट (Mother Wit) और इनर डाँस (Inner Dance) पुस्तकों की लेखिका हैं। अनेक कार्यशालाओं का आयोजन करके वे महिलाओं और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये व्याख्यान देती हैं।
महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) (1869-1948): महात्मा गांधी भारत के प्रमुख समाज सेवक होने के साथ-साथ अध्यात्म और स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। उन्होंने सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जो अहिंसा के आधार पर थी और जिसके ज़रिये भारत को स्वतंत्रता मिली। उन्होंने सामाजिक अधिकार और स्वतंत्रता आंदोलनों की विश्व भर में प्रेरणा दी। वे विश्व भर में महात्मा गांधी के नाम से लोकप्रिय हैं। महात्मा गांधी को आधिकारिक तौर से भारत का ‘राष्ट्रपिता’ घोषित किया गया। उनका जन्मदिन, दो अक्तूबर, भारत में राष्ट्रीय अवकाश और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस (International Day of Non-Violence) के रूप में मनाया जाता है।
महाराज चरन सिंह (Maharaj Charan Singh) (1916-1990): महाराज चरन सिंह जी का जन्म मोगा (पंजाब) में हुआ था। वे राधास्वामी सत्संग ब्यास के संत-सतगुरु हुज़ूर महाराज सावन सिंह जी के शिष्य थे। पेशे से आप वकील थे। सन् 1951 में महाराज जगत सिंह जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। महाराज जी ने अगले चार दशक तक समस्त भारत और विश्व का भ्रमण किया, स्थान-स्थान पर प्रवचन किये और बारह लाख से अधिक जीवों को नामदान बख़्शा। उन्होंने जीवों को जाति‑पाँति, क़ौम और मज़हब से ऊपर उठकर शब्द या नाम की कमाई करने पर बल दिया। उनकी शिक्षा कई पुस्तकों में दर्ज है जिनमें उनके लेख, वार्तालाप तथा पत्र शामिल हैं। सन् 1990 में नश्वर शरीर त्यागने से पूर्व उन्होंने बाबा गुरिन्दर सिंह ढिल्लों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।
महाराज जगत सिंह (Maharaj Jagat Singh) (1884-1951): महाराज जगत सिंह जी का जन्म जालन्धर ज़िले के नुस्सी गाँव में हुआ और छब्बीस वर्ष की आयु में उन्हें महाराज सावन सिंह जी से नामदान की बख़्शिश हुई। सन 1943 में पंजाब एग्रीकलचरल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन ब्यास में रहकर सतगुरु की सेवा में बिताया। सन् 1948 में महाराज सावन सिंह जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनके सत्संगों तथा पत्रों से लिये गए अंशों का संग्रह उनकी आत्म-ज्ञान नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। यह पुस्तक उनके देह त्यागने के बाद प्रकाशित की गई।
मौलाना रूम (Maulana Rum) (1207-1273): मौलाना रूम के नाम से प्रसिद्ध जलालुद्दीन रूमी फ़ारस (Persia) के बल्ख़ (Balkh) शहर के रहनेवाले थे। बाद में वे तुर्की (Turkey) के कोन्या (Konya) शहर में चले गए और एक धार्मिक शिक्षक बन गए। वहाँ उनकी मुलाक़ात सूफ़ी संत शम्स तब्रेज़ से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। मौलाना रूम ने मसनवी और दीवाने-शम्स तब्रेज़ लिखे हैं। इन ग्रंथों ने इन दोनों महान् सूफ़ी रहस्यवादी संत-कवियों को पूर्व और पश्चिम दोनों क्षेत्रों में लोकप्रिय बना दिया है।
वाइस, डॉ. ब्रायन एल. (Weiss, Brian L.): डॉक्टर वाइस अमरीका में एक मनोरोग चिकित्सक हैं। इन्होंने येल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ़ मेडिसन (Yale University School of Medicine) से शिक्षा ग्रहण की। आजकल वे मिआमी में माउंट साइनाइ मेडिकल सेंटर (Mount Sinai Medical Center) में मनोरोग चिकित्सा विभाग के चेयरमैन अमेरिटस (Chairman Emeritus) हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ़ मिआमी, स्कूल ऑफ़ मेडिसन (University of Miami School of Medicine) के मनोरोग चिकित्सा विभाग के क्लिनिकल एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं। उन्होंने पुनर्जन्म के विषय पर सात किताबें लिखीं, जिनमें से ओन्ली लव इज़ रिअल (Only Love is Real) सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई।
वॉशिंग्टन, जॉर्ज (Washington George) (1732-1799): जॉर्ज वॉशिंग्टन एक सर्वेक्षक, किसान और सिपाही थे, जो अमरीकन आंदोलन के दौरान महाद्वीपीय सेना के प्रमुख अधिकारी बने और 1789 से 1797 तक अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति बने। वे अपने देश के ‘राष्ट्रपिता’ माने जाते हैं, क्योंकि अमरीका को प्रारंभिक समय में संगठित करने और नेतृत्व देने के लिये उनका प्रमुख योगदान रहा। वे फ़िलेडेलफ़िया सम्मेलन (Philadelphia Convention) के अध्यक्ष बने जिसने 1787 में अमरीका के संविधान की रचना की। विचारकों व विद्वानों ने जॉर्ज वाशिंग्टन को अमरीका का एक महान् राष्ट्रपति माना है।
विलियम्सन, मेरीएन (Williamson, Marianne) (1952-): मेरीएन विलियम्सन अध्यात्मवाद की कार्यकर्ता, अमरीकन लेखिका और प्राध्यापिका हैं। इन्होंने शांति संगठन (Peace Alliance) बनाया और शासन की तरफ़ से भी युनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ पीस (United States Department of Peace) संगठन की स्थापना कराई और उनकी नियमावली बनाने में पूरा सहयोग दिया। इनकी 9 किताबें प्रकाशित हुई हैं। उनमें से इमैजिन वॉट अमेरिका कुड बी इन द 21 सैंचुरी (Imagine What America Could be in the 21st. Century), विज़न्ज ऑफ़ अ बैटर फ़्यूचर फ़्रॉम लीडिंग अमेरीकन थिंकर्ज़ (Visions of a Better Future from Leading American Thinkers), हीलिंग द सोल ऑफ़ अमेरिका: रिक्लेमिंग अवर वॉएसिज़ ऐज़ स्पिरिचुअल सिटीज़न्ज़ (Healing The Soul of America: Reclaiming Our Voices as Spiritual Citizens) और अ वुमन्ज़ वर्थ (A Woman’s Worth) मुख्य हैं।
सेन, डॉ. अमर्त्य (Sen, Amartya): डॉ. अमर्त्य सेन का जन्म 1933 में पश्चिमी बंगाल के शांति निकेतन में हुआ। वे अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कल्याणकारी आर्थिक सुधारों में योगदान दिया। उन्होंने अकाल, ग़रीबी और असमानता की समस्या को सुधारने तथा मानव-विकास के सिद्धांत में बहुत बड़ा योगदान दिया। सन् 1998 में अर्थशास्त्र में उनको नोबल पुरस्कार मिला और 1999 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारतरत्न मिला। 1998 से 2004 तक वे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के टिर्निटी कॉलेज में अध्यापक रहे और वे सबसे पहले एशियन हैं जो ऑक्सफ़ोर्ड कॉलेज के अध्यक्ष बने। आजकल वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र व दर्शन शास्त्र के प्रोफ़ेसर हैं। उनको विश्वभर के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से लगभग 80 डॉक्टरेट डिग्रियाँ प्राप्त हैं।
हर्बर्ट, जॉर्ज (Herbert, George) (1593-1633): जॉर्ज हर्बर्ट एक अच्छे वैल्श (Welsh) कवि, वक्ता और महात्मा थे। उनका जन्म एक कलाप्रेमी अमीर परिवार में हुआ था। वे इंग्लैंड के चर्च के पवित्र कार्यों की ज़िम्मेदारी लेने से पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और संसद में अच्छे पद पर थे। उन्होंने जीवन भर धार्मिक कविताएँ लिखीं, जिनमें उन्होंने शुद्ध भाषा का प्रयोग किया और छंद रूप में रचना की जो अध्यात्म विद्या के अनुसार सराहनीय थीं। वे कवि के रूप मे याद किये जाते हैं और उनकी कविताएँ कम, माई वे, माई ट्रूथ, माई लाइफ़ (Come, My Way, My Truth, My Life) काफ़ी प्रचलित हैं।
हज़रत सुलतान बाहू (Bahu, Hazrat Sultan) (1629-1691): सैयद अब्दुल रहमान क़ादिरी के शिष्य हज़रत सुलतान बाहू हिंद महाद्वीप के उच्च कोटि के सूफ़ी संतों में से एक थे। यद्यपि उन्होंने औपचारिक तौर पर शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी यह कहा जाता है कि उनकी फ़ारसी और अरबी में सौ से भी अधिक रचनाएँ हैं। उनके पंजाबी भाषा के बैत आज भी सजीव हैं और पंजाब के लोगों में अत्यंत लोकप्रिय हैं।
संपर्क संबंधी जानकारी और अन्य सूचना
भारत में मुख्यालय
सेक्रेटरी
राधास्वामी सत्संग ब्यास
डेरा बाबा जैमल सिंह
ज़िला अमृतसर
ब्यास, पंजाब 143 204, भारत
अन्य सभी देशों में
अन्य सभी देशों में संपर्क संबंधी जानकारी और राधास्वामी सत्संग ब्यास की शिक्षा और गतिविधियों के बारे में सूचना हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है:
www.rssb.org
सत्संग सेंटर
अन्य सभी देशों के सत्संग सेंटर और कार्यक्रम का विवरण हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है:
satsanginfo.rssb.org
ऑनलाइन बुक सेल
RSSB की पुस्तकों को ऑनलाइन ऑर्डर करने की जानकारी हमारी सेल वेबसाइट पर उपलब्ध है:
www.scienceofthesoul.org (विदेशों में सेल के लिए)
www.rssbindiabooks.in (भारत में सेल के लिए)
यह पुस्तक, राधास्वामी सत्संग ब्यास, रजिस्टर्ड चैरिटेबल सोसाइटी (www.RSSB.org), की संगत द्वारा तैयार की गई है। यह सोसाइटी पारमार्थिक ज्ञान और मूल्यों के प्रचार में समर्पित है।