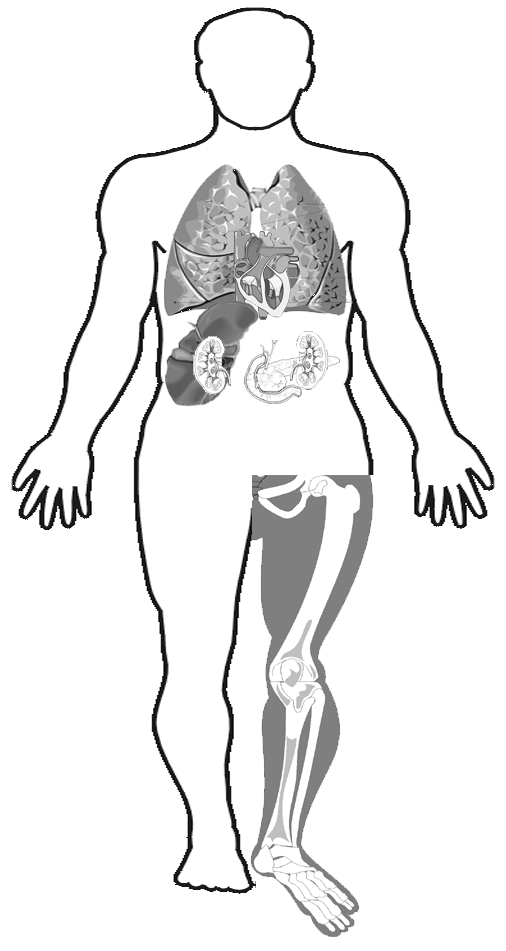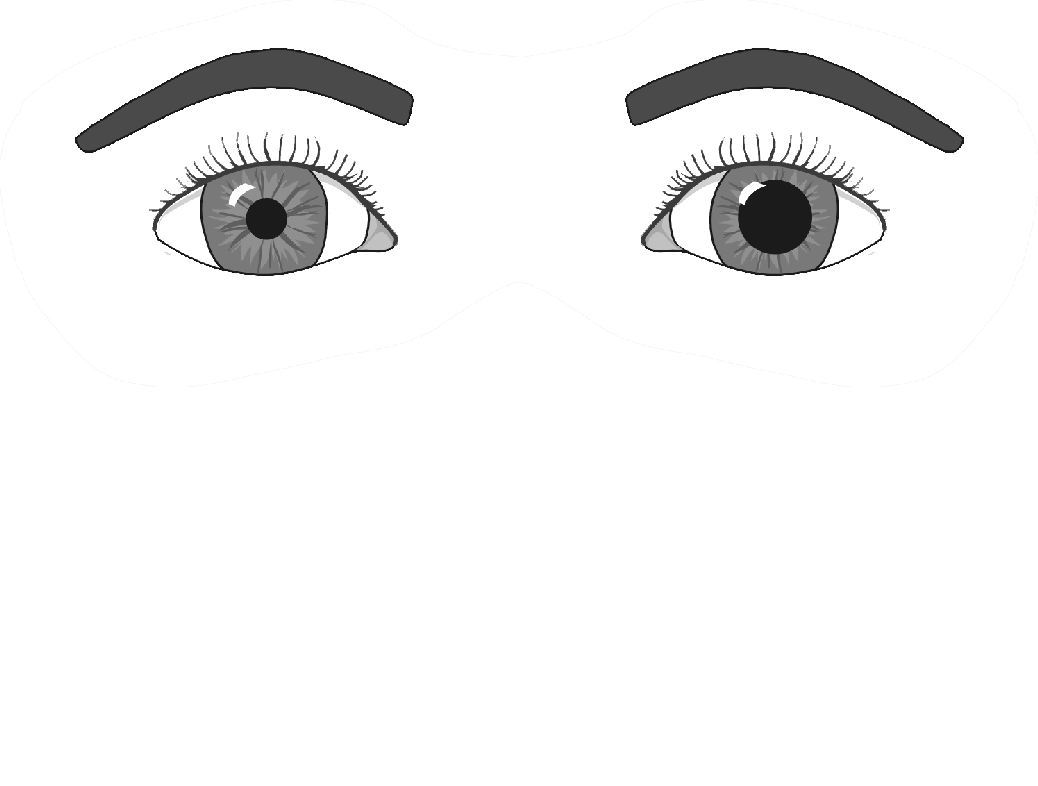स्वास्थ्य की देखभाल
कुछ बुनियादी तथ्य
स्वास्थ्य सुरक्षा
दाँतों की देखभाल
माता और शिशु का स्वास्थ्य
स्वास्थ्य और सफ़ाई
ऐंटीबायोटिक्स के बिना स्वस्थ होना
कैंसर की जल्द पहचान
औरतों के स्वास्थ्य की देखभाल
आँतों का कैंसर
पुरुषों के स्वास्थ्य की देखभाल—प्रोस्टेट कैंसर
कुछ आम बीमारियाँ
दान
रक्त—जीवन का अमृत
आम पूछे जानेवाले प्रश्न
नेत्रदान
अँधेरे से उजाले की ओर
अंगदान: जीवन का एक अमूल्य तोहफ़ा
संपर्क संबंधी जानकारी और अन्य सूचना
प्रकाशक:
जे. सी. सेठी, सेक्रेटरी
राधास्वामी सत्संग ब्यास
डेरा बाबा जैमल सिंह
पंजाब 143 204
© 2012 राधास्वामी सत्संग ब्यास
सर्वाधिकार सुरक्षित
पहला संस्करण 2012
इस पुस्तक के किसी भी भाग की मूल रूप में या स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करके प्रकाशक की अनुमति के बिना प्रतिलिपि बनाई जा सकती है, बशर्ते कि वह प्रतिलिपि मुफ़्त अथवा बिना आर्थिक लाभ के बाँटी जाए।
व्यापारिक उद्देश्य से प्रतिलिपि बनानी हो तो पहले प्रकाशक से अनुमति लेना अनिवार्य है। किसी भी पुस्तक/पुस्तिका/लेख/पेंफ़लेट में अगर इस पुस्तक में से किसी प्रसंग या विषय का प्रयोगकिया जाए , तो उसकी एक प्रति प्रकाशक को भेज दी जाए। हम आपके आभारी होंगे।
यह पुस्तक केवल आपको जानकारी देने के लिए है, डॉक्टर की राय के स्थान पर प्रयोग के लिए नहीं। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह अवश्य ली जाए।
Published by :
J. C. Sethi, Secretary
Radha Soami Satsang Beas
Dera Baba Jaimal Singh
Punjab 143 204
© 2012 Radha Soami Satsang Beas
All rights reserved First edition 2012
ISBN
पहला संस्करण 2012
आँखों की देखभाल
आँखें इस दुनिया को देखने का ज़रिया हैं। ये क़ुदरत की अमूल्य देन हैं। हम एक अंधे इनसान की हालत का अंदाज़ा तभी लगा सकते हैं जब हम आँखें बंद करके कुछ समय बिताएँ।
हम जीवन भर इन आँखों के द्वारा ही देख पाते हैं, इसलिए हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। आँखों की तकलीफ़ जीवन में कभी भी हो सकती है। आँखों की कई बीमारियाँ तो बच्चे को माता के गर्भ में ही हो जाती हैं। कुछ बीमारियाँ जन्म के समय हो जाती हैं, तो कई बचपन में स्कूल जाने से पहले या स्कूल जाने की उम्र के दौरान होती हैं। जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापे में भी आँखों की कई तरह की तकलीफ़ें हो जाती हैं।
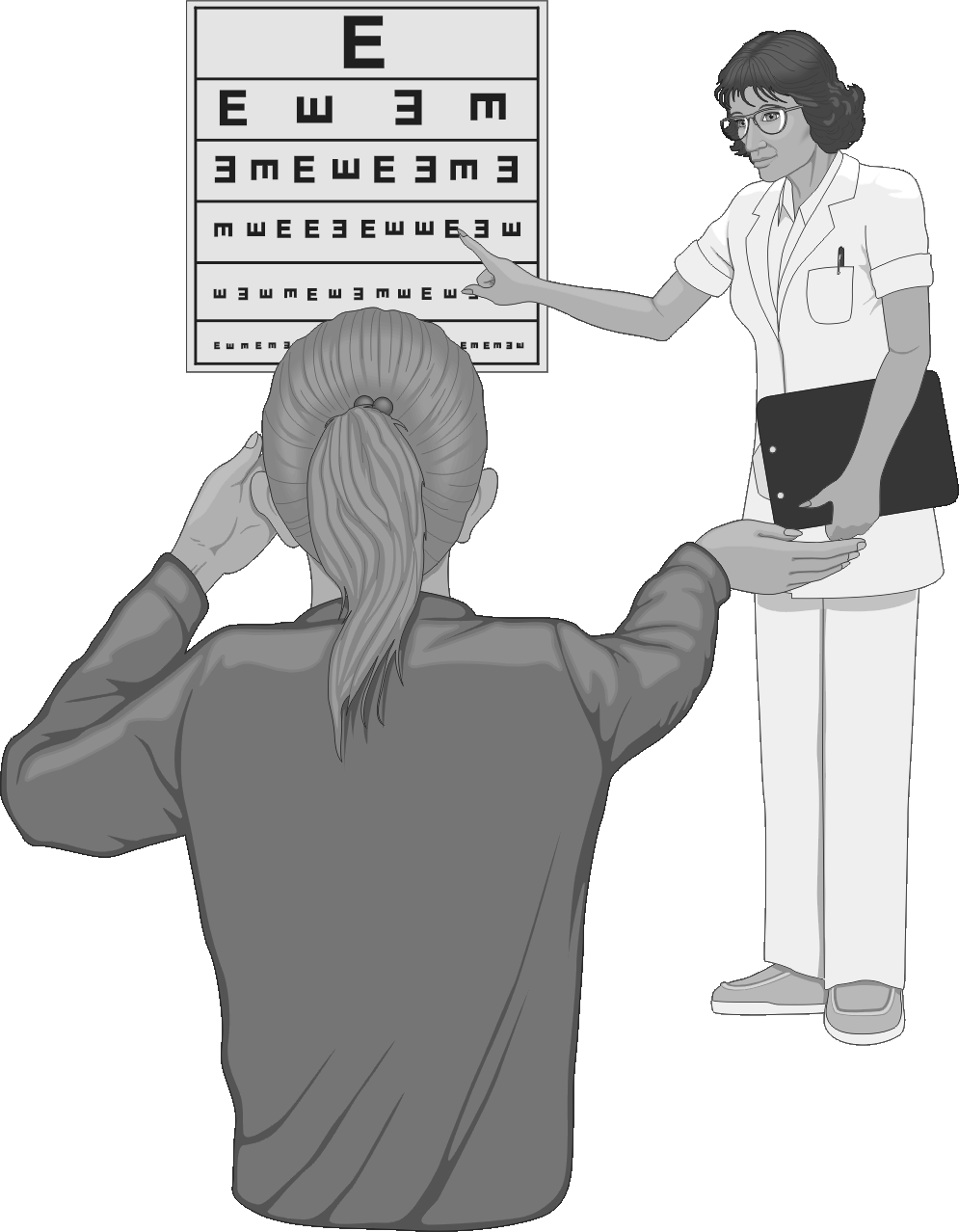 सबसे महत्त्वपूर्ण और याद रखनेवाली बात यह है कि आँखों की अधिकतर बीमारियों की पहचान और इलाज यदि समय पर न करवाया जाए, तो इनसान अंधा हो सकता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अंधेपन की ओर ले जानेवाली बहुत‑सी बीमारियाँ रोकी जा सकती हैं। किसी बीमारी की रोकथाम कर लेना, उसके इलाज करवाने की अपेक्षा ज़्यादा फ़ायदेमंद, आसान, सस्ता और सुविधाजनक है।
सबसे महत्त्वपूर्ण और याद रखनेवाली बात यह है कि आँखों की अधिकतर बीमारियों की पहचान और इलाज यदि समय पर न करवाया जाए, तो इनसान अंधा हो सकता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अंधेपन की ओर ले जानेवाली बहुत‑सी बीमारियाँ रोकी जा सकती हैं। किसी बीमारी की रोकथाम कर लेना, उसके इलाज करवाने की अपेक्षा ज़्यादा फ़ायदेमंद, आसान, सस्ता और सुविधाजनक है।
आइए! अब देखें कि आँखों की देखभाल माता के गर्भ से लेकर जीवन के अंत तक और उसके बाद भी (नेत्रदान के लिए) कैसे करनी है।
गर्भावस्था के दौरान बच्चे की आँखों की देखभालगर्भावस्था के दौरान उचित आहार न लेने से, ख़ून की कमी से, स्टीरॉयड‑युक्त दवाइयों का सेवन करने से, पेट का एक्स‑रे करवाने से या रूबेला (खसरा) का संक्रमण होने से, माता के पेट में पल रहे बच्चे की आँखों को नुकसान पहुँच सकता है। जन्मजात सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया और रेटिनोपैथी के कारण भी अंधापन हो सकता है। ऐसी समस्याओं की रोकथाम के लिए ये उपाय करने चाहिएँ:
- किशोरावस्था से पहले लड़कियों को रूबेला (एम.एम.आर.) का टीका लगवाएँ।
- पेट के अनावश्यक एक्स‑रे न करवाएँ और स्टीरॉयड‑युक्त दवाइयों का सेवन न करें।
- संतुलित आहार लें।
- गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में अनावश्यक दवाइयों का सेवन न करें।
 शिशु के चेहरे, ख़ास तौर पर आँखों के खुलने से पहले, उसके आसपास की जगह की सफ़ाई किसी साफ़ और कीटाणु रहित कपड़े से करें। इसके बाद शिशु की आँखों में ऐंटीबायोटिक (Antibiotic) दवाई की बूँदें डालें। यदि पहले महीने में बच्चे की आँखों से पानी या कोई अन्य स्राव होता है, तो तुरंत आँखों के डॉक्टर से मिलें। यह आई फ़्लू (conjunctivitis) हो सकता है या निम्नलिखित गंभीर बीमारियों में से भी कोई एक हो सकती है:
शिशु के चेहरे, ख़ास तौर पर आँखों के खुलने से पहले, उसके आसपास की जगह की सफ़ाई किसी साफ़ और कीटाणु रहित कपड़े से करें। इसके बाद शिशु की आँखों में ऐंटीबायोटिक (Antibiotic) दवाई की बूँदें डालें। यदि पहले महीने में बच्चे की आँखों से पानी या कोई अन्य स्राव होता है, तो तुरंत आँखों के डॉक्टर से मिलें। यह आई फ़्लू (conjunctivitis) हो सकता है या निम्नलिखित गंभीर बीमारियों में से भी कोई एक हो सकती है:
- ऑफ्थैल्मिया नियोनेटोरम (Ophthalmia neonatorum) (नवजात शिशु की आँखों में संक्रमण होना)।
- जन्मजात काला मोतिया (बच्चे की आँखों में दबाव ज़्यादा होना)।
- नेसोलेक्रिमल नाली (Nasolacrimal-duct) में रुकावट (आँसू निकलनेवाली नाली में रुकावट)।
इन परिस्थितियों में यदि आप डॉक्टर से इलाज करवाएँ तो बच्चे को अंधेपन और अन्य बीमारियों से बचा सकते हैं। यदि बच्चे की आँखों की पुतली में कुछ सफ़ेदी नज़र आए तो यह जन्मजात सफ़ेद मोतिया (Cataract) या आँखों के कैंसर (Retinoblastoma) या किसी और गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए आँखों के डॉक्टर की सलाह लें।
बढ़ते हुए बच्चों में आँखों की तकलीफ़ेंजैसे‑जैसे बच्चा बड़ा होता है, नीचे दी गई समस्याएँ आ सकती हैं:
पौष्टिक आहार की कमी के कारण अंधापनबच्चों में विटामिन‑ए की कमी के कारण रतौंधी (रात का अंधापन) और आँखों में सूखापन हो जाता है। कॉर्निया (जो आँख के सामने की पारदर्शी झिल्ली है) में ज़ख़्म होने पर उसके छिन्न‑भिन्न हो जाने से पूर्ण अंधापन (Keratomalacia) या एक आँख की नज़र ख़त्म हो जाती है। अंधेपन की यह अवस्था पौष्टिक आहार की कमी के कारण होती है। यह ज़्यादातर पाँच साल से कम उम्र वाले बच्चों में पाई जाती है, ख़ास तौर पर उन बच्चों में जिनके आहार में प्रोटीन और कैलोरीज़ की कमी होती है। साँस लेने की ऊपरी नली में संक्रमण (upper respiratory tract infection), खसरा, दस्त और पेट में कीड़े भी इसका कारण हो सकते हैं।
पौष्टिक आहार की कमी से होनेवाले अंधेपन को रोकने के लिए गाजर, आम, पपीता, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ (जैसे पालक और बथुआ) और दूध के पदार्थों का सेवन करें। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को माता का दूध दें।
यदि आपको ये खाद्य पदार्थ उपलब्ध न हों तो बच्चे को हर 6 महीने में (6 महीने से 6 साल की उम्र तक) विटामिन‑ए की दवा दें।
स्कूल जानेवाले 6 से 14 साल के बच्चों में आँखों की समस्याएँनज़र में कमज़ोरी (Refractive errors), कोई स्पष्ट कारण न होने पर भी दृष्टि में कमी (Amblyopia), भेंगापन और रंगों को पहचानने की क्षमता की जाँच करवाएँ।
नज़र की कमज़ोरी (जिसमें चश्मा लगाना ज़रूरी है)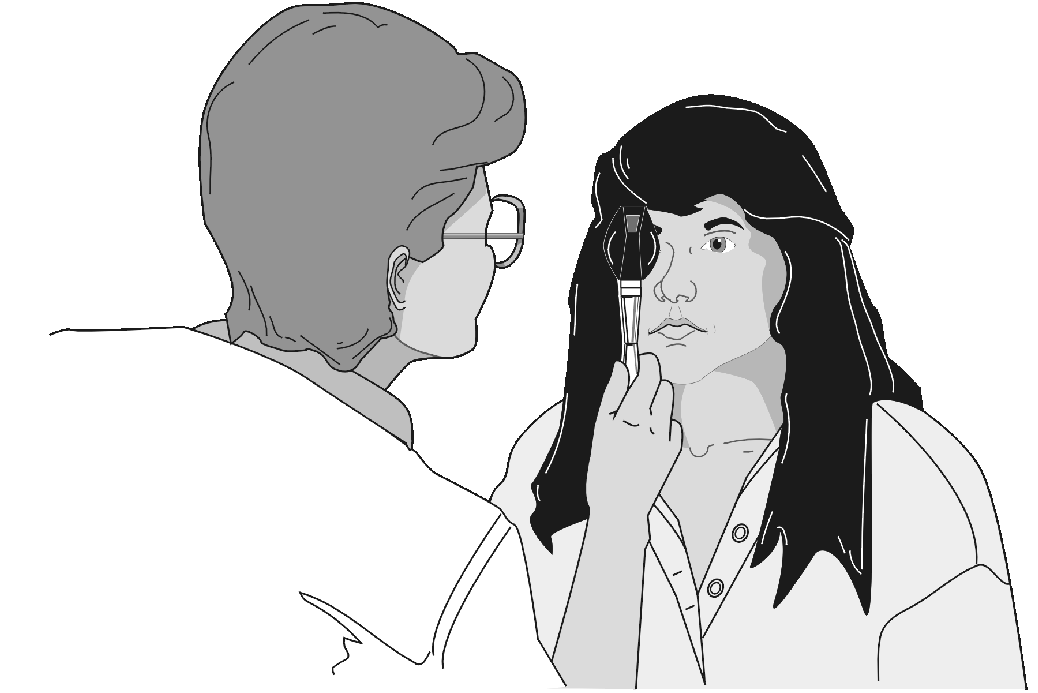 इसमें मुख्य रूप से तीन अवस्थाएँ हैं जिनसे नज़र कमज़ोर हो जाती है और कभी‑कभी अंधापन भी हो जाता है। ये हैं:
इसमें मुख्य रूप से तीन अवस्थाएँ हैं जिनसे नज़र कमज़ोर हो जाती है और कभी‑कभी अंधापन भी हो जाता है। ये हैं:
- केवल पास की वस्तुओं का साफ़ दिखाई देना (Near-sightedness)।
- केवल दूर की वस्तुओं का साफ़ दिखाई देना (Far-sightedness)।
- आँख की बाहर की सतह में असमानता (Astigmatism)।
ये तीनों समस्याएँ हर उम्र के लोगों को हो सकती हैं और आम तौर पर चश्मा लगाने से इनका समाधान भी हो जाता है। आँख के गोले (eye ball) के आकार में बदलाव आने के कारण दूर या पास की नज़र कमज़ोर हो जाती है। बच्चों में यह समस्या जन्म से हो सकती है। यदि बच्चों में इनमें से कोई बीमारी हो, तो वे:
- बार‑बार पलकें झपकते हैं और आँखें मलते हैं।
- पास या दूर की किसी वस्तु को देखने के लिए आँखों को भींचते हैं या उन्हें दबाते हैं।
- किताब को पढ़ते समय उसे आँखों के बहुत पास रखते हैं।
- दूर टँगी हुई घड़ी का समय नहीं देख पाते।
- कम रोशनी में ठीक तरह चल नहीं पाते और लड़खड़ा जाते हैं।
- अपने आसपास हो रहे किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता।
बच्चे आम तौर पर नहीं बताते कि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है कि उन्हें इस समस्या का एहसास ही न हो। वे टेलीविज़न या ब्लैक‑बोर्ड के नज़दीक बैठकर या आँखें भींचकर जैसे‑तैसे काम चला लेते हैं।
बीमारी का पता जल्दी लगाने और उसका इलाज समय से करवाने के लिए स्कूल जाने से पहले बच्चे की आँखों की जाँच करवाएँ। स्कूल जाने वाले बच्चों की (6‑14 साल की उम्र के बीच) साल में कम से कम एक या दो बार आँखों की जाँच ज़रूर करवाएँ।
भेंगापन (आँखों का टेढ़ा होना)भेंगापन न केवल देखने में बुरा लगता है बल्कि इससे अंधापन भी हो सकता है। इसका जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए।
रंगों की पहचान में समस्याइस तरह की समस्या का पता तब चलता है जब बच्चा कोई विशेष व्यवसाय अपनाना चाहता है। रंगों की पहचान न कर पाने की समस्या के कारण बच्चे को उस व्यवसाय के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है। उस समय बहुत निराशा होती है। यदि इस समस्या का पता जल्दी चल जाए तो माता‑पिता और बच्चा पहले से ही ऐसे पेशे के बारे में निर्णय ले सकते हैं जहाँ इस समस्या से कोई बाधा न पड़े।
आँखों में चोटआँखों में चोट लगने के कारण बहुत‑से लोग आँखों की रोशनी गँवा बैठते हैं। बच्चों को चोट लगने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। आँखों में चोट आम तौर पर निम्न कारणों से लगती है:
- आँख में गेंद या किसी ठोस वस्तु का सीधे टकराना।
- आँख में किसी नुकीली वस्तु का चुभ जाना।
- आँख में किसी रसायन का पड़ जाना।
- आँख में ताप, गरमी या आग के कारण लगी चोट।
- बंदूक़ की गोली या बारूदी सुरंग की चोट।
- सिर पर कोई गंभीर चोट लगना।
- सड़क दुर्घटना।
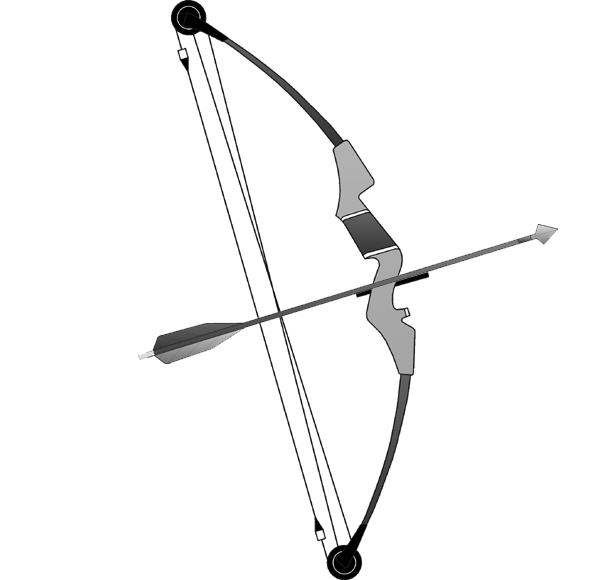
- जब बच्चे गिल्ली‑डंडा, क्रिकेट या तीर‑कमान से खेलें तो उनका ख़याल रखें।
- बच्चों को तीखी नोकवाले खिलौनों, चाकू, कैंची, सुइओं या किसी और नुकीले पदार्थ से न खेलने दें।
- बच्चों को पटाख़ों से न खेलने दें।
- सूर्य की तरफ़, ख़ास तौर पर सूर्यग्रहण के समय, नंगी आँखों से या काला चश्मा लगाकर भी न देखें। ऐसा करने से आँखों का बेहद नाज़ुक अंग रेटिना (Retina) जल जाता है और नज़र कमज़ोर हो जाती है या अंधापन हो जाता है।
- यदि आप बस, ट्रक या कोई और गाड़ी चलाते हैं तो हर साल अपनी नज़र की जाँच करवाएँ। गाड़ी चलाते समय या उससे पहले शराब का सेवन कभी न करें।
- छेनी चलाने, आरी या किसी और मशीन पर काम करते हुए, ख़ास तौर पर वैल्डिंग करते समय आँखों के बचाववाले चश्मे ज़रूर पहनें।
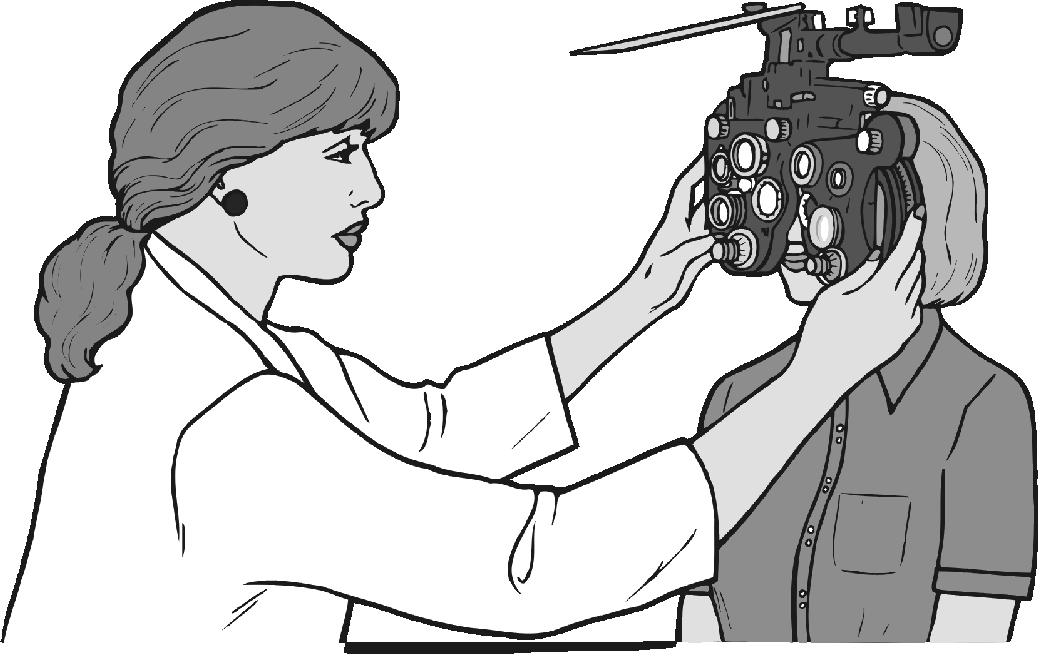 कुकरे आँखों की बीमारी है जो क्लेमाइडीया ट्रेकोमेटिस (Chlamydia trachomatis) नामक जीवाणु द्वारा होती है। यदि इसका इलाज न करवाया जाए तो आँख की रोशनी ख़त्म हो सकती है। भारत में यह एक आम रोग है, ख़ास तौर पर गाँवों में जहाँ लोग अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं। कुकरे होने के कारण:
कुकरे आँखों की बीमारी है जो क्लेमाइडीया ट्रेकोमेटिस (Chlamydia trachomatis) नामक जीवाणु द्वारा होती है। यदि इसका इलाज न करवाया जाए तो आँख की रोशनी ख़त्म हो सकती है। भारत में यह एक आम रोग है, ख़ास तौर पर गाँवों में जहाँ लोग अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं। कुकरे होने के कारण:
- बहुत‑से लोगों का इकट्ठे रहना।
- साफ़ पानी की कमी।
- आँखों पर मक्खियों का बैठना। (भारत में ऐसा आम तौर पर अप्रैल‑मई और जुलाई से सितंबर के महीनों में होता है जब बारिश और ज़्यादा गरमी के कारण मक्खियों की संख्या बढ़ जाती है)।
- एक‑दूसरे के तौलिए, रूमाल और तकिए आदि का प्रयोग करना।
- कई लोगों का एक ही सलाई से आँखों में सुरमा या काजल लगाना।
- शुष्क और धूल भरे वातावरण में रहना।
- ग़रीबी और अज्ञानता के कारण लोगों में निजी‑स्वच्छता या बीमारी फैलने की जानकारी की कमी होना। जैसे‑जैसे रहन‑सहन बेहतर होता है, वैसे‑वैसे बीमारी भी कम होती है।
कुकरे का संक्रमण अपने आप में एक साधारण बीमारी है जिसके कोई विशेष लक्षण नहीं होते। इसलिए इसके इलाज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फिर भी यदि इसका कोई इलाज न किया जाए तो यह बीमारी काफ़ी समय तक बनी रहती है जिसे सबएक्यूट ट्रैकोमा (Subacute trachoma) कहते हैं। आँखों की पारदर्शी झिल्ली यानी कॉर्निया अपारदर्शी हो जाती है और दिखाई देना बंद हो जाता है। कॉर्निया निम्नलिखित कारणों से अपारदर्शी हो जाता है:
- आँखों की पलकों के बाल अंदर की तरफ़ मुड़ जाते हैं जिसके कारण अंदर वाले हिस्से में खुरदरापन और घाव हो जाते हैं जिसे ट्राइकिएसिस (Trichiasis) कहते हैं। पलकों की सतह में असमानता और अंदर मुड़े हुए बाल, पलक झपकने के समय बार‑बार कॉर्निया पर रगड़ खाते हैं और इस रगड़ से बने घावों के कारण कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है।
- कुकरे के जीवाणु सीधे कॉर्निया पर भी ज़ख़्म कर सकते हैं। जब यह ज़ख़्म भरता है तो कॉर्निया अपारदर्शी हो जाता है।
- जिस आँख में कुकरे हों, उसमें दूसरे क़िस्म की बीमारियाँ होने का भी ख़तरा होता है। इसे एक्यूट ट्रैकोमा (Acute trachoma) कहते हैं। इससे कॉर्निया में जल्द ही बहुत गहरे और ख़तरनाक ज़ख़्म हो जाते हैं। ये ज़ख़्म बार‑बार होते रहते हैं जिससे और ज़्यादा अपारदर्शिता हो जाती है और अंधापन हो सकता है।
कुकरे से बचाव के लिए:
आँखों को साफ़ पानी से धोएँ।
अपनी सफ़ाई रखें।
अपने आसपास का वातावरण साफ़ रखें।
यदि आपको आँख का संक्रमण (Infection) हुआ है:
किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएँ
जल्द ही सही (ऐंटीबायोटिक) दवा का प्रयोग करें।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) द्वारा बताए गए सुरक्षा के उपायों पर अमल करें।
- SAFE योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं:
S-Surgery – सर्जरी—अंदर मुड़ी हुई पलकों (Trichiasis) का इलाज करवाने के लिए ऑपरेशन करवाएँ, नहीं तो अंधापन हो सकता है।
A-Antibiotics – ऐंटीबायोटिक दवाएँ—रोग के इलाज के लिए किसी आँखों के डॉक्टर द्वारा बताई गई ऐंटीबायोटिक दवा का इस्तेमाल करें।
F-Facial cleanliness – (फ़ेस) चेहरे की सफ़ाई—बीमारी को फैलने से रोकने के लिए नियमित रूप से चेहरे को साफ़ रखें।
E-Environmental – एनवायर्न्मेंट यानी वातावरण को बेहतर बनाएँ—शौचालय साफ़ होना चाहिए, मक्खियों को दूर रखें, पीनेवाला पानी साफ़ रखें और कूड़ा‑करकट फेंकने की उचित व्यवस्था करें।
कॉर्निया आँख की सबसे सामनेवाली झिल्ली है, जिसके ज़रिए आँखों में रोशनी प्रवेश करती है। इसकी सतही कोशिकाओं (cells) में कोई ख़ाली स्थान (घाव या खरोंच के कारण) आ जाना कॉर्नियल अल्सर कहलाता है। कॉर्नियल अल्सर से आँख की रोशनी जाने का ख़तरा रहता है। 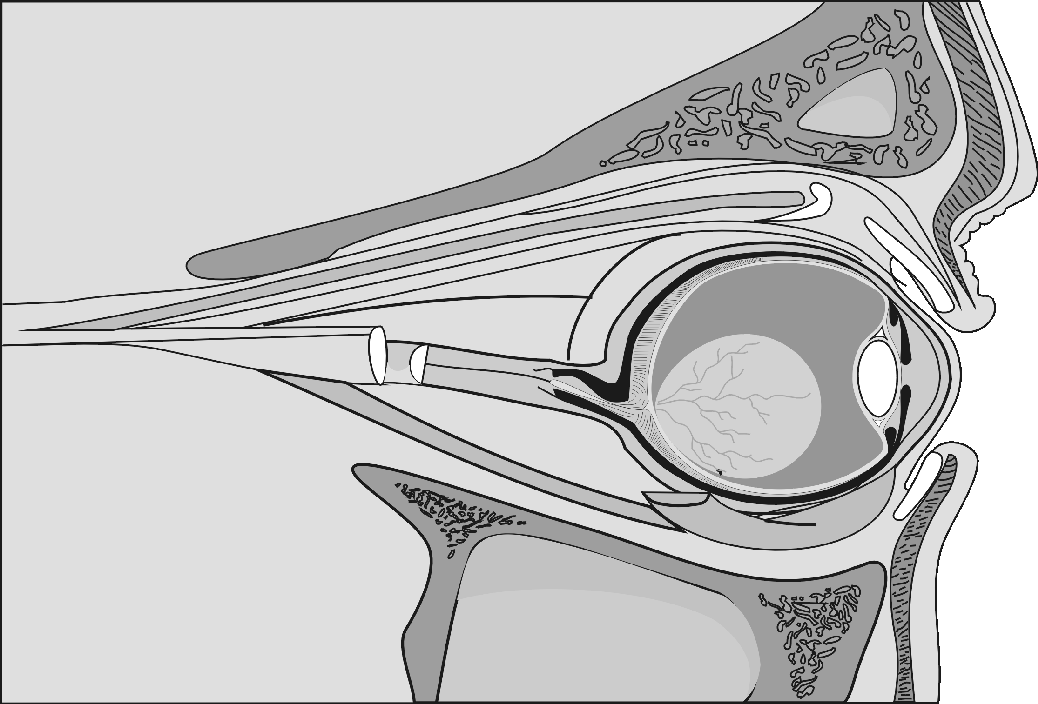 आम तौर पर यह कॉर्निया की सतह पर किसी खरोंच आने से होता है जिस पर बैक्टीरिया, फफूँद या वायरस द्वारा संक्रमण हो जाता है। यह खरोंच किसी मामूली‑सी चोट या कचरा आदि पड़ जाने से आती है। पलकों के बालों का अंदर की तरफ़ मुड़े होने के कारण और पलकों के अंदरवाली सतह पर किसी दानेदार पदार्थ के जमा होने से भी, पलक झपकते समय कॉर्निया पर हर बार रगड़ लगती है जिससे खरोंच आ जाती है।
आम तौर पर यह कॉर्निया की सतह पर किसी खरोंच आने से होता है जिस पर बैक्टीरिया, फफूँद या वायरस द्वारा संक्रमण हो जाता है। यह खरोंच किसी मामूली‑सी चोट या कचरा आदि पड़ जाने से आती है। पलकों के बालों का अंदर की तरफ़ मुड़े होने के कारण और पलकों के अंदरवाली सतह पर किसी दानेदार पदार्थ के जमा होने से भी, पलक झपकते समय कॉर्निया पर हर बार रगड़ लगती है जिससे खरोंच आ जाती है।
नीचे दिए गए कारणों से कॉर्नियल अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है:
- आँखों का सूखापन (Xerosis or Xerophthalmia)—यह विटामिन‑ए की कमी से होता है।
- चेहरे का लकवा होने से आँखें बंद न कर पाना।
- कॉर्निया की संवेदनशीलता कम हो जाना या पूरी तरह ख़त्म हो जाना। ऐसा हरपीज़ (Herpes) या न्यूरोपैरोलिटिक केरेटाइटिस ( Neuroparalytic Keratitis) के कारण होता है।
- कॉर्निया में पानी भर जाना (Corneal Oedema)।
- गोनोकोकस या डिप्थीरिया बेसीलाई (Gonococcus or Diptheria Bacilli), जैसे बैक्टीरिया का कॉर्निया की सतह पर आक्रमण।
- आँखों में स्टीरॉयड‑युक्त दवा डालना।
- शरीर की प्रतिरोधी क्षमता (Immunosuppressant) को कम करनेवाली दवाइयों या स्टीरॉयड का सेवन करना।
- आँसू निकलनेवाली नलिका में कोई रुकावट।
कॉर्नियल अल्सर आपातकालीन स्थिति है। यदि आपकी आँख में तेज़ दर्द या लाली हो, आँखें रोशनी को बर्दाश्त न कर पाएँ, उनसे पानी या कोई और स्राव निकले, तो तुरंत अपने आँखों के डॉक्टर के पास जाएँ ताकि किसी भी गंभीर समस्या का इलाज जल्दी हो सके। कॉर्निया में खरोंच आने से यह झिल्ली अपारदर्शी हो सकती है जिससे आंशिक या पूरी तरह से अंधापन हो सकता है।
कॉर्निया के अल्सर से कैसे बचाव करें?
- आँखों को खरोंच या ज़ख़्म से बचाएँ। आँख में कचरा या धूल न जाने दें और यदि चला जाए तो इन्हें मलें नहीं। आँखों को अच्छी तरह साफ़ पानी से धोएँ। यदि फिर भी आँख में चुभन रहती है, तो शीघ्र ही अपने डॉक्टर से मिलें।
- यदि आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं तो अपने डॉक्टर द्वारा दी गई हिदायतों पर अमल करें। यदि लेंस पहनने से आँखों में दर्द या लाली होती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि कॉर्नियल अल्सर न होने पाए।
- यदि आप खेती का काम करते हैं तो आँखों में पेड़‑पौधों के कण (जैसे कि गन्ने या मक्की के पत्ते) जाने से बचाएँ। इनमें फफूँद (Fungus) हो सकती है। फफूँद से हुए ज़ख़्म बहुत मुश्किल से भरते हैं।
- यदि आपकी आँखें सूखी रहती हैं, तो आँखों को नमी देनेवाली दवाइयों का इस्तेमाल करें और डॉक्टर द्वारा बताई गई विटामिन‑ए की दवा का सेवन करें।
- यदि आपको चेहरे का लक़वा है, तो डॉक्टर की हिदायत के अनुसार इससे प्रभावित आँख पर रात को टेप लगा दें, क्योंकि इस बीमारी में आँख बंद नहीं हो पाती जिसके कारण आँख ख़ुश्क हो जाती है और कॉर्नियल अल्सर बन जाता है।
- पलकों के बाल जो अंदर की तरफ़ मुड़े हों, उन्हें ऑपरेशन द्वारा ठीक करवाएँ या डॉक्टर से बाहर खिंचवा दें ताकि कॉर्निया में ज़ख़्म न होने पाए।
- यदि आँख की कोई और तकलीफ़ हो तो उसका इलाज करवाएँ।
- यदि आँख में अल्सर है, तो उसमें स्टीरॉयड‑युक्त दवा न डालें। साथ ही स्टीरॉयड या शरीर की प्रतिरोधी ताक़त को घटानेवाली (Immununosuppressant) किसी भी दवा का सेवन न करें।
टेलीविज़न देखने से हमारी आँखों पर तनाव बढ़ता है। यदि आपको टेलीविज़न देखना पसंद हो तो इन बातों का ख़याल रखें:
- टेलीविज़न से कम से कम तीन मीटर (आठ से दस फ़ुट) की दूरी पर बैठें।
- टेलीविज़न देखनेवाले कमरे में पर्याप्त रोशनी हो, ताकि कमरे में घना अँधेरा न हो।
- इस बात का ख़याल रखें कि उस रोशनी की चौंध टेलीविज़न से टकराकर आपकी आँखों में न पड़े।
- जब स्क्रीन पर तस्वीरें धुँधली, काँपती हुईं या दानेदार नज़र आएँ तो टेलीविज़न न देखें।
- टेलीविज़न देखते समय थोड़ी‑थोड़ी देर बाद अपनी आँखों को आराम दें। उदाहरण के लिए कमरा छोड़कर बाहर चले जाएँ या कुछ अन्य काम कर लें जैसे चाय आदि बना लें।
मनुष्य की आँखें लंबे समय तक कंप्यूटर पर काम करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कंप्यूटर का प्रयोग दिन‑प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हम कंप्यूटर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। भले ही कंप्यूटर से काम बेहतर और जल्दी होता है लेकिन इसके लिए क़ीमत भी चुकानी पड़ती है यानी कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम का ख़तरा। कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम आँखों और उनके देखने की शक्ति से जुड़ी हुई वे तकलीफ़ें हैं जो कंप्यूटर के प्रयोग से जुड़ी हैं और बार‑बार हो जाती हैं।
कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम के लक्षण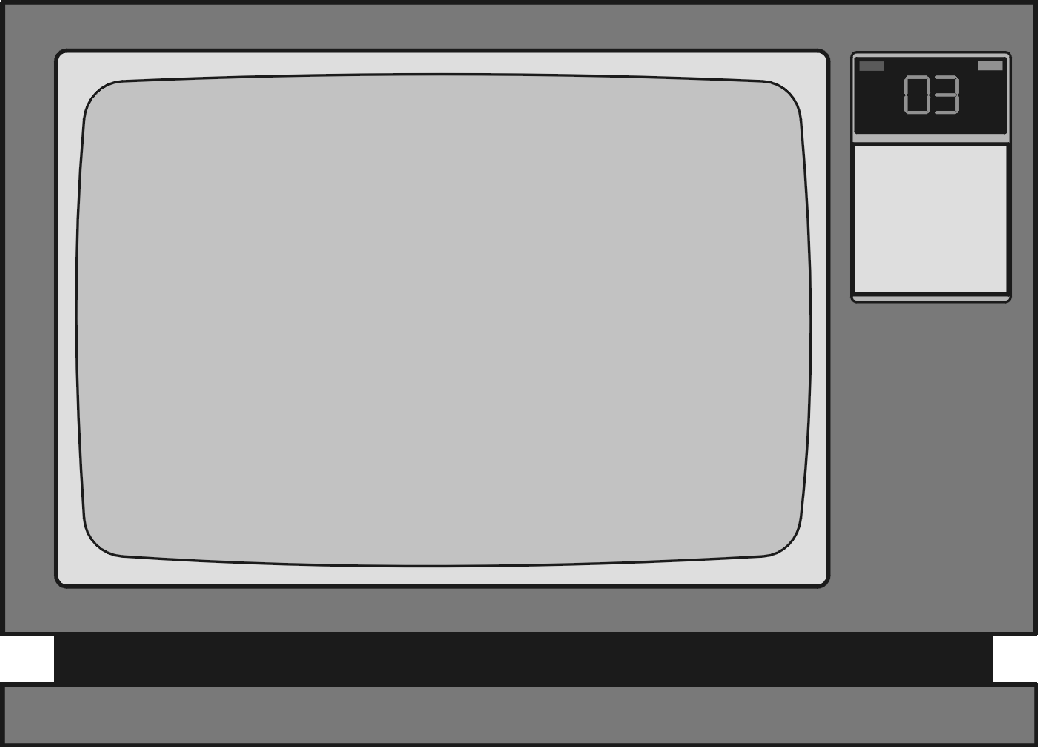
- आँखों का तनाव।
- धुँधला नज़र आना।
- चक्कर आना या जी मतलाना।
- सिर दर्द।
- आँखों में लाली, ख़ुश्की या जलन।
- दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई।
- रंगों की पहचान में मुश्किल।
- किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई।
- Eअधिक थकान।
- गरदन, कंधों और पीठ में दर्द होना।
- कभी‑कभी एक की जगह दो चीज़ें दिखाई देना।
कंप्यूटर से होनेवाली इन सभी समस्याओं की रोकथाम और इलाज हो सकता है।
कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम से बचने के लिए 10 उपाय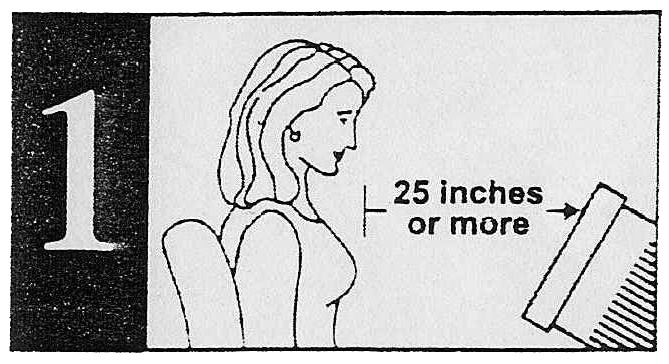
स्क्रीन से दूरी: कम से कम 25 इंच।
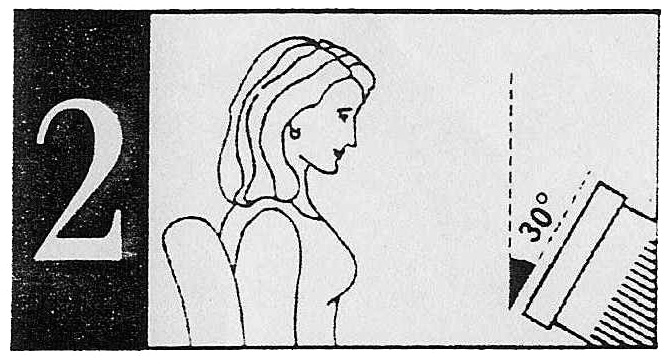
स्क्रीन का झुकाव: मॉनिटर का ऊपरी हिस्सा नीचे वाले हिस्से से अधिक दूर रखें।
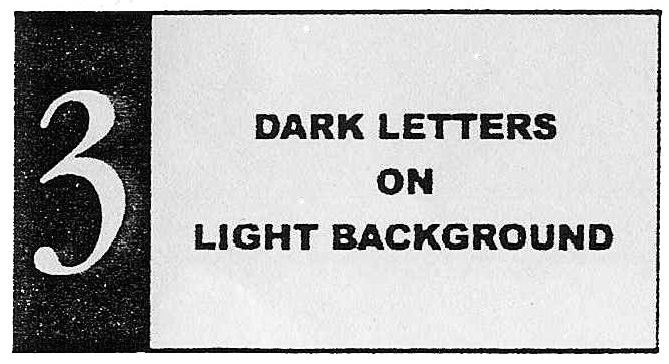
स्क्रीन: हलकी पृष्ठभूमि पर गहरे अक्षर।
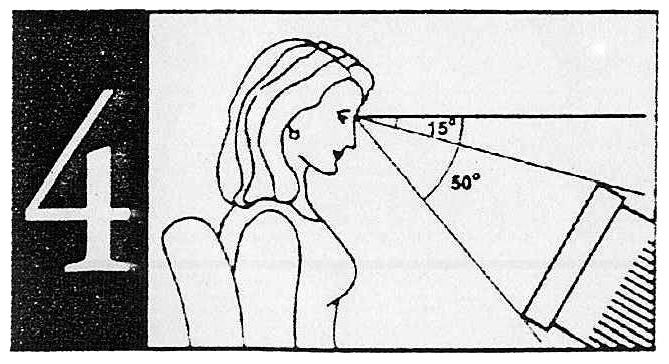
मॉनिटर का देखने का हिस्सा: Vआँखों के स्तर से 15‑50 डिग्री नीचे होना चाहिए।
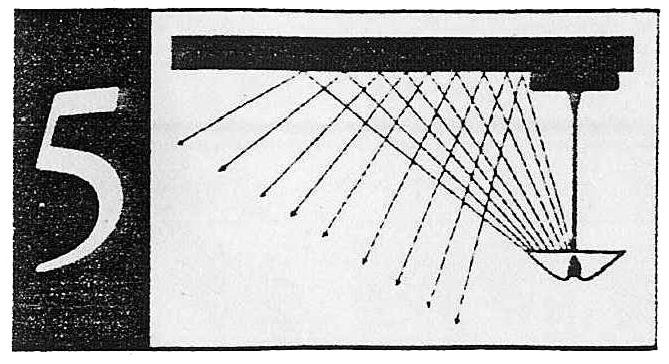
रोशनी: छत पर लगे बल्ब की रोशनी सीधी आप पर नहीं पड़नी चाहिए। बाहर से आ रही सीधी रोशनी या परछाईं से बचने के लिए परदे का प्रयोग करें।
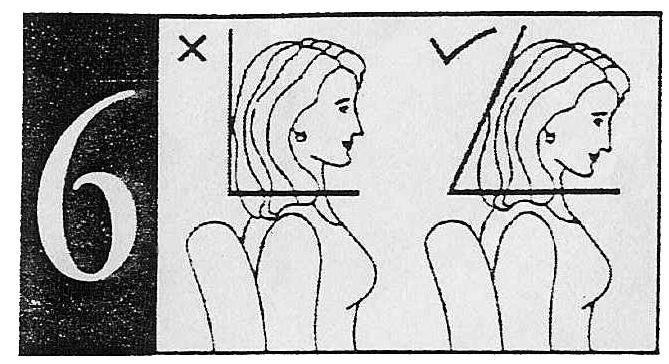
गरदन की स्थिति: बाँहों वाली कुर्सी का प्रयोग करें। थोड़ा सिर झुकाकर काम करने से कम थकान होती है।
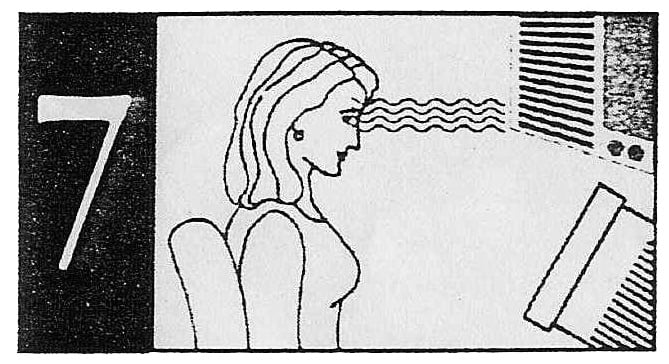
ए.सी. (Air conditioner) की हवा का रुख़: आपकी आँखों में सीधी हवा नहीं आनी चाहिए।
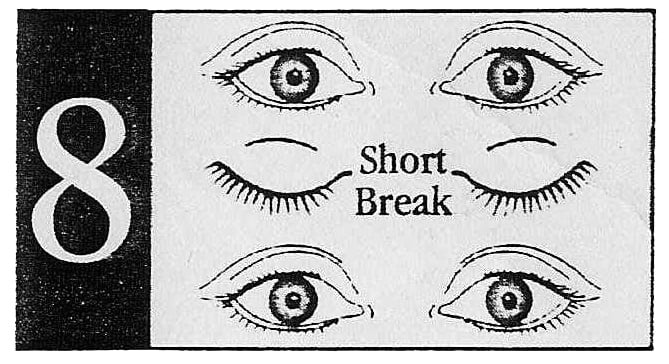
विश्राम: हर बीस मिनट बाद थोड़ा विश्राम करें।
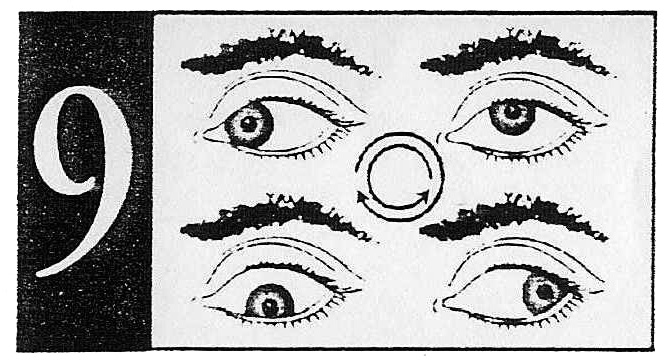
व्यायाम: कुछ समय के लिए पलकें झपकाएँ। आँखें बंद करें और इन्हें बंद रखते हुए पहले दायें से बायें और फिर बायें से दायें घुमाएँ। लंबी साँस लें और साँस बाहर छोड़ते समय आँखें खोलें।
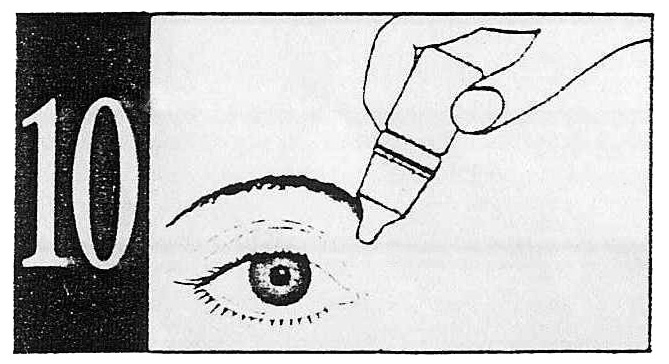
आँखों की नमी: डॉक्टर की हिदायत के अनुसार आँखों को नमी देनेवाली दवा का प्रयोग करें।
अधेड़ उम्र में आँखों की समस्याएँ
मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशरमधुमेह के रोग के कारण हमारे ख़ून में शुगर की मात्रा नियंत्रित नहीं रहती। ख़ून में शुगर को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन नामक एक हॉर्मोन करता है जो पैन्क्रियाज़ से उत्पन्न होता है। जब इंसुलिन बहुत कम हो तो मधुमेह हो जाता है। इस रोग से आँखों समेत शरीर के सभी अंग प्रभावित होते हैं।
चेतावनी! मधुमेह के कारण रेटिना की नाड़ियों को नुकसान होने से अंधापन हो सकता है। मधुमेह के रोगी को गर्भावस्था में, धूम्रपान करने से, मोटापा आने से या ख़ून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से आँखों का ख़तरा और भी बढ़ जाता है।
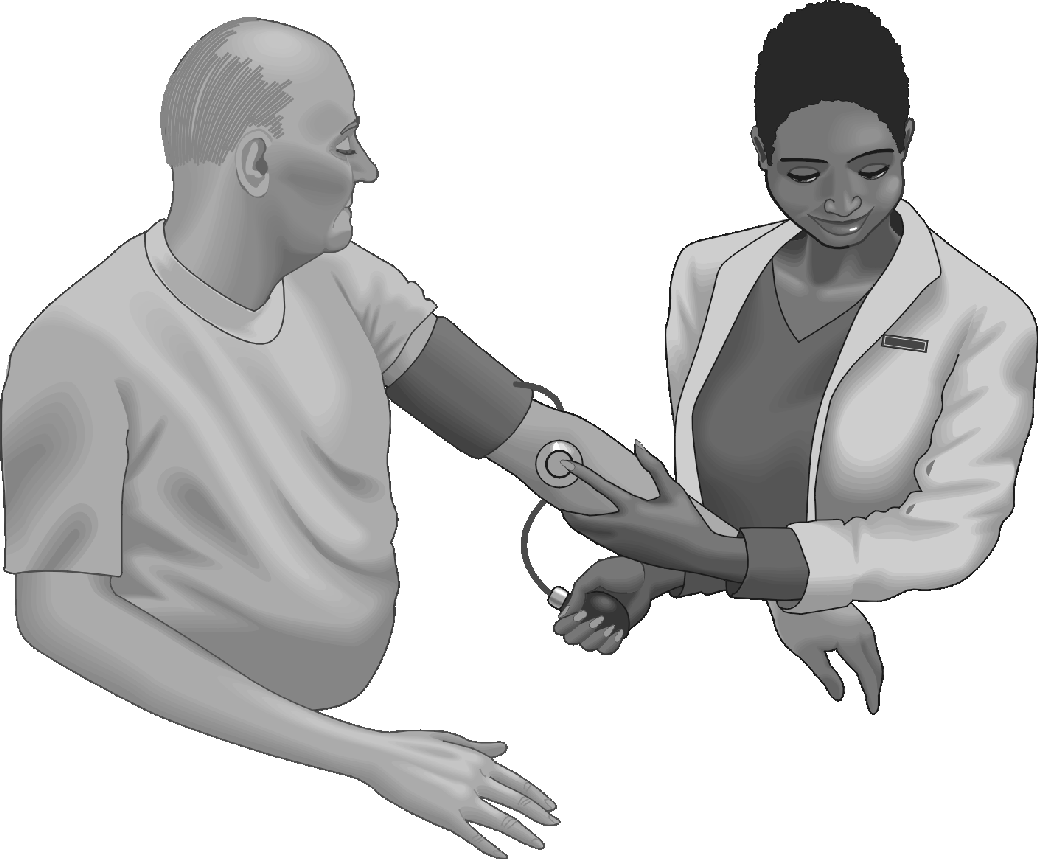 हर साल अपने ब्लड प्रेशर की जाँच करवाते रहें। आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के कोई विशेष लक्षण नज़र नहीं आते, हालाँकि उम्र के बढ़ने से या शरीर का वज़न बढ़ने से इसका ख़तरा और भी बढ़ सकता है।
हर साल अपने ब्लड प्रेशर की जाँच करवाते रहें। आम तौर पर हाई ब्लड प्रेशर के कोई विशेष लक्षण नज़र नहीं आते, हालाँकि उम्र के बढ़ने से या शरीर का वज़न बढ़ने से इसका ख़तरा और भी बढ़ सकता है।
चेतावनी! यदि आपको मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर दोनों हैं तो आपको आँखों की बीमारी होने की संभावना उन लोगों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है, जिन्हें केवल इनमें से एक ही रोग है। अपने डॉक्टर की सलाह से इन रोगों को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से आपकी नज़र ठीक रहेगी।
ब्लड प्रेशर और मधुमेह को नियंत्रित करने के साथ‑साथ फ़ंडस (Fundus) की जाँच करवाना भी ज़रूरी है, जिसमें आँखों की पुतली में दवा डालकर उसे फैलाया (dilate) जाता है और अंदर से जाँच की जाती है। मधुमेह के बारे में और जानकारी पृष्ठ 117 पर पढ़ें।
काला मोतिया (Glaucoma)काला मोतिया इनसान को अंधा कर देता है। इस रोग के कारण आँखों की जो रोशनी चली जाती है, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस रोग में आँख की कई तकलीफ़ों के कारण हमारी ऑप्टिक नर्व (Optic Nerve) को धीरे‑धीरे नुकसान होता जाता है। हमारी आँखें जो कुछ भी देखती हैं, ऑप्टिक नर्व उसका संदेश लेकर मस्तिष्क तक जाती है। यह रोग आम तौर पर दोनों आँखों को प्रभावित करता है।
ऑप्टिक नर्व की क्षति होने से अंधापन हो जाता है। इस क्षति का कारण है, आँख में ज़रूरत से ज़्यादा दबाव होना या नर्व में ख़ून की कमी। यहाँ तक कि जिस आँख के अंदर दबाव ठीक भी हो, यह रोग वहाँ भी हो सकता है। नर्व की क्षति से देखने का दायरा कम होता जाता है और धीरे‑धीरे इनसान पूरी तरह अंधा हो सकता है।
काला मोतिया ऐसा ख़तरनाक रोग है, जिसमें रोगी को पता भी नहीं चलता कि उसकी नज़र ख़त्म हो रही है। आम तौर पर इसमें दर्द नहीं होता और जब तक रोगी को इसके बारे में पता चलता है, नज़र को काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। यह नुकसान किसी भी दवा या ऑपरेशन या लेज़र से ठीक नहीं हो सकता। हालाँकि जब इस रोग का पता चल जाए तो आगे बताए गए उपचारों से रोग को वहीं रोका जा सकता है ताकि आँखों को और ज़्यादा नुकसान न हो।
आँखों की रोशनी को क़ायम रखने के लिए आँखों के डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज पर पूरी तरह अमल करना चाहिए। हो सकता है कि यह इलाज सारी उम्र चले क्योंकि काला मोतिया ठीक नहीं किया जा सकता। इस पर सिर्फ़ नियंत्रण रखा जा सकता है।
जिन कारणों से काला मोतिया होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, वे हैं:
- परिवार में काले मोतिये की बीमारी।
- दूर के चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा होना।
- मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर या थायरॉयड की बीमारी।
- स्टीरॉयड‑युक्त दवा (खानेवाली दवा, आँखों के ड्रॉप्स या मरहम) का प्रयोग करना।
- चश्मे के नंबर का बार‑बार बदलना।
- रात में कम दिखाई देना।
- आँखों में दबाव की समस्या।
यह ख़तरा उम्र के साथ‑साथ बढ़ता जाता है। सब बालिग़ों को समय‑समय पर आँखों की जाँच करवाते रहना चाहिए ताकि काला मोतिया होने पर उसका जल्द पता लग सके। यदि इसका इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो इससे आँखों के अंधेपन को रोकने में सहायता मिल सकती है।
एक ऐसा काला मोतिया भी है जो बहुत जल्द बढ़ जाता है, इसे एक्यूट ऐंगल क्लोज़र ग्लोकोमा (Acute Angle Closure Glaucoma) कहते हैं। यह आपातस्थिति है क्योंकि इससे दृष्टि ख़त्म हो सकती है। इसलिए यदि आपको निम्नलिखित लक्षणों में से कोई हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। याद रखें कि दोनों आँखों का इलाज होगा:
- एक आँख में बहुत तेज़ दर्द।
- आँख में बहुत ज़्यादा लाली।
- बल्ब, मोमबत्ती या और किसी भी रोशनी के आसपास रंगीन घेरे दिखना।
- अचानक ही नज़र कमज़ोर हो जाना।
- जी मतलाना या उलटी होना।
- नज़दीक की नज़र का बहुत कमज़ोर होना।
काला मोतिया आम तौर पर बुज़ुर्गों को होता है, लेकिन यह नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को भी हो सकता है। इसे ‘जन्मजात काला मोतिया’ कहते हैं और नज़र को बचाने के लिए इसका जल्द ही इलाज करवाना चाहिए। यदि आपके बच्चे की आँखें कुछ ज़्यादा ही बड़ी हैं, तो सावधान! यह ‘जन्मजात काला मोतिया’ हो सकता है। बच्चे को जल्द ही किसी आँखों के डॉक्टर के पास ले जाएँ।
याद रखें कि अपनी नज़र को सही रखने के लिए आपको ख़ुद प्रयास करना है।
काले मोतिये के इलाज का मूलमंत्र:
इस रोग की पहचान जल्दी करें!
आँखों की जाँच समय‑समय पर करवाते रहें।
बुढ़ापे में होनेवाली आँखों की समस्याएँ
सफ़ेद मोतिये का अर्थ है आँख के लेंस में धुँधलापन। इस धुँधलेपन की वजह से आँख में रोशनी प्रवेश नहीं कर पाती जिससे देखने में तकलीफ़ होती है। यह रोग आम तौर पर पचास साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है और चूँकि यह अधिकतर बुज़ुर्गों में होता है, इसलिए इसे ‘बुढ़ापे का सफ़ेद मोतिया’ भी कहते हैं। बुढ़ापे के सफ़ेद मोतिये के कारण अभी तक पता नहीं लग पाए हैं। यह जन्म से भी हो सकता है और बहुत कम आयु में भी हो सकता है।
सफ़ेद मोतिये के सामान्य कारण:
- आयु (बुढ़ापे का सफ़ेद मोतिया)।
- आँख में चोट लगना।
- हरी सब्ज़ियाँ कम खाना।
- सूर्य की तेज़ रोशनी (अल्ट्रावॉयलेट किरणें)।
- आँखों की कुछ ख़ास बीमारियाँ।
- मधुमेह, थायरॉयड या पैराथायरॉयड की बीमारी।
- कुछ दवाइयों, जैसे कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल।
- बिना दर्द के लगातार नज़र कमज़ोर होना।
- साफ़ देखने के लिए ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होना।
- बार‑बार चश्मे का नंबर बदलना।
- रोशनी के आसपास रंगीन घेरे दिखाई देना।
- पास की वस्तुओं का चश्मे के बिना पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देना।
- एक की जगह दो या उससे ज़्यादा वस्तुएँ दिखाई देना: जैसे कि एक चाँद की जगह कई चाँद दिखाई देना।
- रात को गाड़ी चलाने में दिक़्क़त होना।
- आँखों की पुतली का रंग सलेटी या सफ़ेद होना।
सफ़ेद मोतिये का इलाज दवा से नहीं हो सकता। इसका एकमात्र इलाज है ऑपरेशन करवाकर धुँधले हो चुके लैंस को निकलवाना। उसकी जगह एक छोटा कृत्रिम लैंस लगा दिया जाता है ताकि व्यक्ति सामान्य रूप से देख सके।
- ऑपरेशन के लिए सफ़ेद मोतिये के पकने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि थोड़े‑से धुँधलेपन में ही आपको दिक़्क़त महसूस होती है तो यह ऑपरेशन जल्दी भी करवाया जा सकता है।
- यदि सफ़ेद मोतिये के बढ़ने का इंतज़ार किया जाए तो फिर बाद में काला मोतिया होने के आसार भी बढ़ जाते हैं।
- ऑपरेशन के बाद आपको ज़्यादा समय के लिए अस्पताल में नहीं रहना पड़ता; हो सकता है कि आपको उसी दिन छुट्टी मिल जाए।
- ऑपरेशन किसी भी मौसम में करवाया जा सकता है।
- सफ़ेद मोतिये का इलाज लेज़र के ज़रिए नहीं होता। इसकी जगह एक नई तकनीक फ़ैकोएमल्सिफ़िकेशन (phacoemulsification) के ज़रिए आँख में एक छोटा सा चीरा लगाकर, लैंस को पिघलाकर निकाला जाता है। इसमें टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हालाँकि यह इलाज कुछ महँगा है लेकिन इससे रोगी जल्दी ठीक हो जाता है।
- इलाज की कम ख़र्चीली तकनीकें भी उपलब्ध हैं। इनमें आई.ओ.एल. की सहायता से किया गया सफ़ेद मोतिये का छोटा‑सा ऑपरेशन सम्मिलित है। इससे भी आँख की नज़र ठीक हो जाती है।
Aरेटिना के मध्य में गोलाकार हिस्सा मैक्युला होता है। यह सबसे भीतरी सतह रोशनी के प्रति संवेदनशील है। यह हमें किसी वस्तु को बेहद बारीक़ी से देखने में और अलग‑अलग रंगों की पहचान करने में सहायता करता है। मैक्युला को उम्र के साथ धीरे‑धीरे क्षति पहुँचती है जिससे अंधापन हो सकता है। यह दोनों आँखों को प्रभावित करता है। विकसित देशों में 65 साल से अधिक आयु के लोगों में अंधेपन का यही मुख्य कारण है। भारत में भी यह तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ व्यक्ति का जीवन पहले से लंबा होता जा रहा है, जिस कारण बुज़ुर्गों की संख्या बढ़ रही है।
मैक्युला की क्षति दो प्रकार की है:- ख़ुश्क मैक्युला की क्षति: मैक्युला के कुल रोगियों में 90% से ज़्यादा इसी प्रकार की क्षति देखने में आती है। ऐसा मैक्युला ऊतकों (Macula tissues) का उम्र बढ़ने के साथ कमज़ोर हो जाने के कारण होता है। इससे आँखों की रोशनी धीरे‑धीरे कम होती जाती है जिसमें कई साल लग सकते हैं। इसका अचूक इलाज अभी उपलब्ध नहीं है। लो विज़िन ऐड (Low Vision Aids—magnifying glass, telescope bioptic eyewear etc.) की सहायता से रोगी पढ़ाई‑लिखाई या अन्य कार्य कर सकता है।
- नमी वाले मैक्युला की क्षति: यह रोग काफ़ी कम पाया जाता है, लेकिन पहले वाले से कहीं अधिक ख़तरनाक होता है। यह सिर्फ़ 10% रोगियों में ही पाया जाता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मैक्युला की क्षति के कारण जितने लोगों में अंधापन होता है, उसमें 90% लोग इसी श्रेणी में आते हैं। रेटिना की पिगमेंट वाली तह के नीचे कुछ ख़ून की नई नाड़ियाँ पैदा हो जाती हैं। इन नाड़ियों से ख़ून का रिसाव हो सकता है जिससे मैक्युला पर निशान पड़ जाते हैं। ऐसा होने से नज़र काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। इस रोग का मुख्य लक्षण है—बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा नज़र की कमज़ोरी। फ़ंडस फ़्लोरोसीन एनजियोग्राफ़ी (Fundus Flourescein Angiography) से ख़ून की नई नाड़ियों के बनने का पता लग सकता है।
- आयु: यदि किसी की आयु 65 वर्ष से ज़्यादा है तो उसमें मैक्युला की क्षति के आसार बढ़ जाते हैं।
- पारिवारिक इतिहास: यह रोग एक से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है।
- लिंग: यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज़्यादा होता है।
- भौगोलिक स्थिति: यह रोग उत्तरी यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है।
- धूम्रपान: धूम्रपान वातावरण से जुड़ा एकमात्र कारण है जो निश्चित रूप से मैक्युला को हानि पहुँचाता है। यह रोग धूम्रपान करनेवालों को ज़्यादा होता है
- हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, ख़ून में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, मोटापा और अधिक चिकनाई वाला भोजन करने से इस रोग के होने का ख़तरा बढ़ जाता है।
- यदि आपको पढ़ने या नज़दीक का काम करने में दिक़्क़त महसूस हो, किताब में लिखे शब्द अस्पष्ट या धुँधले दिखाई दें।
- रंग फीके नज़र आएँ।
- सीधी पंक्तियाँ टेढ़ी‑मेढ़ी नज़र आएँ।
- वस्तु का आकार छोटा‑बड़ा लगे।
- देखते समय बीच का स्थान ख़ाली या काला नज़र आए।/li>
ऐंटीऑक्सीडैंट: ARMD के शुरुआत में कुछ ऐंटीऑक्सीडैंट के प्रयोग से मैक्युला की क्षति धीमी हो जाती है, इसलिए हमें हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों का जीवन भर सेवन करना चाहिए।
लेज़र: नमी वाले मैक्युला की क्षति के रोग में लेज़र कुछ लोगों को सहायक हो सकता है। आँख की जितनी रोशनी जा चुकी हो, लेज़र से उसे वापिस नहीं लाया जा सकता। इस रोग के बढ़ जाने पर Low Vision Aids का प्रयोग लाभप्रद होता है।
पी.डी.टी. (Photodynamic therapy) और टी.टी.टी. (Transpupillary Thermo-therapy) ऐसी नई तकनीकें हैं जिनके द्वारा इसका इलाज किया जाता है।
इलाज का मुख्य उद्देश्य आँख की मौजूदा नज़र को उसी स्तर पर बनाए रखना है।
आँखों की देखभाल के लिए ऐसा करें- चेहरे और आँखों को धोने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करें।
- ड्रिल, वैल्डिंग, किसी धातु को काटने का काम करते हुए या मिट्टी और धूलभरे वातावरण में काम करते समय आँखों पर सुरक्षा के लिए पहने जानेवाले चश्मे का इस्तेमाल करें।
- हरी सब्ज़ियाँ, गाजर और फल, जैसे आम और पपीते का सेवन करें।
- हमेशा सही रोशनी में और सही स्थिति में बैठकर पढ़ें। पढ़ते समय किताब मेज़ पर होनी चाहिए और रोशनी:
- दायें हाथ का इस्तेमाल करनेवाले व्यक्ति के लिए सामने से और बाईं तरफ़ से आनी चाहिए।
- बायें हाथ का इस्तेमाल करनेवाले व्यक्ति के लिए सामने से और दाईं तरफ़ से आनी चाहिए।
- यदि बच्चे की आँखों में भेंगापन है या लेज़ी आइज़ (lazy Eyes) हैं तो उसे डॉक्टर के पास ले जाएँ।
- बच्चे को स्तनपान कराएँ ताकि उसमें पौष्टिक आहार की कमी के कारण अंधापन न हो।
- क्रिकेट और बॉक्सिंग जैसे खेल खेलते समय आँखों का बचाव करें।
- यदि आयु 35 वर्ष से ज़्यादा है और आप पेशे से ड्राइवर हैं तो हर साल अपनी आँखों की जाँच ज़रूर करवाएँ।
- बच्चों को स्कूल भेजने से पहले और स्कूल की पढ़ाई के दौरान कम से कम 1‑2 बार आँखों की जाँच ज़रूर करवाएँ।
- यदि धुँधला दिखाई दे, रोशनी के इर्द‑गिर्द रंगीन घेरे दिखाई दें, अँधेरे में देखने में दिक़्क़त हो या फिर एक अथवा दोनों आँखों में बार‑बार दर्द हो तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें।
- यदि आप चालीस साल के आसपास हैं और आपको पढ़ने में दिक़्क़त आती है तो पढ़नेवाले चश्मे की ज़रूरत हो सकती है। यह चश्मा डॉक्टर की सलाह पर ही पहनें, न कि चश्मा बेचनेवाले दुकानदार की सलाह पर।
- दूसरों के द्वारा प्रयोग किए तौलिए और रूमाल का प्रयोग न करें।
- बच्चों को एक ही सलाई से सुरमा या काजल न लगाएँ।
- अपने बच्चों को नुकीली वस्तुओं, छर्रे वाली बंदूक़ों, पटाख़ों इत्यादि से न खेलने दें। उन्हें गिल्ली‑डंडा और तीर‑कमान से भी न खेलने दें।
- सूर्य की तरफ़ नंगी आँख से न देखें, ख़ास तौर पर सूर्यग्रहण के वक़्त।
- यदि आँख में कुछ पड़ जाए तो आँख न मलें बल्कि इसे साफ़ पानी से धोएँ। यदि आराम न आए तो डॉक्टर के पास जाएँ।
- नाक़ाबिल नीम‑हकीमों के पास न जाएँ। (ऐसे लोग इलाज करने का दावा तो करते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती) उनकी दवाएँ उलटा नुकसान पहुँचा सकती हैं।
- आँख में कौन‑सी दवा डालनी है, यह ख़ुद न तय करें।
- कम रोशनी में न पढ़ें।
- भेंगापन, लाल‑आँख, कोई भी समस्या जिसमें चश्मा लगाने की ज़रूरत हो, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, आँख की किसी भी चोट का इलाज शीघ्र करवाएँ।
- किसी और व्यक्ति के चश्मे का इस्तेमाल न करें।
अपने जीते‑जी प्रण लें कि मृत्यु के बाद
अपनी आँखें दान करेंगे।
इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए
स्थानीय आई बैंक से संपर्क करें। देखें पृष्ठ
181
दाँतों की देखभाल
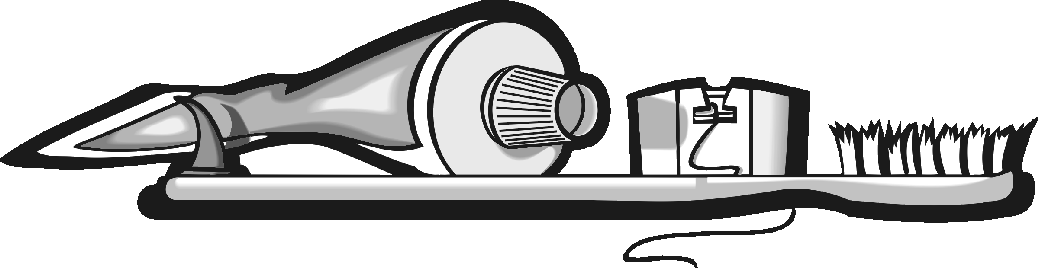 मुँह और दाँतों की सफ़ाई शरीर के स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। भारत में बहुत‑से लोग मुँह से संबंधित रोगों से ग्रस्त हैं जैसे—दाँतों में खोड़, मसूड़ों के रोग, दाँतों का आकार बिगड़ना, मुँह का कैंसर आदि। सब जानते हैं कि दाँतों का इलाज काफ़ी महँगा है, इसलिए ज़रूरी है कि शुरू में ही इन बीमारियों की जाँच करके इनकी रोकथाम की जाए।
मुँह और दाँतों की सफ़ाई शरीर के स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। भारत में बहुत‑से लोग मुँह से संबंधित रोगों से ग्रस्त हैं जैसे—दाँतों में खोड़, मसूड़ों के रोग, दाँतों का आकार बिगड़ना, मुँह का कैंसर आदि। सब जानते हैं कि दाँतों का इलाज काफ़ी महँगा है, इसलिए ज़रूरी है कि शुरू में ही इन बीमारियों की जाँच करके इनकी रोकथाम की जाए।
दाँत शरीर का एक जीवित अंग हैं। इनकी सबसे बाहर वाली सफ़ेद और सख़्त सतह को इनेमल (Enamel) कहते हैं। इसके अंदर के हिस्से को, जो इससे कम सख़्त होता है डैंटाइन (Dentine) कहते हैं। यह पल्प के इर्द‑गिर्द होता है, जिसमें दाँतों की नसें और ख़ून की नाड़ियाँ होती हैं। दाँत जबड़े की हड्डी में गड़े होते हैं जो बाहर से मसूड़ों द्वारा ढकी होती है। दाँत जीवन में दो बार आते हैं।
- दूध के दाँत
इनकी संख्या बीस होती है। ये 6 महीने की आयु से निकलने शुरू हो जाते हैं और दो साल तक बीस दाँत निकल आते हैं। इन्हें दूध के दाँत भी कहते हैं। ये प्रारंभिक दाँत 6 साल की आयु से गिरना शुरू होकर 12 साल तक गिर जाते हैं। इनकी जगह स्थायी दाँत आ जाते हैं। - स्थायी दाँत
इनकी संख्या 32 होती है। ये 6 साल की आयु से निकलना शुरू हो जाते हैं और 12‑13 साल तक 28 दाँत निकल आते हैं। बची हुई चार अक़्ल दाढ़ें (Wisdom teeth) आम तौर पर 18 से 24 साल तक निकलती हैं।
मीठा या नमकीन, कुछ भी खाएँ
खाने के बाद कुल्ला करना न भूलें
दाँतों की चार आम बीमारियाँ और उनकी रोकथाम
1. दाँतों की सड़नदाँतों की सड़न या दाँतों में कीड़ा लगना बच्चों और बड़ों, सबके दाँतों में हो सकता है।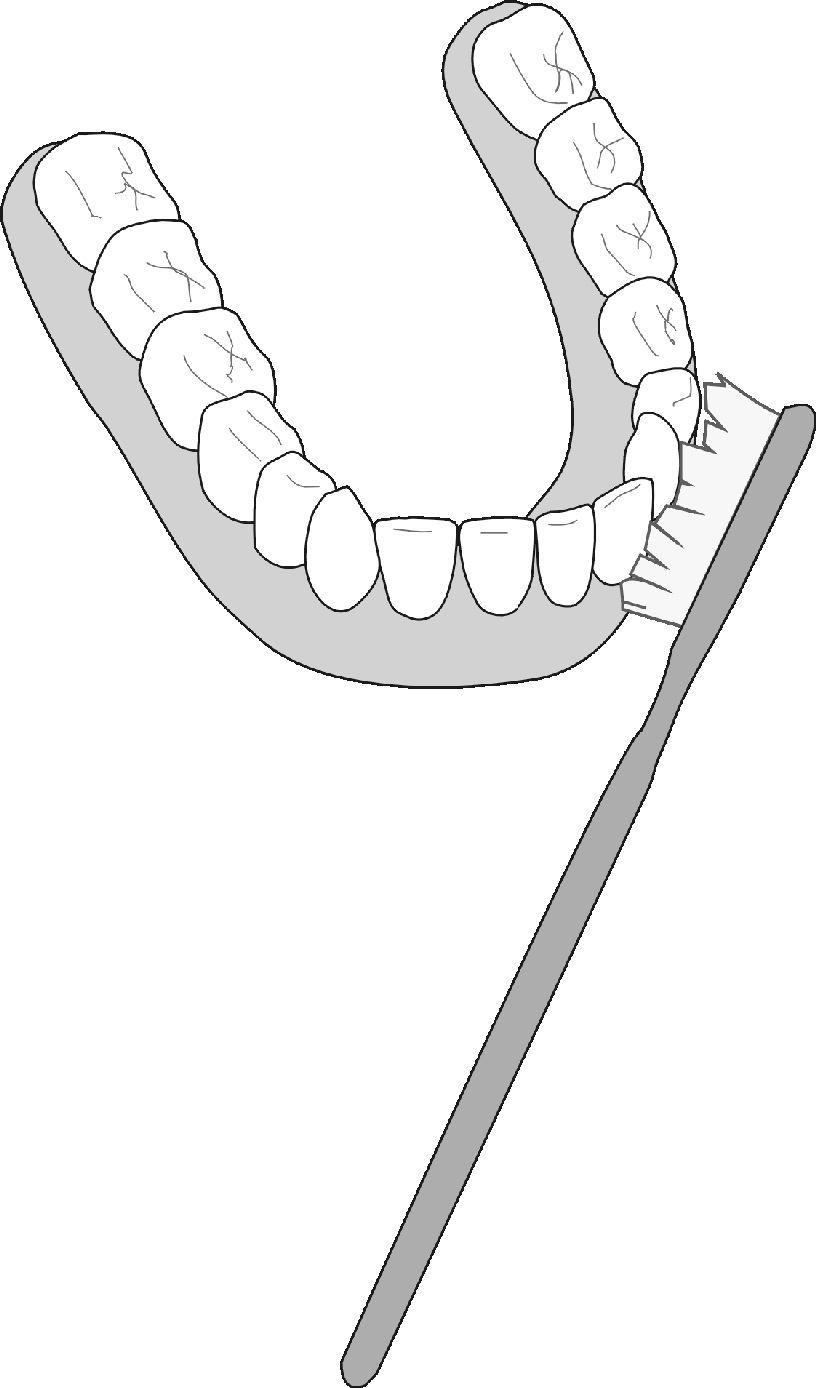 यह बीमारी आम तौर पर चबानेवाली सतह पर या दो दाँतों के बीच के जुड़े हुए स्थान के नीचे होती है।
यह बीमारी आम तौर पर चबानेवाली सतह पर या दो दाँतों के बीच के जुड़े हुए स्थान के नीचे होती है।
जब भोजन और भोजन के अवशेषों में पाए जानेवाले बैक्टीरिया दाँत की सतह के साथ चिपककर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो यह बीमारी उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति के मुँह में बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया दाँतों पर पाई जानेवाली लिसलिसी (slimy) और पारदर्शी तह में रहते हैं। इस लिसलिसी तह को प्लाक कहते हैं। जब मुँह में पड़े खाने के अवशेष बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो ख़मीर बनने (fermentation) की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया के कारण तेज़ाब बनता है जिससे दाँतों की सतह घुलनी शुरू हो जाती है और इस प्रकार दाँतों की सड़न शुरू हो जाती है।
2. मसूड़ों के रोग (Gingivitis)मसूड़ों के रोग प्लाक यानी पपड़ी जम जाने से भी हो जाते हैं। प्लाक में मौजूद बैक्टीरिया विषैला पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है। यदि प्लाक को नियमित रूप से न उतारा जाए तो यह सख़्त होकर टार्टर (tartar) यानी दाँतों की मैल बन जाता है।
दाँतों को मोतियों जैसा सफ़ेद रखने के लिए
दिन में दो बार ब्रश करें
दाँतों की सड़न और मसूड़ों के रोगों का प्रमुख कारण दाँतों में प्लाक का जमना है। इसलिए यदि प्लाक को जमने से रोक लिया जाए तो बीमारियों की रोकथाम हो सकती है। प्लाक इन तरीकों से रोका जा सकता है:
यांत्रिक विधियाँप्लाक को रोकने में यह तरीक़ा सबसे महत्त्वपूर्ण है। दाँतों में ब्रश पेस्ट के साथ करना है। 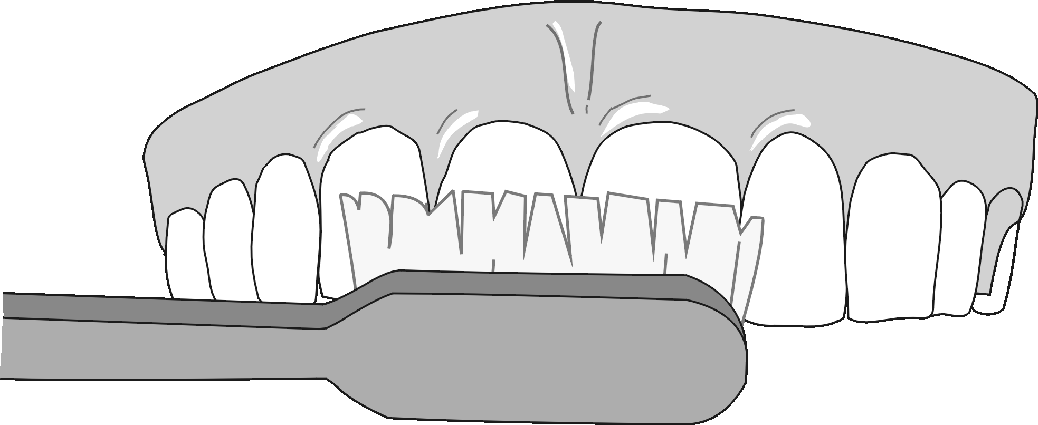 इनकी सफ़ाई का सबसे अच्छा तरीक़ा है कि ऊपर के दाँतों को ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे के दाँतों को नीचे से ऊपर की ओर साफ़ किया जाए। दाँतों को अंदर और बाहर, दोनों तरफ़ से साफ़ करना चाहिए। खाना चबानेवाली सतह को साफ़ करने के लिए ब्रश को गोलाकार घुमाएँ ताकि गड्ढों और दरारों की सफ़ाई ठीक से हो। ब्रश करने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करें, उँगली से जीभ को साफ़ करें और मसूड़ों की मालिश करें।
इनकी सफ़ाई का सबसे अच्छा तरीक़ा है कि ऊपर के दाँतों को ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे के दाँतों को नीचे से ऊपर की ओर साफ़ किया जाए। दाँतों को अंदर और बाहर, दोनों तरफ़ से साफ़ करना चाहिए। खाना चबानेवाली सतह को साफ़ करने के लिए ब्रश को गोलाकार घुमाएँ ताकि गड्ढों और दरारों की सफ़ाई ठीक से हो। ब्रश करने के बाद अच्छी तरह से कुल्ला करें, उँगली से जीभ को साफ़ करें और मसूड़ों की मालिश करें।
एक टाँका गर उखड़ जाए और जल्दी लगा लिया जाए,
तो दूसरे टाँके बच जाते हैं।
एक दाँत में गर पस पड़ जाए और जल्दी इलाज कर लिया जाए,
तो और सब दाँत बच जाते हैं।
कुछ रसायन जैसे कि क्लोरहैक्सीडाइन (chlorhexidine) और फ़्लोराइड (fluoride) बैक्टीरिया के प्लाक को कम करने में सहायक होते हैं। ये कुल्ला करनेवाली दवाइयों (mouth wash) के रूप में मिलते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए।
दाँतों की सड़न रोकने में आहार का योगदान दाँतों की सड़न में मीठे का बहुत योगदान है, इसलिए भोजन में मीठे की मात्रा कम लेनी चाहिए। ख़ासकर दो बार के भोजन के बीच में मीठे खाद्य पदार्थ, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट्स, मीठे बिस्कुट, केक, पेस्ट्रीज़, शीतल पेय और आइसक्रीम आदि का सेवन कम करें। मीठे का प्रयोग किसी मुख्य भोजन के साथ ही होना चाहिए। दो बार के भोजन के बीच में फल, सलाद, गिरियों, मकई, सब्ज़ियों और सैंडविच आदि का सेवन किया जा सकता है।
दाँतों की सड़न में मीठे का बहुत योगदान है, इसलिए भोजन में मीठे की मात्रा कम लेनी चाहिए। ख़ासकर दो बार के भोजन के बीच में मीठे खाद्य पदार्थ, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट्स, मीठे बिस्कुट, केक, पेस्ट्रीज़, शीतल पेय और आइसक्रीम आदि का सेवन कम करें। मीठे का प्रयोग किसी मुख्य भोजन के साथ ही होना चाहिए। दो बार के भोजन के बीच में फल, सलाद, गिरियों, मकई, सब्ज़ियों और सैंडविच आदि का सेवन किया जा सकता है।
मीठा खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ला करना चाहिए। दाँतों के अच्छे विकास के लिए विटामिन और खनिजों का महत्त्वपूर्ण योगदान है इसलिए बच्चों को छोटी आयु में ही कैल्शियम और विटामिन‑युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्तनपान करानेवाली माताओं को भी ऐसा ही आहार लेना चाहिए। छोटे बच्चों को रात के समय बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए।
सड़न! सड़न! सड़न!
दूर भाग जाओ!
मैं खाने के बाद ब्रश करती हूँ
जिससे मेरे दाँत हर समय सुरक्षित रहते हैं!!
फ़्लोराइड दाँतों को मज़बूत बनाते हैं और सड़न को रोकते हैं। फ़्लोराइड का प्रयोग करने का सबसे आसान तरीक़ा है कि फ़्लोराइड‑युक्त पेस्ट से ब्रश किया जाए। 6 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को फ़्लोराइड‑युक्त पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए।
मसूड़ों के रोगों की रोकथाम और उनका नियंत्रणहम जानते हैं कि सही तरीक़े से ब्रश करने से प्लाक और बैक्टीरिया कम होंगे और इससे मसूड़ों को भी फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिएँ:
- धूम्रपान न करें क्योंकि ज्यों‑ज्यों उम्र बढ़ती है, धूम्रपान से मसूड़े अस्वस्थ होते जाते हैं।
- खाने के बाद हर बार सादे पानी या माउथ वॉश (Mouth wash) से कुल्ला करें।
- उँगलियों से दाँतों और मसूड़ों की मालिश करें।
- दो दाँतों के बीच की जगह साफ़ करने के लिए डैंटल फ़्लौस या सिंगल‑टफ़्ट ब्रश या रबर टिप का प्रयोग करें।
- समय‑समय पर दाँतों के डॉक्टर से दाँत साफ़ करवाकर पॉलिश करवाएँ।
- 6 महीने में कम से कम एक बार दाँतों के डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
मैं रोज़ दो बार ब्रश करता हूँ
और धूम्रपान तो कभी नहीं करता।
तभी मेरे जीवन में प्लाक नहीं सिर्फ़ मुस्कराहट ही रहती है!
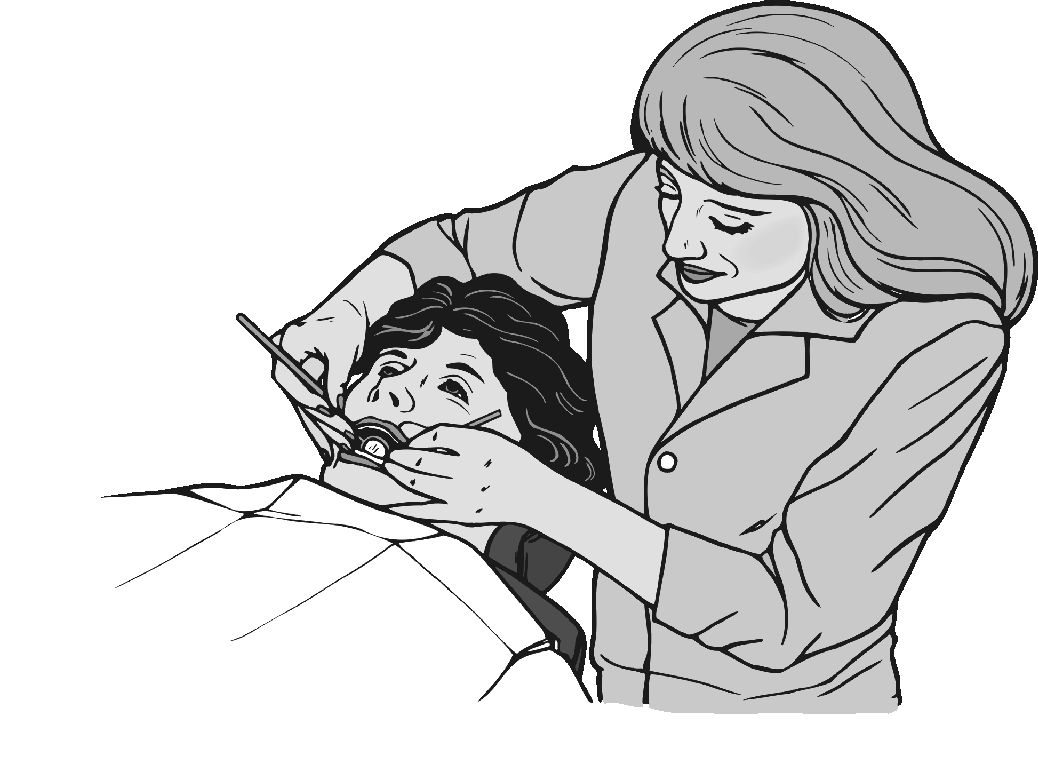 इस विकार में दाँत एक‑दूसरे के बहुत ज़्यादा क़रीब होते हैं या उनमें बहुत ज़्यादा ख़ाली जगह होती है; वे ज़्यादा आगे या ज़्यादा पीछे झुके होते हैं या टेढ़े‑मेढ़े होते हैं।
इस विकार में दाँत एक‑दूसरे के बहुत ज़्यादा क़रीब होते हैं या उनमें बहुत ज़्यादा ख़ाली जगह होती है; वे ज़्यादा आगे या ज़्यादा पीछे झुके होते हैं या टेढ़े‑मेढ़े होते हैं।
हमारे देश में लगभग 30‑40% बच्चों के दाँत टेढ़े‑मेढ़े होते हैं। इसके मुख्य कारण हैं—अँगूठा चूसना, जीभ बाहर निकालना और मुँह से साँस लेना। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है दाँतों की सड़न या किसी कारणवश दूध के दाँतों का जल्दी गिर जाना। दूध के दाँत स्थायी दाँतों के लिए उचित जगह बनाकर रखने में सहयोग देते हैं। दाँत यदि टेढ़े‑मेढ़े हों, तो इसके कारण सड़न या मसूड़ों के रोग और टैंपोरो‑मैंडीबुलर (Temporo-mandibular) यानी जोड़ में तकलीफ़ हो जाती है।
दाँतों के टेढ़ेपन की रोकथामदाँतों को इस रोग से बचाने के लिए ज़रूरी है कि दूध के दाँतों को सड़न से बचाया जाए और बच्चों को मुँह की सफ़ाई की आदत डाली जाए। यदि दूध के दाँत ज़्यादा समय तक रह गए हैं, तो उन्हें दाँतों के डॉक्टर की सलाह के अनुसार निकलवाना ही सही है।
4. मुँह का कैंसरभारत में यह तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जानेवाला कैंसर है। जो लोग ज़्यादा पान, सुपारी तथा तंबाकू चबाते हैं, धूम्रपान और मद्यपान करते हैं, उनको यह बीमारी अधिक होती है। इस बीमारी के अन्य कारण हैं:
- मुँह की सफ़ाई न रखना।
- मुँह में लंबे समय तक कोई चुभन रहना (जैसे खुरदरे दाँत, नक़ली दाँत और दाँतों की फ़िलिंग इत्यादि)।
मुँह के कैंसर का पता जल्दी नहीं चलता क्योंकि इस रोग के लक्षण शुरू में प्रबल नहीं होते। यदि आपको निम्नलिखित लक्षण दिखाई दें तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए:
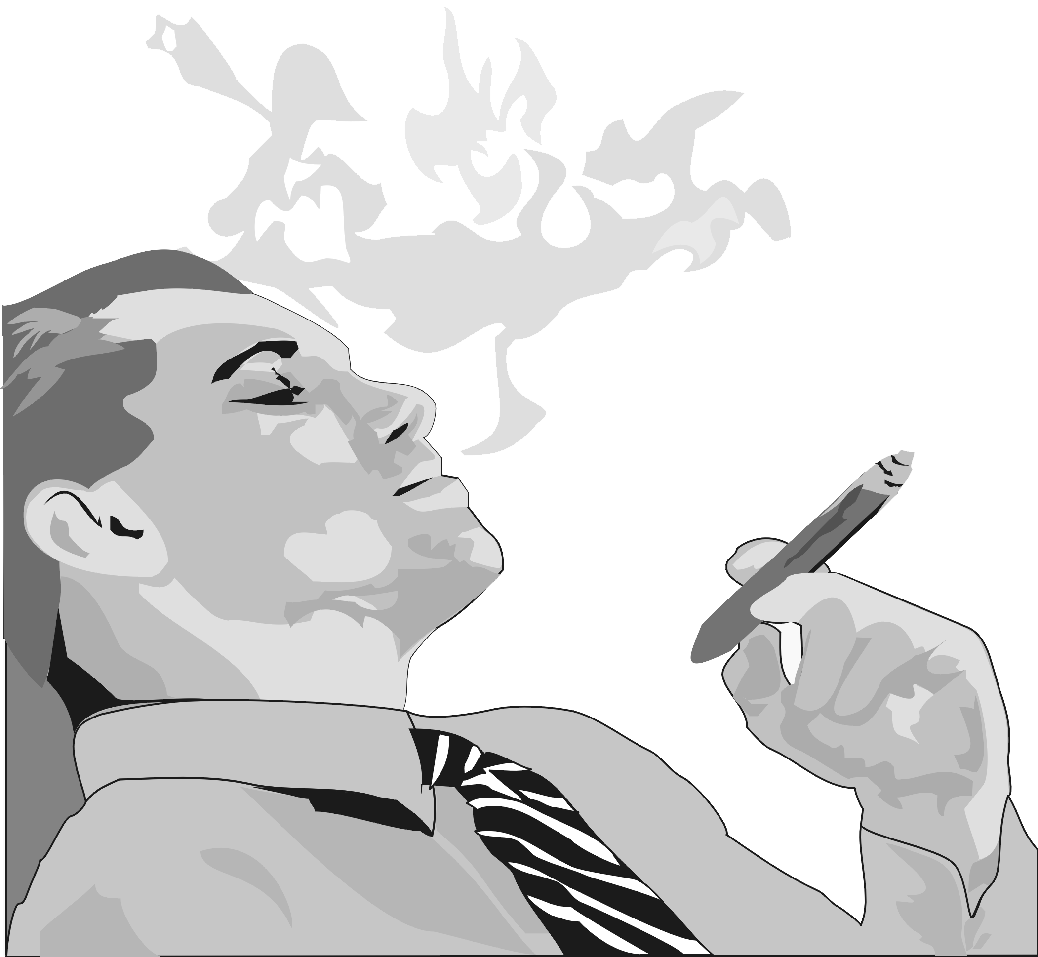
- दो हफ़्ते या उससे ज़्यादा समय से मुँह में कोई ज़ख़्म हो, जो ठीक न होता हो।
- मुँह में सफ़ेद या लाल रंग का उभरा हुआ धब्बा।
- मुँह खोलने में दिक़्क़त होना।
- मुँह में कोई उभार (Lump) या ग्रंथि (Growth) बनना।
- दाँतों का ज़्यादा ढीला हो जाना या बिना कारण ख़ून बहना।
- गले में ख़राश होना या ऐसा महसूस होना कि कुछ अटका हुआ है।
- चबाने और निगलने में दिक़्क़त होना।
- जीभ और मुँह के अन्य हिस्सों का सुन्न होना या संवेदना की कमी होना।
- आवाज़ का भारी होना या फटा स्वर।
सावधान! सावधान!! सावधान!!!
पान‑मसाला और गुटका चबानेवालो,
और बीड़ी‑सिगरेट पीनेवालो,
आप शायद कैंसर के अभिशाप को निमंत्रण दे रहे हैं।
- तंबाकू से बने हर पदार्थ से परहेज़ रखें। शराब से भी दूर रहें।
- अपनी जाँच ख़ुद करें ताकि कैंसर का संकेत देनेवाले घावों का जल्दी पता लग सके और उनका इलाज हो सके:
- अपने मुँह के अंदर की जाँच, अच्छी रोशनी में शीशे के सामने खड़े होकर दो मिनट में ठीक तरह से हो सकती है।
- दोनों होंठ, दोनों गाल, जीभ के आसपास का ऊपरी और नीचे वाला हिस्सा, मुँह का ऊपर और नीचे वाला हिस्सा तथा गले की अच्छी तरह से जाँच करें।
- ध्यान दें कि इनमें कहीं भी रंग और लिसलिसेपन में कोई बदलाव तो नहीं अथवा कहीं कोई सूजन, रसौली या फोड़ा तो नहीं है।
यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण मिलता है तो जल्द ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें।
शिशु के दाँतों की देखभालबच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। यदि हम बच्चों को बीमारियों से दूर रखेंगे, तो आनेवाली पीढ़ी स्वस्थ और प्रगतिशील होगी। गर्भवती महिलाओं और माताओं को यह जानकारी दी जानी चाहिए:
- पौष्टिक आहार महत्त्वपूर्ण है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार और संतुलित भोजन करना चाहिए ताकि बच्चे के साथ‑साथ उसके दाँतों तथा मसूड़ों का सही और स्वस्थ विकास हो सके।
- गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की राय के बिना किसी भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने डॉक्टर को अपने गर्भवती होने के बारे में बताना चाहिए ताकि उन्हें टेट्रासाइक्लीन (tetracycline) जैसी दवाएँ न दी जाएँ। इनसे बच्चों के दाँतों का रंग ख़राब हो सकता है।
- जन्म के समय बच्चे के मुँह में बैक्टीरिया नहीं होते। दरअसल जब माँ‑बाप बच्चे को प्यार से सहलाते और चूमते हैं तो बच्चे के मुँह में कीटाणु चले जाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि माता‑पिता अपना मुँह साफ़ रखें और बच्चे को मुँह पर चूमने से परहेज़ करें। एक दूसरे के चम्मच और बरतन इस्तेमाल करने से भी परहेज़ करें।
- ऐसा देखने में आया है कि छोटे बच्चों के दाँतों में सड़न होने का मुख्य कारण दूध की बोतल है। इसलिए माताओं को चाहिए कि वे बच्चे को पहले साल तक स्तनपान कराएँ और उसके बाद बोतल का प्रयोग करने के बजाय सीधे ही कप या चम्मच का इस्तेमाल करें।
- बच्चे को दूध पिलाने के बाद हर बार एक घूँट पानी पिलाना चाहिए ताकि मुँह में बचा बाक़ी दूध साफ़ हो जाए। उसके बाद बच्चे को पाँच से दस मिनट के लिए सीधा उठाकर पकड़ें।
- माँ को चाहिए कि दूध पिलाने के बाद हर बार एक साफ़, गीले, मुलायम सूती कपड़े से बच्चे के मसूड़ों और जीभ की सफ़ाई करे। साफ़ सूती कपड़े को पहले उबाल लें। फिर इसे उँगली पर लपेटकर ऊपरी और निचले मसूड़ों को एक ही बार में साफ़ करें। इसके बाद कपड़े की तह बदलकर जीभ को भी एक ही बार में साफ़ करें।
- जब बच्चे के मुँह में दूध के दाँत निकल आएँ तो बच्चों के नरम ब्रश का प्रयोग शुरू कर दें।
- जब बच्चों के दाँत निकल रहे होते हैं तो उन्हें मसूड़ों में खुजली महसूस होती है इसलिए वे मुँह में कोई न कोई वस्तु, खिलौने आदि डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी आदत से उन्हें संक्रमण हो सकता है जिससे दस्त लग सकते हैं। इसलिए माताओं को चाहिए कि अपने बच्चे की पूरी निगरानी रखें। बच्चे को रस्क (Rusk) या फल दे दिए जाएँ ताकि उन्हें खुजली से भी राहत मिले और वे चबाना भी सीखें।
- यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि दूध के दाँतों का पूरा ख़याल रखा जाए। यदि दूध के दाँतों में सड़न नहीं है तो इससे स्थायी दाँतों को एक स्वस्थ शुरुआत मिलती है और वे सही जगह पर निकलते हैं।
बच्चों में दंत‑रोगों की रोकथाम
1. दिन में दो बार ब्रश = स्वस्थ दाँत
2. संतुलित आहार = स्वस्थ दाँत
3. स्वस्थ दाँत = स्वस्थ शरीर
भोजन में मीठा कम = 32 दाँत सही‑सलामत
 बच्चों में गिरने से, खेलते समय चोट लगने से, साइकिल चलाते समय या सड़क दुर्घटनाओं के कारण चेहरे और मुँह पर चोट लगने के आसार ज़्यादा होते हैं। कभी‑कभी एक छोटी‑सी लापरवाही से गंभीर चोट लग जाती है जिससे बच्चे और उसके परिवार के जीवन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ बातों का ख़याल रखकर इन छोटे‑बड़े हादसों से बचा जा सकता है:
बच्चों में गिरने से, खेलते समय चोट लगने से, साइकिल चलाते समय या सड़क दुर्घटनाओं के कारण चेहरे और मुँह पर चोट लगने के आसार ज़्यादा होते हैं। कभी‑कभी एक छोटी‑सी लापरवाही से गंभीर चोट लग जाती है जिससे बच्चे और उसके परिवार के जीवन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ बातों का ख़याल रखकर इन छोटे‑बड़े हादसों से बचा जा सकता है:
- तीन साल तक का बच्चा जब चलना सीखता है तो उसकी पूरी सहायता करें।
- जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल में दोनों तरफ़ सप्पोर्ट स्टैंड (छोटे पहिए) लगवाएँ।
- बच्चे को समझाएँ कि जब वह सीढ़ियाँ चढ़ या उतर रहा हो तो अपने हाथ जेब में न डाले।
- बच्चे को सड़क‑सुरक्षा नियम सिखाएँ और देखें कि वह उनका पालन कर रहा है।
- जो दाँत कुछ ज़्यादा ही आगे की तरफ़ आ रहे हों, उन्हें दाँतों के डॉक्टर से ठीक करवाएँ।
- जो बच्चे या युवा खेलों में भाग लेते हैं, वे अपने चेहरे और दाँतों की सुरक्षा के लिए दाँतों के डॉक्टर से ख़ास सुरक्षा यंत्र बनवा सकते हैं।
यदि दाँत हैं स्वस्थ, तो ज़िंदगी है मस्त
माता और शिशु का स्वास्थ्य
भारत में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर अभी भी बहुत ज़्यादा है। पुस्तक के इस भाग का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं के मन से गर्भाधान, डिलीवरी और नवजात बच्चे की देखभाल से जुड़ी सभी भ्रांतियाँ और डर दूर करना है। दरअसल लोगों में गर्भावस्था और नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित बुनियादी जानकारी की कमी है जिसकी वजह से उनके मन में कई प्रकार का डर समाया रहता है। यदि हम माँ और शिशु की देखभाल के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियाँ बरतें तो अनेक माताओं और बच्चों की ज़िंदगी बचा सकते हैं।
गर्भावस्था के दौरान देखभाल माँ और उसके होनेवाले बच्चे की अच्छी सेहत के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि बच्चे की देखभाल उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि हर गर्भवती स्त्री को अपनी देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। इन छोटी‑छोटी बातों का ख़याल रखना चाहिए:
माँ और उसके होनेवाले बच्चे की अच्छी सेहत के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि बच्चे की देखभाल उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि हर गर्भवती स्त्री को अपनी देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए। इन छोटी‑छोटी बातों का ख़याल रखना चाहिए:
- अपने गर्भधारण का पता चलते ही आप पास के किसी अस्पताल, डिस्पेंसरी, हेल्थ सेंटर या सब‑सेंटर में गर्भ के देखभाल वाले क्लीनिक (ए.एन.सी./Antenatal Clinic) में अपना नाम दर्ज करवा लें।
- डॉक्टर की सलाह के अनुसार समय‑समय पर इस क्लीनिक में जाएँ। आपको इस क्लीनिक में कम से कम तीन बार जाँच करानी चाहिए: पहली बार अपना नाम दर्ज करवाते समय, दूसरी बार गर्भावस्था के 24‑28 सप्ताह के बीच और तीसरी बार बच्चा पैदा होने की तारीख़ से 3‑4 हफ़्ते पहले। इस क्लीनिक में हर बार आपकी ऊँचाई, भार और ब्लड प्रेशर मापा जाएगा। इसके साथ‑साथ हीमोग्लोबिन, पेशाब की जाँच इत्यादि की जाएगी।
- जिन महिलाओं को गर्भ संबंधी गंभीर समस्या हो, उन्हें ए.एन.सी. में ज़्यादा बार जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के दौरान तकलीफ़ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। गर्भ संबंधी गंभीर समस्या की श्रेणी में वे महिलाएँ आती हैं जिनमें नीचे दिए गए कोई भी लक्षण मौजूद हों:
- 18 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा आयु।
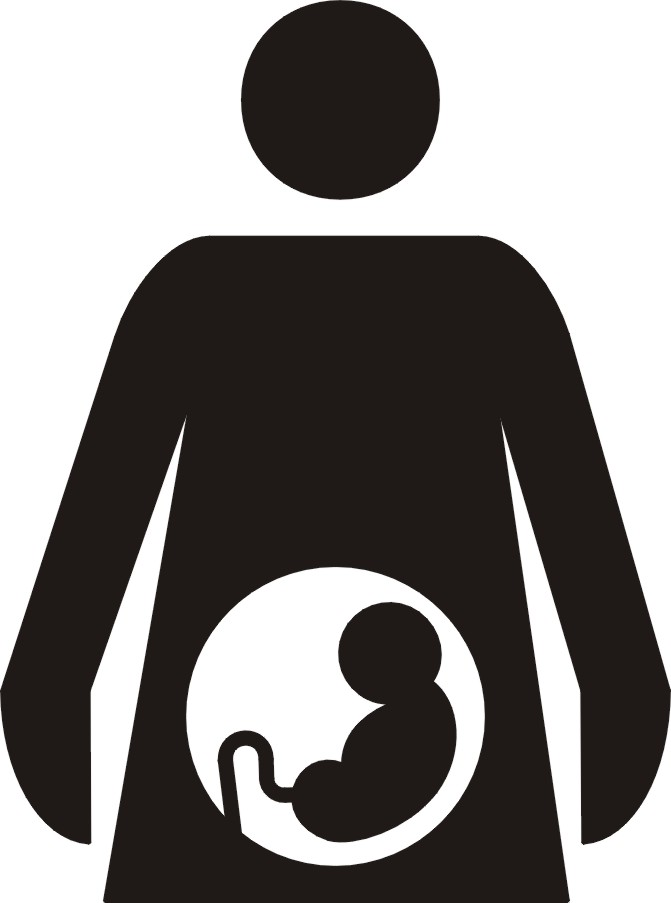 140 सेंटीमीटर या इससे कम ऊँचाई।
140 सेंटीमीटर या इससे कम ऊँचाई।- गर्भावस्था के दौरान योनि से ख़ून बहना या पेट में दर्द होना (यह गर्भपात होने के ख़तरे का संकेत है)।
- गर्भावस्था के दौरान अनीमिया (ख़ून की कमी), पैरों में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर और पेशाब में प्रोटीन आना (प्री‑एकलैंपसिया) या दौरे पड़ना (एकलैंपसिया)।
- गर्भ में जुड़वाँ बच्चे हों।
- इस गर्भ से पहले आपका बच्चा ऑपरेशन द्वारा या फ़ोरसेप्स से हुआ हो।
- बच्चा गर्भ में असामान्य स्थिति (Abnormal Position) में हो।
- माँ को हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे का रोग, मधुमेह, टी. बी. या लिवर की बीमारी हो।
- माँ की आयु तीस वर्ष से ज़्यादा हो और वह पहली बार गर्भवती हुई हो।
- गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्सॉयड (टी.टी.) के टीके ज़रूर लगवाने चाहिएँ। यदि आप पहली बार गर्भवती हुई हैं तो 4‑6 सप्ताह के अंतराल पर दो बार टेटनस के टीके लगवाएँ। ये टीके गर्भावस्था में कभी भी लगवाए जा सकते हैं। ये टीके टेटनस जैसी जानलेवा बीमारी से आपको और आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं।
- यदि आपने दूसरी बार गर्भ धारण किया है और यह पहले गर्भ धारण के तीन साल के अंदर ठहरा है और यदि आपने पहली बार टेटनस के दोनों टीके लगवाए थे, तो आपको इस बार सिर्फ़ एक ही टीका लगवाना है। लेकिन यदि पहली बार दो टीके नहीं लगे थे तो इस बार दो टीके लगवाने ज़रूरी हैं।
- गर्भावस्था के पहले तीन महीने में फ़ोलिक एसिड की गोलियाँ खाएँ और उसके बाद आयरन, फ़ोलिक एसिड, और कैल्शियम की गोलियाँ लेती रहें ताकि गर्भ के दौरान अनीमिया (ख़ून की कमी) से बचा जा सके। (याद रखें कि यदि आपको पहले से ही ख़ून की कमी है तो आपको आयरन और फ़ोलिक एसिड दोनों गोलियाँ लेने की ज़रूरत है।)
- रात को कम से कम आठ घंटे की नींद लें और यदि संभव हो तो दोपहर को भी दो घंटे आराम करें।
- धूम्रपान या शराब का सेवन न करें। यह भी ध्यान रखें कि आपके आसपास भी कोई धूम्रपान न करता हो।
- डॉक्टर से पूछे बताए बिना कोई दवा न खाएँ। साथ ही अपनी मरज़ी से एक्स‑रे या अल्ट्रासाउंड जैसी जाँच न करवाएँ। ये ख़तरनाक हो सकते हैं।
- अपने आपको साफ़ और स्वच्छ रखें।
- अपने स्तन साफ़ रखें, उन्हें रोज़ धोएँ। यदि स्तन के निप्पल अंदर की तरफ़ मुड़े हुए हैं, तो इस समस्या का अभी समाधान करें। उन्हें हलके से बाहर की तरफ़ खींचें और कुछ समय तक ऐसे ही खींचे रखें। दिन में 5‑6 बार ऐसा करें।
- गर्भावस्था के पहले तीन महीने और आख़िरी 6 सप्ताह में यौन‑संबंध न बनाएँ।
- नीचे लिखे लक्षणों के प्रति सावधान रहें। ये ख़तरनाक हो सकते हैं। इनका तुरंत इलाज करवाएँ:
- लगातार सिरदर्द
- नज़र कमज़ोर होना या धुँधला दिखाई देना
- एड़ियों के आसपास सूजन
- पेट दर्द
- योनि से ख़ून बहना या पानी जैसे द्रव का बहुत ज़्यादा बहना
- बच्चा पैदा होने की अनुमानित तारीख़ से कुछ सप्ताह पहले ही डिलीवरी की तैयारी कर लें। यह बेहद ज़रूरी है कि डिलीवरी किसी कुशल डॉक्टर/नर्स द्वारा एक साफ़ और सुरक्षित जगह पर हो।
- अपने नज़दीकी अस्पताल की जानकारी हासिल करें, ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में आपको वहाँ ले जाया जा सके। किसी गाड़ी का पहले से ही इंतज़ाम करना ना भूलें।
- संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। गर्भ धारण करने से पहले आप जितना खाना खाती थीं, गर्भ के दौरान उससे डेढ़ गुणा भोजन खाएँ। याद रखें, यदि आप पौष्टिक आहार लेंगी तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी अच्छी ख़ुराक मिलेगी और जन्म के वक़्त उसका वज़न अच्छा होगा। अपने भोजन में आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, विटामिन के लिए मौसम के ताज़े फल, ताक़त के लिए गुड़ और प्रोटीन के लिए चने, मटर तथा दालों का सेवन करें। ये सब शरीर की ताक़त के लिए ज़रूरी हैं। अगर हो सके तो दिन में आधा लीटर यानी दो गिलास दूध भी ज़रूर पिएँ।
भोजन में आयरन का अंश
| भोजन में आयरन की मात्रा 5 मिलिग्राम/100 ग्राम से अधिक | |
|---|---|
| पूरे गेहूँ का आटा | हरे केले |
| व्हीट जर्म (Wheat germ) | भिस (कमल ककड़ी) |
| दलिया | तरबूज़ |
| राइस फ़्लेक्स (पोहा) | बादाम |
| बाजरा | किशमिश |
| सूखे मटर | तिल |
| सोयाबीन | कलौंजी |
| राजमा | इमली का गूदा |
| लोबिया | धनिये के बीज |
| दालें | जीरा |
| चने की दाल | अजवायन |
| साबुत चने | अमचूर |
| भुने हुए चने | हल्दी पाउडर |
| चने के पत्ते | मुनक्का |
| अरबी के पत्ते | गुड़ |
| फूल गोभी के पत्ते | प्याज़ के पत्ते |
| सरसों के पत्ते | शलगम के पत्ते |
| मूली के पत्ते | |
| जन में आयरन की मात्रा 5 मिलिग्राम/100 ग्राम से कम | |
|---|---|
| ज्वार | हरे मटर |
| मकई | बथुआ के पत्ते |
| जौ | सेम की फलियाँ |
| चावल | सेब |
| रागी | आमला |
| पालक | काजू |
| मेथी | चीकू |
| चौलाई | |
जन्म के समय देखभाल
डिलीवरी का स्थान
- हो सके तो पहली डिलीवरी अस्पताल में करवाएँ।
- यदि डिलीवरी घर में होनी हो तो किसी कुशल नर्स/दाई/डॉक्टर द्वारा होनी चाहिए। कमरा साफ़‑सुथरा, हवादार, हलका गरम और ज़रूरत के मुताबिक़ रोशनी वाला होना चाहिए। चारपाई, चटाई और कंबल आदि का इस्तेमाल करने से पहले इन्हें धूप लगवा लें।
- बच्चा पैदा करने में सहायता करनेवाले के हाथ साफ़ होने चाहिएँ। उसके नाख़ून कटे हों और डिलीवरी से पहले साबुन और साफ़ पानी से हाथ धो लेने चाहिएँ। उसे अपने हाथ पोंछने नहीं चाहिएँ और न ही किसी चीज़ को छूना चाहिए।
- डिलीवरी साफ़ जगह या साफ़ बिस्तर पर होनी चाहिए।
- नाल (Umbilical cord) को बाँधने के लिए साफ़ धागे का इस्तेमाल करें।
- नाल को काटने के लिए नए और साफ़ ब्लेड का प्रयोग करें।
- नाल पर कुछ न लगाएँ। इसे साफ़ रखें।
- डॉक्टर, दाई या नर्स को सूचित करें।
- नीचे लिखा सामान तैयार रखें: नया ब्लेड, साबुन, धागा, दस्ताने, (दाई द्वारा इस्तेमाल करके फेंके जानेवाला सामान), बच्चे को लपेटने के लिए साफ़ कपड़ा, माँ के लिए सेनिटरी नैपकिन, रुई और कपड़े की पट्टी और गरम पानी।
- डिलीवरी की दर्द के दौरान काफ़ी मात्रा में तरल पदार्थ पिएँ।
- दर्द के शुरुआती दौर में पैदल चलें।
- जब पानी की थैली फट जाए तो बैड पर लेटकर लंबी‑लंबी साँस लें।
- पेट को बाहर से न दबाएँ और न ही पेट के बल लेटें।
- पानी की थैली को ब्लेड या नाख़ून से न फोड़ें।
- बच्चे को जल्दी पैदा करने के लिए कोई टीका न लगवाएँ।
- डिलीवरी की दर्दों के बीच के समय में बच्चे को नीचे धकेलने की कोशिश न करें।
- बच्चे को ज़बरदस्ती बाहर न खींचें।
- योनि की जाँच बार‑बार न करवाएँ।
- पैदा होने पर स्वच्छ और मुलायम कपड़े से बच्चे को साफ़ करें।
- कपड़े की दो तह करके बच्चे को उसमें लपेटें और माँ के बग़ल में लिटाएँ। माँ के शरीर की गरमी बच्चे को गरम रखेगी।
- बच्चे के पैदा होने के आधे घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर दें। बच्चे को सीधी हवा न लगने दें। यदि बच्चे का भार कम है (2.5 किलोग्राम से कम) तो उसे जन्म के एक सप्ताह तक न नहलाएँ।
- ध्यान रखें कि बच्चे की देखभाल सिर्फ़ एक या दो लोग ही करें।
यदि माँ और बच्चे में इनमें से कोई भी ख़तरे का लक्षण दिखाई दे तो उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाएँ:
- बच्चा पैदा होने से पहले या बाद में योनि से अत्यधिक रक्त बहना।
- अगर डिलीवरी के दर्द को शुरू हुए 24 घंटे हो जाएँ और फिर भी बच्चा पैदा न हो।
- बच्चे का हाथ या पैर पहले बाहर आए।
- यदि योनि से गंदा द्रव्य निकले।
- डिलीवरी के दौरान माँ को दौरे पड़ें।
- माँ को पेट में अत्यधिक दर्द हो या त्वचा पीली पड़ जाए या साँस ठीक से न आए।
- बच्चे का रंग पीला या नीला हो या वह रोता न हो।

- बच्चे को जन्म देने के बाद माँ के लिए पौष्टिक भोजन बहुत ज़रूरी है।
- आयरन, कैल्शियम की गोलियाँ लेते रहें और प्रोटीनयुक्त भोजन लें।
- दूध और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें।
- सही समय पर बच्चे का टीकाकरण करवाएँ।
- 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ़ माँ का दूध ही दें। दूध पिलाने से पहले स्तनों के निप्पल और उसके आसपास की जगह को साफ़ करें।
- रोज़ाना स्नान करें और 6‑8 घंटे बाद पैड बदलते रहें।
- बच्चा पैदा होने के 6 सप्ताह के अंदर माँ को कम से कम तीन बार नर्स या दाई से या अस्पताल में जाँच ज़रूर करवानी चाहिए।
- बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर‑अंदर माँ को बहुत तेज़ बुख़ार होना और योनि से दुर्गंधपूर्ण स्राव होना।
- बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर योनि से अत्यधिक ख़ून आना।
- सिरदर्द और उलटी आना या दौरे पड़ना।
- बच्चा पैदा होने के 40 दिन के अंदर पेट में अधिक दर्द रहना।
नवजात बच्चे की देखभाल गर्भ से ही शुरू हो जाती है। डिलीवरी अस्पताल में या कुशल दाई के हाथों घर में करवाएँ। इसके अलावा:
- पैदाइश के समय बच्चे को साँस लेने में दिक़्क़त हो तो साँस लेने में उसकी सहायता करें। (देखें पृ.47 पर पाँचवा नंबर)
- सामान्य से कम तापमान वाले बच्चे की देखभाल।
- बच्चे को कोई संक्रमण (Infection) होने से बचाव।
- साधारण से कम वज़नवाले (2.5 किलोग्राम से कम) बच्चों की देखभाल।
- गंभीर समस्या वाले नवजात शिशु की पहचान।
- 95% बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं। उनकी त्वचा का रंग गुलाबी होता है और वे आसानी से साँस लेते हैं। उनके दिल की धड़कन 120‑160 प्रति मिनट होती है। ऐसे बच्चे को एक साफ़ और मुलायम कपड़े से पोंछकर गरम कपड़े में लपेट दें और स्तनपान के लिए माँ के पास लिटा दें।
- कुछ बच्चे जन्म लेने के बाद रोते नहीं और साँस भी अनियमित रूप से लेते हैं। उनकी त्वचा का रंग नीला या पीला होता है। उनके दिल की धड़कन 100 प्रति मिनट से कम होती है या फिर सुनाई ही नहीं देती। इसका मतलब है कि बच्चे को साँस लेने में कहीं रुकावट हो रही है।
- बच्चे को शरीर गरम रखनेवाली मशीन (Warmer) या बल्ब के नीचे लिटा दें।
- बच्चे को करवट देकर लिटाएँ ताकि द्रव्य आसानी से बाहर आ सके।
- यदि संभव हो तो थूक खींचने वाले यंत्र से द्रव्य को बाहर निकालें। बच्चे का मुँह, नाक और गला साफ़ करें ताकि साँस की नली में कोई रुकावट न हो।
- साँस की नली की सफ़ाई के बाद बच्चा आराम से साँस लेता है और उसके बाद रो भी पड़ता है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा न हो, तो उँगलियों से उसके पैरों के तलवों या पीठ को धीरे-धीरे मलें।
- मुँह से मुँह लगाकर बच्चे को साँस दें। अपने गालों में हवा भरके बच्चे के मुँह में हवा भरें। ज़्यादा ज़ोर न लगाएँ क्योंकि बच्चों के फेफड़े बहुत छोटे व कोमल होते हैं।
- यदि ये सभी उपाय काम न करें, तो बच्चे को तुरंत पास के अस्पताल ले जाएँ।
- बच्चे को उलटा न करें।
- बच्चे को मुँह के बल न लिटाएँ।
- बच्चे की पीठ पर ज़ोर से न थपथपाएँ।
- बच्चे का पेट न दबाएँ।
- बच्चे पर गरम या ठंडा पानी न छिड़कें।
 Iइस रोग में नवजात बच्चे के शरीर का तापमान कम हो जाता है। उसका शरीर सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए गरमी पैदा नहीं कर सकता। यदि इसका इलाज न किया जाए तो शरीर का तापमान बहुत जल्दी गिर जाता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। बग़ल का तापमान लेकर इसका पता लगाया जा सकता है (सामान्य तापमान 98.40 F होता है)।
Iइस रोग में नवजात बच्चे के शरीर का तापमान कम हो जाता है। उसका शरीर सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए गरमी पैदा नहीं कर सकता। यदि इसका इलाज न किया जाए तो शरीर का तापमान बहुत जल्दी गिर जाता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। बग़ल का तापमान लेकर इसका पता लगाया जा सकता है (सामान्य तापमान 98.40 F होता है)।
यदि हथेलियाँ और तलवे ठंडे हों, लेकिन छाती और पेट गरम हों, तो यह ठंड का बुरा प्रभाव है।
हाइपोथर्मियायदि शरीर के सभी अंग ठंडे हों तो बच्चे को हाइपोथर्मिया है। आम तौर पर स्वस्थ नवजात बच्चे की त्वचा छूने में गरम और देखने में गुलाबी होती है।
हाइपोथर्मिया की रोकथाम- बच्चे के पैदा होते ही उसे साफ़, गरम तौलिए से पोंछें।
- फिर उसे सिर से पैर तक गरम, सूखे तौलिए या रुई में लपेटें।
- नवजात बच्चे को माँ के साथ लिटाएँ।
- कमरा हलका गरम होना चाहिए और पंखे बंद कर दें।
- यदि गरम करनेवाली मशीन (Warmer) उपलब्ध हो, तो बच्चे को उसमें लिटा दें, नहीं तो 200 वॉट के बल्ब से डेढ़ फ़ुट दूर लिटा दें। कमरे को हीटर से गरम रखें या गरम पानी की बोतल इस्तेमाल करें।
- बच्चे को माता के स्तनों के बीच (कंगारू की तरह) रखें।
जब बच्चा पैदा होता है तो उसे संक्रमण का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है; बच्चों की मौत का यही सबसे बड़ा कारण है।
- प्रत्येक गर्भावस्था के दौरान टेटनस टॉक्सॉयड (Tetanus Toxoid) के दो टीके ज़रूर लगवाएँ।
- जहाँ डिलीवरी होनी है, वह जगह साफ़, हवादार और अच्छी रोशनीवाली होनी चाहिए।
- डिलीवरी में सहायता करनेवाली नर्स को पहले अपने हाथ पानी और साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिएँ।
- नाल (कॉर्ड) की देखभाल बहुत ज़रूरी है। इसे एक साफ़ और नए ब्लेड से काटें, कीटाणुरहित धागे से बाँधकर साफ़ और सूखा छोड़ दें।
- जिस किसी ने भी बच्चे की देखभाल करनी हो उसे अपने हाथ अच्छी तरह (कम से कम एक मिनट के लिए) धोने चाहिएँ।
- बच्चे के नाख़ून काटें।
- बच्चे को कम से कम 6 महीने तक स्तनपान करवाएँ।
- नवजात बच्चे को साफ़ कपड़े पहनाएँ।
- बच्चे का टीकाकरण करवाएँ।
- बच्चे को शहद, चाय, गुड़, पानी या घुट्टी और बोतल का दूध न दें।
- किसी बीमार व्यक्ति को नवजात बच्चे को उठाने या सँभालने न दें।
- बच्चे को भीड़ वाली जगह पर न लेकर जाएँ।
- जहाँ नवजात शिशु हो, उस कमरे में बहुत से लोगों को न जाने दें।
नवजात बच्चे का सामान्य वज़न 2.5 किलोग्राम होता है। यदि बच्चे का भार जन्म के समय इस से कम है, तो उसे ‘कम वज़न वाला बच्चा’ माना जाता है। जिन बच्चों का भार 2.0 से 2.5 किलोग्राम के बीच होता है उनकी देखभाल घर पर ही की जा सकती है, लेकिन जिनका वज़न 2 किलोग्राम से भी कम होता है उन्हें अस्पताल में रखने की ज़रूरत पड़ सकती है।
कम वज़न वाले बच्चों की घर पर देखभाल- पहले सप्ताह में बच्चे को रोज़ाना गीले कपड़े से साफ़ करें। सप्ताह के अंत में उसे नहलाएँ।
- यदि शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाए तो इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को गरम कपड़ों में लपेटकर रखें या माता के शरीर के साथ लिटाएँ। कंगारू की तरह, बच्चे को माता के स्तनों के बीच लिटाएँ।
- बच्चे को साफ़ और हवादार कमरे में लिटाएँ, कमरे को हलका गरम रखें।
- बच्चे को सिर्फ़ स्तनपान ही कराएँ। कम से कम हर दो घंटे बाद दूध ज़रूर दें क्योंकि बच्चा थोड़ा‑सा दूध पीने के बाद जल्दी थक जाता है।
- यदि बच्चा स्तनपान न कर पाता हो तो स्तनों से दूध निकालकर बच्चे के मुँह में डालें या किसी कटोरी में डालकर चम्मच से पिलाएँ।
- ध्यान रखें कि बच्चे को दस्त या फेफड़ों का संक्रमण न होने पाए। यदि दस्त लगें, तो बच्चे को ओ.आर.एस. (oral rehydration solution) का घोल दें और जल्द ही डॉक्टर के पास ले जाएँ।
- कमज़ोर बच्चे संक्रमणों का शिकार जल्दी होते हैं इसलिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है।
- बच्चे को कम से कम लोग उठाएँ। बीमार लोगों को बच्चे के पास न आने दें।
भविष्य में माँ बननेवाली महिलाओं को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:
- बारह साल की आयु के बाद लड़कियाँ ताक़त (आयरन) की गोलियों का सेवन शुरू कर दें।
- 21 वर्ष की आयु से पहले गर्भ धारण न करें।
- गर्भावस्था में सामान्य से ज़्यादा भोजन करें और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम न करें।
- धूम्रपान और शराब का सेवन न करें।
- दिन में कम से कम दो घंटे आराम करें और रात को आठ घंटे नींद ज़रूर लें।
- गर्भावस्था के पहले तीन महीने केवल फ़ोलिक एसिड और उसके बाद आयरन, फ़ोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियाँ लेते रहें।
- गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर से कम से कम तीन बार जाँच ज़रूर करवाएँ।
- ख़ून की कमी (अनीमिया), हाई ब्लड प्रेशर और ख़ून बहने का पता लगते ही तुरंत अस्पताल जाएँ।
- दो बच्चों के जन्म में कम से कम तीन साल का अंतर ज़रूर रखें।
यदि बच्चे में निम्नलिखित में से कोई भी लक्षण हो, तो उसे अस्पताल ले जाएँ:
- जन्म के समय बच्चे का वज़न 1 किलो 800 ग्राम से कम हो, या पूरे समय से पहले डिलीवरी हो।
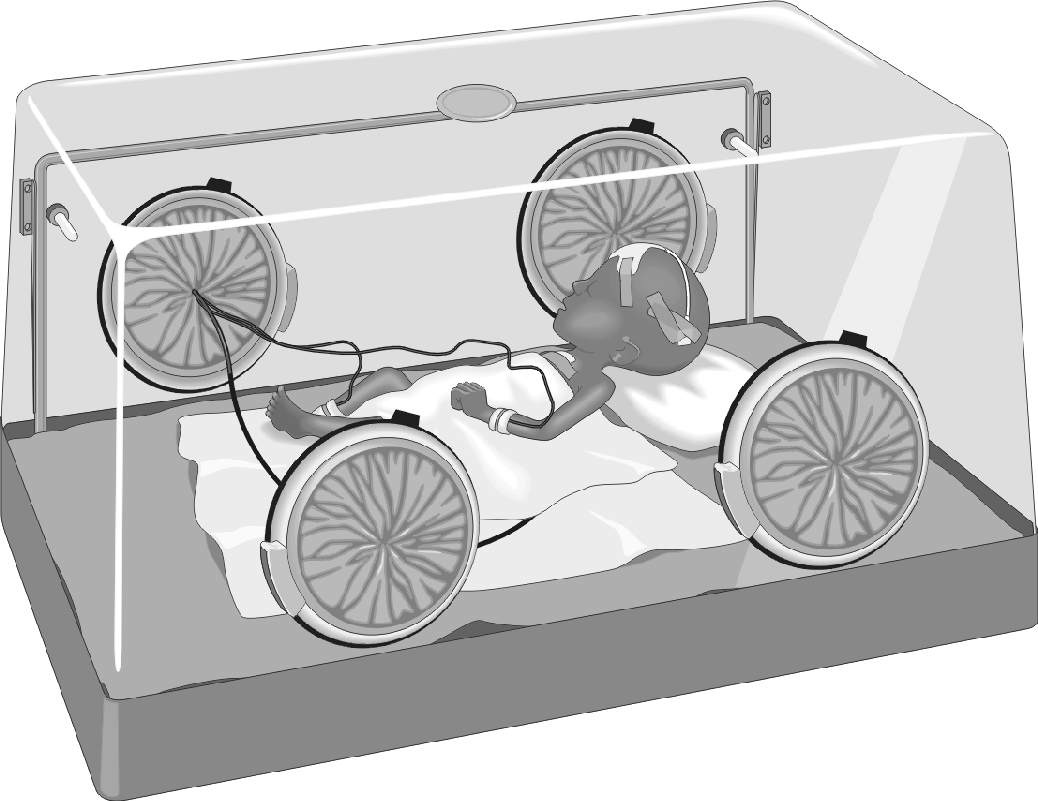 साँस मुश्किल से आ रही हो या साँस लेने में तकलीफ़ हो।
साँस मुश्किल से आ रही हो या साँस लेने में तकलीफ़ हो।- बच्चा स्तनपान न कर पा रहा हो।
- बच्चे को झटके या दौरे आ रहे हों।
- बच्चे को ज्यादा नींद आती हो या बहुत ज़्यादा रोता हो।
- बच्चे का चेहरा सफ़ेद/पीला लगे।
- बच्चे को बुख़ार हो या उसका शरीर ठंडा हो।
- कहीं से भी ख़ून निकल रहा हो।
- बच्चे का पेट फूला हुआ हो या उसे उलटियाँ आएँ।
- उसकी नाल से पस निकल रही हो।
- बच्चे में कोई जन्मजात दोष हो।
- माँ का दूध पहले 6 महीने बच्चे के लिए संतुलित आहार है। बच्चे को माँ का पहला दूध (Colostrum) ज़रूर दें, क्योंकि इसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है।
- पैदा होने के आधे घंटे से दो घंटे के बीच या जितना जल्दी हो सके, स्तनपान शुरू कर दें।
- जब बच्चा दूध के लिए रोए, तब या हर दो घंटे में स्तनपान कराएँ।
- पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ़ स्तनपान ही कराएँ।
- बच्चे को पानी, घुट्टी या बोतल का दूध न दें।
- जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो धीरे‑धीरे स्तनपान कम बार करवाएँ। उसे तरल आहार, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी और लस्सी देना शुरू कर दें। उसके बाद कुछ गाढ़ा आहार जैसे दलिया, खिचड़ी, सूजी की खीर, उबालकर मसले हुए आलू, मसला हुआ केला और घर में बनाया हुआ सैरेलैक खिलाएँ। माँ का दूध भी देते रहें।
- शुरू‑शुरू में यह सब दिन में तीन से चार बार दें।
- धीरे‑धीरे इनकी मात्रा बढ़ा दें और भोजन ज़्यादा बार दें।
- नौ महीने की आयु से उसे वे सब खिलाएँ जो आप अपने लिए पकाते हैं।
- डेढ़ साल के बच्चे को एक बड़े आदमी के भोजन की आधी मात्रा खानी चाहिए।
नवजात बच्चे में इन लक्षणों का ध्यान रखें:
- बच्चे का शरीर ठंडा हो या बुख़ार और कंपन हो।
- साँस तेज़ और मुश्किल से आती हो।
- बच्चा दूध न ले पा रहा हो या खाना नहीं खा पा रहा हो।
- बच्चा सामान्य से ज़्यादा सोता हो और उसे जगाने में मुश्किल होती हो।
- जब बच्चा आराम से लेटा हो तो छाती अंदर की तरफ़ खिंची हो यानी जब बच्चा अंदर साँस भरे, तो छाती और पेट के बीच में खिंचाव के कारण गड्ढा नज़र आता हो।
- जब बच्चा आराम से लेटा हो तो छाती से सीटी जैसी आवाज़ आती हो।
- तरल पदार्थ ख़ूब दें।
- माँ का दूध देते रहें।
- बच्चे को गरम रखें।
- बच्चे को साफ़ और धुएँ से रहित कमरे में रखें।
- यदि ऊपर दिए गए लक्षणों में से कोई नज़र आए तो बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएँ।
- यदि इनमें से कोई लक्षण नज़र आए तो कोई घरेलू नुसख़ा न दें।
- बच्चे को किसी नीम‑हकीम डॉक्टर के पास न लेकर जाएँ।
 बच्चे को टी.बी., डिप्थीरिया, काली खाँसी, टेटनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस‑बी जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे का इन रोगों से बचने के लिए टीकाकरण नहीं करवाया गया है, तो वह विकलांग हो सकता है या कमज़ोरी से उसकी मौत भी हो सकती है।
बच्चे को टी.बी., डिप्थीरिया, काली खाँसी, टेटनस, पोलियो, खसरा और हेपेटाइटिस‑बी जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे का इन रोगों से बचने के लिए टीकाकरण नहीं करवाया गया है, तो वह विकलांग हो सकता है या कमज़ोरी से उसकी मौत भी हो सकती है।
टीकाकरण की समय सूची
| 1. | जन्म के समय | बी.सी.जी. और ओ.पी.वी. (पोलियो) की ज़ीरो ख़ुराक |
| 2. | 1½ महीना होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. की पहली ख़ुराक + हेपेटाइटिस बी की पहली ख़ुराक |
| 3. | 2½ महीना होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. की दूसरी ख़ुराक + हेपेटाइटिस बी की दूसरी ख़ुराक |
| 4. | 3½ महीना होने पर | हेपेटाइटिस बी की तीसरी ख़ुराक |
| 5. | 9 महीना होने पर | खसरा और विटामिन‑ए की पहली ख़ुराक |
| 6. | 16 – 24 महीना होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. बूस्टर + विटामिन‑ए की दूसरी ख़ुराक |
| 7. | 2 साल होने पर | विटामिन‑ए की तीसरी ख़ुराक |
| 8. | 2½ साल होने पर | विटामिन‑ए की चौथी ख़ुराक |
| 9. | 3 साल होने पर | विटामिन‑ए की पाँचवीं ख़ुराक |
| 10. | 4½ to 5 साल होने पर | डी.पी.टी. और ओ.पी.वी. बूस्टर+हेपेटाइटिस बी बूस्टर |
| 11. | 10 & 16 साल होने पर | टेटनस टॉक्सॉयड (टी.टी.)+ हेपेटाइटिस बी बूस्टर |
- 0‑5 साल के सभी बच्चों को पल्स पोलियो कार्यक्रम के दौरान ओ.पी.वी. की दो बूँदें ज़रूर देनी चाहिएँ।
- टीकाकरण बेहद ज़रूरी है और जन्म के पहले साल में ही हो जाना चाहिए।
- दस्त लगने से बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे मृत्यु भी हो सकती है।
- यदि बच्चा स्तनपान न कर रहा हो तो बच्चे को तरल पदार्थ ज़्यादा दें, जैसे नारियल पानी, नीबू पानी, हलकी चाय, छाछ, सूप, खिचड़ी, हलकी दाल, दलिया, पके हुए चावल, उबालकर मसले हुए आलू।
- ओ.आर.एस. (Oral rehydration solution) यानी जीवन रक्षक घोल दें।
- माँ का दूध पिलाते रहें।
- यदि दो हफ़्ते से ज़्यादा दस्त चलें या साथ में ख़ून आए तो डॉक्टर से मिलें।
- जब बच्चा दस्त के बाद ठीक हो तो उसे अगले दो हफ़्ते तक सामान्य भोजन के अलावा एक और बार अतिरिक्त भोजन ज़रूर दें।

- बच्चे की उलटियाँ और दस्त पर क़ाबू न पाया जा सके।
- दस्त में ख़ून आए।
- बच्चा कुछ खा‑पी न रहा हो।
- बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आती हो और उसे जगाना मुश्किल हो।
- बच्चा पानी की कमी के कारण बेहोश हो गया हो।
- बच्चा धीमे‑धीमे रोता हो, आँखों से आँसू न आएँ, मुँह और होंठ सूखे हों।
- त्वचा में लचीलापन कम हो।
- आँखें धँसी हुई हों और सिर का ऊपरी हिस्सा धँसा हो (बच्चे के सिर की हड्डी में नरम जगह)।
- पेशाब कम आए।
- केवल माँ का दूध दें: बच्चे को पहले 6 महीने में घुट्टी या बोतल से दूध न दें।
- भोजन और पीने के पानी को ढककर मक्खियों से बचाकर रखें।
- बच्चे को साफ़–सुथरा रखें और उसके नाख़ून नियमित रूप से काटते रहें।
- खाने से पहले और शौच के बाद साबुन और साफ़ पानी से हाथ धोएँ।
कुपोषण (Malnutrition)
कुपोषण के कारण- सातवें महीने से पहले स्तनपान बंद करना।
- ठीक से सफ़ाई न होना/पौष्टिक आहार की कमी।
- पेट में कीड़े होना।
- बार‑बार दस्त आना या छाती में संक्रमण होना।
- बच्चे का वज़न या क़द ठीक तरह न बढ़ना।
- उम्र के हिसाब से वज़न कम होना।
- पूरे शरीर में सूजन या बहुत पतला होना।
- त्वचा में बार‑बार संक्रमण, जैसे फोड़े, फुंसी आदि।
- बच्चे को ऐसी चीज़ें खाने की आदत, जो खाने लायक़ नहीं हैं—जैसे मिट्टी, काग़ज़, चॉक, पेंसिल, बाल आदि।
- प्रोटीन से भरपूर भोजन करना।
- पेट के कीड़ों का इलाज करवाना।
- पौष्टिक आहार जैसे घर में बना सैरेलैक:
- 250 ग्राम भुने हुए चने + 100 ग्राम मुरमुरे लें।
- इनको अलग‑अलग पीसें और छान लें।
- आपस में मिलाकर, सील बंद डिब्बे में रखें।
- एक कटोरी दूध में इस मिश्रण के चार चम्मच और चीनी डालकर खिलाएँ।
- शादी 18 साल की उम्र के बाद होनी चाहिए।
- 21 साल की उम्र से पहले गर्भाधान करना माँ और बच्चे, दोनों की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है।
- 10‑14 साल की लड़कियों को हर दूसरे दिन आयरन की गोली खानी चाहिए ताकि ख़ून की कमी (अनीमिया) से बचा जा सके।
- अगर लड़की की शादी होने तक और गर्भ होने तक आयरन की गोली दी जाए तो अनीमिया और कम वज़न के बच्चे होने की समस्या को रोका जा सकता है। आयरन की गोली हफ़्ते में तीन बार हर नव-विवाहित लड़की को भी देनी चाहिए जब तक वह गर्भ धारण न करे।
- आयरनयुक्त आहार लेने से अनीमिया की रोकथाम हो सकती है। साग, पालक, चौलाई, मेथी, मूली, अंकुरित दालों का सेवन करें।
- लोहे के बरतनों में खाना पकाना भी लाभदायक है।
- माहवारी के दौरान सफ़ाई का ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है। सैनेटरी नैपकिन का प्रयोग प्रजनन‑प्रणाली के संक्रमण की रोकथाम के लिए ज़रूरी है।
स्वास्थ्य और सफ़ाई
 विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी या दुर्बलता का न होना ही नहीं है बल्कि यह पूर्ण रूप से शारीरिक तथा मानसिक तंदुरुस्ती और सामाजिक कुशलता का नाम है। हर स्वस्थ इनसान सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक उत्तम जीवन जी सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी या दुर्बलता का न होना ही नहीं है बल्कि यह पूर्ण रूप से शारीरिक तथा मानसिक तंदुरुस्ती और सामाजिक कुशलता का नाम है। हर स्वस्थ इनसान सामाजिक और आर्थिक तौर पर एक उत्तम जीवन जी सकता है।
- स्वस्थ और विकसित बालक।
- स्वस्थ और आकर्षक नौजवान।
- स्वस्थ और सफल बालिग़।
- स्वस्थ और सक्रिय बुज़ुर्ग।
स्वस्थ रहकर आप ज़िंदगी की उँचाइयों को छू सकते हैं—
स्वास्थ्य की जानकारी सफलता में मदद करती है।
जीवन शैली से भाव है हम कैसे रहते हैं, हम क्या खाते‑पीते हैं, कौन‑से शारीरिक काम करते हैं और कौन‑सी अच्छी‑बुरी आदतें अपनाते हैं। यदि हमारी जीवन शैली अच्छी है तो हम बीमार कम पड़ेंगे और हमेशा चुस्त और बलवान रहेंगे। जीवन शैली बेढंगी होने से हमारी उम्र कम हो सकती है और बीमार और असहाय होने के कारण हमारा जीवन कठिन हो सकता है।
स्वस्थ जीवन आपके हाथ में है—अच्छा भोजन लें, नियमित रूप से व्यायाम करें, तंबाकू तथा शराब से दूर रहें। हम अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इन अच्छी आदतों के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपने आप से और अपने परिवार से स्वस्थ जीवन की शुरुआत के बाद हम समाज को भी स्वस्थ बनाने में सहायता कर सकते हैं।
आइए हम सब स्वस्थ जीवन का आनंद लें!
आपका स्वास्थ्य आपकी निजी ज़िम्मेदारी है!
आपकी देखभाल आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता!
- क्या मेरा आहार मेरे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है?
- क्या मेरे शरीर को उचित व्यायाम मिलता है?
- क्या तंबाकू से मेरे शरीर को नुकसान होता है?
इन सवालों के जवाब पाने के लिए आगे पढ़ें।
स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप| अच्छे दिखेंगे: | आपका शरीर सुडौल, मांसपेशियाँ मज़बूत, आँखों में चमक और त्वचा तथा बाल सुंदर होंगे। |
| अच्छा महसूस करेंगे: | आप में ज़्यादा चुस्ती होगी, आप अच्छी तरह सोएँगे और तनाव से मुक्त रहेंगे। |
| खुश रहेंगे: | आप अपना काम और पढ़ाई बेहतर ढंग से कर सकेंगे और अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ ज़िंदगी ख़ुशी‑ख़ुशी बिता सकेंगे। |
आप ऐसा कर सकते हैं—ज़िंदगी का पूरा आनंद लीजिए।
स्वस्थ रहना सीखो! स्वास्थ्य‑लाभ कमाओ।
आज भी और कल भी
ख़ुद अर्जित कर सकते हो स्वास्थ्य तुम,
पर उधार नहीं ले सकते।
- बुरी आदतें न अपनाना।
- बुरी आदतों को छोड़ देना।
- अच्छी आदतें अपनाना।
हमारे देश में दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कैंसर, साँस की समस्याएँ और दिमाग़ी बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। अच्छी आदतों को अपनाकर और बुरी आदतों को छोड़कर इन बीमारियों की रोकथाम के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। बचपन में अच्छी आदतें अपनाना आसान होता है। इससे हम जीवन में आगे चलकर अस्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। यदि हम इक्कीसवीं सदी में अपनी और अपने देश की सफलता चाहते हैं तो हमें अपना अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए जो ज़िंदगी भर हमारा साथ देगा। अपनी उचित देखभाल से (संतुलित भोजन खाकर, चुस्त रहकर और धूम्रपान न करके) हमें अच्छा लगेगा और हमें अधिक काम करने और खेलने की शक्ति मिलेगी।
स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?हृदयरोग, मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर से बचें।
जीवन का आनंद लेने के लिए स्वस्थ बनें।
अपना वज़न अपने क़द के अनुसार रखें ताकि आप मोटे न हों।
ध्यान रखें कि बढ़ी हुई तोंद सेहत के लिए ख़तरनाक है।
मूलमंत्र हैं: नियमित दिनचर्या, संतुलन, संतोष और विविधता
- भोजन सीमित मात्रा में नियमित अंतराल में खाएँ
 क्या आप जानते हैं कि जो लोग दिन में सिर्फ़ एक या दो बार ही भोजन करते हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ने या मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है? इससे कहीं बेहतर है दिन में कई बार थोड़ी‑थोड़ी मात्रा में खाएँ। सुबह या शाम के नाश्ते में कभी नागा न डालें। सुबह और शाम के भोजन के अलावा फल खाएँ और सब्ज़ियों के सैंडविच लें।
क्या आप जानते हैं कि जो लोग दिन में सिर्फ़ एक या दो बार ही भोजन करते हैं, उन्हें दिल का दौरा पड़ने या मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है? इससे कहीं बेहतर है दिन में कई बार थोड़ी‑थोड़ी मात्रा में खाएँ। सुबह या शाम के नाश्ते में कभी नागा न डालें। सुबह और शाम के भोजन के अलावा फल खाएँ और सब्ज़ियों के सैंडविच लें। - अपनी उम्र के अनुसार सही भोजन करें
बच्चे एक बार में बड़ों जितना खाना नहीं खा सकते। सारे दिन में वे काफ़ी शक्ति भी इस्तेमाल करते हैं। इस शक्ति को बनाए रखने के लिए उन्हें दिन भर थोड़ी‑थोड़ी मात्रा में भोजन और स्नैक्स खाने चाहिएँ। लेकिन इसके साथ इस बात का ख़याल भी रखें कि कभी ज़रूरत से ज़्यादा न खाएँ।
- शारीरिक गतिविधि के अनुसार भोजन करें
भोजन शरीर का ईंधन है। ज़्यादा शारीरिक काम करनेवाले लोगों को ज़्यादा और कम शारीरिक काम करनेवालों को कम भोजन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोगों की शक्ति की खपत उनके शारीरिक काम से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए, एक बढ़ई और डाकिया, जो शारीरिक रूप से ज़्यादा काम करते हैं, उन्हें एक क्लर्क या अधिकारी की अपेक्षा ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है, क्योंकि क्लर्क और अधिकारी अधिकतर बैठकर ही कार्य करते हैं।
- बाहर का खाना कम खाएँ
ढाबे या रेस्तराँ में खाना खाने की अपनी आदत न बना लें, क्योंकि इससे अंटशंट खाने का सेवन बढ़ जाता है। इस भोजन में घी‑तेल, मसाले और नमक अधिक होता है। संभव है कि यह खाना साफ़‑सुथरे ढंग से न बना हो और इसमें कुछ हानिकारक पदार्थों की मिलावट भी हो, जैसे कि मिठाई में रंग या रसायन का इस्तेमाल।
आवश्यक भोजन—अन्न जैसे चावल, रोटी, डबलरोटी—ये खेल और काम के लिए शक्ति देते हैं।
शरीर के विकास के लिए भोजन—दालें, राजमा, दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही और पनीर (जो कम वसा वाले दूध या बिना वसा वाले दूध से बना हो), मेवे, मग्ज़, गिरियाँ इत्यादि जो विकास में मदद करते हैं क्योंकि उनमें प्रोटीन होता है।
चेहरे पर निखार लानेवाले भोजन—फल और सब्ज़ियों से विटामिन, खनिज (Mineral) और फ़ाइबर (Fibre) प्राप्त होते हैं।

- ताज़े फल और सब्ज़ियाँ
इनसे विटामिन, खनिज (Mineral) और फ़ाइबर (Fiber) प्राप्त होते हैं।
- रेशेदार पदार्थ (फ़ाइबर)
फल और सब्ज़ियों के अलावा हमें अन्न (जैसे आटा और दलिया) से भी फ़ाइबर मिलता है। सब्ज़ियों से मिलनेवाले फ़ाइबर से हमें भोजन अच्छी तरह पचाने में सहायता मिलती है। ये मधुमेह, दिल के दौरे तथा कई क़िस्म के कैंसर को रोकने में भी सहायक होते हैं। इनसे ख़ून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी सीमित रहती है।
- चिकनाई
अच्छे विकास और स्वास्थ्य के लिए वसा, जैसे घी और तेल बेहद महत्त्वपूर्ण है। लेकिन भोजन में वसा का अधिक मात्रा में सेवन करने से मोटापा, दिल का दौरा या कई तरह के कैंसर होने का ख़तरा भी रहता है। इसलिए तली हुई चीज़ों, प्रोसेस्ड चीज़, मक्खन, मलाई, आइसक्रीम और चॉकलेट का सेवन कम मात्रा में और कभी‑कभी करें।
- चीनी, चाशनी
मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने से दाँत ख़राब हो जाते हैं और उनमें सड़न आ जाती है। इनसे मोटापा और आलस्य भी बढ़ता है। हालाँकि आपको बढ़ने और काम करने के लिए शक्ति की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप रोटी, चावल, आलू और अरबी जैसे मिश्रित कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा लें और साधारण चीनी से परहेज़ रखें तो यह बेहतर होगा। खाने के बाद मीठी चीज़ें कम लेना और दूध, कॉफ़ी और चाय में चीनी कम या न डालना ही अच्छा है।
- नमक
ज़्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर का ख़तरा बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा और लक़वा होने का प्रमुख कारण है। अपने भोजन में नमक की मात्रा कम रखें क्योंकि हमें इतने नमक की ज़रूरत नहीं है जितना कि हम लेते हैं। खाना बनाते समय नमक का प्रयोग कम करें तथा खाते समय ऊपर से और नमक न डालें। अचार, चटनियाँ, पापड़, चिप्स और नमकीन इत्यादि में बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसलिए ये कम खाने चाहिएँ।
खाना बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें:
- फल और सब्ज़ियों को खाने, काटने और पकाने से पहले अच्छी तरह धोएँ।
- फल और सब्ज़ियों को काटने के बाद कभी न धोएँ, क्योंकि इससे विटामिन और खनिज पदार्थ नष्ट हो जाते हैं।
- कच्ची सब्ज़ियों का सेवन ज़्यादा करें क्योंकि इनसे विटामिन, खनिज और फ़ाइबर अधिक मात्रा में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित पदार्थों का सेवन फ़ाइबर प्रदान करता है:
- बिना छाने हुए आटे का इस्तेमाल करें।
- सेब, चीकू, अमरूद आदि का सेवन छिलके के साथ ही करें।
- सफ़ेद ब्रैड और नान के बजाय तंदूरी रोटी और चपाती खाएँ, क्योंकि नान मैदे से बनता है और इसमें फ़ाइबर बहुत कम होता है।
- फलों के रस के बजाय ताज़े फलों का सेवन करें।
- कोला जैसी सॉफ़्ट ड्रिंक के बजाय फलों का रस पीना कहीं बेहतर है।
- फलों के रस के बजाय पूरा फल खाना बेहतर है।
- भाप से पकाना, बेकिंग या भूनकर खाना पकाना, उबालने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे खाने के पोषक तत्त्व कम नष्ट होते हैं।
- तलने से खाने में चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मोटापा, हृदय‑रोग और मधुमेह जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। तलने से खाने के पोषक तत्त्व भी नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, वड़ा खाने से इडली खाना बेहतर है क्योंकि वड़ा तला जाता है, इसलिए इसमें काफ़ी वसा होती है, जबकि इडली को भाप में पकाया जाता है जिस कारण इसमें वसा नहीं होती।
- इसी तरह चिकनाई से परहेज़ करने के लिए तले हुए आलू के चिप्स की जगह भुनी हुई मूँगफली खानी चाहिए। मूँगफली को भूनते समय कम तेल का इस्तेमाल करें।
- पालक और तोरई जैसी सब्ज़ियों में क़ुदरती तौर पर नमक होता है, इसलिए इन्हें पकाते समय कम नमक का इस्तेमाल करें।
- नमक का सेवन कम करने के लिए खाने में ऊपर से नमक न छिड़कें।
 काम करने और जीवन का आनंद लेने के लिए शरीर में बल होना चाहिए। शरीर को यह शक्ति भोजन से मिलती है। लेकिन यदि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे तो हमारे शरीर पर चर्बी बढ़ जाएगी। शारीरिक विकास तथा काम करने, पढ़ाई, व्यायाम करने और बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति के साथ‑साथ पोषण की भी ज़रूरत होती है।
काम करने और जीवन का आनंद लेने के लिए शरीर में बल होना चाहिए। शरीर को यह शक्ति भोजन से मिलती है। लेकिन यदि हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाएँगे तो हमारे शरीर पर चर्बी बढ़ जाएगी। शारीरिक विकास तथा काम करने, पढ़ाई, व्यायाम करने और बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति के साथ‑साथ पोषण की भी ज़रूरत होती है।
कुछ खाद्य पदार्थ आपको काम करने की शक्ति तो देते हैं लेकिन विकास या चेहरे पर निखार लानेवाले पौष्टिक तत्त्व इनमें कम होते हैं। जिस खाने में पोषक तत्त्वों की कमी हो, वह हमें मोटा कर सकता है, थका सकता है और अस्वस्थ भी बना सकता है। पोषण से भरपूर खाना जैसे अनाज, दूध, फल, सब्ज़ियाँ और दालों से हमें बढ़ने की शक्ति मिलती है और शरीर तेजस्वी बनता है। हाई कैलोरीयुक्त खाद्य पदार्थ जैसे सॉफ़्ट ड्रिंक, चिकनाई वाला भोजन और चॉकलेट किसी ख़ास मौक़े पर ही खाएँ और इनका सेवन कम मात्रा में करें।
आहार में पोषक तत्त्वों के मुख्य शाकाहारी स्रोत
| पोषक तत्त्व | आहार |
|---|---|
| शक्ति/बल | अनाज, दालें, कंदमूल, वसा और तेल, चीनी और गुड़। |
| प्रोटीन | दूध और दूध से बने पदार्थ, दालें, मेवे और गिरियाँ। |
| वसा/चिकनाई | मक्खन, घी, वनस्पति तेल, वनस्पति घी, मेवे और गिरियाँ। |
| कार्बोहाइड्रेट | अनाज, दालें, चीनी और गुड़, जड़ें, कंदमूल जैसे आलू, गाजर आदि। |
| रेशा/फ़ाइबर | हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, फल, बिना छना अनाज, दालें और फलियाँ। |
| कैल्शियम | दूध और दूध से बने पदार्थ, रागी, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ। |
| आयरन | हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, राइस-फ़्लेक्स, गेहूँ का आटा, दालें। |
| विटामिन‑ए, बीटा कैरोटीन और विटामिन‑बी | मक्खन, घी, दूध, गाजर, रागी, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, पपीता, आम। |
| विटामिन‑बी कॉम्पलेक्स | दूध, हाथ से कूटकर निकाला गया चावल (मोटा चावल), गेहूँ, साबुत चने, दालें, हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ, मेवे और गिरियाँ। |
| विटामिन‑सी | आमला, नीबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, सलाद के पत्ते, अंकुरित दालें। |
| विटामिन‑डी | दूध, सूर्य की रोशनी। |
| आयोडीन और स्वास्थ्य |
|---|
|
आयोडीन के मुख्य स्रोत : आयोडाइज़्ड नमक और केल्प (सुखाया हुआ समुद्री शैवाल (Seaweed)) हैं। दही, गाय का दूध और स्ट्राबेरी भी इसके अच्छे स्रोत हैं। आयोडीन की कमी से यह बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं: फ़ाइब्रोसिस्टिक—छाती की बीमारी, घेंघा गोइटर (Goiter), हाइपरथायरॉयडिज़्म, (Hyperthyroidism) हाइपोथायरॉयडिज़्म (Hypothyroidism) और बार‑बार गर्भपात का होना। |
- नियमित समय पर भोजन लें, आप एक बार में ज़्यादा न खाएँ।
- भोजन करने के बीस मिनट बाद आपकी भूख मिटती है। थोड़ा कम खाने के लिए छोटे ग्रास लें, उन्हें अनेक बार चबाएँ और धीरे धीरे खाएँ।
- कच्ची या पकी हुई सब्ज़ियाँ और फल फ़ाइबर देते हैं जिससे पेट जल्दी भर जाता है और आप संतुष्ट भी महसूस करते हैं।
- व्यस्त रहें, ख़ाली रहने से कुछ न कुछ खाने का मन करता रहता है।
| आहार की जानकारी |
|---|
शक्ति से भरपूर खाद्य पदार्थ: ये हमें ज़्यादा कैलोरीज़ देते हैं लेकिन वे पोषक तत्त्व नहीं देते जो हमें स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं—चॉकलेट, आइसक्रीम, आलू के चिप्स, सॉफ़्ट ड्रिंक आदि। पौष्टिक खाद्य पदार्थ: ये हमें शक्ति के साथ‑साथ बढ़ने और आभायुक्त होने के लिए कैलोरीज़ और पोषक तत्त्व भी देते हैं। पोषक तत्त्वों से भरपूर ऐसे भोजन हैं: रोटी, चावल, दालें, राजमा, सब्ज़ियाँ, फल, दूध और दूध से बने पदार्थ। |
सफ़ाई की आदत
हाथ धोने से हम स्वस्थ रहते हैं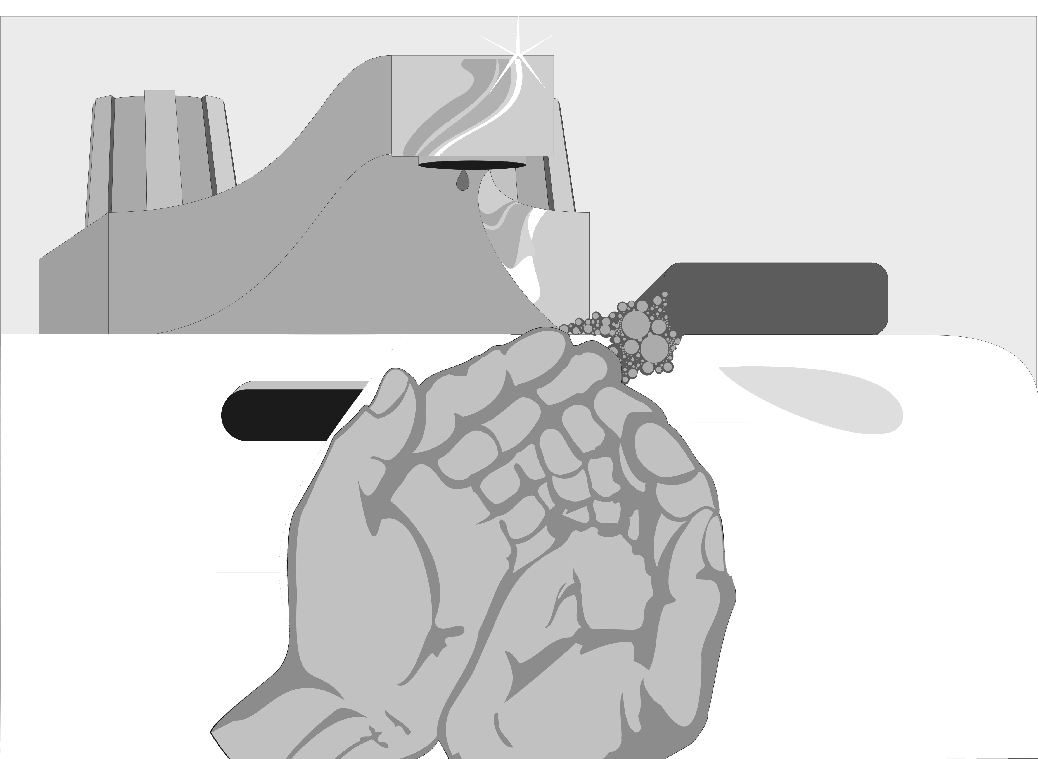
हमारे हाथों में हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस चिपक सकते हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हाथ धोना सबसे अच्छा तरीक़ा है। यह आदत सबके लिए ज़रूरी है। ध्यान रखें कि रसोई में काम करनेवाले अपने हाथ ज़रूर धो लें।
- हाथों को गुनगुने पानी की धार में धोएँ।
- गीले हाथों पर साबुन लगाएँ।
- 5 से 10 सेकंड साबुन को अच्छी तरह हथेलियों पर, उनके पिछले भाग पर और उँगलियों के बीच में मलें।
- नाख़ून साफ़ करने के लिए ब्रश का प्रयोग करें।
- चलते पानी की धार में हाथों को अच्छी तरह धोएँ।
- साफ़ तौलिए से हाथों को पोंछें।
- शौचालय जाने के बाद।
- बच्चे को शौचालय ले जाने के बाद।
- बच्चे के नैपकिन बदलने के बाद।
- अपना नाक साफ़ करने के बाद।
- किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करने से पहले और उसके बाद।
- खाने से पहले तथा खाने के बाद।
खाँसते या छींकते समय मुँह और नाक को ढकने से बीमारी से बचा जा सकता है
खाँसते और छींकते समय मुँह और नाक को रूमाल से ढकें। यदि आपके पास रूमाल न हो तो कुहनी के अंदर के भाग का इस्तेमाल करते हुए छींकें और खाँसें, परंतु हाथों का इस्तेमाल न करें क्योंकि इन्हीं हाथों से हम खाना खा लेते है और अन्य लोगों को छूते हैं। ऐसा करने से हवा के ज़रिए फैलनेवाली बीमारियों, जैसे फ़्लू, ज़ुकाम, तपेदिक आदि से बचाव होता है।
सार्वजनिक जगह पर थूकने से बीमारियाँ फैलती हैंथूकना एक बुरी आदत है क्योंकि इससे वातावरण दूषित होता है। थूक में कीटाणु (बैक्टीरिया और वायरस) होते हैं जो बीमारियाँ फैलाते हैं।
आपकी सेहत आपके हाथ में है- खुली जगह, ख़ाली ज़मीन और पार्क आदि में कूड़ा न फेंकें।
- अपनी सहूलियत के लिए कूड़ा फेंकने की अनुचित जगह न बनाएँ। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।
- कूड़ेदान के आसपास कूड़ा न फेंकें।
- स्कूल, कॉलेज इत्यादि की दीवारों के पास कूड़ा न फेंकें।
- अपने घरों की दीवारों के पीछे कूड़ा फेंककर अस्वच्छ वातावरण पैदा न करें।
- झाड़ियों या मलबे के ढेर पर कूड़ा न फेंकें।
- अपने घर में काम करनेवालों को कूड़ा नियमित स्थान पर ही फेंकने की शिक्षा दें।
- अपने आसपास का वातावरण साफ़ रखें।
- अपने घर/दुकान आदि में कूड़ेदान रखें।
- सोने से पहले अपनी रसोई के कूड़ेदान को ख़ाली करें।
- स्कूल जानेवाले बच्चों को अपनी और आसपास के वातावरण की सफ़ाई के बारे में शिक्षा दें।
- कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकें, उसके आसपास नहीं।
- अपने मुहल्ले के सफ़ाई कर्मचारी और स्वास्थ्य इंस्पेक्टर को सहयोग देकर सहायता करें।
तंबाकू
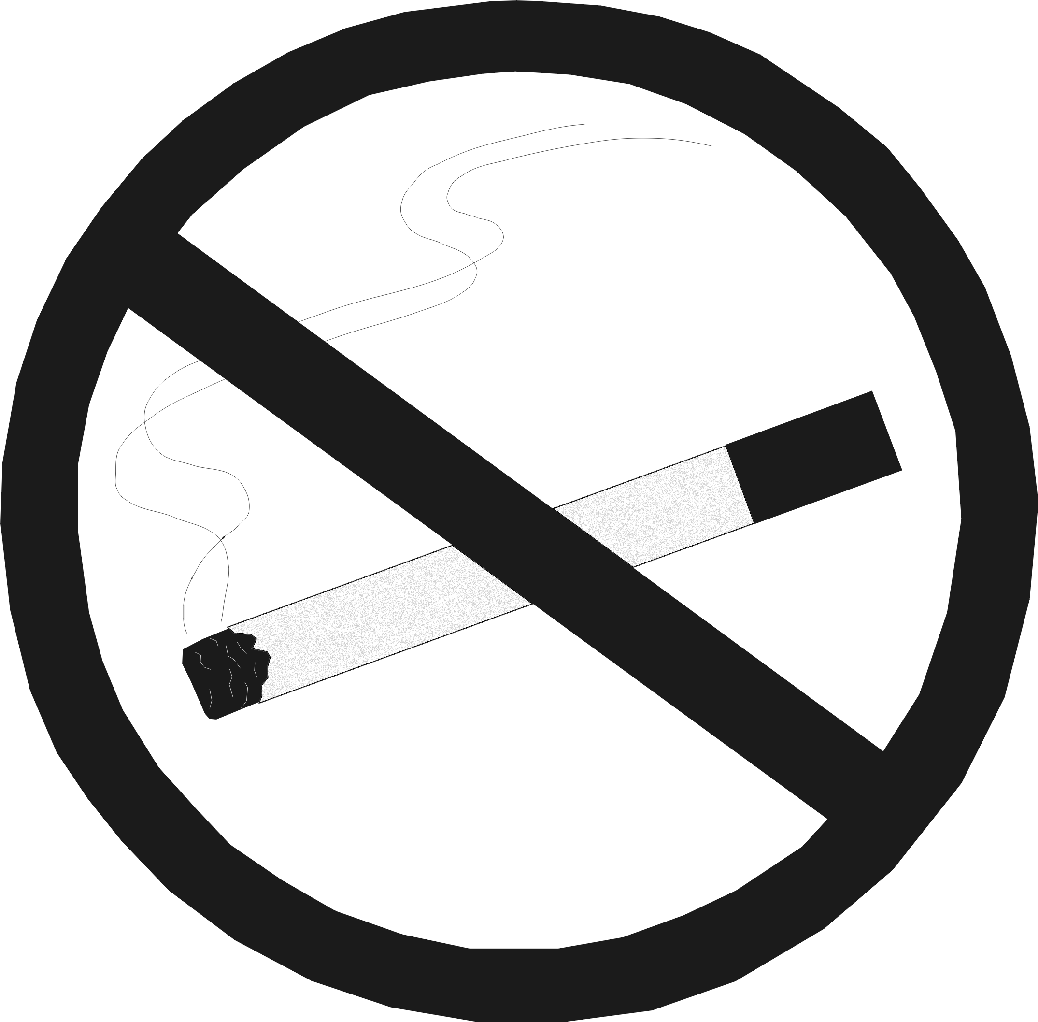
- धूम्रपान न करना स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है।
- तंबाकू के धुएँ में 4000 से भी ज़्यादा हानिकारक या ज़हरीले रसायन पदार्थ होते हैं जैसे निकोटीन, टार (Tar), कार्बन मोनॉक्साइड आदि। सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, चिलम, पाइप आदि सभी हानिकारक हैं।
- कोकेन, हेरोइन इत्यादि दूसरे नशीले पदार्थों की तरह निकोटीन के नशे की भी आदत पड़ जाती है। यदि इसकी आदत पड़ जाए, तो इनसान इसका ग़ुलाम हो जाता है और इसे आसानी से नहीं छोड़ सकता। इसी लिए धूम्रपान करनेवाले बहुत‑से लोग यह आदत छोड़ नहीं पाते। तंबाकू का धुआँ आपके शरीर को नुकसान पहुँचाता है और फेफड़ों, गले आदि का कैंसर, हृदय रोग और लंबे समय तक रहनेवाली फेफड़ों की बीमारियाँ जैसे ब्रोंकाइटिस, दमा आदि का कारण है। इससे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे बाँझपन (Infertility) हो सकता है और गर्भ में पल रहा बच्चा जन्म से पहले ही मर सकता है। यदि आप चुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो धूम्रपान को “ना” कहिए। अपने दोस्तों या सिगरेट के विज्ञापनों से प्रभावित न हों। धूम्रपान करने की ललक को ख़ुद पर हावी न होने दें। यह कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है।
- धूम्रपान करनेवाला अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुँचाता है। जलती हुई सिगरेट या बीड़ी हवा में धुआँ छोड़ती है। साथ ही जब धूम्रपान करनेवाला व्यक्ति अंदर लिया गया धुआँ बाहर छोड़ता है, तो उस कमरे में धुएँ की मात्रा बढ़ जाती है। इस तरह कमरे में बैठे अन्य लोगों को भी उसी धुएँ में साँस लेनी पड़ती है। वे निष्क्रिय धूम्रपान करनेवाले (Passive Smokers) बन जाते हैं, जिसका अर्थ है कि भले ही वे ख़ुद धूम्रपान न करें, फिर भी धुएँ से उनके फेफड़ों और हृदय को नुकसान हो सकता है। इस तरह धूम्रपान करनेवाला अपने परिवार, दोस्तों और पास बैठे लोगों को नुकसान पहुँचाता है।
उन 1000 युवकों में से जो आज धूम्रपान करते हैं:
• 500 की मृत्यु तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण होगी।
• 250 लोग कम उम्र में मर जाएँगे। वे धूम्रपान न करनेवाले लोगों की तुलना में अपनी आयु औसतन 22 साल कम कर लेते हैं।
• 250 लोगों की मृत्यु चाहे बुढ़ापे में होगी लेकिन जैसे‑जैसे उम्र बढ़ेगी, उन्हें तंबाकू के सेवन से जुड़ी बीमारियाँ होंगी जिनसे उनकी सेहत ख़राब रहेगी।
धूम्रपान करनेवाला व्यक्ति यदि अपना इरादा पक्का कर ले, तो धूम्रपान छोड़ सकता है। इसके लिए इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। इसकी आदत पड़ने के कारण कभी‑कभी ऐसा करना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी कोशिश और परिवार एवं दोस्तों के सहयोग से ऐसा किया जा सकता है।
यदि आप धूम्रपान नहीं करते- सावधान रहें, इसके चंगुल में न फँसें।
- लोगों को अपने आसपास धूम्रपान करने से रोकें। निष्क्रिय धूम्रपान (Passive Smoking) भी ख़तरनाक है।
- यदि आपके परिवार या दोस्तों में से कोई धूम्रपान करता है तो उन्हें इस आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित करें। उन्हें इसे छोड़ने के फ़ायदे बताएँ।
- अपने बड़े अफ़सर से आग्रह करें कि वे ऑफ़िस में धूम्रपान की अनुमति न दें।
- सरकार से आग्रह करें कि सभी कार्यक्षेत्रों में ‘धूम्रपान निषेध’ हो।
- धूम्रपान छोड़ने से आपको फेफड़ों का कैंसर और दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा बहुत कम हो जाएगा।
- धूम्रपान से होनेवाली खाँसी ग़ायब हो जाएगी।
- आप पहले की अपेक्षा ज़्यादा आसानी से साँस ले पाएँगे।
- आप ज़्यादा तंदुरुस्त महसूस करेंगे।
- आप अपने प्रियजनों को और नुकसान नहीं पहुँचाएँगे।
- आपके पैसे बचेंगे।
- आपके कपड़ों से तंबाकू के धुएँ की नहीं, बल्कि ताज़ा ख़ुशबू आएगी।
- आपकी साँसों में ताज़गी होगी।
- आपका घर साफ़ रहेगा।
तंबाकू भारत में पहली बार 17 वीं शताब्दी में लाया गया परंतु 20 वीं शताब्दी तक यह काफ़ी प्रचलित हो गया। तंबाकू का इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है, उदाहरण के लिए—धूम्रपान में, चबाने के लिए और नसवार बनाकर। धूम्रपान का प्रचलन आज पूरी दुनिया में हो रहा है। धूम्रपान के धुएँ में हाइड्रोकार्बन, बैनज़ीन व कैडमियम जैसे विषैले पदार्थ होते हैं। तंबाकू में भी निकोटीन और नाइट्रोसैमाइंज़ जैसे हानिकारक पदार्थ होते हैं। जब तंबाकू को गुटके के रूप में मुँह के भीतर देर तक रखा जाता है तो यह बहुत हानिकारक होता है। मुँह के कैंसर को बढ़ाने में तो इसका बहुत बड़ा हाथ है।
मुँह के कैंसर के कारण- छोटी उम्र में पान या तंबाकू का प्रयोग।
- दाँतों तथा मुँह की सफ़ाई में देख‑रेख की कमी।
- मुँह के छाले जो बहुत समय से ठीक न हो रहे हों।
- बहुत अधिक गरम खाना खाने की आदत।
- मुँह, होंठ, मसूड़ों और ज़बान पर सफ़ेद दानों का उभरना।
- मुँह से दुर्गंध आना तथा खाने और पीने के समय दर्द होना।
- ज़बान में कोई उभार (Lump) महसूस होना जो निगलने में तंग करे।
- कानों में दर्द और नाक से बोलना।
इलाज : ज़्यादातर ऑपरेशन, कीमोथेरेपी (Chemotherapy) और रेडियोथेरेपी (Radiotherapy) द्वारा होता है।
फेफड़ों के कैंसर का कारण- धूम्रपान।
- एस्बेस्टॉस फ़ाइबर का प्रभाव।
आम तौर से शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। परंतु बाद की अवस्था में ये लक्षण दिखाई देते हैं:
- हर वक़्त रहनेवाली खाँसी।
- साँस लेने में तकलीफ़।
- साँस लेते समय छाती से सीटी की तरह भारी आवाज़।
- खाँसी में ख़ून का निकलना।
- छाती में दर्द।
- थूक की जाँच।
- छाती का एक्स‑रे।
- ब्रोंकोस्कोपी द्वारा साँस की नलियों का परीक्षण (शरीर को सुन्न करके मुँह में से छाती के अंदर ट्यूब डाली जाती है) और बायोप्सी (Biopsy)।
इलाज: ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी।
एक बार आप धूम्रपान करना बंद कर देते हैं तो आपका शरीर
पहले से हो चुके नुकसान को सुधारना शुरू कर देता है।
- तंबाकू किसी भी रूप में ख़तरनाक है। तंबाकू से बने पदार्थों को चबाने से मुँह, पेट और मूत्राशय का कैंसर होता है।
- सिगरेट बनाने के लिए हर साल बहुत‑से पेड़ काटे जाते हैं (तंबाकू को बनाने के लिए लकड़ी जलाई जाती है)। हर 300 सिगरेट बनाने के लिए कहीं न कहीं किसी ने एक पेड़ काटा है।
- अपनी सेहत के लिए आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। जो लोग आपको धूम्रपान करने के लिए उकसाते हैं, उनकी बात न सुनें।
शारीरिक क्रिया (Physical Activity)
शारीरिक क्रिया क्या है शरीर की कोई भी गतिविधि, जिसमें शक्ति का प्रयोग हो (कैलोरीज़ की खपत हो) वह शारीरिक क्रिया कहलाती है। इसलिए किसी भी प्रकार की गतिविधि शारीरिक क्रिया है। जब हम तेज़ी से चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, कोई खेल खेलते हैं, नाचते हैं, या घर की सफ़ाई करते हैं, तो हम शारीरिक क्रियाएँ कर रहे हैं। इन कार्यों में इस्तेमाल होनेवाली शक्ति के आधार पर शारीरिक क्रियाओं को इन श्रेणियों में बाँटा गया है: हलका, मध्यम और कठोर।
शरीर की कोई भी गतिविधि, जिसमें शक्ति का प्रयोग हो (कैलोरीज़ की खपत हो) वह शारीरिक क्रिया कहलाती है। इसलिए किसी भी प्रकार की गतिविधि शारीरिक क्रिया है। जब हम तेज़ी से चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, कोई खेल खेलते हैं, नाचते हैं, या घर की सफ़ाई करते हैं, तो हम शारीरिक क्रियाएँ कर रहे हैं। इन कार्यों में इस्तेमाल होनेवाली शक्ति के आधार पर शारीरिक क्रियाओं को इन श्रेणियों में बाँटा गया है: हलका, मध्यम और कठोर।
शारीरिक क्रियाओं की क़िस्म और मात्रा
| चुस्त जीवन के लिए | स्वस्थ रहने के लिए गतिविधि | तंदुरुस्ती के लिए व्यायाम | खेलों के लिए अभ्यास |
|---|---|---|---|
| हलकी से मध्यम गतिविधि | मध्यम गतिविधि | मध्यम से तेज़ गतिविधि | बहुत ज़ोर से की गई गतिविधि |
| 10 मिनट या उससे ज़्यादा—दिन में कुछ बार | हफ़्ते में तीन बार, दिन में बीस मिनट या उससे अधिक | रोज़ाना तीस मिनट या इससे ज़्यादा | अपनी‑अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार जितनी बार और जितनी देर कर सकें |
नियमित रूप से मध्यम दर्जे की शारीरिक क्रियाओं से हमें स्वास्थ्य के अनेक फ़ायदे होते हैं, ख़ास तौर पर कई बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। हालाँकि कठोर शारीरिक गतिविधि से हृदय, फेफड़ों और मांसपेशियों की कार्यकुशलता और सहनशक्ति बढ़ती है, लेकिन इससे सेहत से जुड़े अन्य फ़ायदे उतने नहीं होते। तंदुरुस्त होने से आप ऊँचे दर्जे के व्यायाम तो आसानी से कर पाएँगे, लेकिन मध्यम दर्जे की गतिविधियों से सेहत से जुड़े काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ज़्यादा शारीरिक व्यायाम करने से ज़्यादा कैलोरीज़ की खपत होती है, इसलिए यह वज़न को नियंत्रण में रखने के लिए फ़ायदेमंद है।
| मध्यम स्तर की नियमित शारीरिक क्रिया | = | सेहत से जुड़े फ़ायदे (बीमारी होने का कम ख़तरा) |
| तीव्र गति से बार‑बार की गई शारीरिक क्रिया | = | बेहतर तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य लाभ |
शारीरिक व्यायाम के क्या फ़ायदे हैं?
नियमित शारीरिक व्यायाम- अकाल मृत्यु का ख़तरा कम करता है।
- हृदय रोग या स्ट्रोक से मृत्यु का ख़तरा कम करता है। एक तिहाई लोगों की मृत्यु इन्हीं कारणों से होती है।
- हृदय रोग या कोलन के कैंसर के ख़तरे को 50% कम करता है।
- टाइप II मधुमेह के ख़तरे की संभावना को भी 50% तक कम करता है।
- हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम या इसे कम करने में मदद करता है। दुनिया के 20% लोग (18 साल की उम्र से ज़्यादा) इस रोग से पीड़ित हैं।
- हड्डियों की कमज़ोरी को रोकता है। महिलाओं में कूल्हे का फ़्रैक्चर होने के ख़तरे को 50% तक कम करता है।
- पीठ के निचले हिस्से में दर्द के ख़तरे को कम करता है।
- मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाता है। तनाव, चिंता और उदासी तथा अकेलेपन का एहसास कम करता है।

- आचरण को नियंत्रित करने में और उसके दुष्प्रभाव को रोकने में मदद करता है (ख़ास तौर पर बच्चों और जवान लोगों में) जैसे—धूम्रपान, शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन, बदपरहेज़ी वाला भोजन और हिंसा।
- वज़न कम करने में सहायता करता है। जो लोग कोई व्यायाम नहीं करते, उन लोगों की तुलना में व्यायाम करनेवालों में मोटापा होने की संभावना को 50% तक कम करता है।
- हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। जो लोग किसी लंबी बीमारी और विकलांगता से पीड़ित हैं, उनकी सहनशक्ति बढ़ाता है।
- शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताक़त देता है जिससे संक्रमण से बचाव होता है।
- पीठ और घुटने के दर्द के नियंत्रण में सहायता करता है।
- स्वास्थ्य सुदृढ़ करता है और कार्यक्षमता बढ़ाता है।
- खेलों में कुशलता को बढ़ाता है।
- सामूहिक खेल या कार्य से सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को मज़बूत बनाता है।
- नगर-योजना को कार्यशील करने में सहायक होता है। पैदल चलने के रास्ते, साइकिल चलाने के रास्ते, उद्यान, साफ़ हवा और वातावरण की माँग पैदा करता है।
व्यायाम के लाभ जीवन भर के लिए हैं।
बचपन में व्यायाम करने से- हड्डियाँ मज़बूत होती हैं और शरीर का विकास बेहतर होता है।
- हृदय और फेफड़ों की क्षमता पहले से बेहतर होती है।
- ज़िंदगी में आनेवाले कठिन शारीरिक कार्यों और तनाव से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।
- शरीर की कार्य‑प्रणाली सुचारु हो जाती है जिससे ब्लड प्रेशर, नाड़ी गति (Pulse), ख़ून में कोलेस्ट्रॉल तथा ग्लूकोज़ की मात्रा और वज़न आदि नियंत्रण में रहते हैं।
- हड्डियाँ मज़बूत और मांसपेशियाँ बेहतर होती हैं।
- शरीर का आकार, चाल‑ढाल और आत्मविश्वास बेहतर होने से दूसरे लोग आकर्षित होते हैं।
- मानसिक तनाव का सामना करने में सहायता मिलती है।
- खेलों में कुशलता बढ़ जाती है।
- अनावश्यक रूप से वज़न नहीं बढ़ता।
- बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और संक्रमण से बचाव होता है।
- भूख बढ़ती है और पोषण बेहतर होता है।
- हाई ब्लड प्रेशर से बचाता है।
- मधुमेह से रक्षा करता है।
- ख़ून में वसा (Blood Fats) की मात्रा उचित रखता है।
- वज़न और शरीर में चर्बी का संतुलन रखता है।
- रोज़मर्रा की मुश्किलों का सामना तनाव के बिना करने में मदद करता है।
- दिल के दौरे के ख़तरे को कम करता है।
- कोलन का कैंसर होने के आसार कम करता है।
- ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखता है (130/85)।
- ख़ून में असामान्य वसा को नियंत्रित करता है।
- मधुमेह नियंत्रित करता है।
- चिंता और उदासी दूर करता है।
- शरीर का संतुलन बेहतर करता है।
- जोड़ों के रोग होने का ख़तरा कम करता है।
- गिरने और हड्डी टूटने का ख़तरा कम करता है।
- नियमित रूप से पेट साफ़ करता है और कब्ज़ से बचाता है।
- टाँगों की मांसपेशियों में ऐंठन से बचाव करता है।
- सुचारु जीवन सुनिश्चित करता है।
नियमित रूप से व्यायाम करने से इन ख़तरनाक बीमारियों से बचाव होता है
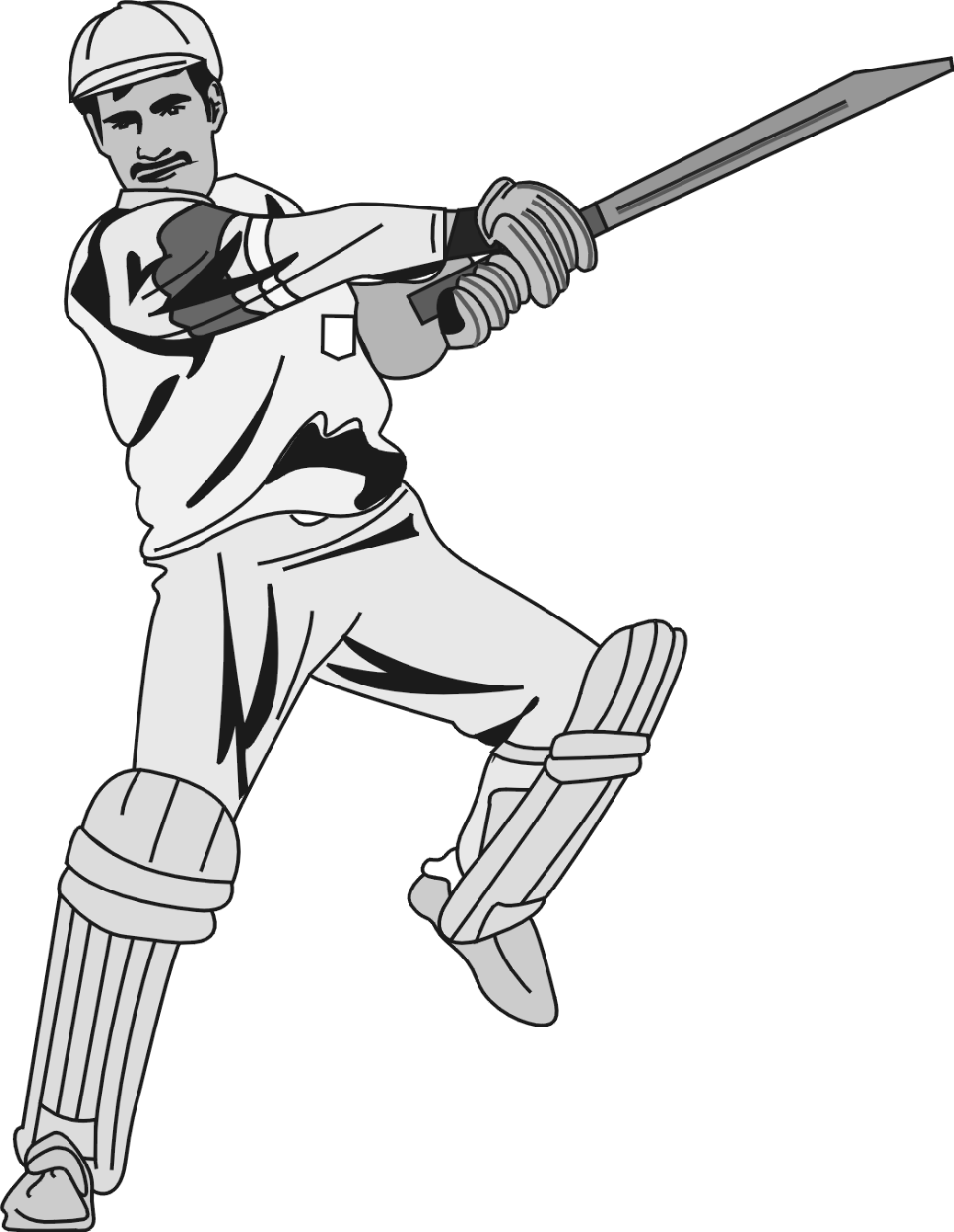
नियमित तौर पर व्यायाम करते रहने से ब्लड प्रेशर और हार्ट‑रेट (प्रति मिनट में दिल की धड़कन) साधारणतया कम रहते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा कम हो जाता है। इससे ख़ून में एच.डी.एल. की मात्रा बढ़ती है। यह अच्छी क़िस्म का कोलेस्ट्रॉल है जो नाड़ियों में चर्बी को जमने से रोकता है। ब्लड प्रेशर कम होने से लक़वे से भी बचाव होता है।
कैंसरजो लोग व्यायाम करते हैं, उनमें आँतों का कैंसर होने की संभावना कम रहती है। नियमित व्यायाम करने से स्तन‑कैंसर को भी रोका जा सकता है। नियमित रूप से व्यायाम करनेवालों को अन्य प्रकार के कैंसर भी कम होते हैं।
मधुमेहयदि नियमित रूप से व्यायाम के साथ‑साथ सही भोजन लें तो मधुमेह होने के आसार बहुत कम हो जाते हैं।
हड्डियों की कमज़ोरी (Osteoporosis)- व्यायाम से हड्डियों को बनने में और फिर से मज़बूत होने में बढ़ावा मिलता है। बुज़ुर्गों की हड्डियाँ भी मज़बूत बनी रहती हैं।
- व्यायाम से हड्डियों में कैल्शियम की कमी नहीं होती और ये बुढ़ापे में कमज़ोर नहीं पड़तीं।
- हड्डियों में दर्द और उनका टूटना बहुत कम होता है।
- जोड़ों में लचीलापन बना रहता है, जोड़ों के दर्द की परेशानी कम होती है। मांसपेशियाँ सुचारु रूप से काम करती हैं और अच्छे संतुलन की वजह से बुज़ुर्गों को भी गिरने का ख़तरा कम रहता है।
ज़्यादा वज़न और मोटापा होने से दिल का दौरा, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, ख़ून में चर्बी की मात्रा, जोड़ों के दर्द और फेफड़ों के रोग आदि होने का ख़तरा बढ़ जाता है। नियमित व्यायाम से शरीर का वज़न नियंत्रण में रहता है और समस्याओं से बचा जा सकता है। जो शारीरिक रूप से चुस्त हैं और अपने वज़न को नियंत्रित रखते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।
मानसिक स्वास्थ्यशारीरिक स्वास्थ्य ख़राब होने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। शारीरिक व्यायाम चिंता और तनाव से बचाने में सहायता करता है।
यदि आप रोज़ाना साधारण शारीरिक व्यायाम करना चाहते हैं- दिन में तीन बार, दस मिनट के लिए तेज़‑तेज़ चलें।
- सीढ़ियाँ चढ़ें। (कम से कम तीसरी मंज़िल तक लिफ़्ट का इस्तेमाल न करें।)
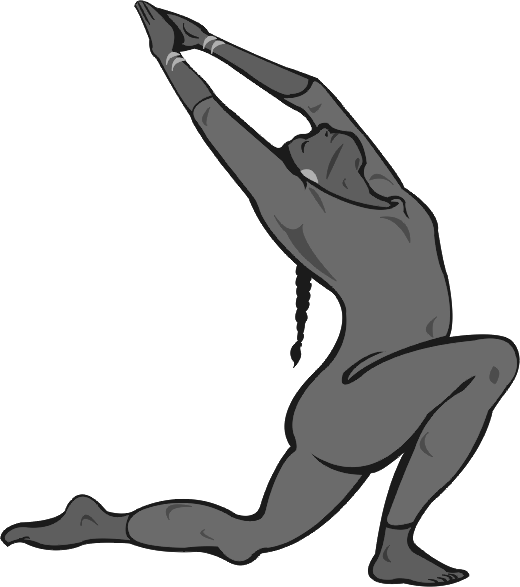 नज़दीक के बाज़ार में स्कूटर या कार के बजाय पैदल या साइकिल पर जाएँ।
नज़दीक के बाज़ार में स्कूटर या कार के बजाय पैदल या साइकिल पर जाएँ।- घर के काम करें (सफ़ाई, झाड़ू‑पोंछा, कपड़े धोना आदि)।
- बाग़बानी, खुदाई, सफ़ाई और पौधों को पानी देने जैसे काम करें।
- नाचिए। (यदि घर में ही नाचें तो भी यह इतना पागलपन नहीं है, जितना आप सोच रहे हैं!)
- बच्चों और दोस्तों के साथ खेलें।
- ऐरोबिक व्यायाम करें।
- रस्सी कूदें।
- योग सीखें और अभ्यास करें।
व्यायाम के दौरान कितनी कैलोरीज़ की खपत होती है, इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें:
- व्यायाम की क़िस्म।
- व्यायाम का समय और इसकी तीव्रता।
- व्यायाम कर रहे व्यक्ति का वज़न—व्यक्ति का वज़न जितना अधिक होगा, उतनी ज़्यादा कैलोरीज़ की खपत होगी।
नीचे दी गई चर्चा के लिए हम व्यायाम का समय 30 मिनट और व्यक्ति का वज़न 180 पाउंड या 82 किलो मानते हैं। आइए देखें कि भिन्न‑भिन्न व्यायामों से कितनी कैलोरीज़ की खपत होती है।
| एरोबिक गतिविधियाँ (30 मिनट, शारीरिक वज़न 180 पाउंड या 82 किलो) |
कैलोरीज़ की खपत |
|---|---|
| सामान्य एरोबिक्स, कम उग्रता से | 215 |
| सामान्य एरोबिक्स, अधिक उग्रता से | 300 |
| एक ही स्थान पर (Stationary) साइकिल चलाना, सामान्य ज़ोर से | 300 |
| एक ही स्थान पर (Stationary) साइकिल चलाना, अधिक ज़ोर से | 450 |
| एक ही स्थान पर (Stationary) नौका के चप्पू चलाना, सामान्य ज़ोर से | 300 |
| एक ही स्थान पर (Stationary) नौका के चप्पू चलाना, अधिक ज़ोर से | 360 |
| 6 मील प्रति घंटा की रफ़्तार से दौड़ना (10 मिनट/मील) | 330 |
| 8 मील प्रति घंटा की रफ़्तार से दौड़ना (7.5 मिनट/मील) | 450 |
| 10 मील प्रति घंटा की रफ़्तार से दौड़ना (6 मिनट/मील) | 533 |
| सामान्य तेज़ी से रस्सी कूदना | 430 |
| तेज़ गति से रस्सी कूदना | 510 |
| मशीन पर सामान्य ज़ोर से सीढ़ियाँ चढ़ना | 380 |
| सामान्य ज़ोर से फ़्री स्टाइल तैराकी | 300 |
| अधिक ज़ोर से फ़्री स्टाइल तैराकी | 430 |
| 3 मील प्रति घंटा की रफ़्तार से समतल जगह पर चलना (सामान्य गति से) | 140 |
| 4 मील प्रति घंटा की रफ़्तार से समतल जगह पर चलना (तेज़ गति से) | 215 |
| 3.5 मील प्रति घंटा की रफ़्तार से चढ़ाई चढ़ना | 260 |
| शरीर को मज़बूत बनाने के लिए व्यायाम | कैलोरीज़ की खपत |
|---|---|
| सामान्य गति से दंड‑बैठक, उठक‑बैठक, जंपिग जैक पर व्यायाम | 200 |
| तीव्र गति से की गई दंड‑बैठक, उठक‑बैठक | 340 |
| मध्यम प्रयास से भार उठाना | 200 |
| अधिक प्रयास से भार उठाना | 260 |
| खेल की गतिविधियाँ | कैलोरीज़ की खपत |
|---|---|
| बैडमिंटन | 200 |
| बास्केटबॉल का मैच | 340 |
| बिना मैच के बास्केटबॉल खेलना | 260 |
| बास्केटबॉलâ बास्केट में डालना | 200 |
| बेसबॉल/सॉफ़्टबॉल | 230 |
| बिलियर्ड्स | 110 |
| बॉलिंग | 130 |
| रिंग में बॉक्सिंग | 510 |
| पंचिंग बैग से बॉक्सिंग | 260 |
| बॉक्सिंग का अभ्यास | 390 |
| तलवारबाज़ी | 260 |
| फ़ुटबाल | 350 |
| गोल्फ़ में चलना और सामान उठाना | 200 |
| बिना सामान उठाए गोल्फ़ खेलना | 150 |
| लघु गोल्फ़ | 130 |
| सामान्य जिम्नास्टिक्स | 170 |
| टीम में हैंडबॉल खेलना | 350 |
| हॉकी—बर्फ़ पर या मैदान में | 350 |
| उछलते हुए घोड़े पर सवारी | 110 |
| चलते हुए घोड़े की पीठ पर सवारी | 280 |
| बाज़ीगरी | 170 |
| किकबॉल | 300 |
| मार्शल आर्ट्स (जूडो, जुजित्सु, कराटे, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो) | 430 |
| पोलो | 340 |
| रोलर स्केटिंग | 300 |
| बोर्ड पर स्केटिंग | 215 |
| सॉकर | 370 |
| टेबल टेनिस | 170 |
| ताई ची | 170 |
| टेनिस | 300 |
| वॉलीबॉल का मैच | 340 |
| सामान्य वॉलीबॉल | 300 |
- ये आँकड़े 180 पाउंड या 82 किलो वज़न वाले व्यक्ति के लिए हैं, जिसने ऊपर सूची में दिए गए व्यायाम में से कोई भी आधे घंटे के लिए किया हो।
- यदि किसी व्यक्ति का भार 180 पाउंड से कम है, तो ऊपर दिए गए आँकड़ों की तुलना में कम कैलोरीज़ की खपत होगी।
- यदि किसी व्यक्ति का वज़न 180 पाउंड से ज़्यादा है, तो ऊपर दिए गए आँकड़ों की तुलना में अधिक कैलोरीज़ की खपत होगी।
अपने लिए सही आँकड़े देखने के लिए, व्यायाम के दौरान कैलोरीज़ की खपत की तालिका पृष्ठ 85‑86 पर देखें।
कम समय में अधिक उपयोगी व्यायाम चुनने का तरीक़ाऊपर दी गई तालिकाएँ भिन्न‑भिन्न व्यायामों में खपत होनेवाली कैलोरीज़ का तुलनात्मक ब्योरा देती हैं। निस्संदेह जो व्यायाम उतने ही समय में ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, वे ज़्यादा उपयुक्त हैं।
उपर्युक्त व्यायामों की सूची से आप देख सकते हैं कि ये व्यायाम सबसे उपयुक्त हैं:- दौड़ना (8‑10 मील प्रति घंटा की गति से)
- रिंग में बॉक्सिंग
- तेज़ी से रस्सी कूदना
- मार्शल आर्ट्स
- एक ही स्थान पर (Stationary) तेज़ी से साइकिल चलाना
- बहुत तेज़ तैरना
- उपर्युक्त तालिका में से वह व्यायाम चुनें जो आधे घंटे में 250 कैलोरीज़ से अधिक की खपत करता हो।
- उसके बाद वह व्यायाम चुनें जिसे करने में आपको ज़्यादा आनंद आए और जिसे आप आसानी से कर सकें।
आप किसी भी क़िस्म के व्यायाम का चुनाव करें, व्यायाम के दौरान तीव्रता बढ़ाकर अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं। लगातार मध्यम तीव्रता से व्यायाम करने से बेहतर है कि कुछ समय के लिए तीव्रता से व्यायाम करें, फिर कम तीव्रता से करें; इस तरह अदल‑बदल कर व्यायाम करने के तरीक़े को ‘इंटरवल ट्रेनिंग’ कहते हैं। दुनिया भर के खिलाड़ी इसी तरह से व्यायाम करते हैं।
इंटरवल ट्रेनिंग के फ़ायदे- कम तीव्रता से व्यायाम करते समय आपकी शक्ति को पुन: उभरने का समय मिल जाता है।
- इससे उतने प्रयास में ही ज़्यादा शक्ति की खपत होती है।
उदाहरण के लिए यदि आप दौड़ने का व्यायाम चुनते हैं तो आप मध्यम गति, 6 मील प्रति घंटा की रफ़्तार से दौड़ सकते हैं और फिर 1‑2 मिनट के लिए अपनी गति बढ़ा सकते हैं (8‑10 मील प्रति घंटा की रफ़्तार से)। फिर मध्यम गति पर वापस आ जाने के बाद इसे फिर दोहरा सकते हैं। जैसे आपको आदत पड़ती जाएगी, आप कम गति वाली दौड़ के बजाय अधिक गति वाली दौड़ का समय बढ़ा सकेंगे। तैराकी, चलना, साइकिल चलाना, सामान्य एरोबिक्स, एक जगह नौका के चप्पू चलाना, वज़न उठाने आदि व्यायामों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है।
सर्किट ट्रेनिंगव्यायाम के दौरान अधिक ऊर्जा की खपत करने के लिए एरोबिक और शरीर को मज़बूत करनेवाली साधारण कसरत दोनों करें। इस व्यायाम को ‘सर्किट ट्रेनिंग’ कहते हैं। इससे पूरे व्यायाम की प्रक्रिया के दौरान पहले आप तीव्र व्यायाम करें, फिर साधारण कसरत करें, जैसे उठक‑बैठक। इससे आपको पहले किए गए व्यायाम से उभरने का समय मिल जाता है या फिर पहले साधारण कसरत करें और फिर तीव्र व्यायाम करें। इससे आपके व्यायाम की प्रक्रिया का स्तर तीव्र बना रहता है।
व्यायाम के दौरान कैलोरीज़ की गणना (प्रति मिनट)कैलोरीज़ की खपत प्रति मिनट किए गए व्यायाम पर निर्भर करती है। खपत हुईं कैलोरीज़ दरअसल आपके वज़न पर निर्भर करती हैं, जितना अधिक शरीर का वज़न होगा, उतनी अधिक कैलोरीज़ की खपत होगी।
| गतिविधि | वज़न (पाउंड) | |||
|---|---|---|---|---|
| 105-115 | 127-137 | 160-170 | 180-200 | |
| एरोबिक नृत्य | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 8.6 |
| बास्केटबॉल | 9.8 | 11.2 | 13.2 | 14.5 |
| एक जगह साइकिल चलाना (10 मील प्रति घंटा) |
5.5 | 6.3 | 7.8 | 8.3 |
| एक जगह साइकिल चलाना (20 मील प्रति घंटा) |
11.7 | 13.3 | 15.6 | 17.8 |
| गोल्फ़ | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 |
| पीठ पर सामान उठाकर चढ़ाई पर चलना | 5.9 | 6.7 | 7.9 | 8.8 |
| धीमे दौड़ना (5 मील प्रति घंटा) | 8.6 | 9.2 | 11.5 | 12.7 |
| दौड़ना (8 मील प्रति घंटा) | 10.4 | 11.9 | 14.2 | 17.3 |
| ढलान पर स्कीइंग | 7.8 | 10.4 | 12.3 | 13.3 |
| ढलान और चढ़ाई, दोनों तरह की सतह पर स्कीइंग | 13.1 | 15 | 17.8 | 19.4 |
| मध्यम गति से बर्फ़ खोदना | 9 | 9.1 | 10.8 | 12.5 |
| तीव्र गति से बर्फ़ खोदना | 13.8 | 15.7 | 18.5 | 20.5 |
| सीढ़ियाँ चढ़ना | 5.9 | 6.7 | 7.9 | 8.8 |
| तैराकी (20 गज़ प्रति मिनट) | 3.9 | 4.5 | 5.3 | 6.8 |
| तैराकी (60 गज़ प्रति मिनट) | 11 | 12.5 | 14.8 | 17.9 |
| टेनिस (Singles) | 7.8 | 8.9 | 10.5 | 11.6 |
| वॉलीबॉल | 7.8 | 8.9 | 10.5 | 11.6 |
| चलना (4 मील प्रति घंटा) | 4.5 | 5.2 | 6.1 | 6.8 |
| शारीरिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण | ||
|---|---|---|
| कार या मोटर साइकिल को धोना या पॉलिश करना | 45 – 60 मिनट | कम ताक़त से, ज़्यादा समय के लिए |
| खिड़कियों या फ़र्श को साफ़ करना/ धोना | 45 – 60 मिनट | 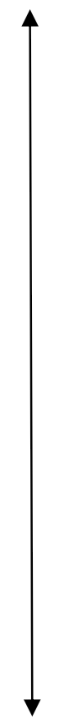 |
| वॉलीबॉल या बैडमिंटन खेलना | 45 मिनट | |
| बाग़बानी/खुदाई करना | 30 – 45 मिनट | |
| 1¾ मील चलना | 35 मिनट
(20 मिनट/प्रति मील) |
|
| बास्केटबॉल (बास्केट शूटिंग) (shooting baskets) |
30 मिनट | |
| पाँच मील साइकिल चलाना | 30 मिनट (10 मील/प्रति घंटा) |
|
| तेज़ नाचना | 30 मिनट | |
| दो मील चलना | 30 मिनट (4 मील/प्रति घंटा) |
|
| पानी में एरोबिक व्यायाम करना | 30 मिनट | |
| तैरना | 20 मिनट | |
| बास्केटबॉल खेलना | 15 – 20 मिनट | |
| चार मील साइकिल चलाना | 15 मिनट | |
| रस्सी कूदना | 15 मिनट | |
| डेढ़ मील दौड़ना | 15 मिनट (10 मिनट/प्रति मील) |
|
| सीढ़ियाँ चढ़ना | 15 मिनट | ज़्यादा ताक़त से, कम समय के लिए |
ऐंटीबायोटिक्स के बिना स्वस्थ होना
ऐंटीबायोटिक्स क्या हैं?ऐंटीबायोटिक्स वे तेज़ दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया द्वारा किए गए संक्रमण (Infection) के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये वायरस को नहीं मार सकतीं।
क्या ऐंटीबायोटिक्स का प्रयोग साधारण बीमारियों, जैसे खाँसी, सर्दी और ‘फ़्लू’ के लिए किया जाना चाहिए?नहीं! ये आम बीमारियाँ वायरस के कारण होती हैं बैक्टीरिया के कारण नहीं। इन बीमारियों के इलाज के लिए साधारण दवाइयों का प्रयोग करें जो केमिस्ट के पास उपलब्ध हों। खूब पानी पिएँ और आराम करें।
 ऐंटीबायोटिक्स का बार-बार प्रयोग करने से क्या होता है?
ऐंटीबायोटिक्स का बार-बार प्रयोग करने से क्या होता है?
छोटी‑मोटी बीमारियों के लिए अगर हम ऐंटीबायोटिक्स का बार‑बार इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया पर ऐंटीबायोटिक्स बेअसर हो जाएँगी। इसे ऐंटीबायोटिक प्रतिरोध (Antibiotic Resistance) कहते हैं।
उपर्युक्त हालत में क्या हम किसी अन्य ऐंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं?जी हाँ, ऐसा किया जा सकता है लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। कुछ समय तक अन्य ऐंटीबायोटिक लेने से बैक्टीरिया पर इस ऐंटीबायोटिक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह, हमारे इलाज के लिए कोई ऐंटीबायोटिक उपयुक्त ही नहीं रहेगा जब तक किसी नई ऐंटीबायोटिक का आविष्कार नहीं होता। इसमें लंबा समय लग सकता है। यदि हर कोई ऐंटीबायोटिक्स का अधिक इस्तेमाल करता है, तो दुनिया में ऐंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यह पहले से ही गंभीर समस्या बन चुकी है।
ऐंटीबायोटिक प्रतिरोध को कैसे दूर किया जाए?सिर्फ़ बैक्टीरिया के संक्रमण के लिए ही ऐंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें।
ऐंटीबायोटिक की ज़रूरत कब होती है?कभी‑कभी वायरस द्वारा हुए साधारण ज़ुकाम में बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है और बीमारी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। कुछ गंभीर बीमारियाँ जैसे दिमाग़ी बुख़ार, निमोनिया और गुर्दे के संक्रमण में ऐंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। इस बात का फ़ैसला आपका डॉक्टर करेगा कि आपको कब ऐंटीबायोटिक की ज़रूरत है।
मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ?केवल ज़रूरत पड़ने पर ही ऐंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि डॉक्टर द्वारा दी गई पूरी दवा खाएँ। यदि इनका प्रयोग सावधानी से किया जाए तो ये इनसान को स्वस्थ करती हैं, उसकी ज़िंदगी बचा सकती हैं। ऐंटीबायोटिक प्रतिरोध पूरी दुनिया में एक गंभीर समस्या बन गई है और इसमें हम सब का योगदान है। बैक्टीरिया हमेशा जैविक‑विकास और ऐंटीबायोटिक प्रतिरोध के ज़रिए बचने की कोशिश करता है, इसलिए हमें उनसे एक क़दम आगे ही रहना है यानी हमें ऐंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं, कम करना चाहिए।
कैंसर की जल्द पहचान
किसी भी उम्र में जब शरीर के किसी अंग की कोशिकाएँ (Cells) और ऊतक (Tissues) असामान्य और अनियंत्रित ढंग से बढ़कर एक ग्रंथी का रूप ले लेते हैं तो वह कैंसर हो सकता है। जब कैंसर शरीर के अन्य अंगों में फैल जाता है तब इसका ख़तरा बढ़ जाता है। अगर इसकी पहचान जल्दी हो जाए तो यह इलाज से ठीक हो जाता है। इसी लिए यह अत्यंत ज़रूरी है कि अगर आपको अपने शरीर में ऐसी कोई ग्रंथि या उभार दिखे या दर्द हो जो ठीक न हो रहा हो, तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर की मदद लें।
कैंसर: चेतावनी के संकेत- ऐसा कोई रिसाव हो जो माहवारी का हिस्सा न हो, जो रजोनिवृत्ति के बाद शुरू हुआ हो या जिसमें दुर्गंध आती हो तो डॉक्टर की मदद लें।
- आदमी या औरत के शरीर में, छाती में या कहीं भी, कोई उभार या ग्रंथि दिखाई पड़े।
- स्तनों की त्वचा में बदलाव, जिससे वह संतरे के छिलके की तरह लगे या उसका रंग लाल या भूरा हो जाए। निप्पल से रिसाव निकलता हो।
- कोई छाला जो इलाज के बावजूद ठीक न हो।
- शौच की आदतों में बदलाव—जैसे कि कब्ज़ और दस्त का बार‑बार होना या कब्ज़ और दस्त का एक के बाद एक होना।
- मूत्र त्याग में कठिनाई।
- पाख़ाने या मूत्र में रक्त का आना।
- ख़ाँसी जो बहुत समय से ठीक न हो रही हो, आवाज़ का फटना, थूक में रक्त का आना।
- खाना या पानी निगलने में कठिनाई, भोजन ठीक से न पचना, उलटी में ख़ून का दिखना।
- मस्से या तिल में बदलाव, उसका बड़ा या छोटा होना; रंग बदलना, खुजली होना या ख़ून निकलना।
- बिना किसी कारण के शरीर का वज़न घट जाना, भूख न लगना; बहुत थकान महसूस होना।
- गरदन, बग़ल या जाँघ के जोड़ में किसी ग्रंथि या उभार का होना।
- हड्डी के ऊपरी भाग में, जोड़ में या मांसपेशी पर कोई ग्रंथि।
अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे या कोई ऐसा लक्षण जिसका कारण समझ में न आए, तो आप तुरंत डॉक्टर की मदद लें। यदि कैंसर की पहचान जल्दी हो जाए और इसका इलाज भी जल्दी शुरू हो जाए तो ठीक होने के आसार बढ़ जाते हैं। इलाज सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन किसी के भी द्वारा हो सकता है।
यह जान लेना भी ज़रूरी है कि कैंसर की रोकथाम हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के सभी पहलुओं के बारे में सोचें जैसे कि खान‑पान, व्यायाम और शरीर का वज़न। अपने जीवन से कैंसर के कुछ मूल कारणों को दूर करके आप कैंसर से बचाव कर सकते हैं। आप कैंसर के शिकार नहीं विजेता हो सकते हो।
औरतों के स्वास्थ्य की देखभाल
कैंसर की प्रारंभिक पहचान जाँच द्वारा की जाती है। औरतें ज़्यादातर सरवीकल या स्तन के कैंसर का शिकार होती हैं।
स्तन कैंसर की जाँचसबसे पहला क़दम ख़ुद ही अपने स्तनों का परीक्षण करना है। हर महीने माहवारी से पहले या रजोनिवृत्ति पा लेनेवाली महिलाओं को महीने की किसी एक निश्चित तारीख़ पर करना चाहिए। छ: महीने से एक साल के बीच डॉक्टर से जाँच ज़रूर करवाएँ। स्तन कैंसर की जाँच के चार तरीक़े हैं:
स्तनों का अपने आप परीक्षण यह ज़रूरी है कि आपका डॉक्टर आपको ख़ुद स्तनों का परीक्षण करना सिखाए। स्तनों के परीक्षण के दो भाग हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
स्तनों का परीक्षण यह अच्छी रोशनी में शीशे के सामने खड़े होकर या बैठकर करना चाहिए।
1: दोनों बाँहों को छाती के दोनों ओर रखें और देखें यदि:
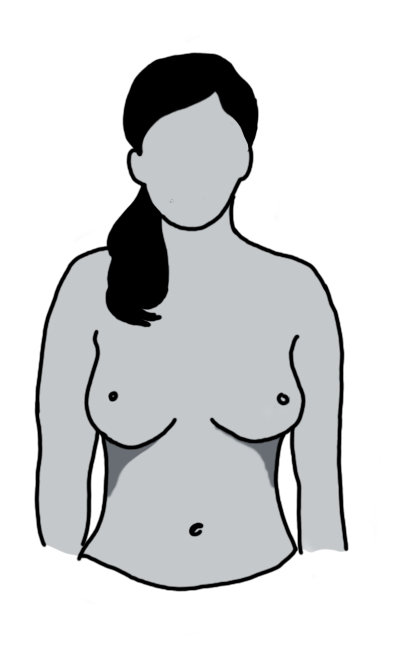
- स्तन के आकार या गोलाई में कोई बदलाव दिखाई दे।
- स्तन की त्वचा में कोई गड्ढा या खिंचाव हो।
- निप्पल के इर्द‑गिर्द ख़ारिश या सूखी त्वचा।
- निप्पल का अंदर की तरफ़ मुड़ना।
- स्तन की त्वचा में सूजन, लाली या निशान।
- निप्पल में से रिसाव।
2: दोनों बाँहों को सिर के ऊपर या पीछे जकड़ लें और देखें यदि: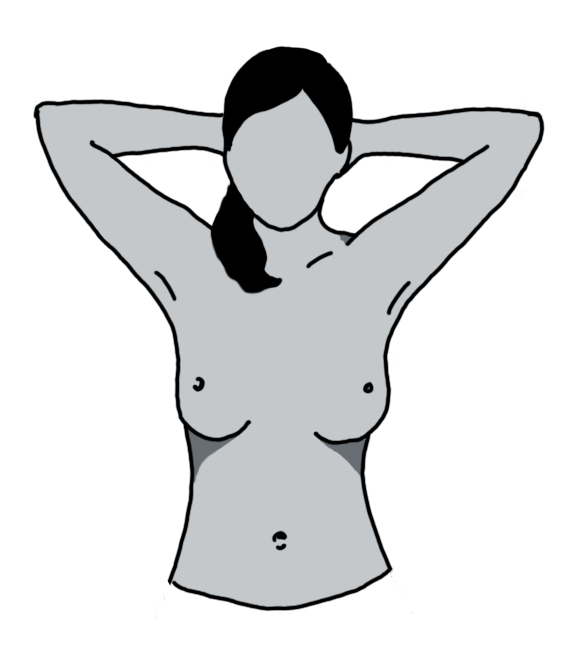
- स्तन के आकार या गोलाई में कोई बदलाव हो।
- दोनों निप्पल एक ही सीधी रेखा में होने चाहिएँ। अगर कोई बदलाव नज़र आए तो यह बीमारी का लक्षण हो सकता है।
3: दोनों हाथों को अपने कूल्हों पर रखकर दबाएँ। ऐसा करने से स्तन का उभार बढ़ जाता है। अब आप फिर स्तन के उभार, गोलाई, गतिविधि और आकार में कोई बदलाव की जाँच करें।
4: नीचे की ओर झुकें और देखें कि स्तन दोनों तरफ़ ठीक ढंग से गिर रहे हैं और निप्पल भी बाहर की तरफ़ हैं।
हाथों से स्तन का परीक्षण करना
लेटकर —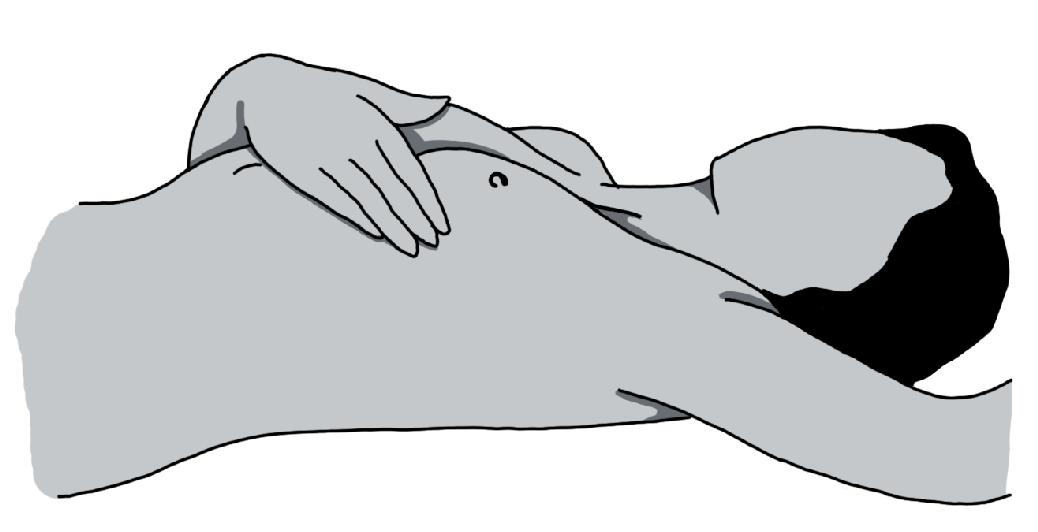 पीठ के बल लेट जाएँ। कंधों के नीचे तकिया या तह किया हुआ तौलिया रखें ताकि स्तन उपर की ओर उठ जाएँ। उलटे तरफ़ के हाथ की उँगलियों के नीचे वाले भाग से सीधे तरफ़ के स्तन की जाँच करें। हाथ का यह भाग धीरे से गोलाई में घुमाएँ और हलके‑से दबाव डालकर जाँच करें कि स्तन में कोई सूजन, दर्द या और कोई असमानता तो नहीं है।
पीठ के बल लेट जाएँ। कंधों के नीचे तकिया या तह किया हुआ तौलिया रखें ताकि स्तन उपर की ओर उठ जाएँ। उलटे तरफ़ के हाथ की उँगलियों के नीचे वाले भाग से सीधे तरफ़ के स्तन की जाँच करें। हाथ का यह भाग धीरे से गोलाई में घुमाएँ और हलके‑से दबाव डालकर जाँच करें कि स्तन में कोई सूजन, दर्द या और कोई असमानता तो नहीं है।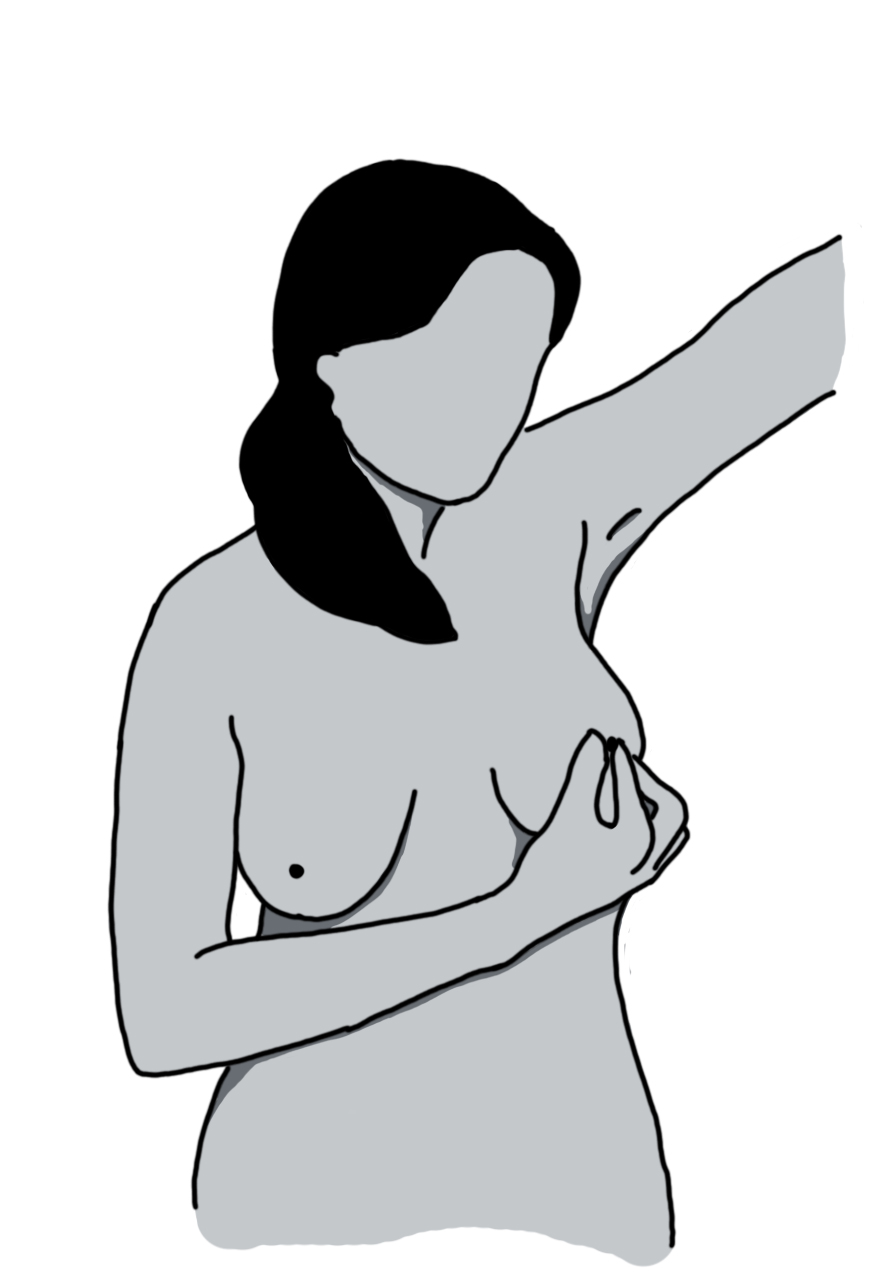 अपने निप्पल को दबाकर देखें। पानी जैसा लाल या भूरा रिसाव सही लक्षण नहीं है। बग़ल, छाती और गरदन सब अच्छी तरह से दबाकर देखें कि कोई उभार या ग्रंथि तो नहीं है।
अपने निप्पल को दबाकर देखें। पानी जैसा लाल या भूरा रिसाव सही लक्षण नहीं है। बग़ल, छाती और गरदन सब अच्छी तरह से दबाकर देखें कि कोई उभार या ग्रंथि तो नहीं है।दूसरी तरफ़ के स्तन की जाँच भी इसी तरह से करें।
खड़े होकर —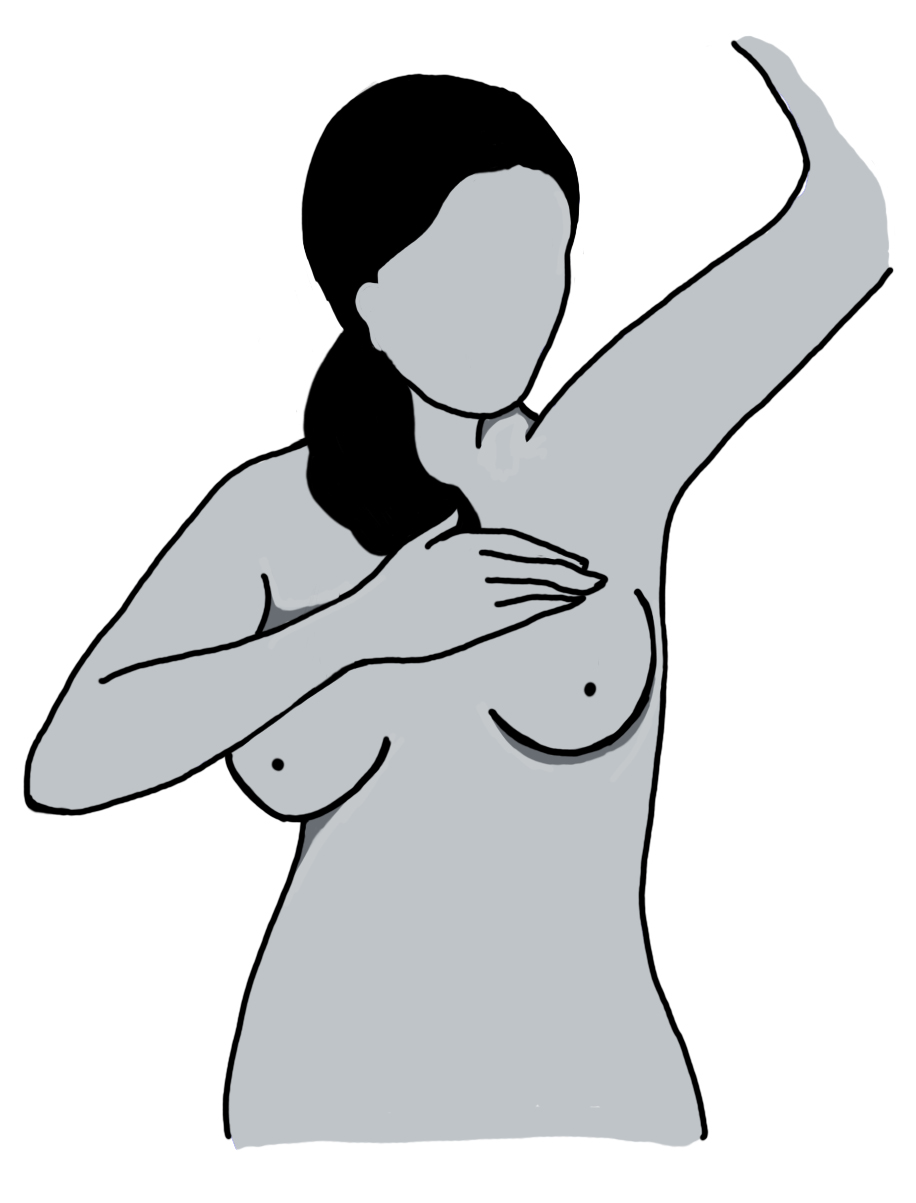 उसी तरीक़े से यह परीक्षण आप नहाते वक़्त फ़व्वारे (Shower) के नीचे खड़े होकर भी कर सकते हैं। साबुन लगाते वक़्त गीले हाथों से स्तन के ऊतकों का परीक्षण ज़्यादा गहराई और आसानी से किया जा सकता है। नहाते वक़्त जाँच करने की आदत डालें।
उसी तरीक़े से यह परीक्षण आप नहाते वक़्त फ़व्वारे (Shower) के नीचे खड़े होकर भी कर सकते हैं। साबुन लगाते वक़्त गीले हाथों से स्तन के ऊतकों का परीक्षण ज़्यादा गहराई और आसानी से किया जा सकता है। नहाते वक़्त जाँच करने की आदत डालें।- मैमोग्राफ़ी — 30‑35 वर्ष की उम्र में मैमोग्राफ़ी करवानी चाहिए, 40‑50 साल तक हर तीन साल में करवानी चाहिए और 50 साल के बाद हर साल करवानी चाहिए।
- सोनोमैमोग्राफ़ी— ऐसी ग्रंथियाँ जिनमें कोई तरल पदार्थ भरा हो, उनका परीक्षण बाहर से ही बिना चीर‑फाड़ किए किया जाता है, इसमें कोई सर्जरी नहीं होती। इसको गर्भावस्था में भी बिना किसी डर के करवा सकते हैं।
- संदेहजनक ग्रंथियों का परीक्षण पतली सुई से स्तन के अंदर के तरल पदार्थ को निकालकर बायोप्सी द्वारा किया जा सकता है।
- स्तनों में होनेवाले कई उभार या ग्रंथियाँ हमेशा कैंसर नहीं होते। (कई महिलाओं को माहवारी से पहले इस तरह की सूजन अपने स्तनों में महसूस होती है।)
- अगर आपको अपने स्तनों में इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। कोई सूजन या अलग तरह का उभार, निप्पल का अंदर की तरफ़ धँसना, निप्प्ल से ख़ून का रिसाव, स्तन की त्वचा में किसी तरह का खिंचाव, एक या दोनों स्तनों में किसी प्रकार की असामान्यता।
- स्तन कैंसर होने की संभावना: बढ़ती उम्र में गर्भधारण करना, चाहे वह पहला गर्भ हो या आख़िरी; कोई बच्चा न होना; स्तनपान न करवाया हो; बढ़ती उम्र के साथ मोटापे का बढ़ना।
- कैंसर से सुरक्षा के लिए, तनावरहित स्वस्थ जीवन जीएँ। नियमित रूप से व्यायाम करें और अपने वज़न को सही रखें। अधिक रेशेवाली लाल, पीली, हरी सब्ज़ियाँ और फल खाएँ।
- यदि आपके किसी नज़दीकी रिश्तेदार को स्तन कैंसर है, तो आपको भी इस रोग की संभावना हो सकती है। इसलिए सावधान रहें।
सरवीकल कैंसर मुख्य रूप से उन महिलाओं में होता है जो यौन संबंध बनाती हैं।
सरवीकल कैंसर की संभावना इन कारणों से बढ़ सकती है:- छोटी उम्र से या बीस साल की उम्र से पहले यौन संबंध की शुरुआत।
- Human Papilloma Virus (HPV) का संक्रमण।
- धूम्रपान करना या तंबाकू का सेवन।
- बार‑बार गर्भधारण, गर्भपात या डिलीवरी होना।
- पति या पार्टनर को लिंग का कैंसर होना।
- ग़रीबी, समाज में आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होना जिस कारण शरीर की सफ़ाई की तरफ़ ध्यान न देना।
- इम्यूनो‑सप्रेशन (Immuno-Supression) जैसा कि एच.आई.वी. के संक्रमण के कारण हो जाता है।
शुरू‑शुरू में सरवीकल कैंसर के कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन नियमित रूप से पैप स्मीअर टेस्ट (Pap Smear test) तथा परीक्षण से इसका पता चल जाता है।
पैप स्मीअर की जाँच के लिए बच्चेदानी के मुँह से, किसी लकड़ी के स्पैटुला या ब्रश से कोशिकाओं को इकट्ठा किया जाता है। इन कोशिकाओं को काँच के स्लाइड पर फैला देते हैं। डॉक्टर या अनुभवी तकनीशियन (Technician) माइक्रोस्कोप द्वारा कैंसर की कोशिकाओं की जाँच करता है।- यौन संबंध बना रही हर महिला को पैप स्मीअर टेस्ट करवाना चाहिए।
- पहला पैप स्मीअर 21 वर्ष की आयु में होना चाहिए।
- 20 से 30 वर्ष तक पैप स्मीअर हर दो साल के बाद होना चाहिए।
- 30 वर्ष की आयु के बाद यह जाँच हर 3 साल बाद होनी चाहिए।
- 65 वर्ष की आयु के बाद अगर लगातार 3 बार की जाँच में सब सही हो तो इसे फिर से करवाने की ज़रूरत नहीं है।
- जिन महिलाओं की बच्चेदानी कैंसर के अलावा किसी अन्य कारण से निकाल दी गई है, उनको यह जाँच करवाने की ज़रूरत नहीं है।
कॉल्पोस्कोपी देखकर की गई सरविक्स की जाँच — जाँच के बाद जिस स्मीअर में (H.P.V.) एच.पी.वी. का संक्रमण पाया जाए उसका कॉल्पोस्कोपी द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। संदेहजनक हिस्से की कैंसर की जाँच के लिए बायोप्सी की जाती है।
कृपया याद रखें!अगर आपको निम्नलिखित लक्षण दिखाई दें तो अपने डॉक्टर को तुरंत मिलें:
- रजोनिवृत्ति के बाद भी रक्त का रिसाव, यौन संपर्क के बाद या दो माहवारियों के दौरान रिसाव।
- योनि से दुर्गंधमय रिसाव।
- योनि के पास कोई ग्रंथि या सूजन।
- योनि के पास ख़ारिश, छाले या सफ़ेद दाग।
आँतों का कैंसर
आँतों का कैंसर (Colorectal Caner) स्त्री और पुरुष दोनों को हो सकता है।
आँतों के कैंसर के कारण:- सब्ज़ियाँ कम खाना और मांस का अधिक सेवन।
- धूम्रपान करना।
- शराब पीना।
- व्यायाम की कमी।
- शरीर का वज़न ज़्यादा बढ़ना।
- परिवार में किसी को यह रोग होना।
- अलसरेटिव कोलाइटिस।
- मल त्याग की आदत में बदलाव—जैसे पहले कब्ज़ होना, फिर दस्त लगना; ऐसा बार‑बार होते रहना।
- मल त्याग में दर्द।
- थकान, ख़ून की कमी।
- गुदा से रक्तस्राव।
- मल में मिश्रित दिखाई न देनेवाले रक्त की हर साल जाँच।
- हर साल प्रोक्टोस्कोपी (Proctoscopy) और मलाशय की जाँच।
- अगर कैंसर होने का संदेह है तब परीक्षण के अन्य तरीक़े अपनाए जाते हैं—जैसे एक्स‑रे, कोलोनोस्कॉपी या मलाशय की जाँच (एक लंबी ट्यूब को गुदा के अंदर डालकर जाँच की जाती है)।
- शाकाहारी भोजन जिसमें सब्ज़ियाँ ज़्यादा हों।
- व्यायाम।
- शरीर का वज़न को बढ़ने न दें।
- तंबाकू और शराब का सेवन न करें।
पुरुषों के स्वास्थ्य की देखभाल–प्रोस्टेट कैंसर
प्रोस्टेट (Prostate) मूत्राशय के पास अख़रोट के आकार की एक छोटी ग्रंथि है। बुज़ुर्गों में प्रोस्टेट का आकार बढ़ जाता है, लेकिन आम तौर पर यह कैंसर नहीं होता। इसे बैनाइन प्रोस्टेटिक हाईपरप्लेसिया (Benign Prostatic Hyperplasia/B.P.H.) कहते हैं। इसकी वजह से मूत्र से संबंधित अनेक परेशानियाँ हो जाती हैं जैसे रात को मूत्र त्याग करने के लिए कई बार उठना और मूत्र के वेग का धीमा हो जाना। दवाइयों से बी.पी.एच. का सफल इलाज हो सकता है। यदि दवाई से इलाज न हो, तो छोटा‑सा ऑपरेशन करके समस्या को दूर कर दिया जाता है जैसे कि मूत्र‑मार्ग में किसी रुकावट को दूर करना।
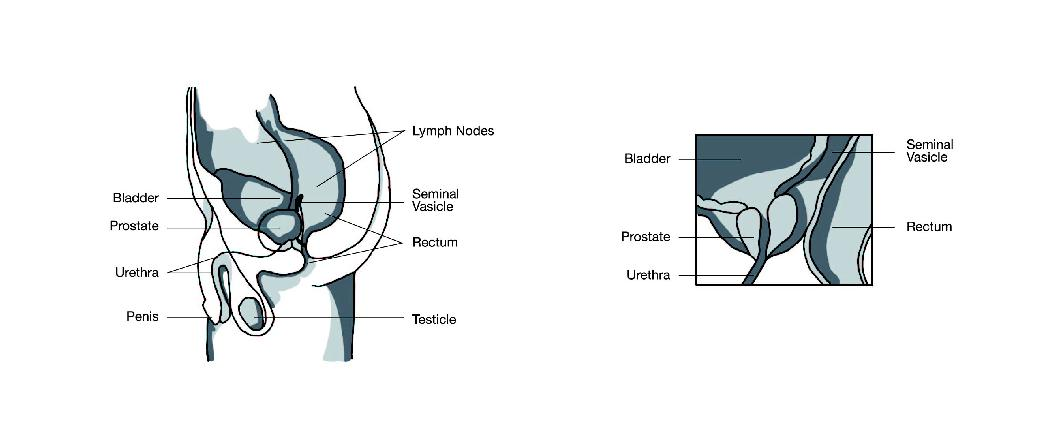
कुछ पुरुषों में प्रोस्टेट की बीमारी कैंसर बन जाती है। इसमें कई साल लग जाते हैं। बीमारी की शुरुआत में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। यदि आपका डॉक्टर जल्द ही प्रोस्टेट कैंसर का पता लगा ले तो इसका इलाज संभव है।
चरम अवस्था में जब प्रोस्टेट कैंसर पीठ की हड्डियों और पसलियों तक फैल जाए तो इससे पीड़ा होती है।
किसे ज़्यादा ख़तरा है?40 वर्ष की आयु से ऊपर के पुरुषों को प्रोस्टेट कैंसर का ख़तरा ज़्यादा है क्योंकि इस आयु के बाद कैंसर होने के आसार धीरे‑धीरे बढ़ जाते हैं।
किसान और वे लोग जो कैडमियम (रासायनिक तत्त्व) और एक्स‑रे के संपर्क में ज़्यादा आते हैं, उन्हें भी प्रोस्टेट कैंसर का ख़तरा ज़्यादा होता है।
यदि मुझे प्रोस्टेट कैंसर हो जाए तो इसका जल्दी पता लगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?40 वर्ष की आयु के बाद साल में कम से कम एक बार अपने डॉक्टर से प्रोस्टेट की जाँच करवाएँ।
यदि ख़ून की जाँच (पी.एस.ए.) उपलब्ध हो तो इसका पता जल्दी लगाया जा सकता है।
यदि कोई शक हो, तो बायोप्सी (Biopsy) करवाई जा सकती है जिसमें एक सुई के द्वारा प्रोस्टेट का नमूना लेकर जाँच की जाती है।
प्रोस्टेट कैंसर का इलाजयदि इस रोग का पता शीघ्र चल जाए तो इसका इलाज संभव है। अनेक प्रकार के वििकरण (Radiation) और ऑपरेशन के ज़रिए इसका इलाज सफलतापूर्वक हो सकता है।
यदि कैंसर बढ़ जाए तो इलाज में सबसे पहले ख़ून में मौजूद पुरुष‑हॉर्मोन (एण्ड्रोजन) की मात्रा को कम कर दिया जाता है।
हृदय रोग
दुनिया में कॉरोनरी आर्टरी की बीमारी (Coronary Artery Disease/CAD) से मरनेवाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। भारत के शहरों में रहनेवाले 10% लोग इस रोग से पीड़ित हैं। यूरोप या एशिया के दूसरे लोगों की तुलना में भारतीयों में सी.ए.डी. कुल मिलाकर दो से चार गुणा ज़्यादा है और 40 साल से कम उम्र वालों में तो पाँच से दस गुणा ज़्यादा है। अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर भारत के शहरों में रहनेवाले 7‑10% और दक्षिण भारत के शहरों में रहनेवाले 14% लोग सी.ए.डी. से पीड़ित हैं।
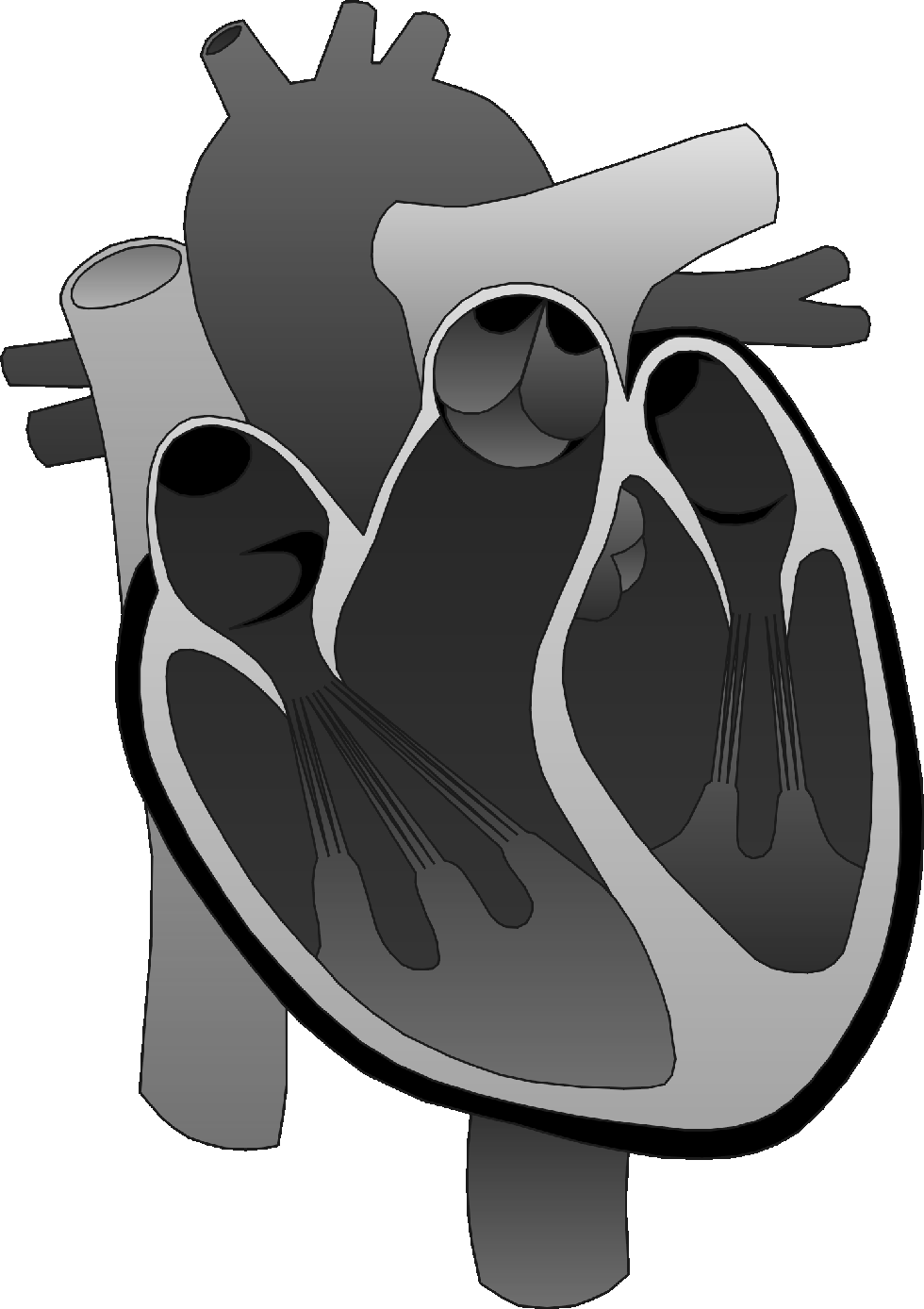 हृदय के रोगों में सी.ए.डी. सबसे ज़्यादा पाया जानेवाला रोग है। यह छाती में दर्द, दिल के दौरे और अचानक मृत्यु के रूप में प्रकट होता है।
हृदय के रोगों में सी.ए.डी. सबसे ज़्यादा पाया जानेवाला रोग है। यह छाती में दर्द, दिल के दौरे और अचानक मृत्यु के रूप में प्रकट होता है।
हृदय शरीर के सभी हिस्सों में नाड़ियों के ज़रिए ख़ून पहुँचाता है ताकि उन्हें ऑक्सीजन और पोषण मिल सके। ऑक्सीजन वह ईंधन है जो शरीर को शक्ति देता है। हृदय को भी ख़ून की ज़रूरत होती है जिसे कॉरोनरी आर्टरीज़ द्वारा पहुँचाया जाता है। जब इन कॉरोनरी आर्टरीज़ में से किसी एक में कोई रुकावट पैदा हो जाती है तो ख़ून का थक्का (Clot) बन जाने के कारण दिल का दौरा पड़ सकता है। वास्तव में आर्टरी की दीवार पर धीरे‑धीरे कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) जमना शुरू हो जाता है जो जमकर प्लाक (Plaque) बन जाता है। इससे आर्टरी में रुकावट पैदा हो जाती है।
दिल के दौरे की संभावना के लक्षण- छाती में तकलीफ़
यदि छाती में दबाव, कसाव, पीड़ा हो और छाती में भारीपन महसूस हो, जो कुछ मिनटों तक रहे और फिर बार‑बार हो, तो ये दिल के दौरे के सूचक हैं (अगर ऐसा तीस मिनट से ज़्यादा रहे और नाईट्रेट (Nitrate) की गोली का भी कोई असर न हो)।
- छाती के अलावा शरीर के अन्य अंगों में तकलीफ़
बाज़ू, पीठ, गरदन या जबड़े में भी तकलीफ़ (पीड़ा या भारीपन) हो सकती है। छाती से शुरू होकर यह दर्द बाज़ू, कंधे, जबड़े या गरदन तक जा सकता है या इन भागों से शुरू होकर छाती में जा सकता है। इनके अलावा कुछ रोगियों में पेट के ऊपरी भाग में दर्द या भारीपन का एहसास, खट्टापन या बदहज़मी भी होती है और उन्हें ऐंटैसिड (Antacid) दवाइयों से आराम नहीं मिलता। इन अवस्थाओं को नज़रअंदाज़ मत करें और दिल के दौरे की संभावना समझते हुए जाँच करवा लें।
- साँस लेने में तकलीफ़
छाती में दर्द के दौरान, इससे पहले या बाद में, साँस लेने में तकलीफ़ आती है या साँस फूलती है। इसके साथ‑साथ मितली, पसीना या चक्कर भी आ सकते हैं। कभी‑कभी बिना दर्द के साँस फूलना या बिना दर्द के दम घुटना ही दिल के दौरे का एकमात्र लक्षण हो सकता है।
 सी.ए.डी.के ख़तरे के जाने पहचाने कारण
सी.ए.डी.के ख़तरे के जाने पहचाने कारण
इन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है।
- कारण जिन्हें बदला नहीं जा सकता :
- पुरुषों में 55 और महिलाओं में 65 वर्ष से ज़्यादा आयु।
- पुरुषों की आर्टरीज़ में चर्बी जमने के आसार ज़्यादा होते हैं।
- परिवार में 55 वर्ष की आयु से पहले सी.ए.डी. होने का इतिहास (माता‑पिता, दादा‑दादी या नाना‑नानी को 55 साल की आयु से पहले सी.ए.डी. हुई हो)।
- कारण जिन्हें बदला जा सकता है :
- ख़ून में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता।
- धूम्रपान या तंबाकू चबाना (अब कर रहे हों या पहले कभी किया हो)।
- हाई ब्लड प्रेशर (BP)।
- शारीरिक व्यायाम की कमी।
- मधुमेह।
- मानसिक तनाव।
- मोटापा, ख़ास तौर से तोंद होना (कमर और कूल्हे का अनुपात, पुरुषों में 0.95 से ज़्यादा और महिलाओं में 0.85 से अधिक होना।)
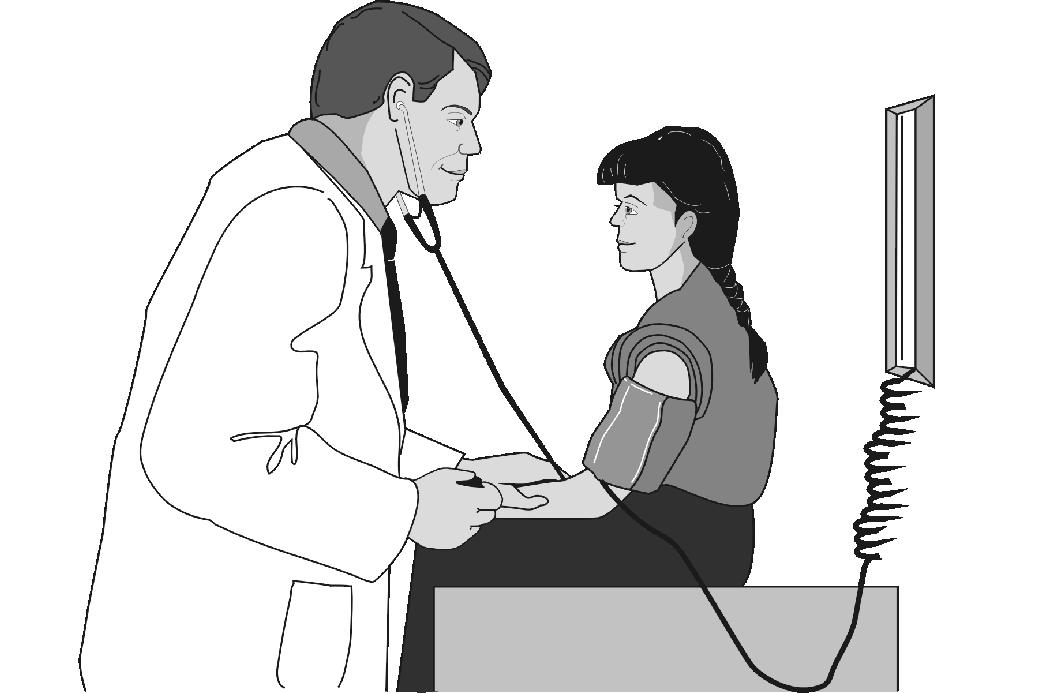
- भारत में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं है; धूम्रपान ज़्यादातर पश्चिमी देशों में ही व्याप्त है।
- भारतीयों में कोलेस्ट्रॉल की औसत मात्रा भी कम है। फिर भी कम उम्र के भारतीयों में सी.ए.डी. होने के आसार काफ़ी हैं।
- मधुमेह के रोगियों की बढ़ती संख्या।
- ख़ून में ट्राइग्लिसराइड्स (Triglycerides) का अधिक होना या अच्छे कोलेस्ट्रॉल (एच.डी.एल.) की मात्रा कम होना।
- पेट का ज़्यादा मोटापा, सी.ए.डी. के ख़तरे का एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा, ख़ून में इंसुलिन की अधिकता के कारण और इंसुलिन के असर में रुकावट के कारण है। इस रुकावट से ख़ून में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा अधिक और एच.डी.एल. की मात्रा कम हो जाती है, पेट पर चर्बी जमा हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह होने के आसार अधिक हो जाते हैं और इन सब की वजह से सी.ए.डी. होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसे सिंड्रोम एक्स (Syndrome X) या मेटाबॉलिक सिंड्रोम (Metabolic Syndrome) भी कहा जाता है।
- शारीरिक व्यायाम की कमी।
- देसी घी और नारियल के तेल का अधिक इस्तेमाल।
- वनस्पति घी (हाइड्रोजिनेटड फ़ैट्स) का अधिक प्रयोग।
- लाइपोप्रोटीन ए: यह एक ख़ास तरह का कोलेस्ट्रॉल है जो सी.ए.डी. का ख़तरा पैदा करता है। यूरोप और चीन के लोगों की तुलना में भारतीयों में इसकी मात्रा तीन से चार गुणा अधिक पाई गई है।
- आनुवंशिक तौर पर (Genetically) ट्राइग्लिसराइड्स का अधिक और एच.डी.एल. का कम होना।
आम तौर पर सुबह 4 से 10 बजे के बीच सबसे ज़्यादा दिल के दौरे पड़ते हैं। ऐसा शायद इसलिए है कि सुबह के समय ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, ख़ून को जमने से रोकनेवाली प्रक्रिया इस समय नाममात्र होती है। सुबह के वक़्त कॉरोनरी आर्टरीज़ भी संकुचित रहती हैं।
यदि दिल का दौरा पड़ने का शक हो तो क्या करें?- तुरंत किसी पास के अस्पताल में जाएँ।
- यदि चक्कर न आ रहे हों तो अस्पताल जाते समय सीधे बैठें।
- यदि डॉक्टर ने छाती में दर्द के लिए पहले से नाइट्रोग्लिसरीन की गोली का सेवन करने को कहा हो तो एक गोली जीभ के नीचे रखें।
- पानी के साथ ऐस्प्रिन की एक गोली लें, यह दिल के नुकसान को रोक सकती है।
सी.ए.डी. की रोकथाम
सी.ए.डी. की रोकथाम में भोजन की भूमिकाइसकी रोकथाम के लिए संतुलित आहार लेना और ख़ुशनुमा जीवन व्यतीत करना बहुत महत्त्वपूर्ण है। कुछ हालात में दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ सकती है।
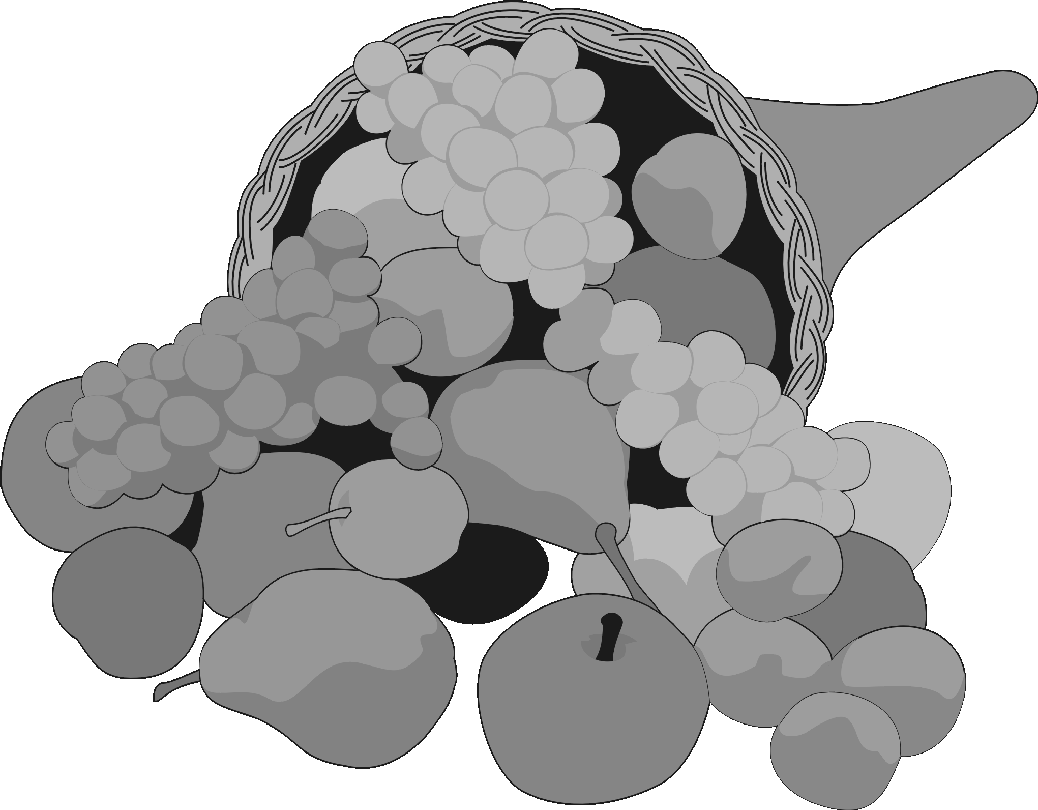 स्वस्थ आहार लेने के मूलभूत नियम
स्वस्थ आहार लेने के मूलभूत नियम
- विविध प्रकार के भोजन का सेवन करें।
- संतुलित मात्रा में ज़रूरत के मुताबिक़ खाएँ।
- चिकनाई वाले पदार्थ कम खाएँ।
- सैचुरेटिड फ़ैट्स (जैसे मक्खन, क्रीम, चॉकलेट आदि) का सेवन कम करें।
- हाइड्रोजिनेटिड फ़ैट्स (जैसे कि वनस्पति घी) कम खाएँ।
- कोलेस्ट्रॉल बढ़ानेवाली चीज़ें कम मात्रा में खाएँ।
- फ़ाइबर वाले खाद्य पदार्थ सही मात्रा में खाएँ।
- चीनी, मैदा, कैफ़ीन (चाय, कॉफ़ी) और नमक आदि का प्रयोग कम करें।
- अनाज, दाल, फल और सब्ज़ियों का सेवन ख़ूब करें।
- कम चिकनाई वाले दूध से बने पदार्थों का सेवन करें।
- चिकनाई वाली चीज़ों का प्रयोग कम करें, ख़ास तौर पर तले और मीठे पदार्थ कम खाएँ।
- बिना चिकनाई का दूध (toned or double toned) पिएँ और इसी दूध के पदार्थों का सेवन करें।
- ताज़ा फल और सब्ज़ियों का सेवन अधिक करें।
- कम चिकनाई की मिठाइयों और स्नैक्स का सेवन करें।
- खाना बनाने में तेल का प्रयोग कम करें ताकि भोजन में चिकनाई की कुल मात्रा कम रहे।
- खाना बनाने की इन विधियों का प्रयोग करें—भाप में पकाना, ग्रिल पर भूनना, उबालना, सेंकना और माइक्रोवेव में पकाना।
सैचुरेटिड फ़ैटी एसिड्स के बजाय अनसैचुरेटिड फ़ैटी एसिड्स (पूफ़ा/PUFA—Polyunsaturated fatty acids और मूफ़ा/MUFA—Monounsaturated fatty acids) का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। सैचुरेटिड फ़ैटी एसिड्स (ख़राब कोलेस्ट्रॉल) एल.डी.एल. को बढ़ाते हैं, जिनसे सी.ए.डी. होने का ख़तरा बढ़ जाता है, जबकि अनसैचुरेटिड फ़ैटी एसिड्स (पूफ़ा और मूफ़ा) एल.डी.एल. को कम करते हैं।
हालाँकि जिन अनसैचुरेटिड फ़ैटी एसिड्स में पूफ़ा की मात्रा ज़्यादा होती है, वे भी हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि इनसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल (एच.डी.एल.) की मात्रा कम हो सकती है। इसलिए उन रिफ़ाइंड तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें पूफ़ा और मूफ़ा का सही संतुलन हो ताकि सैचुरेटिड फ़ैटी एसिड्स का इस्तेमाल कम हो।
कोई भी एक रिफ़ाइंड तेल ऐसा नहीं है जिसमें पूफ़ा और मूफ़ा का सही संतुलन हो। यदि हम भिन्न‑भिन्न प्रकार के तेलों का इस्तेमाल करें तो उपयुक्त संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सूर्यमुखी तेल (जिसमें पूफ़ा की मात्रा ज़्यादा होती है) और सरसों के तेल (जिसमें मूफ़ा की मात्रा अधिक होती है) का प्रयोग करें। कुछ तेलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं जिनके मिश्रण से पूफ़ा और मूफ़ा का सही संतुलन प्राप्त हो सकता है:- मूँगफली का तेल + सरसों का तेल
- तिल का तेल+सरसों का तेल
- चावल की भूसी का तेल + सोयाबीन का तेल
सैचुरेटिड फ़ैटी एसिड्स सामान्य तापमान पर जमी हुई या आधी जमी हुई (Solid or semi solid) अवस्था में होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं: नारियल का तेल, वनस्पति और देसी घी। अनसैचुरेटिड फ़ैटी एसिड्स सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं: कुसुंभ (Safflower), सूर्यमुखी, तिल, चावल की भूसी का तेल, सरसों, मूँगफली और सोयाबीन के तेल।
सी.ए.डी. की रोकथाम में फ़ाइबर (Fibre) का महत्त्वफ़ाइबर या रेशा भोजन का वह भाग है जो हज़म नहीं होता। घुलनेवाले फ़ाइबर कब्ज़ और अँतड़ियों के कैंसर को रोकते हैं।
 घुलनेवाले फ़ाइबर या रेशे (soluble Fibre) के स्रोत
घुलनेवाले फ़ाइबर या रेशे (soluble Fibre) के स्रोत
जई (Oats), फलियाँ, गुड़, जौ, सेब, गाजर और नीबू, संतरा, मौसम्मी आदि फल।
न घुलनेवाले फ़ाइबर (Insoluble Fibre) के स्रोतगेहूँ का बिना छना आटा, चोकर, हरी सब्ज़ियाँ और फल इत्यादि।
फ़ाइबर के फ़ायदे- इससे वज़न घटता है।
- ख़ून में मौजूद ग्लूकोज़ और सीरम लिपिड (Serum lipids) कम रहते हैं।
- आँतों की कई क़िस्म की छोटी‑मोटी बीमारियों, विकारों (disorders) और मलाशय के कैंसर से बचाव होता है।
- कब्ज़ दूर करता है।
- ऐसे भोजन से संतुष्टि मिलती है और कम खाने से भी पेट भर जाने का एहसास होता है।
- यह विटामिन्स और खनिज पदार्थों का भी अच्छा स्रोत है।
- सेब और नाशपाती जैसे फलों को छिलके समेत खाएँ।
- अंकुरित दालें, राजमा, काले चने, सोयाबीन का सेवन करें और धुली हुई दालों के बजाय छिलके वाली दालें (मूँग, उड़द) खाएँ।
- गेहूँ का आटा न छानें।
- सफ़ेद ब्रैड के बजाय ब्राउन ब्रैड का इस्तेमाल करें।
- हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ और सलाद नियमित रूप से खाएँ।
- इडली, पोहा, उपमा, चावल, दलिया, नूडल्स, मैकरोनी और पास्ता को बहुत‑सी सब्ज़ियाँ डालकर बनाएँ ताकि आपका भोजन फ़ाइबर से भरपूर हो।
- भोजन में मेथी (बीज/पाउडर) का इस्तेमाल करें।
- नाश्ते में कॉर्न फ़्लेक्स की जगह सफ़ेद जई (White Oats) का इस्तेमाल करें।
- नान, रूमाली रोटी और पराँठे के बजाय बिना छने आटे की रोटी या भरवाँ (पालक, गोभी, मूली) रोटी खाएँ।
ज़्यादा चीनी खाने से वज़न बढ़ता है और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा भी बढ़ती है।
अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर दवाइयाँ लेने की ज़रूरत कब होती है?संतुलित भोजन के साथ‑साथ दवाइयों की ज़रूरत तब पड़ती है जब:
- शरीर में असामान्य लिपिड प्रोफ़ाइल (lipid profile) होने की आनुवंशिक प्रवृत्ति (Genetic Predisposition) हो। (एच.डी.एल, एल.डी.एल, लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स—इन सब के जोड़ को लिपिड प्रोफ़ाइल कहा जाता है।)
- ख़ून में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत बढ़ जाए (कोलेस्ट्रॉल 250 मिलिग्राम/डी एल और ट्राइग्लिसराइड्स 200 मिलिग्राम/डी एल से अधिक)।
- भोजन और दिनचर्या में बदलाव लाने से भी इनमें कोई फ़र्क़ न पड़े।
दवाइयों के असर और सुरक्षा पर नज़र रखने के लिए समय‑समय पर लिपिड प्रोफ़ाइल और लिवर की जाँच कराते रहना चाहिए। दवाइयों का इस्तेमाल जीवन भर करते रहने की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। देखने में आया है कि जब दवाइयों का सेवन बंद होता है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा फिर से बढ़ जाती है। नियंत्रित भोजन और दवाइयों के इस्तेमाल से हृदय रोग नियंत्रण में रहता है, आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल का जमना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि पहले से जमा कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लगता है।
स्वस्थ दिल के लिए भोजन तालिका
| भोजन | क्या खाएँ | क्या कम करें | इन से बचें |
|---|---|---|---|
| अनाज | गेहूँ, चावल, रागी, बाजरा, मकई, ज्वार | मैदे से बने पदार्थ जैसे (सफ़ेद ब्रैड और बिस्कुट) | केक, पेस्ट्री, नान, रूमाली रोटी, नूडल्स |
| दालें | साबुत और अंकुरित दालें | – | – |
| सब्ज़ियाँ | हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ और अन्य सब्ज़ियाँ | सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के नीचे पैदा होती हैं जैसे आलू, अरबी, ज़मींकंद | तली सब्ज़ियाँ, केले के चिप्स, डिब्बाबंद सब्ज़ियाँ |
| फल | ताज़े फल | – | सूखे मेवे, चाशनी वाले डिब्बाबंद फल |
| दूध के पदार्थ | कम वसा वाला दूध, छाछ, बिना मलाई का दूध | मलाई वाला दूध, दूध पाउडर | चीज़, मक्खन, खोया, कंडैंस्ड मिल्क, क्रीम |
| वसा | एक से अधिक प्रकार का वनस्पति तेल या उनका मिश्रण | कुल वसा की मात्रा, नारियल का तेल, घी | अधिक तेलवाला भोजन, मक्खन, घी, नारियल तेल, वनस्पति घी, अधिक तेल में तला भोजन |
| चीनी और चीनी से बने पदार्थ |
चीनी, गुड़ | घर पर बने किसी पेय में चीनी, सब प्रकार की गिरियाँ | मिठाइयाँ, चॉकलेट, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, जलेबी आदि |
| गिरियाँ | – | सभी गिरियाँ | – |
| पेय | पानी, ताज़े फलों का जूस (बिना चीनी के), हलकी चाय | कॉफ़ी, कोला, सॉफ़्ट ड्रिंक्स | अल्कोहल/शराब |
| नमक | प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध भोजन (बिना नमक के) (डिब्बाबंद नहीं) | भोजन में अधिक नमक | अचार, पापड़, चटनियाँ, नमक, बिस्कुट, तेल में तले चिप्स आदि |
भोजन में नमक की मात्रा
| सब्ज़ियाँ | मिलिग्राम |
|---|---|
| करेला | 2.4 |
| परवल | 2.6 |
| बैंगन | 3.0 |
| प्याज़ | 4.0 |
| फ़्रेंच बीन | 4.3 |
| कद्दू | 5.6 |
| भिंडी | 6.9 |
| हरे मटर | 7.8 |
| अरबी | 9.0 |
| शकरकंदी | 9.0 |
| खीरा | 10.2 |
| आलू | 11.0 |
| पका हुआ टमाटर | 12.9 |
| सफ़ेद मूली | 33.0 |
| टिंडा | 35.0 |
| गाजर | 35.6 |
| फूल गोभी | 53.0 |
| लैट्यूस (सलाद के पत्ते) | 58.0 |
| पालक | 58.2 |
| धनिये के पत्ते | 58.3 |
| चुकंदर | 59.8 |
| कटहल | 63.2 |
| लाल मूली | 63.5 |
| मेथी के पत्ते | 76.1 |
| कमल ककड़ी (भिस) | 438.0 |
| अन्य | मिलिग्राम |
|---|---|
| भैंस का दूध | 19.0 |
| धनिया (साबुत) | 32.0 |
| गाय के दूध से बना दही | 32.0 |
| नीम के पत्ते | 72.0 |
| गाय का दूध | 73.0 |
| जीरा | 126.0 |
| फल | मिलिग्राम |
|---|---|
| आलू बुख़ारा | 0.8 |
| अनार | 0.9 |
| आड़ू | 2.0 |
| फालसा | 4.4 |
| संतरा | 4.5 |
| अमरूद | 5.5 |
| चीकू | 5.9 |
| पका हुआ पपीता | 6.0 |
| नाशपाती | 6.1 |
| हरा पपीता (कच्चा) | 23.0 |
| पका हुआ आम | 26.0 |
| तरबूज़ | 27.3 |
| सेब | 28.0 |
| अनानास | 34.7 |
| केला | 36.6 |
| कच्चा आम | 43.0 |
| खरबूज़ा | 104.6 |
| लीची | 124.9 |
| अनाज | मिलिग्राम |
|---|---|
| ज्वार | 7.3 |
| गेहूँ की सेवइयाँ | 7.9 |
| गेहूँ का छाना आटा/मैदा | 9.3 |
| मक्की सूखी | 15.9 |
| गेहूँ का आटा | 20.0 |
| सूजी | 21.0 |
| मूँग छिलका | 27.2 |
| मसूर दाल | 28.5 |
| काला चना | 37.3 |
| उरद दाल साबुत | 38.8 |
| मूँग साबुत | 41.1 |
| चना दाल | 73.2 |
| चौलाई | 230.0 |
बीस वर्ष की आयु के सभी लोगों को लिपिड प्रोफ़ाइल करवाना चाहिए। इससे सी.ए.डी. होने के ख़तरे का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे यह भी पता लग सकता है कि आनुवंशिक रूप से (genetic) कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर ख़तरनाक तो नहीं! यदि बीस वर्ष की आयु में लिपिड प्रोफ़ाइल सही है तो पाँच साल बाद फिर जाँच करवानी चाहिए।
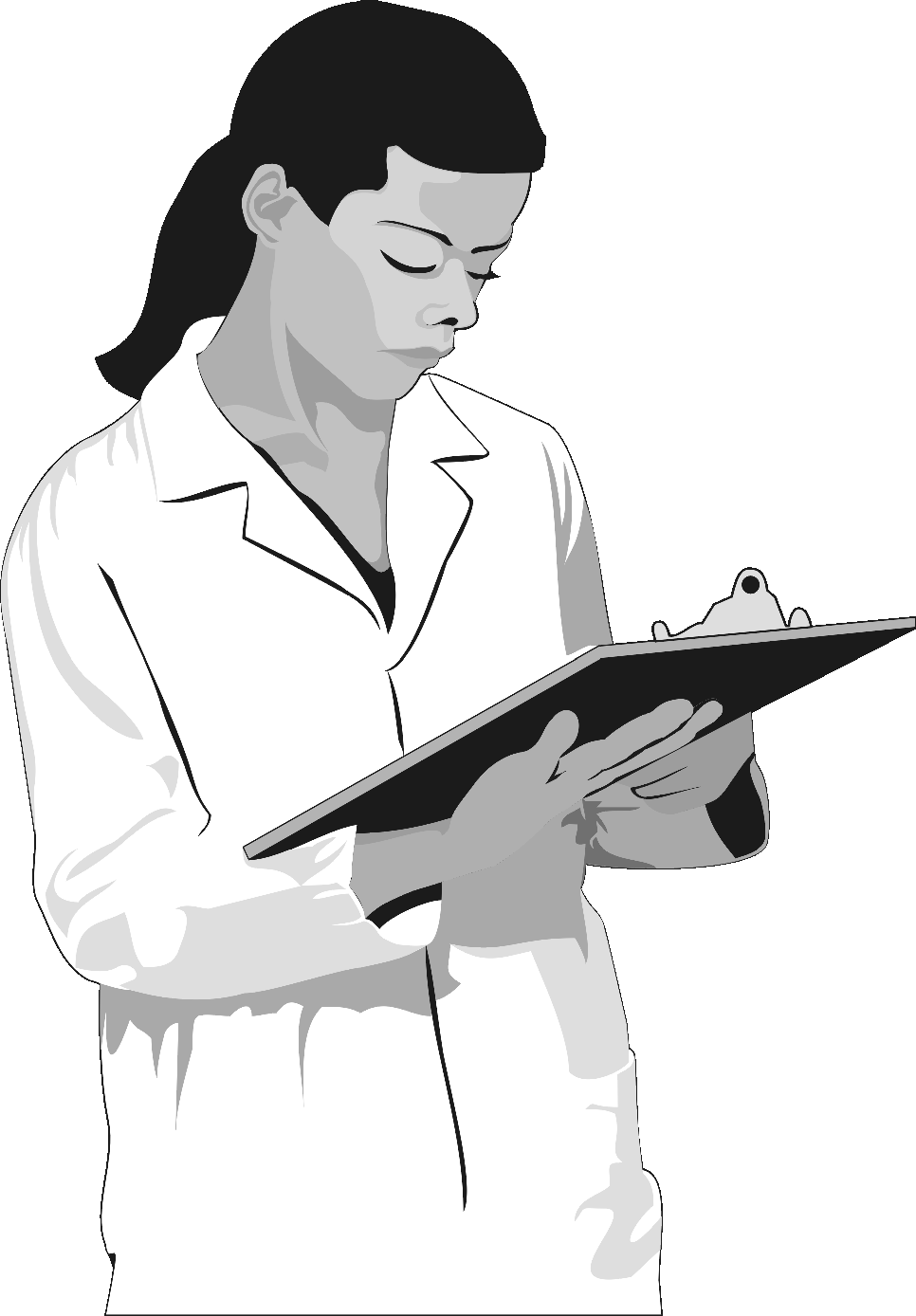
लिपिड की उचित मात्रा
| लिपिड | उचित मात्रा |
|---|---|
| कोलेस्ट्रॉल | 200 मिलिग्राम% से कम |
| एल.डी.एल. कोलेस्ट्रॉल | 100 मिलिग्राम% से कम |
| एच.डी.एल. कोलेस्ट्रॉल | पुरुषों के लिए 40 मिलिग्राम/डी एल से ज़्यादा महिलाओं के लिए 60 मिलिग्राम/डी एल से ज़्यादा |
| ट्राइग्लिसराइड्स | 150 मिलिग्राम/डी एल से कम |
- परिवार में किसी सदस्य का 55 वर्ष की आयु से पहले, सी.ए.डी. या स्ट्रोक होने का इतिहास।
- परिवार में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होने का इतिहास।
- पलकों पर दूधिया चर्बी का धब्बों के रूप में जमना।
- मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह या थायरॉयड की समस्या।
- शराब के अत्यधिक सेवन का इतिहास।
- गर्भनिरोधक गोलियों का कई सालों तक सेवन करना।
स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम सबसे ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करने से सी.ए.डी. और अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। इससे ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन नियंत्रण में रहते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ने के आसार बहुत कम हो जाते हैं। व्यायाम करते रहने से ख़ून में एच.डी.एल. कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है जो ख़ून की नाड़ियों में चर्बी को जमने से रोकता है और दिल के दौरे से बचाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नियमित व्यायाम से अपनी दवा कम या पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। व्यायाम से टाँगों में ख़ून का दौरा बढ़ जाता है और टाँगों में ऐंठन कम होती है।
हफ़्ते में 3‑5 दिन, 30 मिनट के लिए हलकी कसरत करनी चाहिए। धीरे‑धीरे व्यायाम का स्तर बढ़ाया भी जा सकता है। तेज़ चलना, तैरना, साइकिल चलाना या हलके खेल जैसे बैडमिंटन या टेबल टेनिस अच्छे व्यायाम हैं। वज़न उठाने (Weight Lifting) जैसा भारी व्यायाम स्वस्थ रहने में मदद नहीं करता परंतु इससे ताक़त ज़रूर बढ़ती है।
व्यायाम में सुरक्षा के नियम- व्यायाम भोजन से पहले या उसके दो घंटे बाद करें।
- बीमारी की हालत में व्यायाम न करें।
- व्यायाम को दो हफ़्ते से ज़्यादा बंद न करें।
- अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो ज़्यादा भारी व्यायाम से परहेज़ करें।
- साँस रोककर न रखें।
- मुश्किल और ऐसे व्यायाम जिन्हें करने में तकलीफ़ हो, न करें।
- मोटे लोगों को हलकी कसरत करनी चाहिए जैसे तेज़ चलना। धीरे‑धीरे उसके स्तर को बढ़ा सकते हैं।
- ज़्यादा गरमी में व्यायाम कुछ कम कर दें।
- बहुत ज़्यादा सर्दी के मौसम में बचाव के लिए गरम कपड़े पहनें।
- पानी ख़ूब पिएँ।
तनाव से हमारा सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है जिससे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कॉरोनरी आर्टरीज़ सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की माँग बढ़ जाती है। तनाव से इन नाड़ियों में ख़ून के जमने (clot) के आसार भी बढ़ जाते हैं।
यह कहना आसान है पर करना मुश्किल है, लेकिन इन उपायों द्वारा तनाव दूर करने का प्रयास करें:- तनाव दूर करनेवाले व्यायाम।
- ध्यान‑मनन।
- शुग़ल और शौक (Hobbies) पूरे करें।
- चुस्त रहें (Physical Activity)।
- सकारात्मक सोच रखें।
- योगाभ्यास।
धूम्रपान सी.ए.डी. का एक ख़तरनाक कारण है। दरअसल 40 वर्ष से कम आयु के लोगों में सी.ए.डी. का मुख्य कारण धूम्रपान है। धूम्रपान न करनेवालों की तुलना में धूम्रपान करनेवाले लोग सी.ए.डी. से तीन से पाँच गुणा ज़्यादा पीड़ित हैं। तंबाकू में मौजूद निकोटीन से दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं और ख़ून की नाड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं।
क्या धूम्रपान छोड़ने से फ़ायदा होता है?ज़िंदगी भर धूम्रपान करनेवाले लोगों में भी देखा गया है कि धूम्रपान बंद करने के एक साल के अंदर ही सी.ए.डी. का ख़तरा कम होना शुरू हो जाता है। धूम्रपान से परहेज़ करने से सी.ए.डी. का ख़तरा लगातार घटता जाता है। (देखें पृष्ठ 71)
तनाव पर नियंत्रणहम तनाव पर नियंत्रण करना सीख सकते हैं। सबसे पहले, अपने तनाव का कारण पता करें। उसके बाद जब भी संभव हो, उन परिस्थितियों में बदलाव लाने की कोशिश करें। तीसरा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तनाव दूर करने के तरीक़ों को अपनाएँ।
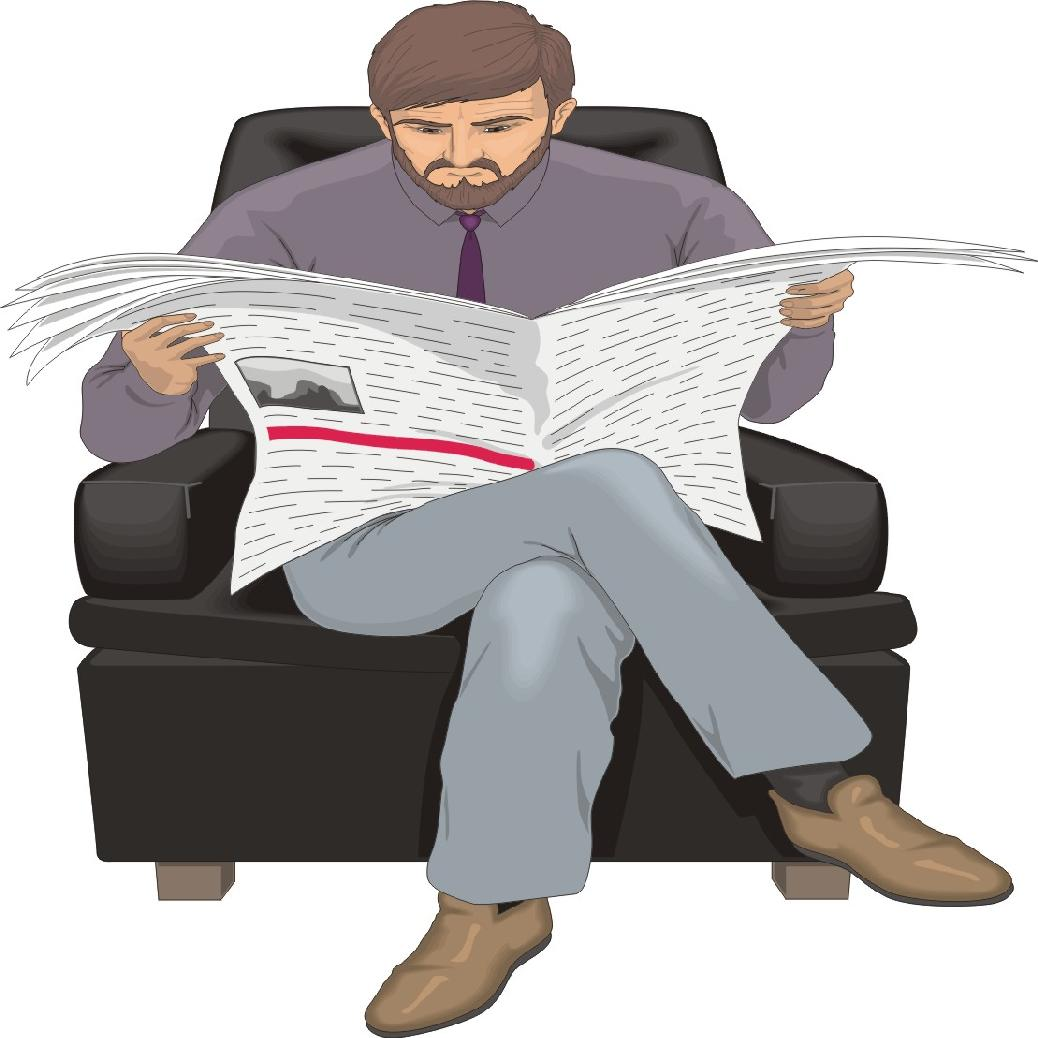 तनाव दूर करने के लिए कुछ सुझाव:
तनाव दूर करने के लिए कुछ सुझाव:
- छोटी‑छोटी बातों से परेशान होकर अपनी ताक़त व्यर्थ न गँवाएँ। याद रखें कि कोई भी स्थिति अपने आप में तनावपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया तनाव पैदा करती है। खुलकर बात करने से अकसर फ़ायदा होता है। दूसरों के विचार सुनकर अन्य पहलू भी सामने आते हैं और अपना दिल हलका करने का अवसर भी मिलता है।
- कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति से दूर चले जाएँ। जैसे तनाव दूर करने में सैर फ़ायदेमंद है। सुबह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए दोपहर के भोजन से पहले सैर करना या दफ़्तर के काम के बाद सैर करना।
- बड़े‑बड़े ख़याली पुलाव न बनाएँ। अपनी प्राथमिकताएँ तय करें, अपने सामने व्यावहारिक लक्ष्य रखें और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम का भार न लें।
- आराम के लिए रोज़ समय निकालें, चाहे तनाव दूर करनेवाले व्यायाम द्वारा या अपने मनपसंद के शौक में समय बिताएँ।
- आलोचना या किसी से हुए वाद‑विवाद को दिल से न लगाएँ। यदि आपको लगता है कि आपकी सोच सही है तो उस पर दृढ़ रहिए, लेकिन दूसरे के नज़रिए को स्वीकार करने की भी कोशिश करें। किसी वाद‑विवाद में या किसी आलोचक में भी अच्छाई ढूँढ़ने का प्रयत्न करें और अपनी सोच भी सकारात्मक रखें।
- अंत में, यदि फिर भी तनाव दूर न हो तो डॉक्टर या स्वास्थ्य परामर्श देनेवालों से इसके बारे में बात करें।
मोटापे से दिल का जानलेवा दौरा पड़ने के आसार बढ़ जाते हैं क्योंकि:
- धूम्रपान के सिवाय मोटापा सी.ए.डी. के सभी कारणों से जुड़ा है।
- वज़न बढ़ने के साथ‑साथ ख़ून में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स तथा शुगर बढ़ जाते हैं, साथ ही ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है।
- ज़रूरत से ज़्यादा मोटापे से अच्छा कोलेस्ट्रॉल (एच.डी.एल.) कम हो जाता है।
बॉडी मास इंडेक्स (बी.एम.आई.) से मोटापे को मापा जा सकता है। बी.एम.आई. इस तरह से आँका जाता है।
| भार ऊँचाई2 | |
|---|---|
| सामान्य बी.एम.आई. | 19 – 24.9 |
| ज़्यादा वज़न | 25 – 29.9 |
| मोटापा | 30 – 40 |
| विकृत मोटापा (Morbid Obesity) | 40 से ज़्यादा |
जी हाँ, वज़न कम करने से हाई ब्लड प्रेशर अकसर सामान्य हो जाता है। इससे शुगर का स्तर ठीक होने लगता है और मधुमेह नियंत्रण में आ जाता है। इससे सीने में दर्द का बार‑बार होना और उसकी तीव्रता भी कम हो जाती है, दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा कम हो जाता है और हृदय की ख़ून को पंप करने की क्षमता बढ़ती है।
दिल के दौरे के लक्षणों को नज़रअंदाज़ मत कीजिए
डॉक्टरी सहायता माँगने से न हिचकिचाइए।
मधुमेह
भारत में मधुमेह की बीमारी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी है। शहरों में हर चौथे या पाँचवें घर में एक मधुमेह का मरीज़ पाया जाता है। पिछले कुछ सालों से मधुमेह के मरीज़ों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। कुछ दशक पहले 2% युवक मधुमेह का शिकार थे लेकिन पिछले बीस‑तीस सालों में इनकी संख्या तेज़ी से बढ़कर 8‑10% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि 2025 तक भारत में इस रोग के पाँच करोड़ सत्तर लाख मरीज़ होंगे। हालाँकि इस रोग का कोई स्थायी इलाज नहीं है लेकिन आधुनिक चिकित्सा में प्रगति के कारण इसका मरीज़ आम लोगों की तरह ही सामान्य, चुस्त और उपयोगी जीवन जीने की आशा कर सकता है।
मधुमेह क्या है?मधुमेह के रोगी के शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण या इंसुलिन के सही ढंग से कार्य न करने से ख़ून में शुगर (ग्लूकोज़) की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। शरीर की कोशिकाओं में शुगर की ज़रूरत होती है जिसे इंसुलिन वहाँ पहुँचाती है। ऐसा समझें कि इंसुलिन के न होने से या कम मात्रा में होने से ख़ून में पैदा होनेवाली शुगर शरीर की कोशिकाओं में नहीं जा पाती और ख़ून में ही अधिक मात्रा में इकट्ठी होने लगती है।
मधुमेह में क्या होता है?जब इंसुलिन (Insulin) की कमी के कारण कोशिकाओं में ग्लूकोज़ नहीं जा पाता तो यह ख़ून में ही इकट्ठा हो जाता है। जब यह एक ख़ास स्तर को पार कर जाए तो पेशाब में आने लगता है। सामान्य पेशाब में ग्लूकोज़ नहीं होता।
जब पेशाब में ग्लूकोज़ आता है तो यह शरीर से बहुत‑सा पानी भी साथ ले आता है, जिसके कारण पेशाब अधिक मात्रा में आता है। ज़्यादा पेशाब आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे प्यास ज़्यादा लगती है। भले ही ख़ून में ग्लूकोज़ ज़्यादा मात्रा में होता है लेकिन इंसुलिन की कमी के कारण कोशिकाओं में नहीं पहुँचता। इसलिए कोशिकाओं में ग्लूकोज़ की कमी हो जाती है। इससे व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगती है। इसलिए मधुमेह का रोगी ज़्यादा खाता है, लेकिन कोशिकाओं को पर्याप्त ग्लूकोज़ नहीं मिलता। कोशिकाओं को ताक़त की सख़्त ज़रूरत होती है इसलिए वे शरीर की चर्बी और प्रोटीन को इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। इस कारण वज़न में कमी और थकान होने लगती है, ऐसा केवल टाइप I मधुमेह में होता है। ख़ून में ज़्यादा ग्लूकोज़ होने से कुछ लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। कभी‑कभी ख़ून में ग्लूकोज़ की मात्रा बहुत अधिक हो जाने से रोगी कोमा (Coma) में भी चला जाता है। साथ ही संक्रमण होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके लक्षण आम तौर पर दिखाई नहीं देते।
मधुमेह के सामान्य लक्षण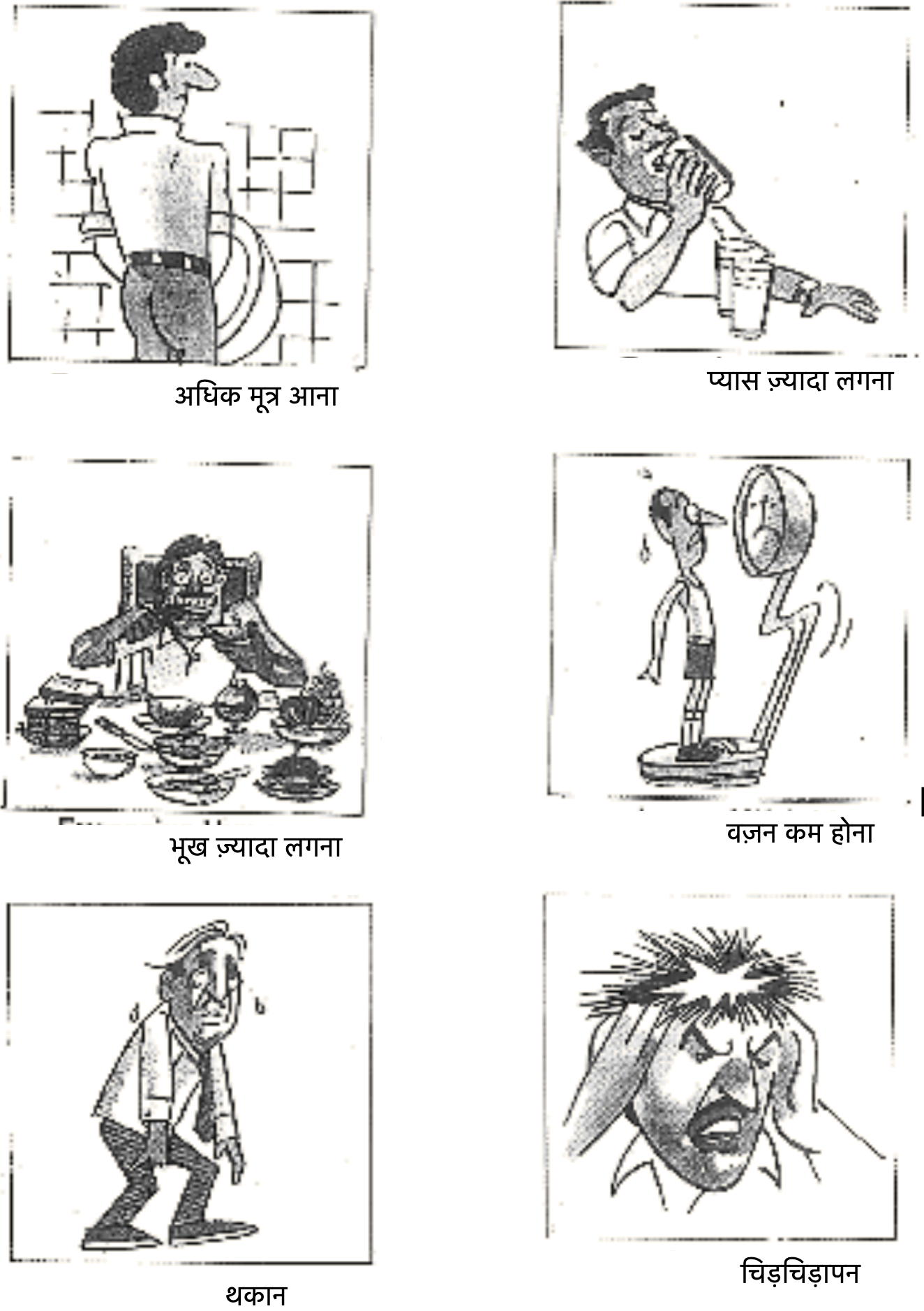 मधुमेह का क्या कारण है?
मधुमेह का क्या कारण है?
मुख्य रूप से मधुमेह के दो कारण हैं:
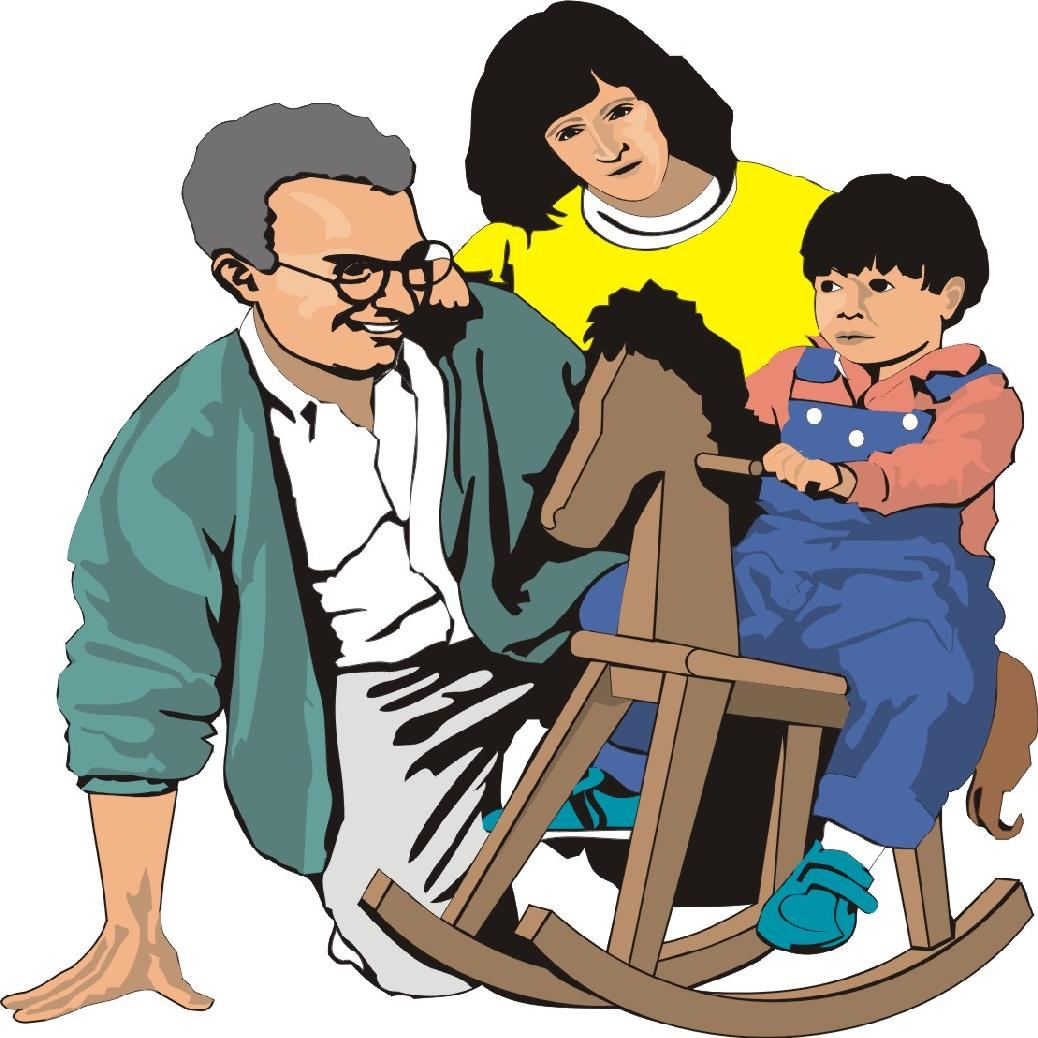
आनुवंशिक कारण (Hereditary factors) : कुछ जन्मजात कारणों से (genetic factors) बच्चे माता‑पिता से यह रोग प्राप्त करते हैं। इसी लिए कुछ परिवारों में यह रोग ज़्यादा होता है। यदि माता या पिता में से किसी एक को यह रोग है तो बच्चे को यह रोग होने की 20% संभावना है और यदि माता और पिता दोनों को मधुमेह है तो बच्चे को मधुमेह होने की संभावना 20‑50% होती है।
- वातावरण और आदतों के कारण (Environmental factors) :
- मोटापा।
- शारीरिक आलस।
- व्यायाम की कमी।
- भोजन का सही चुनाव न करना, जैसे ज़्यादा मीठा, ज़्यादा वसा और कम रेशे वाला भोजन, फ़ास्ट फ़ूड खाना।
इन कारणों से उन लोगों को मधुमेह होने के आसार ज़्यादा हैं जिनमें आनुवंशिक (hereditary) मधुमेह रोग के तत्त्व मिलते हैं।
क्या मधुमेह के सभी रोगी एक-से होते हैं?नहीं, मधुमेह के सभी रोगी एक‑से नहीं होते। मधुमेह के रोगियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।
टाइप I- यह रोग कम उम्र में, ज़्यादातर बचपन में हो जाता है।
- रोगी जवान और दुबले‑पतले होते हैं।
- बीमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है।
- रोगी को सारी उम्र इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है।
- चालीस वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को होता है।
- रोगी का वज़न आम तौर पर ज़्यादा होता है और उसकी तोंद होती है।
- बीमारी धीरे‑धीरे बढ़ती है।
- यह ज़रूरी नहीं है कि रोगी इंसुलिन पर हो लेकिन रोग को नियंत्रित करने के लिए अकसर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है।
- पहले स्तर पर रोकथाम: उन रोगियों पर लागू होती है जिनमें मधुमेह होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप ज़्यादा खतरे वाली श्रेणी में हैं, यदि:
- आपका कोई रिश्तेदार मधुमेह से पीड़ित है।
- आपका वज़न ज़्यादा है (बी.एम.आई.> 25 है)।
- आपने चार किलोग्राम या इससे ज़्यादा वज़न वाले बच्चे को जन्म दिया है।
- गर्भावस्था के दौरान आपको मधुमेह था या ख़ून में ग्लूकोज़ का स्तर ज़्यादा था।
- आप शारीरिक रूप से आलसी हैं अर्थात् आप सप्ताह में तीन बार से कम व्यायाम करते हैं।
- आपको हाई ब्लड प्रेशर है।
- पहले से ही मधुमेह के लक्षण हैं: बिना खाना खाए (Fasting) ग्लूकोज़ की मात्रा 110‑126 मिलिग्राम% है और खाना खाने के बाद 140‑200 मिलिग्राम% है।
- ट्राइग्लिसराइड्स या कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से ज़्यादा है।
- आप शरीर का वज़न सही रखें। यदि वज़न ज़्यादा है तो 5‑7% वज़न घटाएँ। 2‑3 किलोग्राम वज़न कम करने से भी बहुत फ़र्क़ पड़ जाता है।
- ऐसी वस्तुएँ खाएँ जिनका ग्लायसीमिक इंडेक्स (glycemic index) कम हो अर्थात् जिनको खाने के बाद ख़ून में ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा न बढ़े। जैसे गेहूँ, फलियाँ, फल और सब्ज़ियों इत्यादि का सेवन करें। केवल अनसैचुरेटिड वसा (unsaturated fat) यानी वनस्पति तेलों (liquid vegetable oils) का ही प्रयोग करें जो सामान्य तापमान पर न जमें।
- सप्ताह में पाँच बार, तीस मिनट के लिए तेज़ सैर करें या कोई अन्य व्यायाम करें।
- दूसरे स्तर पर रोकथाम: यदि आप ख़ून में ग्लूकोज़ और चर्बी की मात्रा तथा ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखते हैं और साथ ही दूसरे उपाय भी अपनाते हैं, जैसे डॉक्टर के सुझाव के अनुसार ऐस्प्रिन लेना, चर्बी और ब्लड प्रेशर की दवाइयों (Statins and ACE inhibitors) का सही इस्तेमाल करना, तो आप मधुमेह से होनेवाली परेशानियों से बचे रहते हैं।
- तीसरे स्तर पर रोकथाम: मधुमेह के कारण यदि आँख, गुर्दे, हृदय, ख़ून की नाड़ियों या नसों से जुड़ी कोई समस्या पैदा हो जाए और यदि इनका पता जल्दी लग जाए तो आगे के नुकसान को रोका जा सकता है और इन अंगों को बचाया जा सकता है।
यदि आप जानते हैं कि आपको मधुमेह है तो आपके परिवार के अन्य लोगों को भी मधुमेह हो सकता है। यदि आपके भाई‑बहनों में ये लक्षण हैं तो उन्हें जाँच करवाने के लिए प्रेरित करें, ख़ास तौर पर अगर:
- आयु 25 साल से ज़्यादा हो।
- वज़न अधिक हो।
- व्यायाम न करते हों।
- बार‑बार संक्रमण होता हो।
- ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता हो।
- पहले कभी सीने में दर्द या दिल का दौरा पड़ा हो।
- ख़ून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सामान्य से ज़्यादा हो।
- डिलीवरी के समय कोई समस्या रही हो।
भोजन करने के दो घंटे बाद ब्लड शुगर की जाँच करवाएँ। यदि ग्लूकोज़ (blood sugar) का स्तर 140 मिलिग्राम% से अधिक है, तो एक बार और ख़ाली पेट जाँच करवाएँ और फिर 75 ग्राम ग्लूकोज़ खाने के दो घंटे बाद दोबारा जाँच करवाएँ।
| ख़ून में शुगर की मात्रा | |||
|---|---|---|---|
| ख़ाली पेट | खाने के दो घंटे बाद | ||
| सामान्य | 110 मिलिग्राम% से कम | 140 मिलिग्राम% से कम | |
| मधुमेह होने का ख़तरा | 110‑125 मिलिग्राम% | 140‑200 मिलिग्राम% | |
| मधुमेह | 200 मिलिग्राम% से ज़्यादा | ||
यदि ग्लूकोज़ का स्तर अभी ठीक है लेकिन आई.जी.टी. (Impaired Glucose Tolerance) जाँच करवाने के बाद यह स्तर सामान्य से ज़्यादा है, तो हर साल आई.जी.टी की जाँच ज़रूर करवाएँ। इस जाँच को नज़रअंदाज़ न करें। अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके आप मधुमेह से बचाव कर सकते हैं।
मधुमेह की जटिलताओं से बचावयदि मधुमेह पर सही नियंत्रण न रखा जाए तो इससे शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुँचता है और कई गंभीर समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। यदि रोग को नियंत्रित कर लिया जाए तो इनमें से कई समस्याओं को अधिक समय तक टाला या रोका जा सकता है।
गंभीर समस्याएँमधुमेह के जो रोगी ब्लड शुगर की अधिक मात्रा को नज़रअंदाज़ करते हैं, उनके शरीर से पेशाब द्वारा काफ़ी मात्रा में पानी और नमक निकल जाता है। इस कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, यह जानलेवा हो सकता है।
मधुमेह के उस रोगी की आयु लंबी होगी,
जिसे अपनी बीमारी की जानकारी सबसे ज़्यादा होती है।
जब शरीर की चर्बी का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होता, तो इससे एक ख़राब पदार्थ कीटोन बॉडीज़ (Ketone bodies) की उत्पत्ति होती है, जिससे ख़ून अम्लीय (acidic) हो जाता है। इस स्थिति को कीटोएसिडोसिस (Ketoacidosis) कहते हैं। ऐसा उन मरीज़ों में होता है जिन्हें मधुमेह का इलाज करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। यदि मरीज़ इंसुलिन का इस्तेमाल बंद कर दे या किसी बीमारी के कारण इंसुलिन का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़े, तो यह स्थिति पैदा होती है। मरीज़ को उलटियाँ, पेट में दर्द, शरीर में पानी और नमक की बहुत कमी, साँस फूलना, साँस में फलों जैसी गंध जैसे ऐसीटोन (Acetone) और बेहोशी हो सकती है तथा मौत भी हो सकती है।
हाईपोग्लाइसीमिया का अर्थ है ख़ून में ग्लूकोज़ की मात्रा का सामान्य और उचित स्तर से कम हो जाना। इसके कई लक्षण होते हैं। परंतु कई बार यह अवस्था बिना किसी लक्षण के भी पैदा हो सकती है, यहाँ तक कि सोते‑सोते भी! इसके कारण हैं:
- अधिक मात्रा में या ग़लत समय पर इंसुलिन लेना या ग्लूकोज़ कम करनेवाली अन्य दवाइयों का सेवन।
- इंसुलिन लेने के बाद अपर्याप्त मात्रा में भोजन करना।
- अधिक व्यायाम करना।
- ज़्यादा शराब पीना।
हाईपोग्लाइसीमिया (ख़ून में शुगर की कमी) के लक्षण क्या हैं?
| कम ख़तरे के लक्षण | मध्यम ख़तरे के लक्षण | अधिक ख़तरे के लक्षण |
|---|---|---|
| पसीना आना | कमज़ोरी | सोचने‑समझने की शक्ति में कमी, यहाँ तक कि यह भी याद न रहना कि हाईपोग्लाइसीमिया के लिए क्या इलाज करना है। |
| दिल की तेज़ धड़कन | भूख के मारे पेट में दर्द होना | दुविधा, बौखलाना |
| घबराहट | सुस्ती/ज़्यादा नींद आना | ध्यान एकाग्र करने में कठिनाई |
| काँपना | धीमी प्रतिक्रिया |
यदि ख़ून में शुगर की थोड़ी बहुत कमी हो तो उसे शरीर सहज ही ठीक कर लेता है। लेकिन यदि शुगर की कमी बहुत अधिक हो और सही इलाज न किया जाए तो रोगी कोमा में भी जा सकता है।
भोजन, व्यायाम और दवाइयों के सही प्रयोग से हाईपोग्लाइसीमिया से बचा जा सकता है। अपने पास हमेशा कोई मीठी चीज़ रखें और शुगर की कमी के लक्षण होते ही उसका सेवन करें। अपने रिश्तेदारों को अपनी शुगर की कमी के बारे में ज़रूर बताएँ। अपने पास हमेशा एक पहचान‑पत्र (ID Card) रखें जिस पर लिखा हो कि आप मधुमेह के रोगी हैं। यदि ब्लड शुगर बहुत कम हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
2. लंबे समय के लिए होनेवाली समस्याएँ मधुमेह और अंधापनमधुमेह के बहुत‑से रोगी शिकायत करते हैं कि उन्हें बार‑बार चश्मा बदलवाना पड़ता है क्योंकि उनकी देखने की क्षमता में बार‑बार परिवर्तन आ जाता है। ऐसा ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव होने के कारण होता है। यदि ब्लड शुगर पर सही नियंत्रण न रखा जाए, तो बार‑बार नए चश्मे बनवाने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि नए चश्मे बनवाने से पहले कम से कम दो से तीन सप्ताह के लिए ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित किया जाए और फिर उसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश की जाए।
चश्मे का नंबर बदलने का कारण मधुमेह के कारण रेटिना को होनेवाला नुकसान (Diabetic retinopathy) भी हो सकता है। यदि इस रोग का इलाज न करवाया जाए तो अंधापन हो सकता है।
मधुमेह के कारण होनेवाला अंधापनमधुमेह के रोगियों में अंधापन होने का सबसे बड़ा कारण रेटिना को होनेवाला नुकसान है। यदि इस रोग की पहचान करके इलाज जल्द कर लिया जाए तो इसके कारण होनेवाले अंधेपन को रोका जा सकता है। जब रेटिना में ख़ून की नाड़ियाँ फट जाती हैं या नई बनने लगती हैं तो डाइबीटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, जिसके कारण नज़र कमज़ोर हो जाती है और अंधापन हो सकता है।
जिसको मधुमेह का ज्ञान सबसे ज़्यादा है, उस रोगी का जीवन ज़्यादा लंबा होगा।
अंधेपन को कैसे रोका जाए?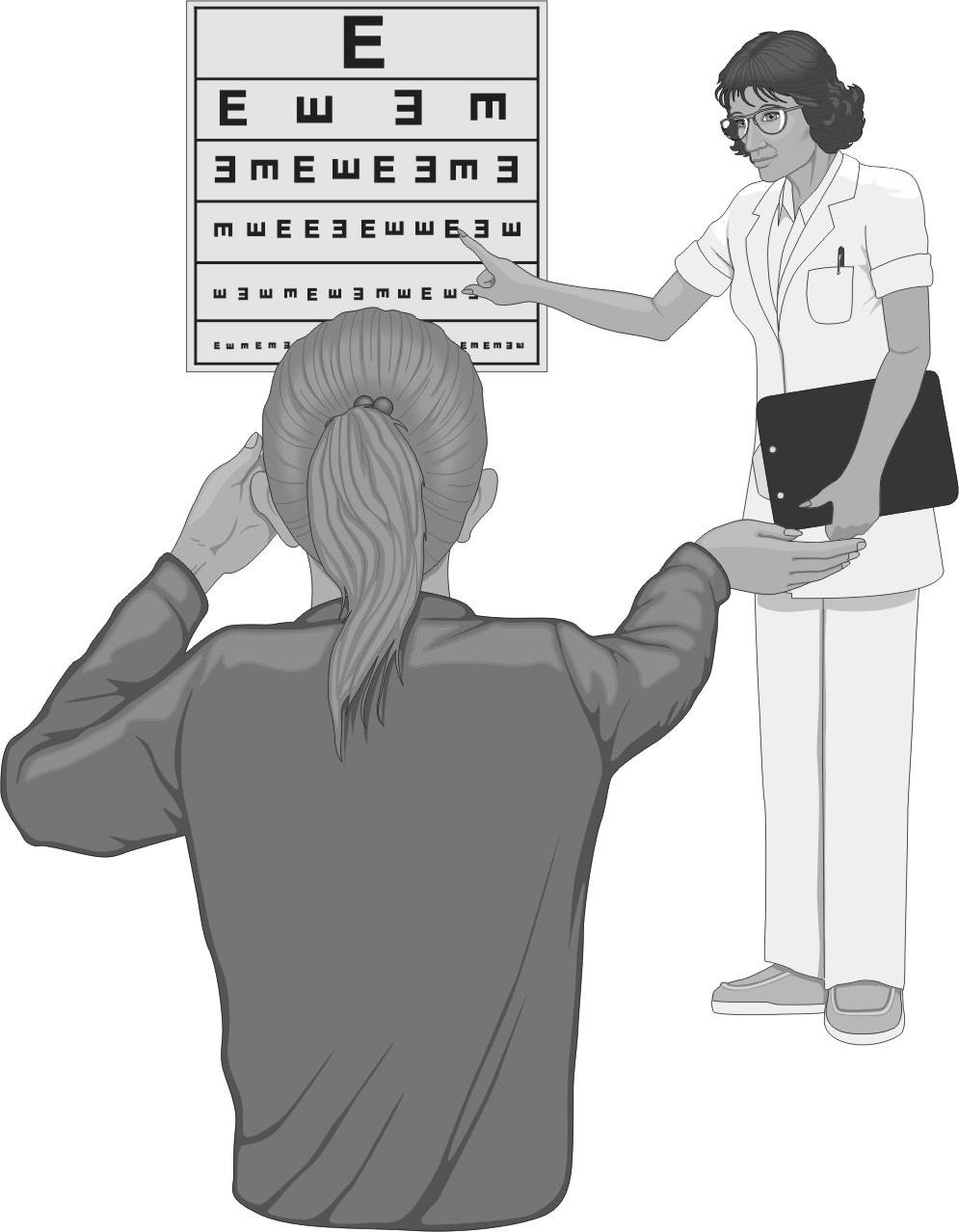
- साल में दो बार या जब भी आपको लगे कि नज़र थोड़ी‑सी भी कम हो रही है, आँखों की जाँच करवाएँ।
- ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का नियंत्रण में रहना बेहद ज़रूरी है।
- यदि यह अवस्था बनी रहती है तो फ़ोटो कोऐग्युलेशन (Photo Coagulation) करवाई जा सकती है जिससे रेटिना में फटी हुई नाड़ियों को बंद किया जाता है।
- यदि नज़र बेहद कमज़ोर हो जाए तो विट्रेक्टॉमी (Vitrectomy) नामक ऑपरेशन पर विचार किया जा सकता है।
अन्य लोगों की अपेक्षा मधुमेह के रोगियों में दिल का दौरा पड़ने की संभावना तीन गुणा ज़्यादा होती है। इन्हें हाई ब्लड प्रेशर होने का ख़तरा भी बना रहता है।
मधुमेह के रोगियों में दिल के दौरे और स्ट्रोक से बचावसामान्य लोगों की अपेक्षा मधुमेह के मरीज़ों में दिल के दौरे की या स्ट्रोक होने की संभावना दो से चार गुणा ज़्यादा होती है। मधुमेह के रोगियों में दिल के दौरे के कुछ ख़ास लक्षण हैं:
- ये कम उम्र के लोगों में होते हैं, कम से कम सामान्य उम्र से दस साल पहले।
- दिल के दौरे में होनेवाला सामान्य दर्द शायद इन मरीज़ों को महसूस न हो।
- कॉरोनरी आर्टरीज़ (दिल को ख़ून पहुँचानेवाली नाड़ियों) में अनेक जगहों पर रुकावट होती है, जिससे बाइपास सर्जरी (Bypass Surgery) करना मुश्किल होता है।
- नाड़ियों में रुकावट की संभावना बनी रहती है।
- आनुवंशिक (Hereditary)।
- बढ़ती आयु।
- शारीरिक कार्य कम करना।
- ख़ून में ग्लूकोज़ का बहुत बढ़ जाना यानी अनियंत्रित ब्लड शुगर।
- हाई ब्लड प्रेशर।
- माईक्रोएल्ब्युमिन‑यूरिया—गुर्दे की नाड़ियों में क्षति की वजह से पेशाब में प्रोटीन आना
- ख़ून में ज़्यादा चर्बी (कोलेस्ट्राल, एल.डी.एल., ट्राइग्लिसराइड्स)।
- ख़ून जमने की प्रक्रिया में बदलाव (altered coagulation factors)।
- सामान्य वज़न।
- नियमित व्यायाम।
- ब्लड प्रेशर 130/85 से कम।
- ब्लड शुगर:
- बिना खाना खाए—110‑120 मिलिग्राम%।
- भोजन के बाद—140 मिलिग्राम% तक।
- ग्लायकेटिड हीमोग्लोबिन (HbA1c) 7% से कम।
- ख़ून में चर्बी (Cholesterol) 150 मिलिग्राम% से कम।
- एच.डी.एल. 50 मिलिग्राम% से ज़्यादा।
- एल.डी.एल. 70 मिलिग्राम% से कम।
- टी.जी.130 मिलिग्राम% से कम।
- पेशाब में एल्ब्यूमिन प्रतिदिन 30 मिलिग्राम% से कम।
अनियंत्रित मधुमेह गुर्दे को नुकसान पहुँचाता है जिससे अकसर गुर्दा फ़ेल हो जाता है। आजकल एक तिहाई मरीज़ों में गुर्दे के फ़ेल होने का कारण मधुमेह है।
गुर्दों का बचाव- भोजन, व्यायाम और दवाइयों के द्वारा ब्लड प्रेशर को सामान्य रखना (130/85)।
- ख़ून में ग्लूकोज़ की मात्रा पर नियंत्रण रखना।
- रोज़ के भोजन में प्रोटीन की मात्रा 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
- पेशाब में एल्ब्युमिन की मात्रा की जाँच नियमित रूप से करवाना।
धमनियों (आर्टरीज़) में चर्बी इकट्ठी हो जाने से ख़ून के बहाव में बाधा पड़ती है। इससे कई बार स्ट्रोक और टाँगों में गैंगरीन हो सकता है।
मधुमेह को नियंत्रित रखने में सफलता
आपके दृष्टिकोण पर निर्भर है।
अनियंत्रित मधुमेह से नसों को नुकसान होता है। इससे शरीर की महसूस करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और छोटे‑मोटे ज़ख़्मों का पता नहीं चलता। इन ज़ख़्मों में संक्रमण हो सकता है और जब ख़ून के बहाव में रुकावट के साथ‑साथ ऐसा हो तो गैंगरीन होने का डर होता है और अंग को काटना भी पड़ सकता है।
अपने डॉक्टर को हर बार अपने पैर ज़रूर दिखाएँ
और पूछें कि कहीं आपके पैरों को कोई ख़तरा तो नहीं!
- ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और लिपिड को नियंत्रण में रखें।
- हर रोज़ पैरों की जाँच करें कि कहीं उनमें कोई चीरा, ज़ख़्म, लाल धब्बे, सूजन या नाख़ूनों में संक्रमण तो नहीं है।
- दिन में हमेशा जूते पहनकर रखें ख़ास तौर पर जब आप घर से बाहर जाएँ। यदि रात को पैर ठंडे रहें तो जुराब पहनें।
- पैरों को रोज़ गुनगुने पानी से धोएँ और अच्छी तरह सुखाएँ। गर्म पानी का इस्तेमाल न करें।
- पैरों को अच्छी तरह सुखाएँ, ख़ास तौर पर उँगलियों के बीच में।
मधुमेह की हर जाँच का अपना महत्त्व है और इससे कुछ न कुछ जानकारी मिलती है। कुछ मापदंड (Parameter) जैसे कि ब्लड शुगर हर मिनट बदलते हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल कई‑कई महीनों तक नहीं बदलता। इसलिए हर जाँच को सही समय पर दोहराया जाना चाहिए, ताकि जाँच सार्थक और कम ख़र्च में हो।
किस तरह की जाँच कब करवानी चाहिए?मधुमेह का पहली बार पता चलने पर जाँच करवाएँ
- वज़न।
- ऊँचाई।
- बी.एम.आई.—किलोग्राम में वज़न/(ऊँचाई मीटर2 ) में: (कम वज़न:यदि बी.एम.आई. 19 से कम है, सामान्य वज़न: 19‑25, अधिक वज़न: 25‑30, मोटापा: 30 से ज़्यादा)।
- ब्लड शुगर—ख़ाली पेट और खाने के बाद: जब तक यह नियंत्रण में न आ जाए, लगातार जाँच करवाते रहें।
- ब्लड प्रेशर।
- हीमोग्लोबिन, ख़ून में टी.एल.सी., डी.एल.सी., और ई.एस.आर. की जाँच।
- लिपिड प्रोफ़ाइल (कोलेस्ट्रॉल, एच.डी.एल., एल.डी.एल., और टी.जी.)।
- सीरम क्रिएटिनिन (Serum Creatinine), ब्लड यूरिया और यूरिक एसिड की जाँच।
- पेशाब की सामान्य जाँच और माइक्रोएल्ब्यूमिन की जाँच।
- लिवर के कार्य की जाँच—एक साल बाद दोबारा करवाएँ।
- फ़ंडस जाँच (आँख की पुतली को फैलाकर आंतरिक जाँच)—एक साल बाद दोबारा करवाएँ।
- ई.सी.जी. (ECG)।
- छाती का एक्स‑रे—हर पाँच साल बाद दोहराएँ।
- मधुमेह कितना नियंत्रण में है।
- किसी होनेवाली समस्या (रोग) की जल्द पहचान।
- रोग की गंभीरता में कमी।
- स्थिति में और गिरावट।
अपनी देखभाल ख़ुद करना सबसे बेहतर और उपयोगी है।
मधुमेह के रोगी की हर 3 महीने में जाँच- वज़न।
- ब्लड शुगर।
- ग्लायकेटिड हीमोग्लोबिन ( HbA1C) यह एक माप है जिससे पता चलता है कि एक निर्धारित समय के दौरान ब्लड शुगर कितनी नियंत्रित हुई है।
- ब्लड प्रेशर का जायज़ा।
- एल्ब्यूमिन की मात्रा नियंत्रण में रखने के लिए पेशाब की जाँच।
- इलाज का जायज़ा।
- लिपिड प्रोफ़ाइल।
- ई.सी.जी.।
- इलाज में कोई बदलाव की ज़रूरत (यदि हो)।
- शरीर के सभी अंगों की व्यापक जाँच।
- फ़ंडस के लिए आँखों की जाँच।
- दिल की जाँच।
- गुर्दे और लिवर की जाँच।
सिर्फ़ जानकारी होने से बात नहीं बनती,
उस पर अमल भी करना पड़ता है।
मधुमेह पर नियंत्रण
मधुमेह पर नियंत्रण से क्या मतलब है?मधुमेह को नियंत्रित करने का हर व्यक्ति का ढंग अलग‑अलग हो सकता है:
- मधुमेह के लक्षणों की रोकथाम।
- ब्लड शुगर को नियंत्रण में करना।
- ग्लायकेटिड हीमोग्लोबिन ( HbA1C) का नियंत्रण।
- मधुमेह से होनेवाली अन्य समस्याओं की रोकथाम। हालाँकि रोगी समझता है कि ब्लड शुगर और मधुमेह के लक्षणों का नियंत्रण करना काफ़ी है, लेकिन डॉक्टर को इसके साथ जुड़ी दूसरी समस्याओं (ब्लड प्रेशर, ख़ून में चर्बी आदि) को भी नियंत्रण में रखना होता है।
- आहार।
- व्यायाम।
- दवाइयाँ।
जब भी हम भोजन करते हैं, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, चिकनाई हों या ये पदार्थ अलग‑अलग अनुपात में हों, ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। जो कुछ हम खाते हैं उसके ग्लायसीमिक इंडेक्स (G I) पर निर्भर करता है कि ब्लड शुगर कितनी बढ़ेगी।
ग्लायसीमिक इंडेक्स का अर्थ है—भोजन करने के बाद ब्लड शुगर का स्तर और उतनी ही कैलोरीज़ में ग्लूकोज़ खाने के बाद ब्लड शुगर के स्तर का अनुपात। ग्लूकोज़ का ग्लायसीमिक इंडेक्स बहुत अधिक होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी ब्लड शुगर तेज़ी से न बढ़े तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसका ग्लायसीमिक इंडेक्स कम हो।
ग्लायसीमिक इंडेक्स (जी.आई) का महत्त्व- कम जी.आई.का अर्थ है खाने के बाद ब्लड शुगर का कम बढ़ना।
- कम जी.आई. का भोजन करने से वज़न घटाने में सहायता मिलती है।
- कम जी.आई. के भोजन से इंसुलिन का शुगर पर ज़्यादा असर होता है।
- कम जी.आई. के भोजन से मधुमेह पर बेहतर नियंत्रण हो सकता है।
- कम जी.आई. के भोजन से आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है।
- कम जी.आई. वाले भोजन से आपकी शारीरिक सहनशक्ति ज़्यादा देर तक बरकरार रहती है।
कुछ खाद्य पदार्थों का ग्लायसीमिक इंडेक्स
| दही | 14 | हरे मटर | 47 |
| चेरीज़ | 22 | जई | 48 |
| राजमा | 29 | गाजर | 49 |
| दालें (हरी, ब्राउन) | 30 | शकरकंदी | 52 |
| मलाईवाला दूध | 32 | आम | 55 |
| बिना मलाई के दूध | 30 | केले | 56 |
| टमाटर का सूप | 38 | आलू | 59 |
| सेब | 38 | गेहूँ | 66 |
| संतरे | 43 | तरबूज़ | 72 |
| अंगूर | 46 | कॉर्न फ़्लेक्स | 83 |
- गेहूँ के आटे या साबुत दाल का जी.आई. उतनी ही मात्रा की सूजी, मैदा और धुली हुई दाल से कम होता है।
- मोटे अनाज, हरी सब्ज़ियाँ और कुछ फलों में फ़ाइबर (रेशे) होने की वजह से उनका जी.आई. कम होता है।
- फ़ाइबर से भोजन का पाचन धीरे‑धीरे होता है, जिससे ब्लड शुगर भी धीरे‑धीरे बढ़ती है।
- कम जी.आई. वाले कुछ स्नैक्स हैं—ढोकला, अंकुरित दालें, आटे के बिस्कुट, भुने हुए चने, पॉपकॉर्न, बेसन का चिल्ला और बेक करके बनाए गए व्यंजन।
- स्टार्च‑युक्त सब्ज़ियों का जी.आई. घटाने के लिए उनमें दही मिला दें।
- दाल या साँभर का जी.आई. घटाने के लिए उनमें हरी सब्ज़ियाँ मिलाएँ।
- थोड़ा‑थोड़ा भोजन बार‑बार खाने से जी.आई. कम किया जा सकता है।
- सामान्य वज़न वाले मधुमेह के रोगी को ऐसा भोजन और स्नैक्स लेने चाहिएँ कि उसे रोज़ 1500 कैलोरीज़ मिलें। इसमें उम्र, लिंग और व्यायाम के अनुपात के अनुसार बदलाव हो सकता है।
- हर रोज़ भिन्न‑भिन्न प्रकार का खाना खाएँ, भोजन में नाग़ा न करें।
- भोजन में फ़ाइबर (रेशेदार भोजन) की मात्रा बढ़ाएँ।
- भोजन पकाने में कम तेल का प्रयोग करें।
- तले भोजन, मलाई और नारियल के तेल में बने भोजन से परहेज़ करें।
- खाने के लिए तैयार भोजन (डिब्बाबंद), मिठाइयों और मीठे पेयों से दूर रहें।
- गुर्दे की समस्या है तो प्रोटीन का सेवन कम करें।
- वज़न पर लगातार नज़र रखें और इसे बढ़ने न दें।
- आपके खाने के समय और इंसुलिन लेने के समय में तालमेल होना चाहिए।
मधुमेह के रोगी का मुख्य आहार कैसा होना चाहिए?
मधुमेह के रोगी के लिए भोजन की हिदायतें- आपका वज़न आपके आदर्श वज़न से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
- कभी भी भूखे न रहें। आगे दी गई उपयुक्त आहार की सूची में से जो भी चाहें जितना मरज़ी खा‑पी सकते हैं।
- दिन में दो या तीन बार भोजन करने के बजाय भोजन की मात्रा और पोषण के हिसाब से खाने को पाँच से छ: भागों में बाँटकर खाएँ।
- व्यायाम करना बहुत अच्छी बात है और इसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाएँ।
- दावतों और व्रतों से दूर रहें यानी न बहुत अधिक खाएँ और न ही भूखे रहें।
- कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत अनाज हैं और इनका सेवन बताई गई मात्रा के अनुसार करें। मिले‑जुले या साबुत अनाज का इस्तेमाल करें।
बिना शक्कर की चाय और कॉफ़ी, नीबू‑पानी, पतला सूप, बिना मीठे का सोडा, सिरका, पतली खट्टी लस्सी, खीरा, ककड़ी, टमाटर, मूली, करेला, साग और पत्तेदार सब्ज़ियाँ।
इन खाद्य पदार्थों से परहेज़ करेंआइसक्रीम, हलवा, आम, केला, सीताफल, किशमिश, अंगूर, चीकू, खजूर, सूखे मेवे, गिरियाँ, आलू, शकरकंदी, कचालू, चुकंदर, अनानास, तला भोजन, तेल वाले अचार, केक, पेस्ट्री और मैदे से बने पदार्थ।
कैलोरीज़ के मुताबिक़ भोजन की सूची
| कैलोरीज़ | 800 |
|---|---|
| प्रोटीन | 40 ग्राम |
| वसा | 14 ग्राम |
| कार्बोहाइड्रेट्स | 130 ग्राम |
| सुबह का नाश्ता | |
|---|---|
| सब्ज़ियाँ डालकर बनाया गया दलिया | 1 कप |
| दही या दूध | 1 कटोरी या 1 कप |
| मिस्सी रोटी या भरवाँ रोटी | 1 छोटी |
| दही या मलाईरहित दूध | 1 कटोरी/1 कप |
| सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच | |
| सब्ज़ियों का सूप या नीबू पानी | 1 कप |
| दोपहर का भोजन | |
| बिना घी के रोटी | 1 छोटी |
| दाल | ½ कटोरी |
| दही | ½ कटोरी |
| मौसम की उबली हुई सब्ज़ी | 1 कटोरी |
| सलाद | ¼ प्लेट |
| शाम की चाय | |
| बिना मलाई का दूध (दोपहर के भोजन में दही कम करें) | 1 कप |
| चाय | 1 कप |
| ‘मेरी’ (Marie) बिस्कुट (कम चीनी वाला बिस्कुट) | 1 |
| रात का भोजन | |
| सब्ज़ियों का सूप | 1 कप |
| बिना घी के रोटी | ½ छोटी रोटी |
| दाल | ¼ कटोरी |
| मौसम की उबली हुई सब्ज़ी | 1 कटोरी |
| सलाद | ¼ प्लेट |
- एक कटोरी दाल=150 मि.ली. (25 ग्राम दाल)
- एक कप दूध=150 मि.ली.
- चाय या दही बनाने के लिए या पीने के लिए बिना मलाई का दूध इस्तेमाल करें
- एक कटोरी दही=25 ग्राम
कैलोरीज़ के मुताबिक़ भोजन की सूची
| कैलोरीज़ | 1300 | 1600 | 1900 |
|---|---|---|---|
| प्रोटीन | 50 ग्राम | 60 ग्राम | 70 ग्राम |
| वसा | 30 ग्राम | 36 ग्राम | 43 ग्राम |
| कार्बोहाइड्रेट्स | 210 ग्राम | 260 ग्राम | 310 ग्राम |
| सुबह का नाश्ता | |||
|---|---|---|---|
| दूध | 1 कप | 1 कप | 1 कप |
| दलिया | 1 कटोरी | 1 कटोरी | 1 कटोरी |
| भरवाँ/मिस्सी रोटी | 1 रोटी | 1 रोटी | 1 रोटी |
| दही | 100 ग्राम | 100 ग्राम | 100 ग्राम |
| सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच | |||
| चाय, लस्सी या नीबू पानी | चाय, लस्सी या नीबू पानी | चाय, लस्सी या नीबू पानी | चाय, लस्सी या नीबू पानी |
| अंकुरित दाल या फल | अंकुरित दाल या फल | अंकुरित दाल या फल | अंकुरित दाल या फल |
| दोपहर का भोजन | |||
| रोटी | 2 छोटी | 3 छोटी | 2 मध्यम |
| दाल | 1 कटोरी | 1 कटोरी | 1 कटोरी |
| सब्ज़ी | 1 कटोरी | 1 कटोरी | 1 कटोरी |
| दही | 100 ग्राम | 100 ग्राम | 100 ग्राम |
| सलाद | ¼ प्लेट | ¼ प्लेट | ¼ प्लेट |
| शाम की चाय | |||
| चाय | 1 कप | 1 कप | 1 कप |
| बिस्कुट | 2 – 3 बिस्कुट | 2 – 3 बिस्कुट | 2 – 3 बिस्कुट |
| पोहा या उपमा | 1 कटोरी | 1 कटोरी | 1 कटोरी |
| रात का भोजन | |||
| रोटी | 1 छोटी | 1 छोटी | 2 मध्यम |
| दाल या पनीर की भाजी |
½ कटोरी | 1 कटोरी | 1 कटोरी |
| सब्ज़ी | 1 कटोरी | 1 कटोरी | 1 कटोरी |
| दही | 100 ग्राम | 100 ग्राम | 100 ग्राम |
| सलाद | ¼ प्लेट | ¼ प्लेट | ¼ प्लेट |
| सब्ज़ियाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्बोहाईड्रेट और कैलोरीज़ नाममात्र | कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम और कैलोरीज़ 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पत्तेदार सब्ज़ियाँ | जड़ वाली सब्ज़ियाँ | मात्रा (ग्राम) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चौलाई | चुकंदर | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बथुआ | गाजर | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पत्ता गोभी | अरबी | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| धनिये के पत्ते | प्याज़ (मध्यम आकार का) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मेथी के पत्ते | आलू | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| करी पत्ता | शकरकंदी | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लैट्यूस (सलाद के पत्ते) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पुदीना | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पालक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सोया के पत्ते | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्य सब्ज़ियाँ | अन्य सब्ज़ियाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सफ़ेद पेठा | बाकला की फली | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| करेला | ग्वारफली | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बैंगन | डबल बीन्ज़ | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ककड़ी | नरम कटहल | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फूल गोभी | कटहल के बीज | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खीरा | मटर | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सहजन (Drumstick) | हरा केला | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ़्रेंच बीन | सिंघाड़ा | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हरा आम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भिंडी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हरे प्याज़ की डंडी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| परवल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कच्चे केले के फूल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कद्दू | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राम तोरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लंबी तोरी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टिंडा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हरा टमाटर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शलगम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम कैलोरीज़ 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फल | मात्रा (ग्राम) | लगभग संख्या और आकार | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आमला | 90 | 20 | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सेब | 75 | 1 | छोटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| केला | 30 | ¼ | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रसभरी | 150 | 40 | छोटी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| काजू | 90 | 2 | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शरीफ़ा/सीताफल | 50 | ¼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खजूर | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंजीर | 135 | 6 | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंगूर | 105 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अमरूद | 100 | 1 | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जामुन | 50 | 10 | बड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नीबू | 90 | 1 | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| लौकाट | 105 | 6 | बड़ी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आम | 90 | 1 | छोटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| खरबूज़ा | 270 | ¼ | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संतरा | 90 | 1 | छोटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पपीता | 120 | 2 | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आड़ू | 135 | 1 | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नाशपाती | 90 | 1 | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनानास | 90 | 1 ½ | गोल फाँक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आलू बुख़ारा | 120 | 4 | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनार | 75 | 1 | छोटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मौसम्मी | 150 | 1 | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्ट्रॉबेरी | 105 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टमाटर | 240 | 4 | मध्यम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| तरबूज़ | 175 | ¼ | छोटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फलियाँ और दालें | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ग्राम = 100 कैलोरीज़, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 6 ग्राम प्रोटीन | |||||||||||||||
| काले चने | काबुली चने | ||||||||||||||
| भुने हुए काले चने | दालें | ||||||||||||||
| बेसन | मोठ | ||||||||||||||
| लोबिया | राजमा | ||||||||||||||
| हरी दाल | सूखे मटर | ||||||||||||||
| अरहर | |||||||||||||||
| अनाज | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ग्राम = 100 कैलोरीज़, 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 2 ग्राम प्रोटीन | |||||||||||||||||||||
| बाजरा | राइस फ़्लेक्स | ||||||||||||||||||||
| जौ | पोहे/मुरमुरे | ||||||||||||||||||||
| ब्रैड (5 ग्राम चीनी के बराबर कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज़ के लिए) | |||||||||||||||||||||
| ज़्वार/जुआर | सेवइयाँ | ||||||||||||||||||||
| कॉर्न फ़्लेक्स (Corn flakes) | सूजी | ||||||||||||||||||||
| सूखी मकई | गेहूँ का आटा | ||||||||||||||||||||
| जई (Oats) | मैदा | ||||||||||||||||||||
| चावल | दलिया | ||||||||||||||||||||
| रागी | सागू (इसके साथ प्रोटीन युक्त अन्य भोजन की ज़रूरत होती है) | ||||||||||||||||||||
| दूध | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कैलोरीज़ 100, प्रोटीन 5 ग्राम | |||||||||||||||||||||
| भोजन | मात्रा | ||||||||||||||||||||
| छाछ/लस्सी | 750 मि.ली | ||||||||||||||||||||
| चीज़ (Cheese) | 30 ग्राम | ||||||||||||||||||||
| दही | 210 ग्राम | ||||||||||||||||||||
| खोया | 30 ग्राम | ||||||||||||||||||||
| भैंस का दूध | 90 मि.ली. | ||||||||||||||||||||
| गाय का दूध | 180 मि.ली. | ||||||||||||||||||||
| बिना मलाई का दूध* | 260 मि.ली. | ||||||||||||||||||||
| बिना मलाई वाले दूध का पाउडर* | 30 ग्राम | ||||||||||||||||||||
| वसा | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कैलोरीज़ 100, वसा 11 ग्राम | |||||||||||||||||||||||||
| भोजन | मात्रा (ग्राम)) | ||||||||||||||||||||||||
| बादाम | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| मक्खन | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| काजू | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| नारियल | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| घी | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| भुनी मूँगफली | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| वनस्पति घी | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| तेल | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| अख़रोट | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| पिस्ता | 15 | ||||||||||||||||||||||||
आम तौर पर प्रयोग होनेवाले भारतीय खाने में पोषण के तत्त्वों की मात्रा
| खाद्य पदार्थ | मात्रा | घरेलू माप | प्रोटीन (ग्राम) | कैलोरीज़ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दूध और दूध के पदार्थ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गाय का दूध | 250 मि.ली. | 1 गिलास | 8.00 | 167.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भैंस का दूध | 250 मि.ली. | 1 गिलास | 10.75 | 292.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बिना मलाई का दूध | 250 मि.ली. | 1 गिलास | 6.25 | 72.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| दही | 125 ग्राम | 1 कटोरी | 3.87 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पनीर | 25 ग्राम | ½“x ½” x 2″ | 6.00 | 87.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| छाछ/लस्सी | 250 मि.ली. | 1 गिलास | 2.00 | 37.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बिना मलाई वाले दूध का पाउडर (गाय) | 100 ग्राम | - | 38.00 | 357.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्य खाद्य पदार्थ और दालें | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेहूँ के आटे की पतली चपाती | 25 ग्राम | 1 | 3.03 | 85.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चपाती (मध्यम) | 30 ग्राम | 1 | 3.63 | 102.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चपाती (बड़ी) | 40 ग्राम | 1 | 4.84 | 136.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गेहूँ का दलिया | 25 ग्राम | 1 कटोरी | 2.95 | 86.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सूजी | 15 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 1.56 | 52.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चावल | 30 ग्राम | 1 कटोरी | 1.92 | 103.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूँग की धुली दाल | 30 ग्राम | 1 कटोरी | 7.35 | 104.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मलका मसूर दाल | 30 ग्राम | 1 कटोरी | 7.53 | 102.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अरहर दाल | 30 ग्राम | 1 कटोरी | 6.69 | 100.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| काले चने | 40 ग्राम | 1 कटोरी | 6.84 | 144.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चने की दाल | 30 ग्राम | 1 कटोरी | 7.20 | 104.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सब्ज़ियाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पालक | 100 ग्राम | 1 कटोरी | 2.00 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मेथी | 100 ग्राम | 1 कटोरी | 4.40 | 49.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पत्ता गोभी/बंद गोभी | 100 ग्राम | 1 कटोरी | 1.80 | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बैंगन | 100 ग्राम | 1 कटोरी | 1.40 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घीया | 100 ग्राम | 1 कटोरी | 0.20 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| हलवा कद्दू | 100 ग्राम | 1 कटोरी | 0.10 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फूल गोभी | 100 ग्राम | 1 कटोरी | 2.60 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आलू | 100 ग्राम | 1 कटोरी | 1.60 | 97.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फ्रेंच बीन | 100 ग्राम | 1 कटोरी | 1.70 | 26.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मशरूम | 100 ग्राम | 1 कटोरी | 3.10 | 43.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| फल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संतरा | 100 ग्राम | 1 piece | 0.70 | 48.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| केला | 100 ग्राम | 1 piece | 1.20 | 116.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पपीता | 100 ग्राम | 1 piece | 0.60 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सेब | 100 ग्राम | 1 piece | 0.20 | 59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अमरूद | 100 ग्राम | 1 piece | 0.90 | 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गिरियाँ और तेल वाले बीज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बादाम | 15 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 3.12 | 98.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| काजू | 15 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 3.18 | 89.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सूखा नारियल | 15 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 1.02 | 99.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अख़रोट | 15 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 2.34 | 103.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| किशमिश | 20 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 0.36 | 61.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूँगफली | 15 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 3.80 | 85.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वसा और तेल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घी और तेल | 15 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मक्खन | 20 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 145.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अन्य खाद्य पदार्थ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| चीनी | 15 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 59.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| गुड़ | 20 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 76.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| साबूदाना) | 20 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 70.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूरी ब्रैड | 25 ग्राम | 1 slice | 2.20 | 61.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सफ़ेद ब्रैड | 25 ग्राम | 1 slice | 1.95 | 61.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कॉर्न फ़्लेक्स | 30 ग्राम | 1 cup | 2.40 | 114.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| न्यूट्री नगेट्स | 5 ग्राम | 5 – 6 pieces | 4.11 | 43.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रोटीन बिस्कुट | 5 ग्राम | 1 | 1.50 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जैम (Jam) | 20 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 55.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जेली (Jelly) | 18 ग्राम | 1 बड़ा चम्मच | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सिर्फ़ जानकारी होने से बात नहीं बनती,
उस पर अमल भी करना है।
- भोजन में मुख्य तत्त्वों का मिश्रण
कार्बोहाइड्रेट्स कुल कैलोरीज़ का 65% प्रोटीन कुल कैलोरीज़ का 15‑30% तेल/वसा कुल कैलोरीज़ का 20% - दिन भर के भोजन में आवश्यक कैलोरीज़
सुबह की चाय कुल कैलोरीज़ का 5‑10% सुबह का नाश्ता कुल कैलोरीज़ का 20% दोपहर का भोजन कुल कैलोरीज़ का 30% शाम की चाय कुल कैलोरीज़ का 10% रात का भोजन कुल कैलोरीज़ का 30%
कम जी. आई. (G. I.) के लिए रोटी और बिस्कुट बनाने की सामग्री
| रोटी | चोकर के बिस्कुट (प्रति बिस्कुट 20 ग्राम) |
|---|---|
| 15 ग्राम गेहूँ का आटा
10 ग्राम चने का आटा 5 ग्राम जौ का आटा |
100 ग्राम गेहूँ का आटा
100 ग्राम गेहूँ का चोकर 10 ग्राम तेल 5 ग्राम नमक 1 ग्राम अजवायन ½ ग्राम बेकिंग पाउडर |
व्यायाम मधुमेह के इलाज का एक ज़रूरी अंग है। व्यायाम सबके लिए लाभदायक है, उनके लिए भी जिन्हें मधुमेह नहीं है। नियमित रूप से व्यायाम करने से, यहाँ तक कि दिन में 3‑4 किलोमीटर चलने से भी बहुत फ़ायदा होता है। व्यायाम:
- शरीर के वज़न को सही रखता है।
- स्वास्थ्य में वृद्धि करता है।
- सेहत अच्छी होने से ख़ुशी का आभास दिलाता है।
- इंसुलिन का असर बढ़ाता है।
- ख़ून में शुगर की मात्रा को नियंत्रण में रखता है, भले ही वज़न कम न हुआ हो।
- लिपिड प्रोफ़ाइल को सही रखता है।
- ख़ून में थक्के के जमाव को रोकता है।
- भोजन का पाचन सही करता है।
- जोड़ों की गतिशीलता को क़ायम रखता है।
- ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सही रखता है जिससे दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा कम होता है।
- हड्डियों और मांसपेशियों की ताक़त बढ़ाता है।
मधुमेह के कारण भविष्य में होनेवाली समस्याओं को
व्यायाम करने से कम किया जा सकता है।
हर रोज़ सैर करने से मधुमेह दूर रहती है।
- समय की कमी
- बहुत ज़्यादा काम
- ख़राब मौसम
- बाहर का प्रदूषण
- इससे ज़्यादा ज़रूरी काम हैं
- एलर्जी होने का डर
- पार्क में चलने से बेहतर है मज़े से सोना!

- यदि आपकी ब्लड शुगर बहुत अधिक है—ग्लूकोज़ का स्तर 400 मिलिग्राम% से ज़्यादा है।
- यदि पेशाब में कीटोन्स (Ketones) हों।
- जब आप किसी संक्रमण या रोग के शिकार हों।
- जब आँखों में दर्द हो या देखने की शक्ति में बदलाव लगे।
- साँस फूले या चक्कर आएँ—यह दिल की किसी बीमारी का लक्षण हो सकता है।
- बहुत ज़्यादा सर्दी या गरमी के मौसम में।
आप में से बहुत‑से लोगों को लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा दवा खा रहे हैं यह असुविधाजनक और महँगा हो सकता है और इसके कुछ हानिकारक असर शरीर पर हो सकते हैं। आपको इन दवाइयों के असर पर पूरा विश्वास नहीं होता क्योंकि इनका असर जल्दी नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ़ डॉक्टर को न केवल जल्दी असर का, बल्कि आगे चलकर होनेवाली अन्य समस्याओं का भी ध्यान रखना होता है।
रोगी और डॉक्टर, दोनों अपनी‑अपनी जगह ठीक हैं। डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वह मरीज़ को बताए और मरीज़ को चाहिए कि वह अच्छी तरह समझे कि कोई ख़ास दवा क्यों और कितने समय के लिए दी गई है। अगर मरीज़ को कुछ समझ न आए तो उसे उसके बारे में पूछ लेना चाहिए।
दवाइयों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है- जो दवाइयाँ ब्लड शुगर के स्तर को सामान्य करने के लिए ज़रूरी हैं:
टाइप I मधुमेह के लिए: इंसुलिन ज़रूरी है और सारी उम्र लेनी पड़ती है।
टाइप II मधुमेह के लिए: रोगी ऐसी गोलियाँ ले सकता है, जो:
- इंसुलिन के प्रतिरोध को कम करें जैसे बायगुअनाइड्स (Biguanides) और थायाज़ोलिडीनडाइओन्स (Thiazolidinediones)
- इंसुलिन के स्राव को बढ़ाए जैसे सलफ़ोनाइलयुरियाज़ (Sulphonylureas)
- कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन को कम करे जैसे अल्फ़ा‑ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर्स (Alpha-glucosidase inhibitors)
- ब्लड प्रेशर को 130/85 से नीचे रखनेवाली दवाइयाँ। इनमें ACE inhibitor को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये गुर्दे और हृदय को नुकसान से रोकती है।
- ख़ून में लिपिड की मात्रा को सही रखनेवाली दवाइयाँ, जैसे स्टेटिन्स (Statins)
- ऐस्प्रिन की छोटी ख़ुराक, 75‑150 मिलिग्राम प्रतिदिन लेने से ख़ून में थक्का नहीं जमता जिससे दिल का दौरा और दिमाग़ में स्ट्रोक (ख़ून का दौरा कम होने से नुकसान) होने का ख़तरा कम हो जाता है।
ये दवाइयाँ महत्त्वपूर्ण हैं और मधुमेह के अधिकांश रोगियों को इनका इस्तेमाल करना पड़ता है।
कोई भी दवा लेने से पहले
अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें।
शरीर की ऊँचाई और वज़न के अनुसार कैलोरीज़ की ज़रूरत, इलाज का मुख्य भाग है। कैलोरीज़ का अनुमान व्यक्ति के आदर्श वज़न (किलोग्राम में) पर निर्भर करता है।
- शरीर की ऊँचाई के अनुसार आदर्श वज़न:
पुरुष स्त्री ऊँचाई, क़द 152 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर वज़न 48 किलोग्राम 45 किलोग्राम प्रत्येक अधिक सेंटीमीटर के लिए, जोड़ें 1.1 किलोग्राम 0.9 किलोग्राम - प्रतिदिन कैलोरीज़ की ज़रूरत जानने के लिए आदर्श वज़न को 22 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से गुणा करें।
- आरामपरस्ती वाली ज़िंदगी जीने वालों के लिए: सामान्य कैलोरीज़ का 25% आम कैलोरी से ज़्यादा जोड़ें।
जो थोड़ा शारीरिक व्यायाम करते हैं: सामान्य कैलोरीज़ का 50% आम कैलोरी से ज़्यादा जोड़ें।
जो ज़्यादा शारीरिक व्यायाम करते हैं: सामान्य कैलोरीज़ का 75% आम कैलोरी से ज़्यादा जोड़ें। - 500 किलो कैलोरीज़ जोड़ें अगर वज़न सामान्य से कम है या 500 किलो कैलोरीज़ घटाएँ अगर वज़न सामान्य से ज़्यादा है।
- आदर्श वज़न आँकें: 52 सेंटीमीटर के व्यक्ति का आदर्श वज़न 48 किलोग्राम है। इसके बाद हर अधिक सेंटीमीटर के लिए 1.1 किलोग्राम जोड़ें, 170 सेंटीमीटर के लिए 152 घटा दें, जो 18 सेंटीमीटर होता है। इसे 1.1 से गुणा कर दें, जो 19.8 किलोग्राम है। आदर्श वज़न है 48+19.8=67.8 यानी लगभग 68 किलोग्राम।
- 68 किलोग्राम वज़न वाले व्यक्ति की कैलोरीज़ की ज़रूरत तय करें: इसका फ़ार्मूला है: 22 किलो कैलोरीज़/किलोग्राम। अत: 68 किलोग्राम वज़न के व्यक्ति के लिए, सामान्य कैलोरीज़ हैं 68 x 22 = 1496 (लगभग 1500) किलो कैलोरीज़।
- जीवन शैली के लिए कैलोरीज़ जोड़ें: ज़्यादा बैठे रहनेवाले लोगों के लिए 25% कैलोरीज़ जोड़ें। 1500 का 25%=375 किलो कैलोरीज़; यानी 375+1500= 1875 किलो कैलोरीज़।
- वज़न के अनुसार कैलोरीज़ घटाएँ या बढ़ाएँ: चूँकि व्यक्ति का वज़न सामान्य से ज़्यादा है (उसका आदर्श वज़न 68 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन वह 80 किलोग्राम है), तो 1875 किलो कैलोरीज़ में से 500 किलो कैलोरीज़ घटा दें, जो 1375 किलो कैलोरीज़ प्रतिदिन है।
इसलिए, अगर किसी पुरुष का भार 80 किलोग्राम है और कद 170 सेंटीमीटर है और जो आरामपरस्ती वाला जीवन व्यतीत करता है, तो उसे दिन भर में 1375 किलो कैलोरीज़ चाहिएँ।
हर रोज़ नियमित रूप से की गई सैर
मधुमेह को दूर रखती है।
एच.आई.वी. और एड्स
 एड्स एक बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा गया है। हम सभी को इस बीमारी से ख़तरा है और हमें ख़ुद ही इससे बचाव करना होगा। इसी लिए एड्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है।
एड्स एक बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा गया है। हम सभी को इस बीमारी से ख़तरा है और हमें ख़ुद ही इससे बचाव करना होगा। इसी लिए एड्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है।
एड्स किसी को भी हो सकता है...
लेकिन हर कोई इससे बच सकता है।
इसलिए इससे बचाव ही एकमात्र और सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय है। एड्स क्या है?
एड्स (AIDS) का अर्थ है (Acquired Immune Deficiency Syndrome):
अर्जित (Acquired)—जो आप ग्रहण कर लेते हैं।
प्रतिशोधक क्षमता (Immunity)—मनुष्य शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता।
क्षीण (Deficiency)—क्षमता में कमी।
लक्षण (Syndrome)—ये लक्षण किसी विशेष रोग का संकेत देते हैं।
एड्स संक्रामक रोग है। यह एच.आई.वी. पॉज़िटिव व्यक्ति या एड्स के किसी रोगी से किसी विशेष माध्यम के द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है। फिर भी यह छूत का रोग नहीं है यानी कि यह एक‑दूसरे को छूने मात्र से नहीं फैलता।
एच.आई.वी. क्या है?एच.आई.वी. (Human Immunodeficiency Virus) मनुष्य में रोगों से लड़ने की क्षमता को घटानेवाला वायरस है। यही वायरस एड्स को उत्पन्न करता है।
एच.आई.वी. से एड्स कैसे उत्पन्न होता है?मनुष्य के शरीर में रोगों से लड़ने और अपने आप को बचाने की क्षमता है। हम इस की तुलना किसी देश की फ़ौज से कर सकते हैं। जब कोई वायरस या ‘दुश्मन’ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या ‘फ़ौज’ उस दुश्मन पर हमला करके उसे मार देती है।
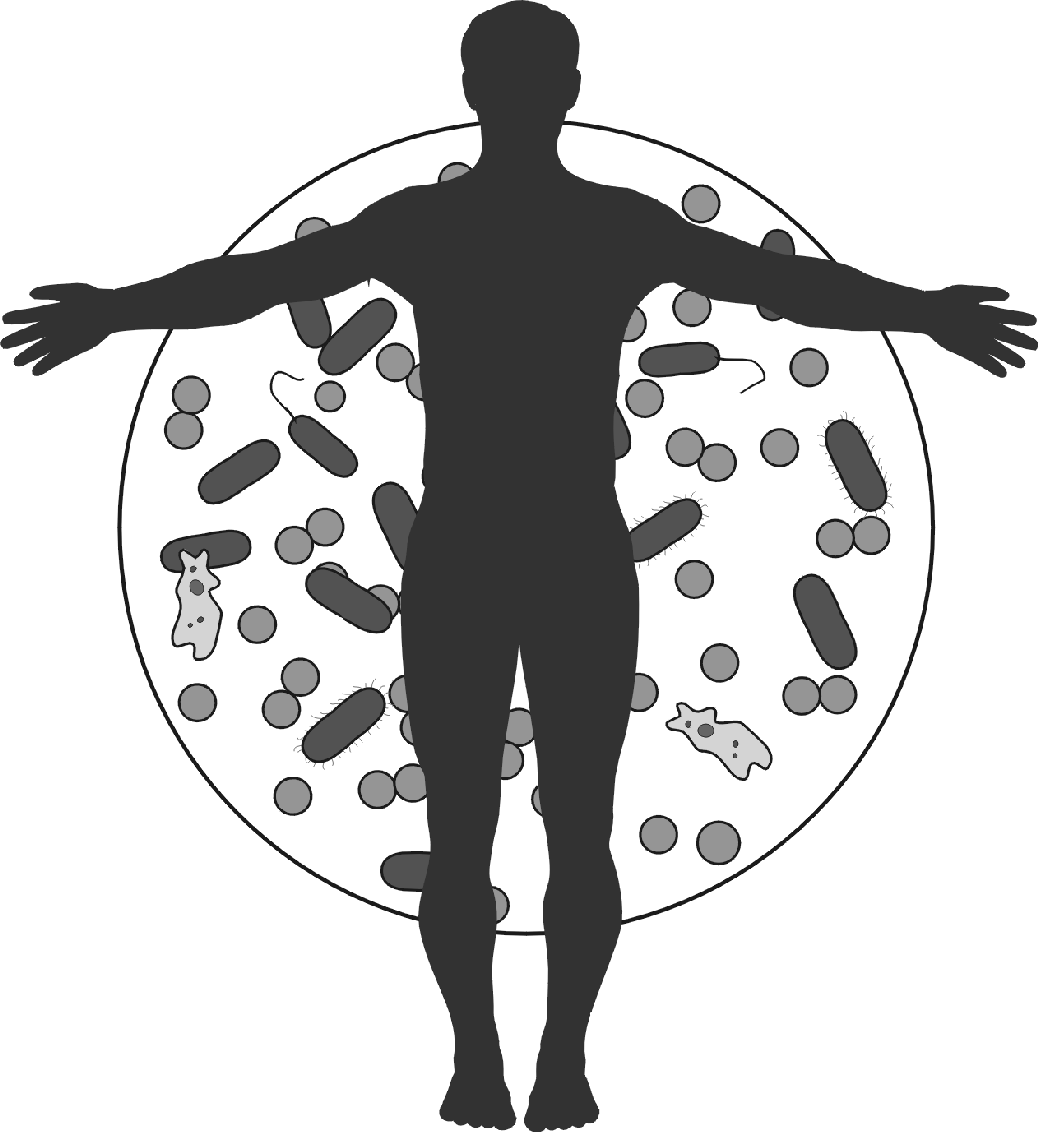 सीधे शब्दों में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (Immune System) वह फ़ौज है जो संक्रमणों और बीमारियों से लड़ती है। इसका एक बेहद महत्त्वपूर्ण भाग CD4 कोशिका है। एक स्वस्थ शरीर में (प्रति मिलिलीटर ख़ून में) CD4 कोशिकाओं की संख्या 500‑1800 होती है।
सीधे शब्दों में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (Immune System) वह फ़ौज है जो संक्रमणों और बीमारियों से लड़ती है। इसका एक बेहद महत्त्वपूर्ण भाग CD4 कोशिका है। एक स्वस्थ शरीर में (प्रति मिलिलीटर ख़ून में) CD4 कोशिकाओं की संख्या 500‑1800 होती है।
एच.आई.वी. इन CD4 कोशिकाओं पर हमला करके इनके अंदर प्रवेश कर जाता है और वहाँ अपनी संख्या बढ़ाकर कोशिकाओं को नष्ट करने लगता है। यह वायरस गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि यह हमारे शरीर की सुरक्षा व्यवस्था के उस अंश को नष्ट करने लगता है जो बीमारी पैदा करनेवाले सूक्ष्म जीवाणुओं से हमारी सुरक्षा करता है जैसे फफूँद (Fungus), बैक्टीरिया और वायरस। कुछ वर्षों बाद CD4 कोशिकाओं की संख्या घटनी शुरू हो जाती है। इससे शरीर की संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है। कुछ ख़ास बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं जो आम तौर पर एच.आई.वी. ग्रस्त लोगों को होती हैं। जब ऐसा होता है तब इसे एड्स कहते हैं।
कुछ ख़ास बीमारियाँ जो एड्स के रोगियों पर हमला करती हैं, वे हैं—तपेदिक, दस्त, बुख़ार, वज़न में कमी, निमोनिया, फफूँद का संक्रमण, हर्पीज़ (त्वचा रोग) और कुछ कैंसर। इन बीमारियों को फैलानेवाले जीवाणु एक सामान्य प्रतिरोधक क्षमतावाले शरीर को कोई ख़तरा नहीं पहुँचाते। लेकिन यदि किसी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एच.आई.वी. के कारण कमज़ोर हो चुकी है, तो ये जीवाणु बेहद घातक रोग पैदा कर सकते हैं और इनके कारण मृत्यु भी हो सकती है।
एच.आई.वी. पॉज़िटिव होने में और एड्स में क्या अंतर है?एच.आई.वी. पॉज़िटिव का अर्थ है कि आपको वायरस का संक्रमण हो चुका है और ख़ून की जाँच के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है। फिर भी जब अलग‑अलग बीमारियाँ उभरने लगें, या CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 प्रति मिलिलीटर से कम हो जाए, तो उसे एड्स कहते हैं। जब से आपको वायरस का संक्रमण हुआ है, तब से एड्स होने में आपको पाँच से दस साल तक का समय लग सकता है।
एच.आई.वी. पॉज़िटिव व्यक्ति को अंत में एड्स हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इन अवस्थाओं का क्रम इस प्रकार है:
साधारण व्यक्ति
एच.आई.वी. संक्रमण
एच.आई.वी. पॉज़िटिव
बिना लक्षणों के एच.आई.वी. पॉज़िटिव
एच.आई.वी. रोग की प्रारंभिक अवस्था
एच.आई.वी. रोग की बाद की अवस्था
एड्स
मृत्यु
एच.आई.वी. की अवस्था का पता जाँच से लगाया जा सकता है।
एच.आई.वी. शरीर में कहाँ रहता है?आम तौर पर यह एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति के शरीर के द्रव्यों में जैसे कि वीर्य, योनि के स्रावों और ख़ून में रहता है।
हालाँकि इस बात के भी प्रमाण हैं कि एच.आई.वी. आँसुओं, लार (Saliva), पसीना और माँ के दूध में भी होता है, लेकिन इन सब में इसकी मात्रा इतनी कम होती है कि यह किसी और के शरीर को संक्रमित नहीं करता।
एच.आई.वी. शरीर में कैसे प्रवेश करता है और कैसे एड्स उत्पन्न करता है?एच.आई.वी. एक व्यक्ति से दूसरे तक तीन तरीक़ों से फैलता है:
- एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित रूप से संभोग द्वारा।
- एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति के ख़ून या ख़ून के अवयव (लाल कोशिकाएँ, प्लाज़्मा, प्लेटलेट्स इत्यादि) के साथ संपर्क में आने से—जैसे संक्रमित व्यक्ति के टीकों और सुइओं के प्रयोग से (आम तौर पर नशा करनेवाले ऐसा करते हैं)।
- एच.आई.वी. संक्रमित माता के द्रव्यों या दूध से नवजात शिशु को।
एड्स फैलने का सबसे बड़ा कारण संभोग है। यदि किसी स्त्री या पुरुष ने कंडोम का प्रयोग किए बिना किसी एच.आई.वी. संक्रमित या एड्स के रोगी स्त्री या पुरुष के साथ संभोग किया है, तो उन्हें भी एच.आई.वी. संक्रमण और एड्स होने का ख़तरा रहता है। यह रोग असुरक्षित संभोग करने (यानी बिना कंडोम के संभोग करने) से फैल सकता है।
एच.आई.वी./एड्स ...
असुरक्षित संभोग से फैल सकता है।

एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति का ख़ून चढ़ाने से फैल सकता है।
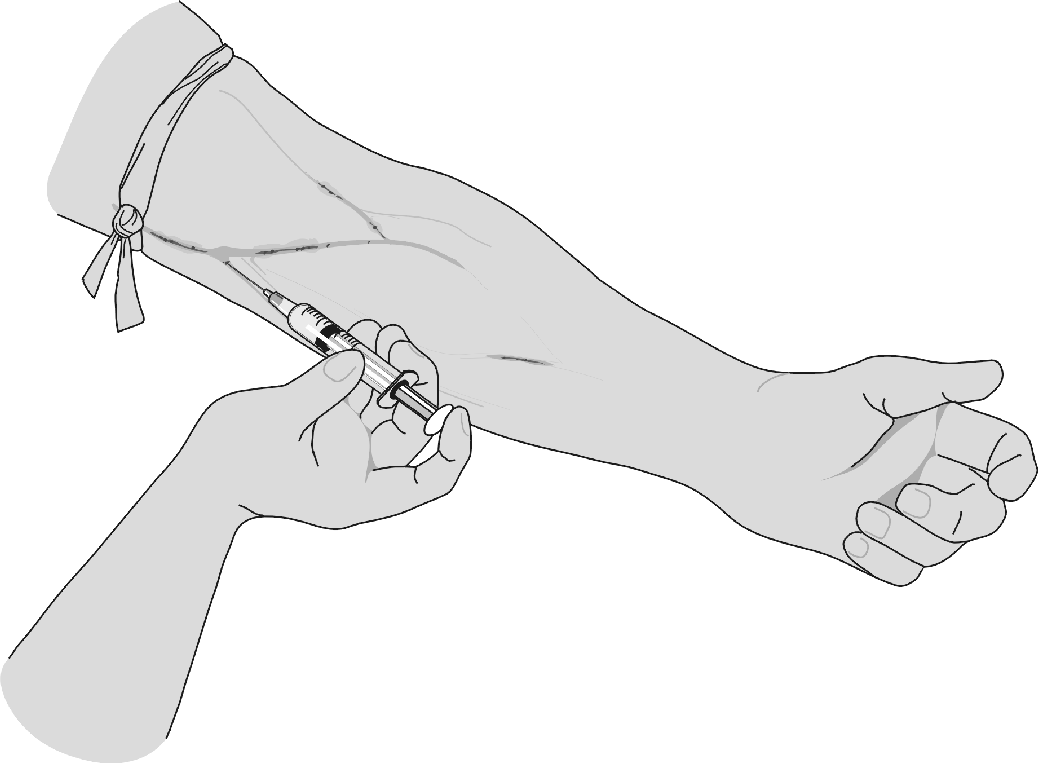
संक्रमित या एच.आई.वी. रोगियों द्वारा इस्तेमाल की गई सुइओं से फैल सकता है।

एच.आई.वी. संक्रमित माता से उसके बच्चे तक फैल सकता है।
- सिरिंजों और सुइओं से जिनमें एच.आई.वी. के जीवाणु हों और उन्हें कीटाणुरहित (Sterilize) किए बिना प्रयोग किया गया हो।
- कान, नाक को छेदनेवाले या टैटू बनानेवाले यंत्रों के इस्तेमाल से जिन्हें कीटाणुरहित न किया गया हो।
- नशा करनेवालों में नशा करते वक़्त यदि एक भी व्यक्ति को एच.आई.वी. हो तो एक दूसरे की सिरिंज और सुई के इस्तेमाल से सबको ख़तरा होता है।
- एच.आई.वी. पॉज़िटिव माँ से उसके बच्चे को एच.आई.वी. का ख़तरा है। यदि कोई एच.आई.वी. पॉज़िटिव स्त्री गर्भवती है तो गर्भाधान के दौरान, डिलीवरी के समय या कभी‑कभी बच्चे को स्तनपान करवाते समय संक्रमण हो सकता है। ऐसा होने का ख़तरा 35% है।
- स्वस्थ व्यक्ति को किसी संक्रमित व्यक्ति का ख़ून चढ़ाने से।
- एच.आई.वी. संक्रमित या एड्स के रोगी के साथ एक ही दफ़्तर या फ़ैक्ट्री आदि में काम करने से।
- एच.आई.वी. संक्रमित या एड्स के रोगी के साथ उठने‑बैठने, उसको छूने, उससे हाथ मिलाने या गले लगने से।
- एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्ति के इस्तेमाल किए हुए पेन, कंप्यूटर, टेलीफ़ोन, टाइपराइटर और किताबें आदि का इस्तेमाल करने से।
- किसी प्रतिष्ठित रक्तदान संस्था में ख़ून दान करने से।
- गालों या होंठों पर धीमे से चूमने से, यदि उन पर कोई ज़ख़्म नहीं है।
- एक साथ बस, ट्रेन या हवाई जहाज़ में सफ़र करने से।
- कीड़े के काटने से।
- एक साथ खाना खाने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से या एक ही शौचालय का इस्तेमाल करने से।
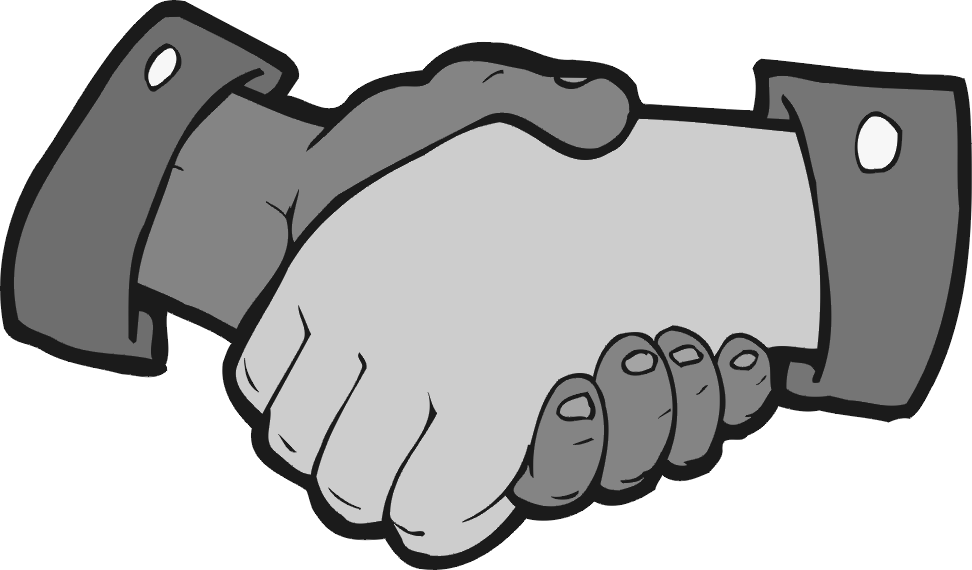
स्पर्श करने से नहीं फैलता
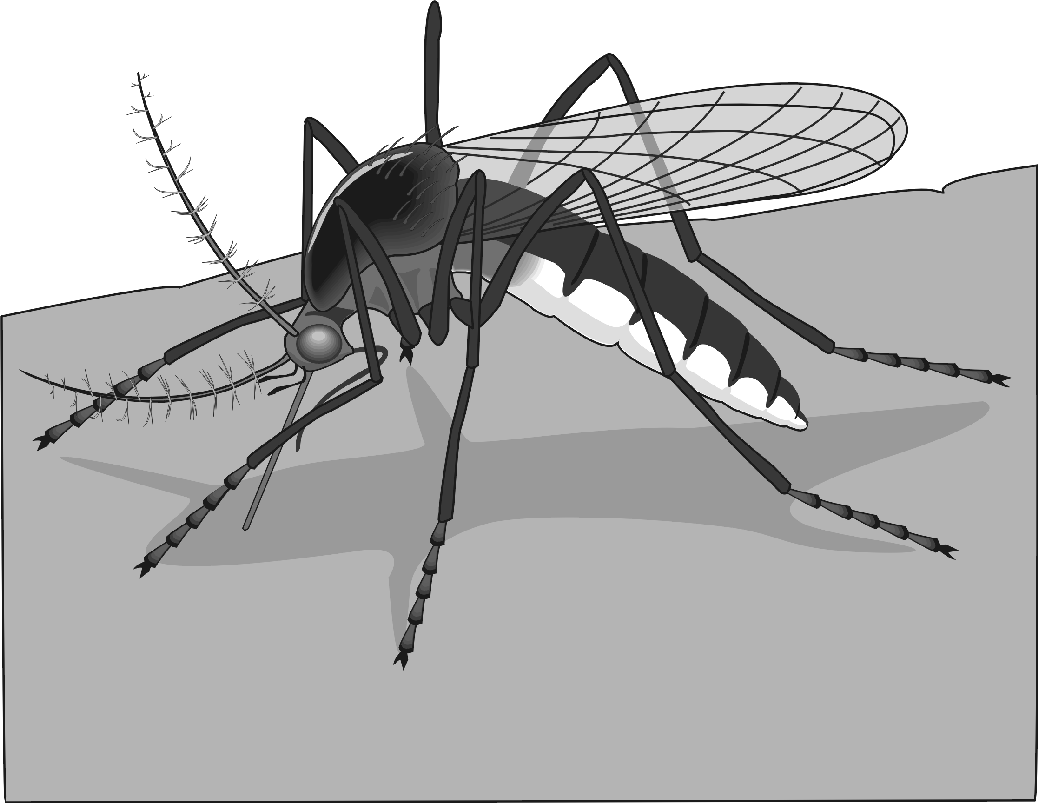
मच्छर काटने से नहीं फैलता

एक‑साथ काम करने से नहीं फैलता

एक दूसरे का भोजन, कपड़े या शौचालय के प्रयोग से नहीं फैलता
एच.आई.वी./एड्स से बचाव बहुत आसान है
यौन संबंधों में संयम और ईमानदारी बरतें- अपने जीवन साथी के साथ ही शारीरिक संबंध बनाएँ।
- यदि कभी किसी अजनबी के साथ संबंध बन जाते हैं, तो कंडोम का सही तरह से प्रयोग करें।
- हमेशा एक बार प्रयोग करके फेंक देनेवाली (disposable) सिरिंजों और सुइओं का ही इस्तेमाल करें।
- उन्हें एक बार इस्तेमाल करके नष्ट कर दें।
- हर व्यक्ति के लिए नई सिरिंज और सुई का प्रयोग करें।
- सड़कछाप नीम‑हकीमों (Quacks) से अपने कान या नाक न छिदवाएँ और न ही उनसे टैटू बनवाएँ, क्योंकि उनके औज़ार ज़्यादातर संक्रमित रहते हैं और उनमें एच.आई.वी. के या दूसरे ख़तरनाक कीटाणु भी हो सकते हैं।
- यदि आपको या आपके रिश्तेदारों को कभी ख़ून चढ़ाने की ज़रूरत हो तो यह सुनिश्चित करें कि ख़ून और ख़ून के अवयव की एच.आई.वी. के लिए जाँच हो चुकी हो। अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर पूछें।
- एच.आई.वी. के लिए जाँच हो चुके ख़ून की ही माँग करें, यह आपका अधिकार है।
यदि आपको संदेह होता है कि आपको एड्स है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपके सभी शक दूर कर देगा और यदि ज़रूरत हो, तो इस बातचीत के बाद वह आपको कुछ जाँच करवाने के लिए कह सकता है। एच.आई.वी./एड्स का पता ख़ून की इन जाँचों से लग सकता है:
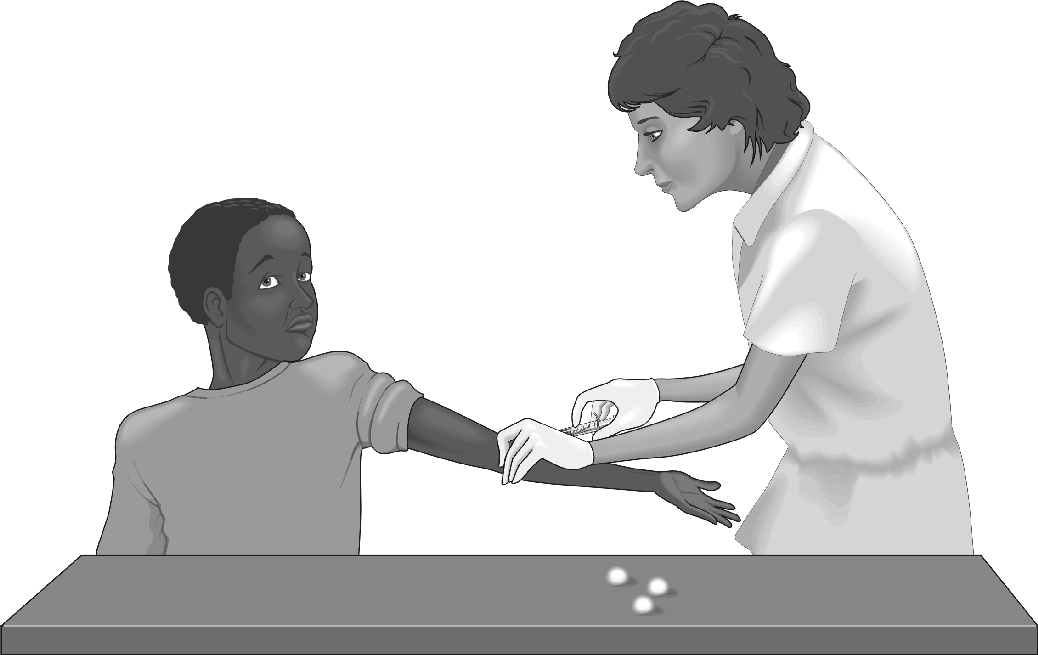
- एच.आई.वी. की पहचान के लिए तुरंत जाँच किए जानेवाला टेस्ट ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है।
- एलाइज़ा टेस्ट (Elisa Test)
- वैस्टर्न ब्लॉट टेस्ट (Western Blot Test)
एलाइज़ा टेस्ट, एच.आई.वी./एड्स होने की संभावना के कम से कम तीन महीने बाद ही करवाना चाहिए। इस तीन महीने के समय को ‘विंडो पीरियड’ (Window period) कहते हैं। इस समय से पहले जाँच करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता और इससे ग़लत परिणाम मिल सकते हैं।
विंडो पीरियड (Window Period)जब एच.आई.वी. मानव शरीर में प्रवेश कर लेता है तो एलाइज़ा जैसे टेस्ट द्वारा तुरंत ही इसकी पहचान हो सकती है। कम से कम तीन महीने बाद ये टेस्ट ख़ून में एच.आई.वी. ऐंटीबॉडीज़ (antibodies) का पता लगा सकते हैं। इस समय से पहले किए गए टेस्ट नेगेटिव हो सकते हैं, भले ही ख़ून में एच.आई.वी. मौजूद हो। एच.आई.वी. के रोगी के टेस्ट भले ही नेगेटिव आ रहे हों, लेकिन वह दूसरों तक यह बीमारी फैलाने में सक्षम ज़रूर है। इस समय को ‘विंडो पीरियड’ कहते हैं; यानी वह बीच का समय जब किसी व्यक्ति को एच.आई.वी. का संक्रमण तो होता है पर टेस्ट में नहीं आता और जब उसके ख़ून में एच.आई.वी. ऐंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, जिनसे उसके ख़ून की जाँच से एच.आई.वी. का मौजूद होना प्रमाणित होता है।
यह जाँच कहाँ की जाती है?भारत में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल संगठन (NACO) के अधीन राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत अधिकांश ज़िला अस्पतालों में स्वैच्छिक परामर्श और जाँच केंद्रों (Voluntary Counselling and testing Centres) में बहुत ही मामूली शुल्क पर एलाइज़ा टेस्ट किए जाते हैं।
एच.आई.वी. पॉज़िटिव व्यक्ति को किन लक्षणों का ध्यान रखना चाहिए?एच.आई.वी. पॉज़िटिव व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा संक्रमण और बीमारियाँ होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। यदि आप डॉक्टर की हिदायत के अनुसार समय पर दवाइयाँ ले रहे हैं और आपकी CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 से ज़्यादा रहती है तो रोग होने के आसार कम हो सकते हैं। इन लक्षणों का ध्यान रखें:
- तीन हफ़्ते से ज़्यादा तक बुख़ार रहना।
- तीन हफ़्ते से ज़्यादा समय तक खाँसी या दस्त होना, जो सामान्य इलाज से ठीक न हों।
- सही भोजन खाने के बावजूद वज़न कम होना।
- बहुत ज़्यादा कमज़ोरी।
- रात को पसीने आना।
- साँस लेने में तकलीफ़।
- मुँह में सफ़ेद दाग, ज़ख़्म, स्वाद बदल जाना, दाँत ढीले होना या त्वचा पर पित्ती आदि होना।
- निगलने में दिक़्क़त।
- गरदन, बग़ल और जाँघ में सूजन या गाँठें होना।
 जैसे‑जैसे बीमारी बढ़ती है, ये लक्षण बढ़ते जाते हैं तथा रोगी कमज़ोर होता जाता है। उस व्यक्ति को लगातार कोई न कोई संक्रमण या रोग होते रहते हैं। उपचार करने से जीवन कुछ लंबा ज़रूर हो जाता है लेकिन एड्स का कोई इलाज नहीं है।
जैसे‑जैसे बीमारी बढ़ती है, ये लक्षण बढ़ते जाते हैं तथा रोगी कमज़ोर होता जाता है। उस व्यक्ति को लगातार कोई न कोई संक्रमण या रोग होते रहते हैं। उपचार करने से जीवन कुछ लंबा ज़रूर हो जाता है लेकिन एड्स का कोई इलाज नहीं है।
ऐसी बहुत‑सी बातें हैं जिनका पालन करके कोई एच.आई.वी. पॉज़िटिव व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। हिम्मत और विश्वास से जीना और अपनी सेहत का ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे शरीर को एच.आई.वी./ एड्स के विरुद्ध लड़ने में सहायता मिलती है। किसी भी वैध या अवैध नशे का शिकार न बनें।
- पौष्टिक आहार लेना बेहद ज़रूरी है। हमेशा संतुलित भोजन करें और अपना वज़न सामान्य बनाए रखें। यह बहुत ज़रूरी है।
- धूम्रपान, पान और तंबाकू चबाना छोड़ दें, क्योंकि इनसे कैंसर हो सकता है। इन्हें छोड़ने से ज़रूर फ़ायदा होता है।
- व्यायाम करें: संतुलित भोजन करने के साथ साथ व्यायाम करने से मांसपेशियाँ मज़बूत होती हैं। आप तनाव से मुक्त रहते हैं, बढ़िया नींद आती है और आप बेहतर महसूस करते हैं। पैदल चलना, तैरना, धीमे दौड़ना और साइकिल चलाना अच्छे व्यायाम हैं। मज़बूत और तंदुरुस्त बने रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम ज़रूर करें।
- तनाव से दूर रहें: योग और ध्यान करें। आपको शांति और सुकून मिलेगा।
- सफ़ाई रखें: अपनी सफ़ाई रखने से आप ख़ुद भी संक्रमणों से बचे रहेंगे और दूसरों में भी संक्रमण नहीं फैलेगा।
- शराब और किसी भी प्रकार के अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहें, क्योंकि ये बीमारियों से लड़नेवाले आपके रक्षा तंत्र को कमज़ोर कर देते हैं।
- एच.आई.वी. पॉज़िटिव व्यक्ति संभोग के समय हमेशा कंडोम का प्रयोग करें।
- यह भी सुनिश्चित करें कि आपका ब्लेड, शेव करनेवाला रेज़र या मशीन और ब्रश कोई और इस्तेमाल न करे।
- ज़ुकाम, गला‑ख़राब आदि के रोगियों से दूर रहें और हर तरह के संक्रमण का इलाज जल्द से जल्द करें।
एच.आई.वी. पॉज़िटिव लोग लगभग सामान्य जीवन जी सकते हैं। यह बहुत महत्त्वपूर्ण कथन है,  हो सकता है कि उनके जीवन के कई उपयोगी साल अभी भी बचे हों!
हो सकता है कि उनके जीवन के कई उपयोगी साल अभी भी बचे हों!
जब एच.आई.वी. संक्रमण प्रमाणित हो जाए तो डॉक्टर की सलाह पर कुछ अन्य ख़ून के टेस्ट करवाएँ। ये टेस्ट CD4 कोशिकाओं की संख्या और वायरल लोड (Viral Load) हो सकते हैं। इन टेस्टों से डॉक्टर यह तय करता है कि आपको एेंटीरेट्रोवायरल दवाइयाँ (ART) कब देनी हैं? इन दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती परंतु नियंत्रण में रहती है।
पिछले कई सालों में अनेक लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एड्स का इलाज खोज लिया है, लेकिन मेडिकल विशेषज्ञों ने इनमें से किसी भी दावे को वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं पाया है। अभी तक तो एड्स का कोई इलाज नहीं है।
ऐंटीरेट्रोवायरल दवाइयाँ (ART)/या रेट्रोवायरस पर तेज़ी से असर करनेवाला इलाज (HAART—Highly Active Antiretroviral Therapy)
ART या HAART का नियमित रूप से सेवन करने से एच.आई.वी./एड्स का रोगी काफ़ी समय तक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। ये दवाइयाँ कुछ सरकारी अस्पतालों में विशेष वर्ग के लोगों के लिए मुफ़्त उपलब्ध हैं:
- पंद्रह साल तक की उम्र के एच.आई.वी. से संक्रमित बच्चे।
- वे महिलाएँ जो माता पिता से बच्चे तक संक्रमण रोकने के कार्यक्रम से जुड़ी हैं (Prevention of Parent to Child Transmission Programme) ।
- जो रोगी पूरी तरह से एड्स से पीड़ित हैं।
- ए.आर.टी. की दवाइयाँ प्रतिदिन उम्र भर लेनी पड़ती हैं।
- ए.आर.टी. के इलाज को बीच में छोड़ने से एच.आई.वी. का संक्रमण और भी ख़तरनाक हो सकता है।
- एच.आई.वी. में ए.आर.टी. के विरुद्ध प्रतिरोध भी पैदा हो सकता है यानी हो सकता है कि ए.आर.टी. की चिकित्सा कोई असर न करे।
- ए.आर.टी. में बहुत‑सी दवाइयाँ सही समय पर और भोजन के अनुसार लेनी पड़ती हैं। कृपया याद रखें कि ये दवाइयाँ काफ़ी महँगी हैं और इनका दुष्प्रभाव भी हो सकता है।
- यह सच है कि एड्स का मुख्य कारण शारीरिक संबंधों में असावधानी (लगभग 75‑80%) है।
- लेकिन संभोग के अलावा संक्रमण होने के अन्य कारण भी (लगभग 20‑25%) हैं।
- इसलिए कृपया एड्स के किसी रोगी को हीन भावना से न देखें। हम में से किसी को भी यह रोग हो सकता है।
जिस तरह आप किसी भी अन्य रोगी के साथ सामान्य रूप से और प्यार से बर्ताव करते हैं, वैसा ही बर्ताव एड्स के रोगियों के साथ भी करें। सभी बीमार लोगों को हमारी सेवा और सहारे की ज़रूरत है।
रक्तदान: एक महान परोपकार
ख़ून जीवन का एक बेहद महत्त्वपूर्ण अंग है। इसमें 55% प्लाज़्मा (Plasma) और 45% कोशिकीय अंश (Cellular Contents) होते हैं—लाल कोशिकाएँ (Red Blood Cells), सफ़ेद कोशिकाएँ (White Blood Cells) और प्लेटलेट्स (Platelets)। प्लाज़्मा में मुख्य रूप से तीन तरह के प्रोटीन होते हैं—एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फ़ाइब्रीनोजन और साथ ही ख़ून को जमानेवाले कुछ तत्त्व भी।
एक मिलिलीटर ख़ून में निम्नलिखित तत्त्व होते हैं:- 50 लाख लाल रक्त कोशिकाएँ (RBCs)
- 4000‑11000 सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ (WBCs)
- 1.5‑4 लाख प्लेटलेट्स
- ख़ून का कोई विकल्प नहीं है।
- ख़ून को किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता।
- सिर्फ़ इनसान ही रक्तदान कर सकते हैं।
- यदि हर स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करने को अपनी ज़िम्मेदारी समझे तो बीमार और ज़ख़्मी लोगों को बचाया जा सकता है।
- रक्तदान करनेवाले व्यक्ति के शरीर में दान के तुरंत बाद ही रक्त निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 24 घंटों के अंदर ही शरीर में रक्त की पूर्ति हो जाती है। ख़ून के बाक़ी अंश भी तीन हफ़्ते तक दोबारा बन जाते हैं।
ख़ून चढ़वाना इन परिस्थितियों और बीमारियों के इलाज में महत्त्वपूर्ण होता है:
| दुर्घटना | नवजात बच्चे में ख़ून बहनेवाली बीमारी |
| अनीमिया (ख़ून की कमी) | अधिक ख़ून बहना (Heamorrhages) |
| डिलीवरी के बाद ख़ून बहना | ख़ून का कैंसर (Leukemia) |
| ख़ून बहने की बीमारी | कोई बड़ा ऑपरेशन |
| जल जाना (केवल प्लाज़्मा) | थैलेसीमिया रोग (Thalassemia) |
- लाल रक्त कोशिकाएँ फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाती हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है।
- सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ शरीर में प्रवेश करनेवाले सभी रोगाणुओं (germs) को नष्ट करती हैं। इनका जीवन काल 7 घंटे से कुछ दिनों तक का होता है।
- शरीर में कोई ज़ख़्म होने पर, प्लेटलेट्स ख़ून को जमने में सहायता करते हैं। इनका जीवन काल पाँच दिन होता है।
- प्लाज़्मा ख़ून की नाड़ियों में बहता है। यह कोशिकाओं और अन्य बहुत‑से रासायनिक पदार्थों और पोषक तत्त्वों को शरीर के हर भाग तक पहुँचाता है।
किसी का जीवन बचाएँ—रक्तदान करें।
ए.बी.ओ.ब्लड ग्रुपहमारा ब्लड ग्रुप जीवन में कभी नहीं बदलता। ब्लड ग्रुप को लाल रक्त कोशिकाओं (Red Blood Cells) की सतह पर पाए जानेवाले प्रोटीन (ऐंटीजन) के आधार पर तय किया जाता है।
| ब्लड ग्रुप | लाल रक्त कोशिकाओं में… |
|---|---|
| ए बी | ए और बी-प्रोटीन (ऐंटीजन) दोनों होते हैं |
| ए | केवल ए-प्रोटीन (ऐंटीजन) होते हैं |
| बी | केवल बी-प्रोटीन (ऐंटीजन) होते हैं |
| ओ | इनमें से कोई प्रोटीन (ऐंटीजन) नहीं होता |
आर एच (Rh) ग्रुप का नाम मकैकस रीसस बंदर के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यह ग्रुप रीसस बंदर की लाल रक्त कोशिकाओं के प्रोटीन के समान होता है।
- यदि इनसान की लाल रक्त कोशिकाओं में आर एच प्रोटीन (ऐंटीजन) मौजूद हों, तो इसे आर एच पॉज़िटिव कहते हैं।
- यदि इनसान की लाल रक्त कोशिकाओं में आर एच प्रोटीन न हों तो इसे आर एच नेगेटिव कहते हैं।
- 95‑98% भारतीय आर एच पॉज़िटिव हैं, 2‑5% आर एच नेगेटिव हैं।

- 18‑60 वर्ष के बीच के कोई भी स्वस्थ महिला या पुरुष रक्तदान कर सकते हैं।
- पुरुष तीन महीने में एक बार और महिलाएँ चार महीने में एक बार रक्तदान कर सकती हैं।
- रक्तदाता का वज़न कम से कम 45 किलो होना चाहिए।
- ख़ून में हीमोग्लोबिन (Haemoglobin) की मात्रा कम से कम 12.5 ग्राम/डी एल होनी चाहिए।
- सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, (Systolic B.P. ) 120‑140 mm और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर (Diastolic B.P.) 70‑90 mm होना चाहिए।
- यदि शरीर में ख़ून की मात्रा वज़न के अनुसार 65‑80 मिलिलीटर प्रति किलोग्राम हो तो आप 6‑8 मिलिलीटर प्रति किलोग्राम रक्तदान कर सकते हैं।
- जितना दर्द एक टीका लगवाते समय होता है, रक्तदान करते हुए उससे ज़्यादा दर्द नहीं होता।
- पंजीकरण (Registration) और मेडिकल जाँच में लगभग बीस मिनट का ही समय लगता है और फिर रक्तदान करने तथा उसके बाद आराम करने में भी बीस मिनट लग जाते हैं।
- पिछले सात दिनों से सर्दी या बुख़ार (जिसका कारण न पता हो) है।
- पिछले 24 घंटों में कोई टीकाकरण (Vaccination) हुआ हो।
- पिछले 6 महीनों में गर्भपात हुआ हो या पिछले 12 महीनों में आप गर्भवती रही हों या बच्चे को स्तनपान करवाया हो।
- गंभीर हृदय रोग है।
- तपेदिक (TB) है।
- अति सक्रिय थायरॉयड (Thyrotoxicosis) है।
- कैंसर, गुर्दे के रोग, ख़ून बहने की प्रवृत्ति, अनीमिया या यौन रोग (Sexually Transmitted Disease) का इतिहास है।
- एड्स या एच.आई.वी. का संक्रमण है।
- ज़्यादा शराब पीने या नशे की आदत है।
- आप पिछले दो बार रक्तदान करते समय बेहोश हो गए हों।
- हेपेटाइटिस‑बी या हेपेटाइटिस‑सी है।
रक्तदान करने से पहले
- पानी पिएँ।
- ज़्यादा चाय या कॉफ़ी न पिएँ।
- रक्तदान से पहले कुछ हलका‑सा खा लें।
- दो घंटे तक अधिक पानी पिएँ और अन्य पेय पदार्थ भी अधिक लें।
- नियमित दिनचर्या जारी रखें लेकिन 24 घंटे तक कोई कठिन और थकानेवाला व्यायाम न करें।
- आधे घंटे तक शराब का सेवन न करें।
- लगभग दो घंटे तक धूम्रपान न करें।
- जहाँ से ख़ून लिया है वहाँ कुछ घंटे पट्टी (Band-Aid) लगी रहने दें।

- रक्तदान में बहुत कम समय लगता है और इसमें नाममात्र ही दर्द होता है।
- आपका नाम और अन्य सूचना दर्ज की जाती है।
- डॉक्टर पहले यह जाँच करता है कि क्या आपका ख़ून दूसरों को चढ़ाने लायक़ है या नहीं। इसके लिए आपके ब्लड प्रेशर, नाड़ी की गति (Pulse), शरीर के तापमान और अनीमिया (Anaemia) की जाँच की जाती है।
- आपको रक्तदान करनेवाली जगह पर ले जाया जाता है और आपकी बाज़ू को ऐंटीसेप्टिक से साफ़ किया जाता है।
- आपकी बाज़ू में से 350 मिलिलीटर ख़ून लेकर एक कीटाणुरहित प्लास्टिक बैग में इकट्ठा किया जाता है। सुई और बैग एक बार इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिए जाते हैं।
- रक्तदान की प्रक्रिया में लगभग 5‑8 मिनट का समय लगता है।
- रक्तदान के बाद आपको हलका जलपान दिया जाता है।
याद रखें कि रक्तदान के कारण शरीर के द्रव्यों में हुई कमी 24 घंटों के अंदर पूरी हो जाती है।
रक्तदान करके आपको एक सुखद एहसास होगा!
आपके द्वारा दान किए गए ख़ून का क्या होता है?ख़ून को एक प्लास्टिक के बैग में इकट्ठा किया जाता है, जिसमें एक ऐसा रसायन (Anticoagulant) मिला होता है जो ख़ून को जमने नहीं देता।फिर इस ख़ून की कई प्रकार की जाँच की जाती है—जैसे कि ए.बी.ओ. ग्रुप के लिए, आर एच फ़ैक्टर के लिए, हर तरह की संक्रामक बीमारियों, जैसे हेपेटाइटिस‑बी, हेपेटाइटिस‑सी, एच.आई.वी., सिफ़लिस और मलेरिया आदि के लिए। इस ख़ून को 4‑6° सेल्सियस तापमान पर फ़्रिज में रख लिया जाता है।
 जो ख़ून प्लेटलेट्स (Platelets) के लिए या प्लेटलेट्स को अलग करने के लिए लिया जाता हैâ उसे सामान्य तापमान पर प्लेटलेट इन्क्युबेटर या शेकर में रखा जाता है। प्लेटलेट्स को 5‑7 दिनों तक रखा जा सकता है, जबकि जमे हुए प्लाज़्मा को -30° सेल्सियस तापमान पर एक साल तक के लिए भी रखा जा सकता है। ख़ून चढ़ाने से पहले मरीज़ के ख़ून और रक्तदान में दिए गए ख़ून का आपस में तालमेल किया जाता है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि दोनों का रक्त एक दूसरे से मिलता है।
जो ख़ून प्लेटलेट्स (Platelets) के लिए या प्लेटलेट्स को अलग करने के लिए लिया जाता हैâ उसे सामान्य तापमान पर प्लेटलेट इन्क्युबेटर या शेकर में रखा जाता है। प्लेटलेट्स को 5‑7 दिनों तक रखा जा सकता है, जबकि जमे हुए प्लाज़्मा को -30° सेल्सियस तापमान पर एक साल तक के लिए भी रखा जा सकता है। ख़ून चढ़ाने से पहले मरीज़ के ख़ून और रक्तदान में दिए गए ख़ून का आपस में तालमेल किया जाता है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि दोनों का रक्त एक दूसरे से मिलता है।
यह समझ लेना ज़रूरी है कि ख़ून में अलग‑अलग तत्त्व होते हैं, जैसे पैक्ड लाल कोशिकाएँ, प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसीपिटेट (Cryoprecipitate) और प्लाज़्मा आदि और ये तत्त्व रक्त केंद्र में ख़ून से अलग करके तैयार किए जाते हैं। हर तत्त्व को कुछ समय के लिए ही सुरक्षित रखा जा सकता है और यह समय सबका अलग‑अलग है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक यूनिट ख़ून, चार या पाँच रोगियों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर ख़ून की कमी के रोगी को सिर्फ़ लाल रक्त कोशिकाओं की ही ज़रूरत होती है। जिसका ख़ून बह रहा हो या ल्यूकीमिया के रोगी को सिर्फ़ प्लेटलेट्स चाहिएँ और जले हुए रोगी को प्लाज़्मा की ज़रूरत होती है। क्रायोप्रेसीपिटेट का इस्तेमाल ख़ास तौर पर हीमोफ़ीलिया (Haemophilia) के लिए या ख़ून बहने के ऐसे किसी अन्य रोग में होता है।
मैं आपका नाम तो नहीं जानता…
लेकिन जीवन के इस तोहफ़े के लिए धन्यवाद।
रक्तदान करें!
किसी का जीवन बचाएँ।
रक्तदान करें।
रक्त–जीवन का अमृत
स्वयंसेवी ब्लड बैंक से मिली जानकारी
- ख़ून और इसके तत्त्वों की बहुत ज़्यादा माँग है और यह माँग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यदि आठ रोगियों को ख़ून चढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो औसतन एक को ही ख़ून मिल पाता है। इसलिए ख़ून की हर बूँद महत्त्वपूर्ण है। हर रक्तदान महत्त्वपूर्ण है। कभी न भूलें कि आप कितना महान काम कर रहे हैं। जब आप रक्तदान करते हैं तो आप वाक़ई किसी को ‘ज़िंदगी का तोहफ़ा दे रहे हैं।’
- आप अपने काम पर ही रक्तदान कर सकते हैं या किसी सार्वजनिक रक्तदान कैंप में जाकर ख़ून दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, मेडिकल जाँच और रक्त देने में लगभग 40‑45 मिनट लगते हैं। जब आप ख़ून देने के लिए आएँ तो आपसे रोज़मर्रा के जीवन के बारे में कुछ साधारण सवाल पूछे जाएँगे। इन सवालों का पूरी ईमानदारी से जवाब दें जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और उस रोगी को भी, जिसे यह ख़ून दिया जाएगा। इसके बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको पहले से ही ख़ून की कमी तो नहीं है, आपकी उँगली से एक बूँद ख़ून लिया जाएगा। यदि सब ठीक है तो आप रक्तदान कर सकते हैं। इसमें सिर्फ़ दस मिनट लगेंगे। फिर थोड़ा आराम और जलपान करके आप जा सकते हैं। जलपान का प्रबंध रक्तदान वाली जगह पर ही होगा।
- हम समझ सकते हैं कि आपके मन में कुछ शंका होगी। जब तक आप एक बार ख़ून दान नहीं करते, मन में शंका होना स्वाभाविक ही है। यदि ज़रूरत हो, तो आपकी सुविधा के लिए सुन्न करनेवाली दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप महसूस करेंगे कि रक्तदान कितना दर्दरहित, आसान और सहज है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह किसी की ‘ज़िंदगी बचाता है’।
- स्वयंसेवी ब्लड बैंकों (Voluntary Blood Banks) में रक्तदाताओं के लिए अलग‑अलग बीमा पॉलिसियाँ होती हैं जो यह निश्चित करती हैं कि भविष्य में जब कभी आपको ख़ून की ज़रूरत हो तो वह अवश्य पूरी की जाएगी। साल में कम से कम दो बार रक्तदान करके नियमित रक्तदाता बनें।
- आप एक रक्तदान से 6 क़ीमती ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है? फिर यह सब कितना आसान है! इसमें सिर्फ़ कुछ मिनट ही लगते हैं। इस दान के लिए आपकी सेहत अच्छी और दिल बड़ा होना चाहिए। क्या आपके पास ये हैं? आगे बढ़ें और आज ही पहला क़दम उठाएँ। कहीं न कहीं, कोई ज़रूर अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए आपसे उम्मीद लगाए बैठा है।
- 18‑60 वर्ष की उम्र का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति बिना किसी ख़तरे के रक्तदान कर सकता है। इसलिए यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, तो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए आप ही सही व्यक्ति हैं। आगे बढ़ें और आज ही एक ज़िंदगी बचाएँ।
- याद रखें! समाज में हमें हर तरह के ख़ून की ज़रूरत है, न कि सिर्फ़ दुर्लभ ब्लड ग्रुप की। दरअसल ब्लड ग्रुप जितना साधारण है, हमें उतनी ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ (O) है, तो साल में दो‑तीन बार रक्तदान करके आप ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं—शायद एक दिन अपनी भी! इसलिए नियमित रूप से रक्तदान करें। आप सचमुच ‘एक महान काम कर रहे हैं’।
- जब आप रक्तदान करते हैं तो आपका ख़ून किसी बेहद ज़रूरतमंद रोगी को दिया जाता है। यह मानवता की उत्तम सेवा है। रक्तदान करके बहुत गर्व महसूस होता है। यह आत्मसंतोष का एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक बार रक्तदान करके आपको पता चलेगा कि यह कितना बड़ा एहसास है! आगे बढ़ें और इसे ख़ुद महसूस करें।
- क्यों न आप अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सही जानकारी लें? हमारे पास बेहद क़ाबिल डॉक्टर हैं जो यह सुनिश्चित करेंगे कि रक्तदान करने से आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी सेहत के बारे में बात करके हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आप रक्तदान करने के योग्य हैं और आपका ख़ून किसी और को देने लायक़ है। फिर भी यदि कुछ स्वास्थ्य कारणों से आप रक्तदान न भी कर पाएँ तो आप अपने संबंधियों और दोस्तों को रक्तदान के लिए प्रेरित करके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं।
- रक्तदान के दौरान संक्रमण होने का कोई ख़तरा नहीं है। जिस सुई और बैग का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें ‘सिर्फ़ एक बार ही इस्तेमाल करके नष्ट कर दिया जाता है’। रक्तदान करने से आपको कोई भी संक्रामक रोग नहीं हो सकता।
- रक्तदान के तुरंत बाद शरीर इसकी भरपाई करना शुरू कर देता है और लगभग 24 घंटे में ख़ून की पूर्ति हो जाती है। रक्तदान करने की वजह से कहीं आपको अनीमिया न हो जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए आप अगला रक्तदान कम से कम तीन‑चार महीने के बाद करें।
- साल में तीन या चार बार रक्तदान करके एक नियमित रक्तदाता बनें। बहुत‑से लोग अपने जीवन में सौ से भी अधिक बार रक्तदान करते हैं—आप भी कर सकते हैं, हमारे समाज को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है।
- स्वयंसेवी ब्लड बैंक एक सामाजिक स्वावलंबी चेरिटेबल संस्था है जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं है। इसका लक्ष्य है समाज की मदद करना, जितना हो सके उतने जीवन बचाना और इसके लिए आपके ख़ून की ज़रूरत है। आप के दिए ख़ून के हर क़तरे की किसी वायरस या अन्य रोगाणु के लिए पूरी जाँच होगी। इसके तत्त्वों को अलग‑अलग कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।
रक्तदान के अलावा, आप केवल प्लाज़्मा भी दान कर सकते हैं।
प्लाज़्मा—ख़ून का सबसे बहुगुणी अंश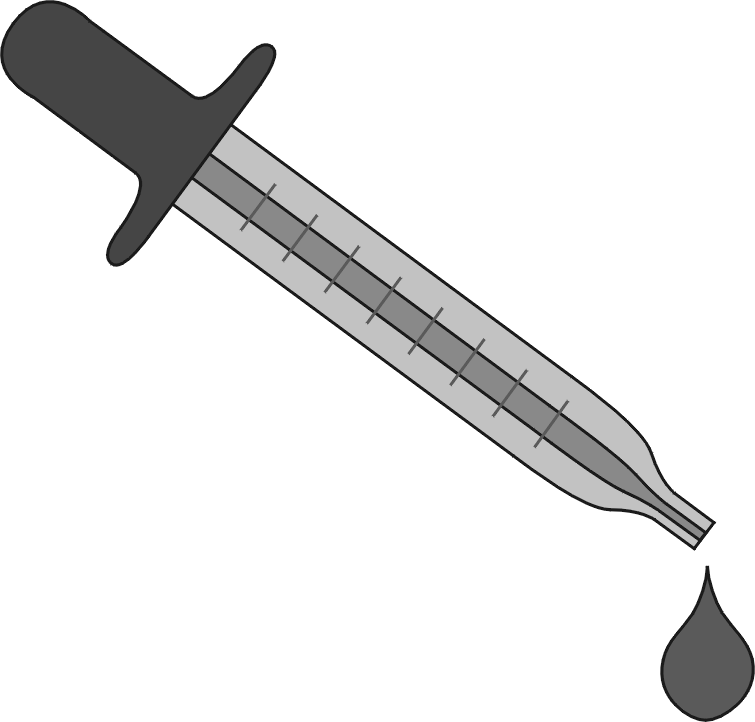 ख़ून में लाल रक्त कोशिकाएँ, सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ और प्लेटलेट्स होते हैं जो प्लाज़्मा नामक द्रव्य में मौजूद रहते हैं।
ख़ून में लाल रक्त कोशिकाएँ, सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ और प्लेटलेट्स होते हैं जो प्लाज़्मा नामक द्रव्य में मौजूद रहते हैं।
- प्लाज़्मा में बहुत महत्त्वपूर्ण प्रोटीन, पोषक तत्त्व और ख़ून को जमानेवाले तत्त्व (clotting factors) भी होते हैं जो ख़ून को बहने से रोकते हैं।
- एक बालिग़ व्यक्ति में लगभग पाँच लीटर ख़ून होता है, जिसमें तीन लीटर प्लाज़्मा होता है।
प्लाज़्मा से तेरह प्रकार के उपयोगी तत्त्व अलग किए जाते हैं। कुछ ऐसे तत्त्व जिनकी बहुत अधिक माँग है:
- बायोस्टैटिक या फ़ैक्टर VIII कॉन्सन्ट्रेट (Biostatic or factor VIII concentrate)—इसका इस्तेमाल हीमोफ़ीलिया‑ए के रोगियों में बहते ख़ून को रोकने के लिए किया जाता है। फ़ैक्टर VIII एक ऐसा प्रोटीन है जो सामान्य रूप से ख़ून के जमने (Blood clotting) के लिए ज़रूरी है। फ़ैक्टर VIII की आनुवंशिक कमी के कारण हीमोफ़ीलिया ए रोग होता है।
- इम्यूनोग्लोबुलिन (Immunoglobulin)—यह एक ख़ास तरह का मिश्रण है जिसमें ऐंटीबॉडीज़ होती हैं। यह संक्रामक रोगों से बचाता है जैसे टेटनस, छोटी माता (चिकन पॉक्स) और हेपेटाइटिस‑बी।
- एल्ब्यूमिन (Albumin)—यह अचानक जल जाने, सदमा या बिजली के शॉक (Shock) के उपचार के लिए ख़ून की मात्रा पूरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसे लिवर या गुर्दे के उपचार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
- इंट्रागाम पी (Intragam P)—इसमें ऐंटीबॉडीज़ होती हैं जो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को मज़बूत करती हैं। इसकी ज़रूरत मज्जा प्रतिरोपण (Bone marrow transplant) में या कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता (Immune system) के कारण हुई बीमारियों में होती है।
लोगों को जीवन की लड़ाई लड़ने में मदद करें
रक्तदान करें!
- प्लाज़्मा दान करने की एक ख़ास विधि होती है जिसे ऐफ़ेरेसिस (apheresis) कहते हैं।
- प्लाज़्मा को निकालने में लगभग 40 मिनट लगते हैं।
- एक बार के प्लाज़्मा दान में लगभग 650 मिलिलीटर प्लाज़्मा लिया जा सकता है।
इस प्रक्रिया में एक बाज़ू में से ही ख़ून लिया जाता है जिसे कोशिकाओं को अलग करनेवाले यंत्र (cell separating machine) से कीटाणुरहित थैली में इकट्ठा किया जाता है। यह यंत्र ख़ून में से केवल प्लाज़्मा ही निकालता है और ख़ून के बाक़ी तत्त्वों (लाल और सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ तथा प्लेटलेट्स) को उसी माध्यम से रक्तदान करनेवाले व्यक्ति के शरीर में वापस डाल देता है।
क्या प्लाज़्मा दान करने की विधि सुरक्षित है?- प्लाज़्मा दान करने की विधि एकदम सुरक्षित है। यह कार्य प्रशिक्षित कर्मचारी ही करते हैं।
- चूँकि प्लाज़्मा दान के समय आपकी लाल रक्त कोशिकाएँ आपके शरीर को वापस मिल जाती हैं, इसलिए हर दो से तीन सप्ताह के बाद आप प्लाज़्मा दान कर सकते हैं।
- यह ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ प्लाज़्मा ही दान करते रहें। आप जब चाहें रक्तदान भी कर सकते हैं।
- जो पहली बार प्लाज़्मा दान कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने पिछले एक साल में बिना किसी तकलीफ़ के कम से कम एक बार रक्तदान किया हो।
- प्लाज़्मा दान के लिए आपका चुनाव आपकी समयानुसार उपलब्धता, नाड़ियों की अनुकूलता, हीमोग्लोबिन के स्तर और ब्लड ग्रुप पर निर्भर करता है।
- प्लाज़्मा दान के लिए आयु 18‑60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 70 साल की आयु तक आप प्लाज़्मा दान कर सकते हैं।
- आपका वज़न 50 किलोग्राम या उससे ज़्यादा होना चाहिए।
- प्लाज़्मा दान के 24 घंटे पहले से ही ख़ूब पानी पिएँ और प्लाज़्मा दान से पहले भोजन ज़रूर करें।
किसी को जीवन का तोहफ़ा दीजिए रक्तदान कीजिए
आम पूछे जानेवाले प्रश्न
मेरा कितना ख़ून लिया जाएगा?मनुष्य के शरीर में 5‑6 लीटर ख़ून होता है। हर बार रक्तदान में 350 मिलिलीटर ख़ून लिया जाता है। दान के 24 घंटे के भीतर ही आपका शरीर अपने आप द्रव्य की पूर्ति कर लेता है और आपको कोई कमज़ोरी भी महसूस नहीं होती। यही कारण है कि कुछ लोग, जिन्हें अपना ऑपरेशन करवाना होता है, वे ऑपरेशन के 3‑4 सप्ताह पहले अपना ही ख़ून दान कर देते हैं, ताकि ऑपरेशन के समय उसका प्रयोग किया जा सके। यह काफ़ी जानी मानी विधि है और इसे ऑटोलोगस ब्लड डोनेशन (autologous blood donation) यानी अपने लिए रक्तदान कहते हैं।
पेशेवर रक्तदाताओं के बजाय अपनी मरज़ी से ख़ून देनेवालों को ज़्यादा महत्त्व क्यों दिया जाता है?पेशेवर रक्तदाता पैसे कमाने के लिए ही ख़ून दान करते हैं। हो सकता है वे अपनी कोई बीमारी, संक्रमण या नशीले पदार्थ के सेवन के बारे में न बताएँ, जिनका पता तुरंत जाँच से नहीं लग पाता। पेशेवर रक्तदाताओं से किसी गंभीर बीमारी का ख़तरा बना रहता है जबकि अपनी मरज़ी से ख़ून देनेवालों को यदि कोई बीमारी है, तो वे ख़ुद ही उसके बारे में बता देते हैं, इसलिए उनका ख़ून लेना सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाता है।
रक्तदान करने से मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा?आप तभी रक्तदान कर सकते हैं अगर आप स्वस्थ हैं। आपका केवल 5% ख़ून लिया जाता है और इससे कोई कमज़ोरी या हानिकारक परिणाम नहीं होता। शरीर से निकले द्रव्य की पूर्ति 24 घंटों में हो जाती है, जबकि रक्त कोशिकाएँ कुछ ही हफ़्तों में दोबारा बन जाती हैं।
यदि मुझे ख़ून की ज़रूरत पड़े तो?यदि आपको ख़ून की तुरंत ज़रूरत है तो आपको रक्त अस्पताल से मिलेगा। ज़्यादातर अस्पताल किसी रोगी को ख़ून देने के लिए उसके किसी संबंधी या मित्र से ख़ून लेना पसंद करते हैं।
क्या मैं रक्तदान के बाद धूम्रपान कर सकता हूँ?अच्छा होगा कि आप रक्तदान के बाद कम से कम दो घंटे तक धूम्रपान न करें, क्योंकि इससे चक्कर आ सकते हैं और आप बेहोश हो सकते हैं। बेहतर तो यह है कि आप धूम्रपान बिलकुल न करें।
क्या मैं किसी मित्र को साथ ला सकता हूँ?जी हाँ, आप अपने मित्र को अवश्य साथ ला सकते हैं। जब वह देखेगा कि रक्तदान कितना आसान है और इसमें कोई दर्द नहीं होता, तो उसे भी रक्तदान करने की प्रेरणा मिलेगी।
क्या मैं काम पर वापस जा सकता हूँ? जी हाँ, यदि आप रक्तदान वाली जगह छोड़ने से पहले कुछ जलपान और थोड़ा आराम कर लें तो काम पर वापस जा सकते हैं। कभी‑कभी रक्तदान करने के कुछ समय बाद कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं (ऐसा बहुत कम होता है)। इसलिए यदि आप ऐसे व्यवसाय में हैं जहाँ आप अपनी या दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप रक्तदान के तुरंत बाद काम पर न जाएँ।
जी हाँ, यदि आप रक्तदान वाली जगह छोड़ने से पहले कुछ जलपान और थोड़ा आराम कर लें तो काम पर वापस जा सकते हैं। कभी‑कभी रक्तदान करने के कुछ समय बाद कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं (ऐसा बहुत कम होता है)। इसलिए यदि आप ऐसे व्यवसाय में हैं जहाँ आप अपनी या दूसरों की ज़िंदगी ख़तरे में डाल सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप रक्तदान के तुरंत बाद काम पर न जाएँ।
यदि आप कोई बस या ट्रेन चलाते हैं या किसी आपातकालीन सेवा में काम करते हैं या ऊँचाई पर चढ़नेवाले काम (सीढ़ी चढ़ना) करते हैं, तो रक्तदान करने के बाद आपको उस दिन काम पर नहीं जाना चाहिए। अपना काम ख़त्म करने के बाद ही आप को रक्तदान करना चाहिए।
रक्तदान करने के लिए मैं कहाँ जा सकता हूँ?आप अपने घर, दफ़्तर या स्कूल के पास लगे किसी रक्तदान कैंप में जा सकते हैं अथवा अपने इलाक़े में किसी मान्यता‑प्राप्त ब्लड बैंक में रक्तदान कर सकते हैं। जानकारी के लिए कृपया स्थानीय भारतीय रैड क्रॉस ब्लड बैंक को फ़ोन करें।
रक्तदान—एक अच्छी आदतसमय‑समय पर रक्तदान करने के कई निजी फ़ायदे हैं:
- जब भी आप रक्तदान करते हैं तो आपसे स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ शारीरिक जाँच भी की जाती है। इस प्रक्रिया में कभी‑कभी आपकी सेहत से संबंधित किसी बीमारी का पता चल जाता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, अनीमिया या दिल की अनियमित धड़कन आदि। इस प्रकार किसी भी नई बीमारी का इलाज समय पर हो सकता है।
- दो अध्ययनों में पाया गया है कि जो पुरुष रक्तदान करते हैं और जो महिलाएँ (जिनकी माहवारी बंद हो चुकी हो) रक्तदान करती हैं, उनमें हृदय रोग कम पाया गया है।
- सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रक्तदान करना वाक़ई में एक ‘अच्छी आदत’ है। दूसरों का जीवन बचाकर आपको बहुत संतुष्टि मिलती है।
ख़ून कहीं बनाया नहीं जा सकता। इसे मनुष्य ही दान कर सकता है। यदि हर योग्य व्यक्ति रक्तदान करता है, तो न कभी इसकी कमी होगी और न ही ज़रूरतमंद लोगों को इससे वंचित रहना पड़ेगा।
आइए, और ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचाने के लिए मिलकर काम करें‑
आज ही रक्तदान करें!
ज़िम्मेदार बनें, रक्तदाता बनें।
किसी का जीवन बचाने में मदद करें!
नेत्रदान
अँधेरे से उजाले की ओर
अगर आप सहायक बनें तो
हमारे देश में दस लाख अंधों को नज़र मिल सकती है।
उन्हें आँखों की ज़रूरत है।
अगर आज आप नेत्रदान का प्रण लें
तो इससे ज़िंदगी बदल सकती है।
अपने प्यारों की आँखें दान करें।
उन्हें बंद न होने दें,
मौत के बाद भी उन्हें खुली रहने दें।
नेत्रदान एक अनमोल तोहफ़ा है,
जिसे केवल आप ही दे सकते हैं॥
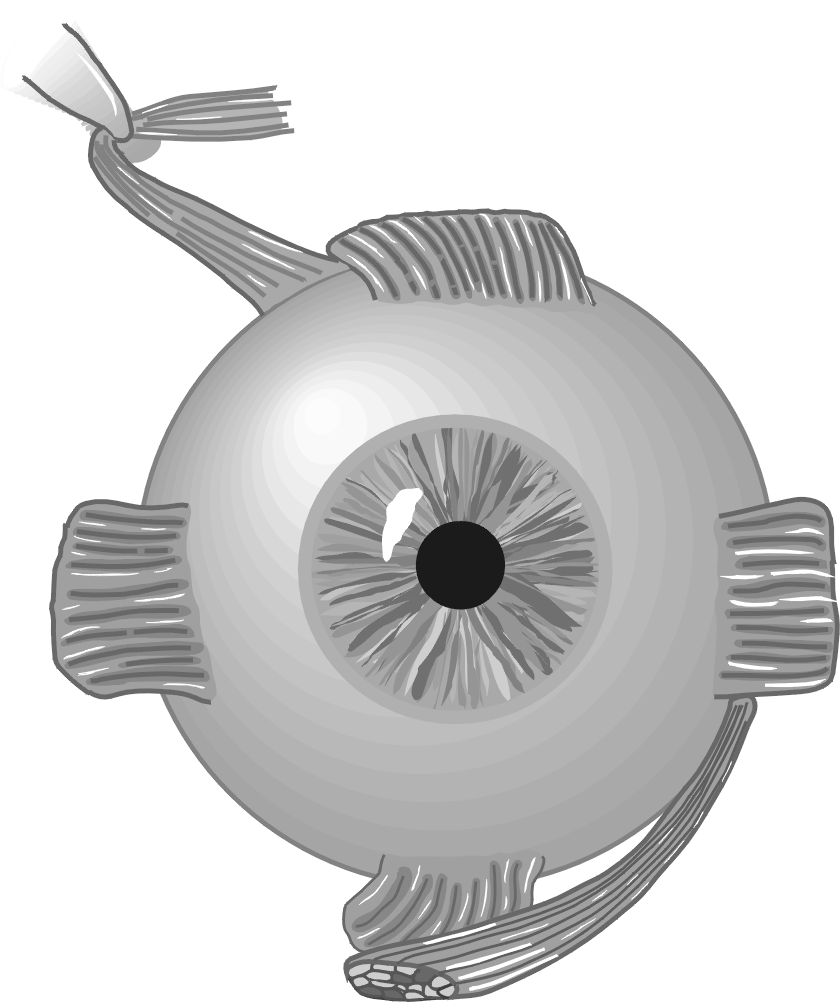
- चश्मा लगानेवाले लोग या जिन्होंने आँख का ऑपरेशन करवाया है, मधुमेह और ब्लड प्रेशर के रोगी, दमा, तपेदिक या हृदय‑रोगी सभी नेत्रदान कर सकते हैं।
- एड्स, ब्लड कैंसर, रेबीज़, ख़ून में संक्रमण (Septicaemia), वायरल हेपेटाइटिस आदि के रोगी नेत्रदान नहीं कर सकते।
- यदि किसी का कॉर्निया एकदम साफ़ है, चाहे उसकी रेटिना या ऑप्टिक नाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी हो, फिर भी वह नेत्रदान कर सकता है।
- अपने प्रियजन की आँखें दान करें। नेत्रदान से कॉर्नियल-अंधेपन के दो रोगियों को रोशनी मिल सकती है। अपने नज़दीकी नेत्र बैंक से संपर्क करें।
- सभी धर्म नेत्रदान का समर्थन करते हैं।
- मृत्यु के 6 घंटों के अंदर आँखें निकालनी ज़रूरी होती हैं; इन्हें निकालने में आधे घंटे से भी कम समय लगता है और जितनी जल्दी यह किया जाए उतना बेहतर है। इसलिए जल्दी ही अपने नज़दीकी नेत्र बैंक को सूचित करें। आप समय पर नेत्रदान करवाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि आपके परिवार या दोस्तों में से किसी की मृत्यु हो जाए तो नज़दीकी नेत्र बैंक को बताना न भूलें। भले ही मरनेवाले व्यक्ति ने नेत्रदान की प्रतिज्ञा की हो या नहीं।
- नेत्र बैंक के सदस्यों के आने से पहले पंखे बंद कर दें, ए.सी.या कूलर चलने दें। बर्फ़ और गीली रुई को बंद पलकों पर रख दें। इससे ऊतकों में नमी रहेगी। तकिया लगाकर सिर ऊँचा उठा दें।
- नेत्र बैंक के कर्मचारी डॉक्टर या किसी कुशल तकनीशियन के साथ दानी के घर आएँगे। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता। दानी का ख़ून जाँच के लिए लिया जाएगा।
- आँख को एक कीटाणुरहित (sterilized) विधि से निकाला जाएगा। इससे चेहरे पर कोई दाग़ या कुरूपता नहीं होती। नेत्रदान से दो अंधे लोगों को रोशनी मिलती है क्योंकि अंधे व्यक्ति को दान की गई एक आँख मिलती है।
- नेत्र बैंक पहुँचने पर ऊतकों की जाँच और तैयारी करके नेत्रों को जल्द से जल्द प्रत्यारोपण के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
- नेत्र बैंक में मौजूद ज़रूरतमंद लोगों की सूची के अनुसार उन्हें संपर्क किया जाता है।
- दान दी गई आँखें कभी ख़रीदी या बेची नहीं जातीं। नेत्रदान के हर प्रार्थनापत्र पर ग़ौर किया जाता है।
- कॉर्निया दान करनेवाले और प्राप्त करनेवाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाता है।
 कॉर्निया आँख के आगे एक पारदर्शी झिल्ली है जिसके द्वारा आँख के अंदर रोशनी केंद्रित होती है। यदि संक्रमण, चोट या किसी अन्य रोग से कॉर्निया धुँधला हो जाए तो दृष्टि बहुत कम हो जाती है या पूरी तरह जा भी सकती है।
कॉर्निया आँख के आगे एक पारदर्शी झिल्ली है जिसके द्वारा आँख के अंदर रोशनी केंद्रित होती है। यदि संक्रमण, चोट या किसी अन्य रोग से कॉर्निया धुँधला हो जाए तो दृष्टि बहुत कम हो जाती है या पूरी तरह जा भी सकती है।
- संक्रमण
- चोट
- रसायन से जलना
- कुपोषण (malnutrition)
- जन्मजात रोग
- ऑपरेशन के बाद कोई समस्या या संक्रमण
ख़ुशक़िस्मती से यदि कॉर्निया का दान मिल जाए तो इसे प्रत्यारोपित कर, अधिकतर रोगियों की दृष्टि वापस आ सकती है।
नेत्रदान से किन रोगियों को फ़ायदा होता है?- केवल कॉर्नियल—अंधेपन के रोगियों को।
आम तौर पर आँख के पारदर्शी भाग (कॉर्निया) का प्रयोग होता है। कभी‑कभी सफ़ेद भाग (Sclera), कंजंकटाइवा और कॉर्निया के आसपास के भाग में मौजूद स्टेम कोशिकाओं (stem cells) का भी प्रयोग होता है।
मैं नेत्रदान की प्रतिज्ञा कैसे कर सकता हूँ?अपने नज़दीकी नेत्र बैंक में एक फ़ॉर्म भरें और इस पर किसी संबंधी के दस्तख़त भी करवा लें।
- नेत्र बैंक आपको एक दानी कार्ड देगा, जिसे आप अपनी जेब में हर वक़्त, रख सकते हैं।
- नेत्रदान करने की इच्छा अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बताएँ।
- अपने परिवार या पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाने पर उन्हें भी नेत्रदान करने के लिए प्रेरित करें और मनाएँ।
- यदि वे लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी नेत्र बैंक से संपर्क करें ताकि वे अपनी टीम समय पर भेज सकें।
- ‘दृष्टिदूत’ बनें।
- नेत्रदान आंदोलन का हिस्सा बनें।
- नेत्रदान की जानकारी बाँटें। आपके प्रचार से इस आंदोलन को बल मिलेगा।
- अपने क्षेत्र में किसी की मृत्यु पर उसके परिवार के लोगों को मृत व्यक्ति की आँखें दान करने के लिए प्रेरित करें।
- अपने क़रीबी रिश्तेदारों और मित्रों के नेत्रदान के लिए अपना समर्थन दें।
- अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर तुरंत किसी नज़दीकी नेत्र बैंक को फ़ोन करें।
अंगदान: जीवन का एक अमूल्य तोहफ़ा
हैं ऐसे सितारे जिनकी चमक देखी जा सकती है,
पृथ्वी पर अब भी
ख़ुद चाहे वे विलुप्त हो गए बहुत समय पहले।
हुईं हैं ऐसी हस्तियाँ प्रतिभा जिनकी कर रही
है आलोकित जग को अब तक
ख़ुद चाहे अब वे ज़िंदा रहे नहीं।
जब रात अँधेरी होती है तो उन ज्योतियों का
प्रकाश कुछ ज़्यादा ही उज्ज्वल होता है॥
हाना सेनेश
मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है! हम जीने और मरने के लिए जन्म लेते हैं। टैगोर के शब्दों में, “जन्म की तरह मृत्यु भी ज़िंदगी का हिस्सा है। चलने के लिए पैर ऊपर उठाकर फिर नीचे भी रखना होता है।” लोग ऐसा मानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है। लेकिन इनसान मरने के बाद भी ज़िंदा रह सकता है। मौत के मुँह में जा रहे कई रोगियों को अंगदान का अमूल्य तोहफ़ा देकर आप अपनी मृत्यु को भी जीवन की तरह सार्थक बना सकते हैं।
किसी अंग के नाकाम हो जाने पर यह अनमोल जीवन व्यर्थ नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जो किसी महत्त्वपूर्ण अंग के काम न करने से अपना जीवन गँवा चुके हैं। सच तो यह है कि अंग प्रत्यारोपण विज्ञान में, ऑपरेशन और अंग संरक्षण के क्षेत्र (Organ preservation) में इतनी तरक़्क़ी हो चुकी है कि महत्त्वपूर्ण अंगों का प्रत्यारोपण करना संभव है। इसलिए कुछ रोग जो किसी अंग को हमेशा के लिए नाकाम कर देते हैं, उनके इलाज के लिए कुछ सार्थक क़दम उठाए जा सकते हैं। आपको बस अंगदान करने की प्रतिज्ञा करनी है और अनमोल ज़िंदगियों को समय से पहले खो जाने से बचाना है।
अंग प्रत्यारोपण से लोग फिर से सामान्य और उपयोगी ढंग से जीवन व्यतीत कर सकते हैं जिससे जीवन काफ़ी बेहतर हो जाता है। गुर्दे के रोगियों में गुर्दे के प्रत्यारोपण से व्यक्ति सामान्य जीवन बिता सकता है और उसे रोज़ाना डायलेसिस (dialysis) पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हृदय और लिवर के रोगियों में जहाँ डायलेसिस जैसी कोई रक्षा प्रणाली भी नहीं है, उनके लिए तो बचाव का एकमात्र उपाय प्रत्यारोपण ही है।
अंगदान करनेवालों की कमी के कारण अनेक रोगी मर जाते हैं और उनके परिवार दुःख के सागर में डूब जाते हैं। लेकिन खेद की बात तो यह है कि यदि हम में से कुछ लोग भी मृत्यु के बाद अंगदान की प्रतिज्ञा करें तो प्रत्यारोपण के लिए अंगों की कमी नहीं होगी।
पूछो अपने आप से
कि क्या स्वर्ग और महानता का स्वप्न
हमें क़ब्रों में हमारा इंतज़ार करता मिले
या वह स्वप्न हम अभी और यहाँ इस धरती पर साकार करें।
आयन रैंड
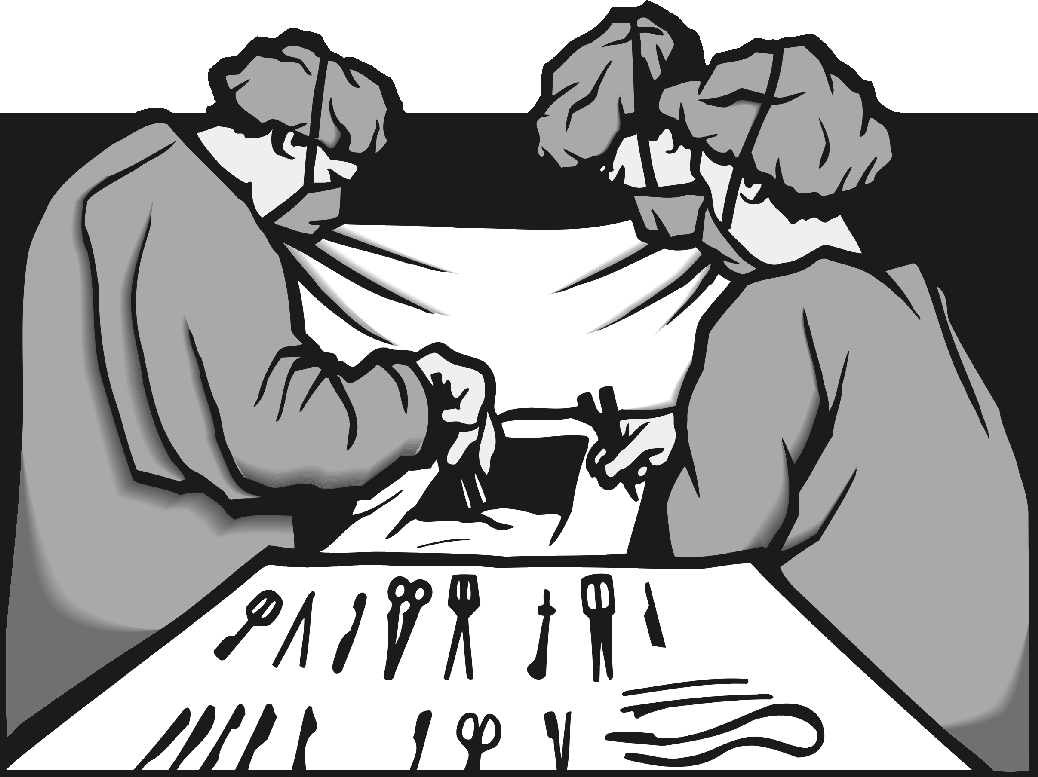 अंगदान का अर्थ है, किसी को जीवन दान देना। जब लोग अंगदान करते हैं तो इसका मतलब है कि वे अंग से भी क़ीमती वस्तु दान कर रहे हैं। दरअसल वे किसी को ज़िंदगी दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि लोग अपने जीवन में ही यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अंगों को उन मरीज़ों में प्रत्यारोपण के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए जिनके बचने की आशा नहीं है, ताकि उन्हें एक नई ज़िंदगी मिल सके।
अंगदान का अर्थ है, किसी को जीवन दान देना। जब लोग अंगदान करते हैं तो इसका मतलब है कि वे अंग से भी क़ीमती वस्तु दान कर रहे हैं। दरअसल वे किसी को ज़िंदगी दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि लोग अपने जीवन में ही यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अंगों को उन मरीज़ों में प्रत्यारोपण के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए जिनके बचने की आशा नहीं है, ताकि उन्हें एक नई ज़िंदगी मिल सके।
रोज़ी चलती है उससे जो हमें मिलता है,
ज़िंदगी बनती है उससे जो हम देते हैं।
नोर्मन मैकइवन
जीवित दानी: ‘मानव अंगों के प्रत्यारोपण अधिनियम’ 1994 (Transplantation of Human Organs act 1994) के अनुसार, कोई व्यक्ति जीते‑जी अपने परिवार में केवल ख़ून के रिश्तेदारों (भाई, बहन, माता‑पिता और बच्चे) को ही अंगदान कर सकता है। एक जीवित अंगदान करनेवाला व्यक्ति कुछ ही अंग दान कर सकता है जैसे एक गुर्दा (क्योंकि एक गुर्दा भी शरीर का कार्य करने में सक्षम है), पैन्क्रियास (Pancreas) का कुछ हिस्सा (आधे पैन्क्रियास से भी शरीर का कार्य चल सकता है) और जिगर (लिवर) का कुछ हिस्सा (क्योंकि प्रत्यारोपण किया गया भाग कुछ समय बाद अपने आप पुनर्विकसित हो जाता है)।
मरणोपरांत अंगदानी: दिमाग़ी मृत्यु के बाद सारे अंग और ऊतक (tissues) दान में दिए जा सकते हैं।
अंगदान तभी दिया जा सकता है जब किसी को दिमाग़ी तौर पर मृत (Brain Dead) घोषित कर दिया जाए। ‘दिमाग़ी तौर पर मृत’ का क्या अर्थ है? यह ऐसी अवस्था है जब दिमाग़ के सभी सामान्य कार्य हमेशा के लिए बंद हो जाएँ और उन्हें फिर शुरू न किया जा सके यानी जब दिमाग़, शरीर को उसके ज़रूरी काम (जैसे साँस लेना, महसूस करना, कोई आदेश मानना) करने के लिए कोई संदेश न भेज सके। ऐसे लोगों को वेंटीलेटर (Ventilator) पर रखा जाता है, ताकि अंगों में ऑक्सीजन का प्रवाह बना रहे और जब तक उन अंगों को निकाल न लिया जाए तब तक वे स्वस्थ हालत में रहें। दिमाग़ी मृत्यु अधिकतर सिर पर चोट लगने के कारण या आइ.सी.यू. में मौजूद दिमाग़ के कैंसर के रोगियों की होती है। इनके अंग निकालकर उन रोगियों के शरीर में डाल दिए जाते हैं जिनके अपने अंग काम करना बंद कर चुके होते हैं।
घर पर हुई मृत्यु में केवल कॉर्निया (आँखें) ही निकाली जाती हैं लेकिन हृदय के वॉल्व, अस्थियाँ, मध्य कर्ण, लिगामेंट और त्वचा आदि लेने के लिए शरीर को मृत्यु हो जाने के कुछ घंटों के भीतर ही अस्पताल ले जाना पड़ता है।
ले चलो मुझको असत्य से सत्य की ओर,
अँधेरे से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर।
दूसरों के जीवन का सहारा बनो।
इसका निर्णय डॉक्टरों का दल करता है, जिनके पास इस कार्य के लिए प्रमाणित योग्यता और अनुभव है। ये डॉक्टर दिमाग़ी मृत्यु की पुष्टि करने के लिए अनेक प्रकार की जाँच करते हैं।
कम से कम 6 से 12 घंटे के अंतराल में दो तरह के टेस्ट किए जाते हैं। दूसरे टेस्ट को मृत्यु का क़ानूनी वक़्त माना जाता है। जब व्यक्ति को दिमाग़ी तौर पर मृत घोषित कर दिया जाता है, तो उसके बाद कोई भी जीवन रक्षक प्रणाली व्यर्थ है तथा इससे मानसिक और आर्थिक हानि ही होती है। यही वक़्त है जब मृत व्यक्ति के अंगों के दान का निर्णय लिया जा सकता है।
अंग कितनी जल्दी दान दिए जाने चाहिएँ?दिमाग़ी मृत्यु के बाद जितनी जल्दी हो सके, स्वस्थ अंगों को अंगदानी के शरीर से निकालकर रोगी के शरीर में प्रत्यारोपित कर देना चाहिए।
अंगदान कौन कर सकता है?कोई भी व्यक्ति—आयु, जाति और लिंग के भेदभाव के बिना अंग और ऊतक दान कर सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र वालों को अंगदान की प्रतिज्ञा के लिए अपने माता‑पिता या क़ानूनी अभिभावकों (Legal Guardian) की अनुमति लेना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति मेडिकल तौर पर अंगदान करने के क़ाबिल है कि नहीं—इसका फ़ैसला मृत्यु के समय ही किया जाता है। एच.आई.वी., हेपेटाइटिस‑बी, हेपेटाइटिस‑सी इत्यादि के रोगी अंगदान करने के योग्य नहीं हैं।
दिमाग़ी मृत्यु के बाद अंगदान की अनुमति कौन दे सकता है?जिन्होंने अपने जीवन काल में दो गवाहों (जिनमें से एक क़रीबी रिश्तेदार होना ज़रूरी है) की मौजूदगी में अंगदान करने की मंज़ूरी दी है, उन्हें अपने साथ यह कार्ड रखना चाहिए तथा अपनी इस इच्छा के बारे में अपने नज़दीकी लोगों को भी बताना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने ऐसी कोई इच्छा ज़ाहिर न की हो या अंगदान का कार्ड न भरा हो, तो जिस व्यक्ति का उसके मृत शरीर पर क़ानूनी अधिकार होता है, वही व्यक्ति अंगदान की मंज़ूरी दे सकता है।
प्रत्यारोपण से कौन-सी जानलेवा बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं?अंगदान से जिन गंभीर बीमारियों को दूर किया जा सकता है, वे हैं:
| अंग/ऊतक | रोग |
|---|---|
| हृदय | हार्ट फ़ेलe |
| फेफड़े | फेफड़ों की बीमारी |
| गुर्दे | गुर्दा फ़ेल हो जाना |
| लिवर | लिवर का काम करना बंद होना |
| पैन्क्रियास | मधुमेह |
| आँखें | अंधापन |
| हृदय के वॉल्व | वॉल्व की बीमारी |
| त्वचा | त्वचा का जल जाना |
| हड्डियाँ | जन्मजात दोष, चोट या कैंसर आदि |
मुख्य अंग और ऊतक जो दान किए जा सकते हैं—हृदय, फेफड़े, लिवर, पैन्क्रियास, गुर्दे, आँखें, हृदय के वॉल्व (Valve), त्वचा, अस्थियाँ, मज्जा (bone Marrow), संयोजी ऊतक (connective Tissue), मध्य कर्ण (Middle Ear) और ख़ून की नाड़ियाँ। इसलिए एक अंगदानी मरणोपरांत गंभीर रूप से बीमार ऐसे अनेक रोगियों को जीवन दान दे सकता है जिनके बचने की उम्मीद नहीं होती।
जो पीछे है हमारे, वह जो आगे है हमारे,
वे दोनों तुच्छ हैं तुलना में उसके
जो हमारे अंदर है।
राल्फ़ वॉल्डो एमर्सन
अंग और ऊतक जो दान किए जा सकते हैं
आपके आंतरिक अंग उन रोगियों में प्रत्यारोपित किए जाएँगे जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जीवन के ये तोहफ़े (अंग) रोगियों की प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा सूची, तालमेल, उनकी ज़रूरत और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करते हैं।
क्या अंगदान के लिए मेरे परिवार को पैसे देने पड़ेंगे?नहीं। अंग या ऊतकों के प्रत्यारोपण के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। अंगदान एक सच्चा तोहफ़ा है।
क्या अंगदान या ऊतक दान से अंतिम संस्कार/दफ़नाने की तैयारी में या शरीर के आकार में कोई फ़र्क़ पड़ता है?नहीं। अंगों या ऊतकों के निकाले जाने से अंतिम संस्कार या दफ़नाने की तैयारी में कोई अंतर नहीं पड़ता। बाहरी तौर से शरीर में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। प्रत्यारोपण में माहिर, कुशल डॉक्टरों का दल शरीर से अंगों या ऊतकों को निकालता है जिन्हें किसी दूसरे मरीज़ में रोपित किया जा सकता है। सर्जन बड़ी कुशलता से शरीर की सिलाई कर देते हैं, इसलिए शरीर के आकार में कोई अंतर नहीं आता। शरीर किसी सामान्य मुर्दे की तरह ही दिखता है और अंतिम संस्कार में देरी नहीं लगती।
ऐसा नहीं कि ज़िंदगी की बेइंसाफ़ी दूर न कर सकें;
हम दूसरों के लिए तो पलड़ों को बराबर
करने में सहायक हो ही सकते हैं, भले ही
हमेशा अपने लिए बराबर न कर सकें।
ह्यूबर्ट हम्फ़्रे
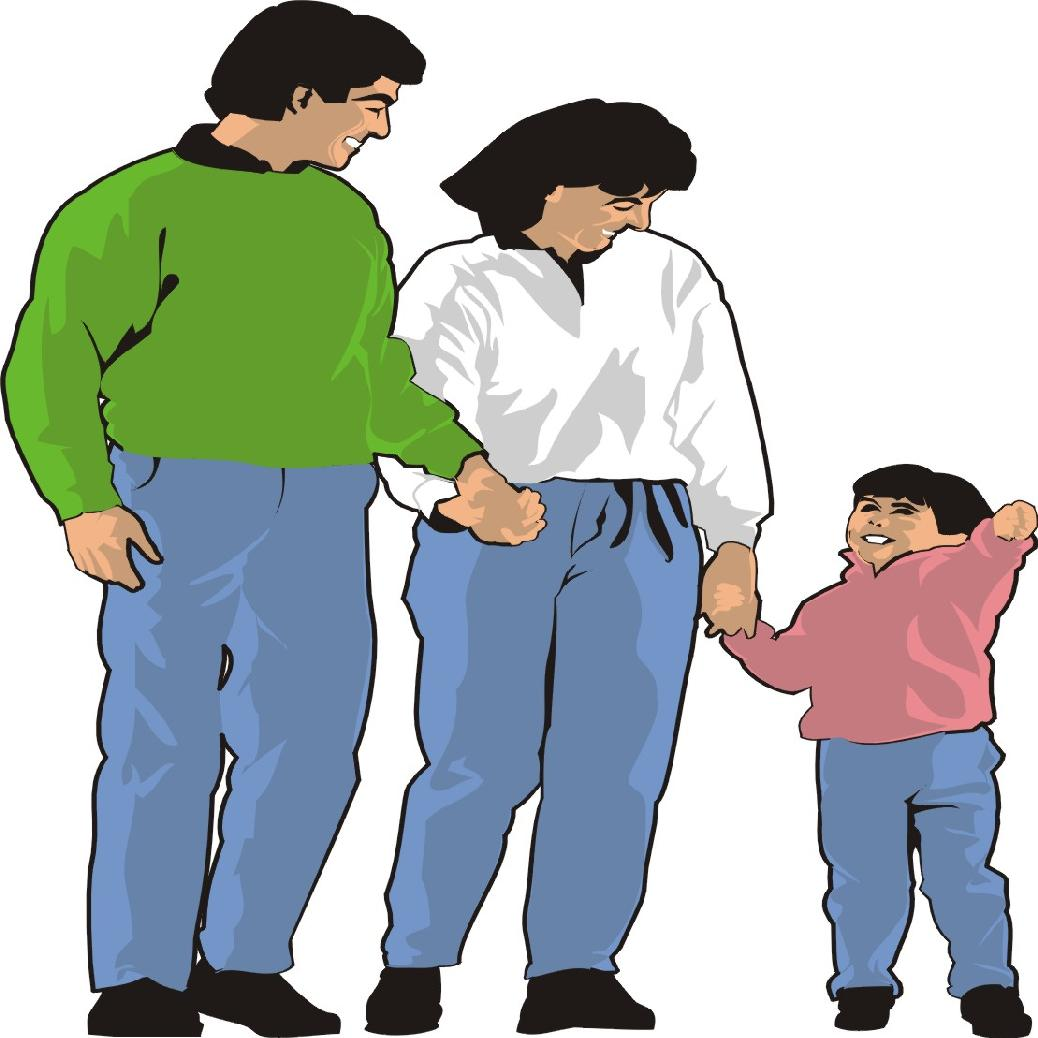 जी हाँ। यदि आपके हस्ताक्षर वाला अंगदान कार्ड मिल जाता है तो भी डॉक्टर आपके परिवार की अनुमति ज़रूर लेंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने परिवार वालों और प्रियजनों से अंगदान करने के अपने फ़ैसले की बात ज़रूर करें, ताकि उन्हें आपकी यह इच्छा पूरी करने में आसानी हो।
जी हाँ। यदि आपके हस्ताक्षर वाला अंगदान कार्ड मिल जाता है तो भी डॉक्टर आपके परिवार की अनुमति ज़रूर लेंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने परिवार वालों और प्रियजनों से अंगदान करने के अपने फ़ैसले की बात ज़रूर करें, ताकि उन्हें आपकी यह इच्छा पूरी करने में आसानी हो।
अंगदान क़ानूनी है। भारतीय सरकार ने फ़रवरी 1995 में “मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994” पारित किया था, जिसके अनुसार जिस व्यक्ति की क़ानूनी तौर पर दिमाग़ी मृत्यु हो चुकी है, उसके अंग दान किए जा सकते हैं।
क्या मानव अंगों को बेचना क़ानूनी है?जी नहीं। “मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994” के अनुसार मानव अंगों और ऊतकों को बेचा नहीं जा सकता। ऐसा करनेवालों को जुर्माना या जेल की सज़ा हो सकती है।
क्या मृत्यु के बाद घर पर ही अंग निकाले जा सकते हैं?जी नहीं। अंग तभी निकाले जा सकते हैं जब किसी व्यक्ति की दिमाग़ी मृत्यु अस्पताल में हुई हो और उसे तुरंत ही वेंटीलेटर या किसी दूसरी जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया हो। मृत्यु के बाद घर पर केवल आँखें ही निकाली जा सकती हैं।
सामने क्या है यह जब निश्चित नहीं।
तो आशा मन में रखना कोई ग़लती नहीं॥
ओ.कार्ल सिमंटन
नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइज़ेशन (ORBO) की स्थापना से अंगदान एक हक़ीक़त बन गया है। यह देश का केंद्रीय सेंटर है जिसका मक़सद लोगों को अंगदान की प्रेरणा देना, मानव अंगों का सही एवं बराबर वितरण तथा इनका एकदम सही इस्तेमाल करना है।
ORBO उन लोगों की सूची रखता है जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें अंग प्रत्यारोपण की ज़रूरत है। यहाँ दानियों की सूची भी होती है। इसके काम हैं—दानी और रोगी के अंगों का तालमेल, अंग निकालने से लेकर उनके प्रत्यारोपण तक तालमेल, संबंधित अस्पतालों और लोगों तक जानकारी पहुँचाना और अंगदान तथा प्रत्यारोपण की गतिविधियों का प्रचार करना। इसका संपर्क दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों से है और यह दायरा बढ़ता जा रहा है।
अंगदान की प्रतिज्ञा करें!
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
ORBO ओ.आर.बी.ओ.
ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइज़ेशन
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
(All India Institute of Medical Sciences)
अंसारी नगर, नई दिल्ली 110029
फ़ोन:1060 (विशेष 24 घंटे हेल्पलाइन),
2659 -3444/2658 8360
फ़ैक्स: 011 -2658 -8402
E-Mail Addresses
Stem Cells: [email protected]
ORBO (ऑर्गन रिट्रीवल बैंकिंग ऑर्गेनाइज़ेशन):
[email protected] / [email protected]
Web site: www.aiims.edu/aiims/orbo www.orbo.org
अंगदान की सुविधा देश के कई भागों में उपलब्ध है जैसे चेन्नई, बैंगलुरू, मुंबई, हैदराबाद और चंडीगढ़। यह सुविधा देश के अन्य भागों में उपलब्ध करवाई जा रही है।
संपर्क संबंधी जानकारी और अन्य सूचना
भारत में मुख्यालय
सेक्रेटरी
राधास्वामी सत्संग ब्यास
डेरा बाबा जैमल सिंह
ज़िला अमृतसर
ब्यास, पंजाब 143 204, भारत
अन्य सभी देशों में
अन्य सभी देशों में संपर्क संबंधी जानकारी और राधास्वामी सत्संग ब्यास की शिक्षा और गतिविधियों के बारे में सूचना हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है:
www.rssb.org
सत्संग सेंटर
अन्य सभी देशों के सत्संग सेंटर और कार्यक्रम का विवरण हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है:
satsanginfo.rssb.org
ऑनलाइन बुक सेल
RSSB की पुस्तकों को ऑनलाइन ऑर्डर करने की जानकारी हमारी सेल वेबसाइट पर उपलब्ध है:
www.scienceofthesoul.org (विदेशों में सेल के लिए)
www.rssbindiabooks.in (भारत में सेल के लिए)